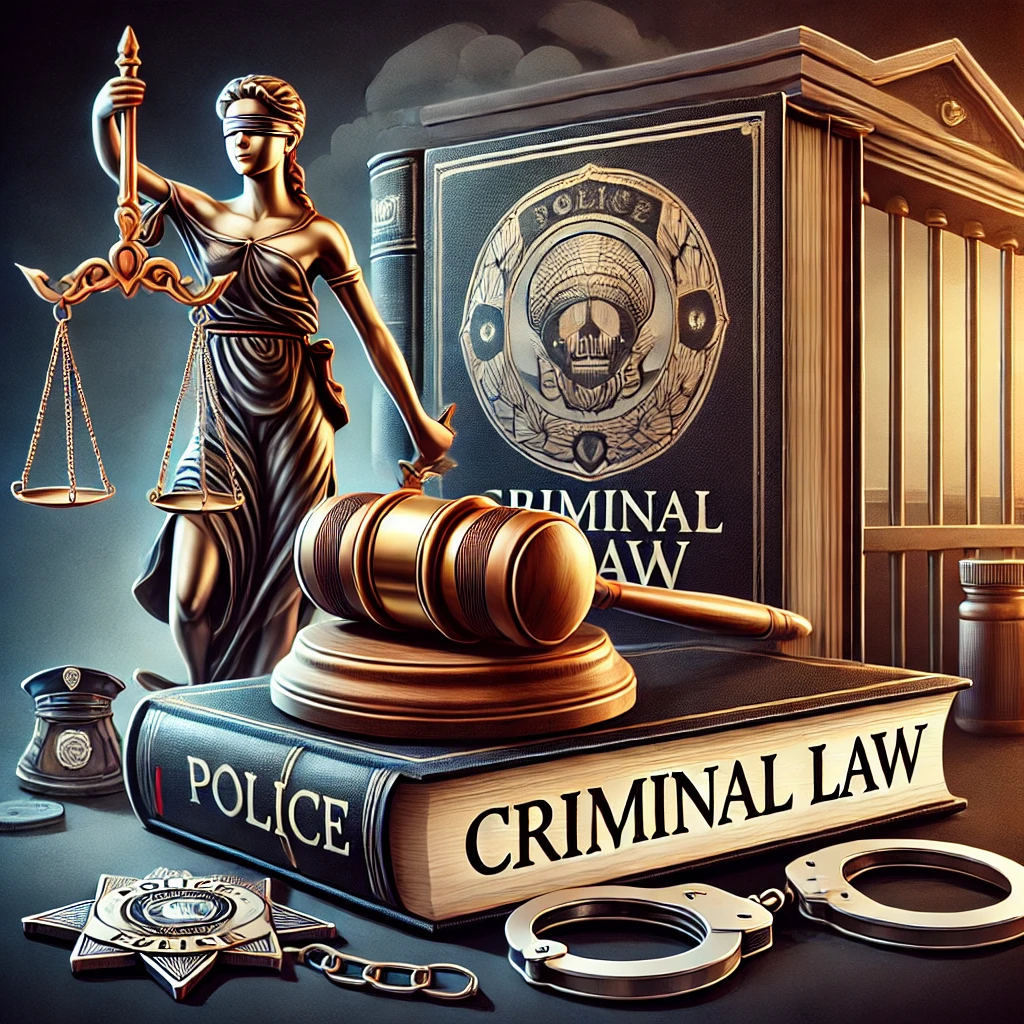भारतीय आपराधिक कानून में पीड़ित के अधिकारों का उद्भव और विकास
(The Emergence and Evolution of Victims’ Rights in Indian Criminal Law)
भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पारंपरिक रूप से अभियुक्त-केंद्रित रही है, जहाँ प्रक्रिया और विधिक अधिकार मुख्य रूप से आरोपी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए केंद्रित थे। किंतु वास्तविक न्याय की प्राप्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक पीड़ित – जो कि अपराध का सीधा भोगी होता है – को सुनवाई, सम्मान, क्षतिपूर्ति और सुरक्षा जैसे मूल अधिकार प्राप्त न हों।
हाल के दशकों में, भारतीय न्याय प्रणाली में पीड़ित के अधिकारों को विधिक, नीतिगत और न्यायिक स्तर पर मान्यता मिलनी प्रारंभ हुई है। यह लेख इस संवेदनशील लेकिन आवश्यक विषय की गहराई से पड़ताल करता है कि कैसे भारत में पीड़ित के अधिकारों का उद्भव और विकास हुआ है।
📜 I. पारंपरिक आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित की स्थिति
प्राचीन काल में – जैसे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के युग में – राजा न्याय का संरक्षक होता था, और पीड़ित की क्षतिपूर्ति पर बल दिया जाता था।
❖ लेकिन आधुनिक भारतीय आपराधिक विधि – विशेषकर भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – राज्य बनाम अपराधी के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पीड़ित केवल एक गवाह की भूमिका में सीमित था।
❖ परिणामस्वरूप, अभियुक्त के अधिकार (जैसे निष्पक्ष सुनवाई, वकील की सहायता, अपील का अधिकार) तो मजबूत थे, लेकिन पीड़ित की आवाज़ और अधिकार अदृश्य रहते थे।
🧭 II. पीड़ित अधिकारों के विकास की आवश्यकता – सामाजिक व न्यायिक दृष्टिकोण
🔹 न्यायिक मान्यता
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने समय-समय पर यह स्वीकार किया कि पीड़ित की उपेक्षा न्याय का उपहास है।
- पीड़ित को सिर्फ एक “औजार” के रूप में नहीं देखा जा सकता।
🔹 वैश्विक प्रभाव
- संयुक्त राष्ट्र की 1985 की “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power” ने देशों को निर्देशित किया कि वे पीड़ितों के लिए मुआवजा, सहायता, पुनर्वास और भागीदारी सुनिश्चित करें।
⚖️ III. भारतीय विधिक व्यवस्था में पीड़ित अधिकारों का विकास: चरणबद्ध विश्लेषण
🧩 1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) में संशोधन
(क) धारा 357 – क्षतिपूर्ति आदेश (Compensation)
- कोर्ट अभियुक्त को दंड देने के साथ-साथ पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दे सकती है।
(ख) धारा 357A (2009 का संशोधन) – पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना
- प्रत्येक राज्य को एक योजना बनानी होगी जिसमें अपराध के शिकार व्यक्ति को सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाए, भले ही अभियुक्त की पहचान न हुई हो या मामला बंद हो गया हो।
(ग) धारा 154(1) (क) – महिला पीड़िता का FIR दर्ज करने की बाध्यता
- किसी महिला पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज करने में पुलिस आनाकानी नहीं कर सकती।
(घ) धारा 164A – बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच का अधिकार
🧩 2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में सुधार
- बलात्कार के मामलों में पीड़िता के चरित्र पर आधारित पूछताछ (Character Assassination) की मनाही (धारा 146 में संशोधन)।
- Consent की परिभाषा को सशक्त और स्पष्ट किया गया।
🧩 3. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय
📌 Bodhisattwa Gautam v. Subhra Chakraborty (1996)
- बलात्कार एक गंभीर अपराध है और पीड़िता को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
📌 Delhi Domestic Working Women’s Forum v. Union of India (1995)
- कोर्ट ने कहा कि बलात्कार पीड़िताओं के लिए मानसिक, चिकित्सा और कानूनी सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
📌 Nilabati Behera v. State of Orissa (1993)
- मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पीड़ित या उसके परिजनों को राज्य द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए।
👩⚖️ IV. न्यायालय में पीड़ित की भागीदारी का अधिकार
✅ CrPC की धारा 301 और 302
- अब पीड़ित या उसका वकील अभियोजन में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं, विशेषकर यदि अभियोजन राज्य द्वारा ठीक से नहीं किया जा रहा।
✅ 2018 का सुप्रीम कोर्ट निर्णय – Satya Pal Singh v. State of M.P.
- बलात्कार पीड़िता के पिता को अपील का अधिकार मान्यता प्राप्त हुआ, भले ही वह अभियोजन पक्ष न हो।
🛡️ V. पीड़ित सुरक्षा (Victim Protection)
- गवाह संरक्षण योजना (Witness Protection Scheme, 2018) में पीड़ितों को भी शामिल किया गया है।
- POSH Act, 2013, POCSO Act, और Domestic Violence Act में पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने और कार्यस्थल/घरों में सुरक्षा प्रदान करने के विशेष प्रावधान हैं।
🧑⚕️ VI. पीड़ित पुनर्वास और सहायता सेवाएँ
- कई राज्यों ने वन-स्टॉप सेंटर (OSC) स्थापित किए हैं जहाँ पीड़िता को एक ही स्थान पर चिकित्सा, काउंसलिंग, विधिक सहायता और सुरक्षा मिलती है।
- निर्भया फंड के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पीड़ित पुनर्वास के लिए योजनाएँ बनाई हैं।
🌐 VII. अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और तुलना
| देश | पीड़ित अधिकार |
|---|---|
| अमेरिका | “Victim Impact Statement”, क्षतिपूर्ति का कानूनी अधिकार |
| यूरोप | EU Victims’ Directive – पीड़ित की गोपनीयता, जानकारी का अधिकार |
| भारत | अब सुधार हो रहे हैं, लेकिन अधिकार अभी भी आंशिक और सीमित हैं |
📌 VIII. वर्तमान चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता
- मुआवजा योजनाओं की असमानता: राज्यों में अलग-अलग मानक, पारदर्शिता की कमी
- पीड़ितों की कानूनी जानकारी का अभाव: अधिकांश पीड़ित अपने अधिकारों से अनजान होते हैं
- न्याय प्रक्रिया में देरी: वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं
- पुनर्वास सेवाओं की पहुंच सीमित: ग्रामीण क्षेत्रों में OSC जैसे केंद्र नहीं
✅ निष्कर्ष (Conclusion)
भारतीय आपराधिक कानून में पीड़ित के अधिकारों का विकास निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिवर्तन है। यह परंपरागत अभियुक्त-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर न्याय के संतुलन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि सुधार हुए हैं, फिर भी एक संगठित और अधिकार-आधारित पीड़ित न्याय प्रणाली की दिशा में अभी और प्रयास आवश्यक हैं।
“सिर्फ अपराधी को सजा देना न्याय नहीं है, जब तक पीड़ित को सम्मान, क्षतिपूर्ति और पुनर्वास न मिले – तब तक न्याय अधूरा है।”