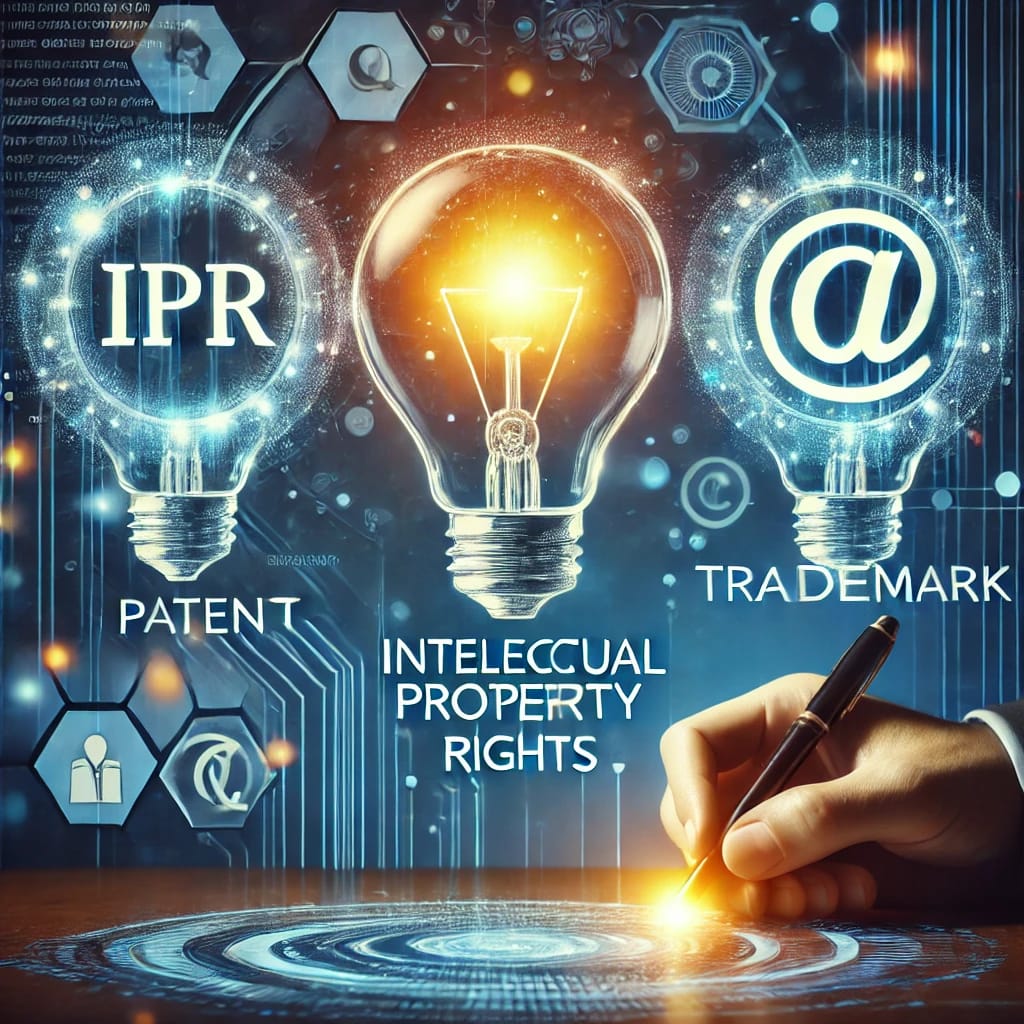बौद्धिक संपदा कानून (Intellectual Property Law)
प्रश्न 1. बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) से आप क्या समझते हैं?
बौद्धिक संपदा उन अमूर्त (Intangible) संपत्तियों को कहा जाता है, जो मानव की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता एवं मौलिकता से उत्पन्न होती हैं। इसमें आविष्कार, साहित्यिक कृतियाँ, कलात्मक रचनाएँ, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, भौगोलिक संकेत, पेटेंट तथा कॉपीराइट शामिल हैं। पारंपरिक संपत्ति (जैसे भूमि, भवन, चल संपत्ति) के विपरीत बौद्धिक संपदा का स्वरूप भौतिक नहीं होता, बल्कि यह कानूनी अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। बौद्धिक संपदा का उद्देश्य रचनाकारों, आविष्कारकों और व्यापारियों को उनके कार्यों पर विशेषाधिकार प्रदान करना है ताकि वे नवाचार, शोध और व्यापार में निवेश करने के लिए प्रेरित हों। भारत में इसके लिए विशेष कानून बनाए गए हैं जैसे—कॉपीराइट अधिनियम, 1957; पेटेंट अधिनियम, 1970; ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999; डिज़ाइन अधिनियम, 2000; और भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999। इन सभी का संरक्षण न्यायालयों के माध्यम से किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WIPO (World Intellectual Property Organization) इसकी देखरेख करता है।
प्रश्न 2. बौद्धिक संपदा कानून का महत्व स्पष्ट कीजिए।
बौद्धिक संपदा कानून आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसका महत्व मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर आधारित है—
(1) नवाचार को प्रोत्साहन: शोधकर्ताओं, आविष्कारकों और कलाकारों को उनके कार्य पर कानूनी सुरक्षा देकर उन्हें नई खोजें करने हेतु प्रेरित किया जाता है।
(2) आर्थिक विकास: बौद्धिक संपदा का व्यावसायिक उपयोग करके उद्योगपति और उद्यमी अपने उत्पादों को विशिष्ट पहचान देते हैं। इससे विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है।
(3) उपभोक्ता संरक्षण: ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत उपभोक्ताओं को यह आश्वासन देते हैं कि उन्हें वास्तविक और गुणवत्ता युक्त उत्पाद ही प्राप्त हो रहा है।
इसके अतिरिक्त, बौद्धिक संपदा कानून अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है क्योंकि यह WTO के TRIPS समझौते से जुड़ा हुआ है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह क्षेत्र रोजगार सृजन और स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक है।
प्रश्न 3. बौद्धिक संपदा के प्रमुख प्रकारों का विवरण दीजिए।
बौद्धिक संपदा मुख्यतः पाँच प्रकार की होती है—
(1) कॉपीराइट: साहित्यिक, संगीत, कला और कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी कृतियों पर सर्जक को विशेषाधिकार प्रदान करता है।
(2) पेटेंट: किसी नये आविष्कार, प्रक्रिया या तकनीकी नवाचार पर अधिकार देता है, जिसकी नवीनता और औद्योगिक उपयोगिता हो।
(3) ट्रेडमार्क: किसी उत्पाद या सेवा की पहचान के लिए प्रयुक्त नाम, प्रतीक या लोगो की सुरक्षा करता है।
(4) औद्योगिक डिज़ाइन: किसी वस्तु के सौंदर्यात्मक स्वरूप, पैटर्न, आकार आदि पर संरक्षण प्रदान करता है।
(5) भौगोलिक संकेत (GI): ऐसे उत्पाद जिनकी विशेष गुणवत्ता या पहचान किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हो, जैसे दार्जिलिंग चाय।
इनके अतिरिक्त “व्यापार रहस्य” और “पौध किस्म संरक्षण” भी आधुनिक बौद्धिक संपदा का हिस्सा माने जाते हैं।
प्रश्न 4. कॉपीराइट (Copyright) का स्वरूप और महत्व समझाइए।
कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक महत्वपूर्ण रूप है जो लेखक, कलाकार या सर्जक को उसकी मौलिक रचनाओं पर विशेष अधिकार देता है। इसका क्षेत्र साहित्यिक कृतियाँ (किताबें, लेख), नाट्य और संगीत कृतियाँ, फिल्में, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तथा कंप्यूटर प्रोग्राम तक विस्तृत है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत यह अधिकार भारत में संरक्षित है।
कॉपीराइट का महत्व यह है कि यह सर्जक को उसकी कृति की प्रतिलिपि बनाने, प्रकाशन करने, अनुवाद करने और सार्वजनिक प्रसारण का विशेषाधिकार देता है। इससे लेखक और कलाकार अपनी बौद्धिक मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त कर पाते हैं और पायरेसी जैसी अवैध गतिविधियों से सुरक्षा मिलती है। कॉपीराइट की अवधि सामान्यतः लेखक के जीवनकाल के साथ-साथ 60 वर्ष तक होती है। डिजिटल युग में कॉपीराइट का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि संगीत, फिल्म और ई-बुक्स जैसी सामग्री आसानी से कॉपी की जा सकती है।
प्रश्न 5. पेटेंट कानून का उद्देश्य क्या है?
पेटेंट कानून का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है। पेटेंट अधिनियम, 1970 (संशोधित 2005) के अनुसार, जब कोई व्यक्ति कोई नया आविष्कार करता है और उसका औद्योगिक उपयोग संभव होता है, तो उसे “पेटेंट” प्राप्त होता है।
पेटेंट धारक को 20 वर्षों तक उस आविष्कार पर विशेषाधिकार प्राप्त होता है, जिससे वह उत्पादन, बिक्री और लाइसेंसिंग कर सकता है। पेटेंट का महत्व यह है कि यह आविष्कारक को आर्थिक लाभ प्रदान करता है और समाज को नई तकनीकें उपलब्ध कराता है। पेटेंट कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद वह ज्ञान सार्वजनिक डोमेन में आ जाए और सभी उसका उपयोग कर सकें।
भारत में दवा उद्योग, जैव-प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पेटेंट का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह क्षेत्र आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से सीधे जुड़ा हुआ है।
प्रश्न 6. ट्रेडमार्क (Trademark) क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
ट्रेडमार्क वह चिन्ह, प्रतीक, नाम, रंग संयोजन या लोगो है जो किसी वस्तु या सेवा को अन्य से अलग पहचान दिलाता है। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत भारत में इसके पंजीकरण और संरक्षण की व्यवस्था की गई है।
ट्रेडमार्क का महत्व यह है कि यह उत्पाद की “ब्रांड वैल्यू” स्थापित करता है और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की पहचान में सहायता करता है। जैसे—टाटा, अमूल, रिलायंस आदि। यह किसी कंपनी की साख और उसके उत्पाद की विशिष्टता को दर्शाता है।
ट्रेडमार्क पंजीकृत होने पर मालिक को उस चिन्ह पर विशेषाधिकार मिलता है और कोई अन्य व्यक्ति इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति समान या भ्रम पैदा करने वाला चिन्ह उपयोग करता है तो वह “पैसिंग ऑफ” या “इंफ्रिंजमेंट” कहलाता है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा का सबसे अधिक उपयोगी साधन है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के विश्वास से जुड़ा होता है।
प्रश्न 7. औद्योगिक डिज़ाइन (Industrial Design) का कानूनी स्वरूप स्पष्ट करें।
औद्योगिक डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत औद्योगिक डिज़ाइन उस बाहरी स्वरूप, पैटर्न, आकार, आकृति या सौंदर्यात्मक रूप को कहा जाता है जो किसी वस्तु को दृश्य रूप से आकर्षक बनाता है। यह तकनीकी या कार्यात्मक नवाचार से अलग है और केवल वस्तु के सौंदर्य पक्ष पर केंद्रित होता है।
डिज़ाइन पंजीकृत होने पर डिज़ाइनर को 10 वर्षों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त होता है जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि में वह अन्य व्यक्तियों को उसकी नकल या अनुकरण करने से रोक सकता है।
औद्योगिक डिज़ाइन का महत्व इसलिए है क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में उपभोक्ता केवल उत्पाद की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि उसकी आकृति और पैकेजिंग को भी महत्व देते हैं। मोबाइल फोन, कार, वस्त्र, घरेलू सामान आदि में डिज़ाइन एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक तत्व बन चुका है।
प्रश्न 8. भौगोलिक संकेत (Geographical Indication) का उद्देश्य स्पष्ट करें।
भौगोलिक संकेत (GI) किसी ऐसे उत्पाद पर अधिकार प्रदान करता है जिसकी विशिष्ट गुणवत्ता, ख्याति या विशेषता किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हो। भारत में इसके लिए “भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999” लागू है।
जैसे—दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी, नागपुर संतरा, आल्फांसो आम आदि। इन उत्पादों की विशिष्टता उनके उत्पादन क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होती है।
GI का उद्देश्य उत्पादकों को उनके क्षेत्रीय उत्पादों पर कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है ताकि नकली उत्पादों पर रोक लगे और वास्तविक उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी रहे।
इससे ग्रामीण और स्थानीय कारीगरों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण मिलता है। WTO के TRIPS समझौते के तहत GI का विशेष महत्व है क्योंकि यह वैश्विक व्यापार में गुणवत्ता और विशिष्टता का प्रतीक है।
प्रश्न 9. WIPO (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) की भूमिका क्या है?
WIPO (World Intellectual Property Organization) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत संस्था है जिसकी स्थापना 1967 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है। WIPO का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास और संरक्षण करना है।
यह संगठन विभिन्न देशों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और GI जैसे अधिकारों पर तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण और कानूनी परामर्श प्रदान करता है। इसके तहत कई अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ संचालित होती हैं, जैसे—पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, पेटेंट को-ऑपरेशन संधि (PCT)।
भारत WIPO का सदस्य है और इसके माध्यम से भारतीय आविष्कारकों और सर्जकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रचनाओं का संरक्षण मिल सकता है।
WIPO वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index) भी प्रकाशित करता है, जिससे देशों की बौद्धिक संपदा नीति और अनुसंधान क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।
प्रश्न 10. TRIPS समझौते का बौद्धिक संपदा कानून में महत्व बताइए।
TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) समझौता विश्व व्यापार संगठन (WTO) का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे 1995 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की वैश्विक स्तर पर एकरूपता और न्यूनतम मानक तय करना है।
TRIPS के अंतर्गत पेटेंट की अवधि 20 वर्ष, कॉपीराइट की अवधि 50 वर्ष (भारत में 60 वर्ष), ट्रेडमार्क पंजीकरण, औद्योगिक डिज़ाइन की सुरक्षा तथा GI का संरक्षण अनिवार्य किया गया।
भारत ने इस समझौते के अनुरूप अपने कानूनों में संशोधन किया—जैसे पेटेंट अधिनियम, 1970 में 2005 का संशोधन। इससे दवा उद्योग और कृषि उत्पादों पर विशेष प्रभाव पड़ा।
TRIPS का महत्व यह है कि यह वैश्विक व्यापार में “न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा” सुनिश्चित करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि बौद्धिक संपदा का दुरुपयोग न हो। हालांकि, विकासशील देशों के लिए यह चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि इसमें कठोर मानक निर्धारित किए गए हैं।
प्रश्न 11. बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन (Infringement) की संक्षिप्त व्याख्या करें।
बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति की बौद्धिक संपदा का उपयोग करता है। जैसे—किसी पुस्तक की अनधिकृत प्रतिलिपि, नकली ब्रांड उत्पाद बेचना, पेटेंटेड दवा का अवैध उत्पादन, या GI वाले उत्पाद की नकल।
भारत में उल्लंघन के खिलाफ सिविल और आपराधिक उपाय उपलब्ध हैं। सिविल उपायों में क्षतिपूर्ति, निषेधाज्ञा (Injunction) और लाभ की वसूली शामिल है। आपराधिक उपायों में जुर्माना और कारावास भी हो सकता है।
कॉपीराइट अधिनियम, पेटेंट अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम में उल्लंघन के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। उदाहरणस्वरूप, ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में नकली उत्पाद बनाने वाले को कठोर दंड मिल सकता है।
IPR का उल्लंघन न केवल रचनाकार को आर्थिक नुकसान पहुँचाता है बल्कि उपभोक्ताओं को भी गुणवत्ता हीन उत्पादों से हानि होती है। इसलिए कानून का उद्देश्य सर्जक और उपभोक्ता दोनों का संरक्षण करना है।
प्रश्न 12. भारत में बौद्धिक संपदा कानून का विकास वर्णन कीजिए।
भारत में बौद्धिक संपदा कानून का विकास औपनिवेशिक काल से आरंभ हुआ। सबसे पहले 1856 में पेटेंट कानून आया और 1860 में कॉपीराइट कानून लागू हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1957 में कॉपीराइट अधिनियम पारित हुआ तथा 1970 में आधुनिक पेटेंट अधिनियम बनाया गया।
1990 के दशक में वैश्वीकरण और WTO की सदस्यता के बाद भारत ने अपने IPR कानूनों को TRIPS समझौते के अनुरूप संशोधित किया। 1999 में ट्रेडमार्क अधिनियम, GI अधिनियम और 2000 में डिज़ाइन अधिनियम पारित हुए। 2005 में पेटेंट अधिनियम संशोधित कर “प्रोडक्ट पेटेंट” प्रणाली को लागू किया गया।
आज भारत में IPR से संबंधित सभी प्रमुख कानून उपलब्ध हैं और विशेष न्यायाधिकरण (IPAB) भी स्थापित किया गया था। भारत WIPO और WTO का सक्रिय सदस्य है।
वर्तमान में भारत का जोर स्टार्ट-अप्स और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर है, जिसके लिए IPR का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
प्रश्न 13. कॉपीराइट और पेटेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए।
कॉपीराइट और पेटेंट दोनों बौद्धिक संपदा अधिकार हैं लेकिन इनमें मूलभूत अंतर है—
- वस्तु: कॉपीराइट साहित्यिक, संगीत, कलात्मक और सॉफ्टवेयर कृतियों पर लागू होता है, जबकि पेटेंट वैज्ञानिक आविष्कारों और तकनीकी प्रक्रियाओं पर।
- पंजीकरण: कॉपीराइट स्वतः प्राप्त होता है, जबकि पेटेंट के लिए आवेदन और परीक्षण आवश्यक है।
- अवधि: कॉपीराइट लेखक के जीवनकाल + 60 वर्ष तक रहता है, जबकि पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होती है।
- उद्देश्य: कॉपीराइट सर्जनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, पेटेंट नवाचार और तकनीकी प्रगति को।
- अधिकार: कॉपीराइट में प्रतिलिपि, प्रकाशन और प्रदर्शन का अधिकार मिलता है, पेटेंट में उत्पादन, बिक्री और लाइसेंसिंग का अधिकार।
इस प्रकार, दोनों का क्षेत्र अलग है लेकिन दोनों ही ज्ञान और रचनात्मकता की रक्षा करते हैं।
प्रश्न 14. भारत में भौगोलिक संकेत (GI) के उदाहरण दीजिए और उनका महत्व स्पष्ट करें।
भारत में कई भौगोलिक संकेत पंजीकृत हैं। उदाहरणस्वरूप—
- दार्जिलिंग चाय (पश्चिम बंगाल)
- बनारसी साड़ी (उत्तर प्रदेश)
- मैसूर सिल्क (कर्नाटक)
- नागपुर संतरा (महाराष्ट्र)
- कंधमाल हल्दी (ओडिशा)
इनका महत्व यह है कि ये उत्पाद अपनी विशिष्ट गुणवत्ता और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हैं। GI कानून उत्पादकों को नकली उत्पादों से सुरक्षा प्रदान करता है और उनके आर्थिक हितों की रक्षा करता है।
GI स्थानीय समुदायों को लाभ पहुँचाकर “ग्रामीण विकास” और “सांस्कृतिक विरासत संरक्षण” दोनों में सहायक होता है। वैश्विक बाजार में GI उत्पादों की मांग अधिक रहती है क्योंकि उपभोक्ता इन्हें विशिष्ट और प्रामाणिक मानते हैं।
प्रश्न 15. भविष्य में बौद्धिक संपदा कानून की चुनौतियाँ और संभावनाएँ बताइए।
भविष्य में बौद्धिक संपदा कानून के सामने कई चुनौतियाँ हैं। डिजिटल तकनीक और इंटरनेट ने पायरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन को आसान बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जैव-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा की परिभाषा जटिल हो रही है।
इसके साथ ही, विकासशील देशों के लिए TRIPS जैसे कठोर मानकों का पालन करना कठिन है क्योंकि इससे दवा और कृषि उत्पाद महंगे हो सकते हैं।
संभावनाओं की दृष्टि से, भारत जैसे देशों के लिए यह क्षेत्र आर्थिक विकास का बड़ा साधन बन सकता है। स्टार्ट-अप्स, रिसर्च संस्थान और कारीगरों को कानूनी सुरक्षा देकर नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है।
यदि उचित जागरूकता और कड़े प्रवर्तन उपाय किए जाएँ, तो बौद्धिक संपदा भारत को “नॉलेज इकॉनमी” बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
प्रश्न 16. कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत “फेयर डीलिंग” का क्या अर्थ है?
फेयर डीलिंग कॉपीराइट कानून के अंतर्गत एक अपवाद है, जिसके तहत कुछ परिस्थितियों में बिना अनुमति के किसी कृति का सीमित उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, शोध, निजी अध्ययन, आलोचना, समीक्षा या समाचार रिपोर्टिंग के उद्देश्य से कॉपीराइट कृति का प्रयोग करना फेयर डीलिंग माना जाता है। यह अवधारणा सार्वजनिक हित और रचनाकार के अधिकार के बीच संतुलन बनाती है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में धारा 52 इस प्रावधान का उल्लेख करती है। इसका उद्देश्य ज्ञान के स्वतंत्र प्रवाह और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। यदि फेयर डीलिंग का दुरुपयोग होता है और कोई व्यक्ति व्यावसायिक लाभ उठाता है तो यह उल्लंघन माना जाएगा।
प्रश्न 17. पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत “पेटेंट योग्य आविष्कार” की परिभाषा समझाइए।
पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2(1)(j) के अनुसार पेटेंट योग्य आविष्कार वह है जिसमें नवीनता (Novelty), आविष्कारक कदम (Inventive Step) और औद्योगिक प्रयोज्यता (Industrial Applicability) हो। इसका अर्थ है कि आविष्कार नया होना चाहिए, पूर्व कला का हिस्सा न हो, सामान्य तकनीकी ज्ञान से परे हो तथा उद्योग में उपयोगी हो। इसके अतिरिक्त, कुछ चीज़ें पेटेंट योग्य नहीं होतीं जैसे—गणितीय सूत्र, व्यावसायिक विधियाँ, कृषि या पौध प्रजातियाँ, और सार्वजनिक नीति या नैतिकता के विरुद्ध आविष्कार। यह परिभाषा सुनिश्चित करती है कि केवल वास्तविक और उपयोगी नवाचारों को ही कानूनी सुरक्षा मिले।
प्रश्न 18. पेटेंट उल्लंघन (Patent Infringement) क्या है?
जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति पेटेंट धारक के आविष्कार का उत्पादन, उपयोग, बिक्री या आयात करता है, तो यह पेटेंट उल्लंघन कहलाता है। भारत में इसके खिलाफ सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार की कार्यवाही संभव है। सिविल उपायों में निषेधाज्ञा (Injunction), क्षतिपूर्ति (Damages) और उल्लंघन से अर्जित लाभ की वसूली शामिल है। आपराधिक उपाय अपेक्षाकृत सीमित हैं। पेटेंट उल्लंघन मामलों का निपटारा उच्च न्यायालय या विशेष बौद्धिक संपदा पीठ में होता है। उदाहरण के लिए, दवा कंपनियों के बीच जेनेरिक दवाओं पर कई पेटेंट विवाद हुए हैं। इसका उद्देश्य आविष्कारक के अधिकारों की रक्षा करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
प्रश्न 19. ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में “पासिंग ऑफ” (Passing Off) की अवधारणा क्या है?
पासिंग ऑफ एक सामान्य विधिक उपाय है जो बिना पंजीकरण वाले ट्रेडमार्क की सुरक्षा करता है। यदि कोई व्यापारी किसी अन्य व्यापारी के चिन्ह, नाम या पैकेजिंग का अनुकरण करके उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है और अपने उत्पाद को प्रसिद्ध ब्रांड के समान प्रस्तुत करता है, तो यह पासिंग ऑफ कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी “Coca-Kola” नाम से पेय बेचे तो यह पासिंग ऑफ होगा। अदालत इस स्थिति में दोषी पक्ष को चिन्ह के प्रयोग से रोक सकती है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को धोखे से बचाना और व्यापारियों की साख की रक्षा करना है।
प्रश्न 20. औद्योगिक डिज़ाइन अधिनियम, 2000 का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
औद्योगिक डिज़ाइन अधिनियम, 2000 का मुख्य उद्देश्य उत्पादों के दृश्य स्वरूप को कानूनी सुरक्षा देना है। आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में उपभोक्ता केवल उत्पाद की कार्यक्षमता नहीं, बल्कि उसके सौंदर्य और आकर्षण को भी महत्व देते हैं। यह अधिनियम डिज़ाइनरों को 10 वर्षों का विशेषाधिकार देता है जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इससे डिज़ाइनर अपनी रचनात्मकता से लाभ कमा सकते हैं और नकल करने वालों को रोक सकते हैं। इसका आर्थिक महत्व विशेष रूप से फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और पैकेजिंग उद्योगों में देखा जाता है।
प्रश्न 21. भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999 के अंतर्गत GI का पंजीकरण कैसे होता है?
भौगोलिक संकेत का पंजीकरण GI रजिस्ट्री, चेन्नई में किया जाता है। इसके लिए उत्पादकों का समूह या संगठन आवेदन करता है। आवेदन में उत्पाद की विशेषता, क्षेत्र की पहचान, उत्पादन विधि और ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं। यदि आवेदन सफल रहता है तो GI को 10 वर्षों के लिए पंजीकृत किया जाता है जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है। पंजीकरण से उत्पादकों को कानूनी अधिकार मिल जाता है कि वे नकली उत्पादों को रोक सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI टैग का लाभ उठा सकें।
प्रश्न 22. व्यापार रहस्य (Trade Secret) क्या है और इसका महत्व समझाइए।
व्यापार रहस्य वह गोपनीय जानकारी है जो किसी व्यवसाय की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने में सहायक होती है। इसमें निर्माण विधि, ग्राहक सूची, सूत्र (जैसे—Coca-Cola का फार्मूला), विपणन रणनीति आदि शामिल हो सकते हैं। भारत में व्यापार रहस्यों के लिए कोई विशेष अधिनियम नहीं है, परंतु अनुबंध कानून और कॉमन लॉ सिद्धांतों के माध्यम से सुरक्षा मिलती है। इसका महत्व यह है कि यह व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा में आगे बनाए रखता है और उन्हें आर्थिक लाभ देता है। आज के डिजिटल युग में साइबर चोरी और डेटा लीक से व्यापार रहस्यों की सुरक्षा और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है।
प्रश्न 23. कॉपीराइट उल्लंघन (Copyright Infringement) क्या है?
जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति किसी अन्य की मौलिक रचना की प्रतिलिपि, वितरण, अनुवाद या सार्वजनिक प्रदर्शन करता है तो यह कॉपीराइट उल्लंघन कहलाता है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत इसके खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, फिल्म की पायरेसी, किताबों की फोटोकॉपी, सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी इत्यादि। उल्लंघन की स्थिति में रचनाकार निषेधाज्ञा, क्षतिपूर्ति और आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है। डिजिटल युग में ऑनलाइन पायरेसी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है।
प्रश्न 24. पेटेंट और व्यापार रहस्य में अंतर बताइए।
पेटेंट और व्यापार रहस्य दोनों नवाचार की रक्षा करते हैं, लेकिन अंतर है—
- पेटेंट सार्वजनिक घोषणा के बाद 20 वर्षों तक सुरक्षा देता है, जबकि व्यापार रहस्य तब तक सुरक्षित रहता है जब तक गोपनीयता बनी रहे।
- पेटेंट कानून द्वारा संरक्षित है, जबकि व्यापार रहस्य कॉमन लॉ और अनुबंध पर आधारित है।
- पेटेंट में सरकार से पंजीकरण आवश्यक है, व्यापार रहस्य में ऐसा नहीं।
- पेटेंट ज्ञान को सार्वजनिक डोमेन में लाता है, जबकि व्यापार रहस्य इसे छिपाकर रखता है।
इस प्रकार दोनों ही अलग परिस्थितियों में उपयोगी हैं।
प्रश्न 25. GI टैग का किसानों और कारीगरों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
GI टैग मिलने से किसानों और कारीगरों को उनके उत्पाद की विशिष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है। इससे नकली उत्पादों पर रोक लगती है और वास्तविक उत्पाद की मांग बढ़ती है। जैसे—दार्जिलिंग चाय या कंधमाल हल्दी को GI टैग मिलने से किसानों को अधिक मूल्य मिला। इसी प्रकार बनारसी साड़ी और कांचीवरम सिल्क से जुड़े बुनकरों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। GI ग्रामीण विकास, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण का माध्यम बन जाता है।
प्रश्न 26. भारत में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) की भूमिका क्या थी?
IPAB की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका उद्देश्य पेटेंट, ट्रेडमार्क, GI और कॉपीराइट संबंधी अपीलों का निपटारा करना था। यह बौद्धिक संपदा विवादों के लिए विशेष न्यायाधिकरण था। 2021 में इसे समाप्त कर दिया गया और इसकी शक्तियाँ उच्च न्यायालयों को सौंप दी गईं। IPAB ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए जिनसे भारतीय IPR न्यायशास्त्र का विकास हुआ। इसका महत्व यह था कि विशेष विशेषज्ञता के कारण विवादों का शीघ्र समाधान होता था।
प्रश्न 27. कॉपीराइट और डिज़ाइन में अंतर बताइए।
कॉपीराइट और डिज़ाइन दोनों रचनात्मक कार्यों की रक्षा करते हैं परंतु अंतर है—
- कॉपीराइट साहित्यिक और कलात्मक कृतियों पर लागू होता है, जबकि डिज़ाइन वस्तुओं के सौंदर्यात्मक रूप पर।
- कॉपीराइट स्वतः प्राप्त होता है, डिज़ाइन पंजीकरण आवश्यक है।
- कॉपीराइट की अवधि लेखक का जीवन + 60 वर्ष, जबकि डिज़ाइन की अवधि 10 + 5 वर्ष है।
- कॉपीराइट का क्षेत्र व्यापक है जबकि डिज़ाइन विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादों तक सीमित है।
प्रश्न 28. बौद्धिक संपदा और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संबंध स्पष्ट करें।
बौद्धिक संपदा उपभोक्ताओं को वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की पहचान करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए, ट्रेडमार्क उपभोक्ता को असली ब्रांड पहचानने में मदद करता है, GI टैग नकली उत्पादों से बचाता है, और पेटेंट सुनिश्चित करता है कि दवा वास्तविक और परीक्षणित तकनीक पर आधारित है। इस प्रकार, IPR केवल सर्जक की रक्षा नहीं करता बल्कि उपभोक्ता को धोखे और नकली उत्पादों से बचाता है।
प्रश्न 29. डिजिटल युग में कॉपीराइट संरक्षण की चुनौतियाँ बताइए।
डिजिटल तकनीक ने कॉपीराइट संरक्षण को कठिन बना दिया है। इंटरनेट पर सामग्री आसानी से कॉपी, साझा और डाउनलोड की जा सकती है। फिल्म और संगीत की पायरेसी, ई-बुक्स का अवैध वितरण, और सॉफ्टवेयर की चोरी आम हो गई है। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (DRM) और साइबर कानून इसके समाधान के साधन हैं, परंतु तकनीकी और कानूनी दोनों स्तर पर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
प्रश्न 30. भारत में IPR जागरूकता की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए।
भारत में IPR कानून तो मजबूत हैं, परंतु जागरूकता की कमी है। छोटे उद्योग, किसान और कारीगर अक्सर अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते। परिणामस्वरूप वे अपने नवाचार और उत्पाद की सुरक्षा नहीं कर पाते। सरकार “IPR Awareness Programmes” चला रही है, परंतु जमीनी स्तर पर और प्रयास की आवश्यकता है। यदि जागरूकता बढ़े तो भारत नवाचार और स्टार्ट-अप संस्कृति में अग्रणी बन सकता है।