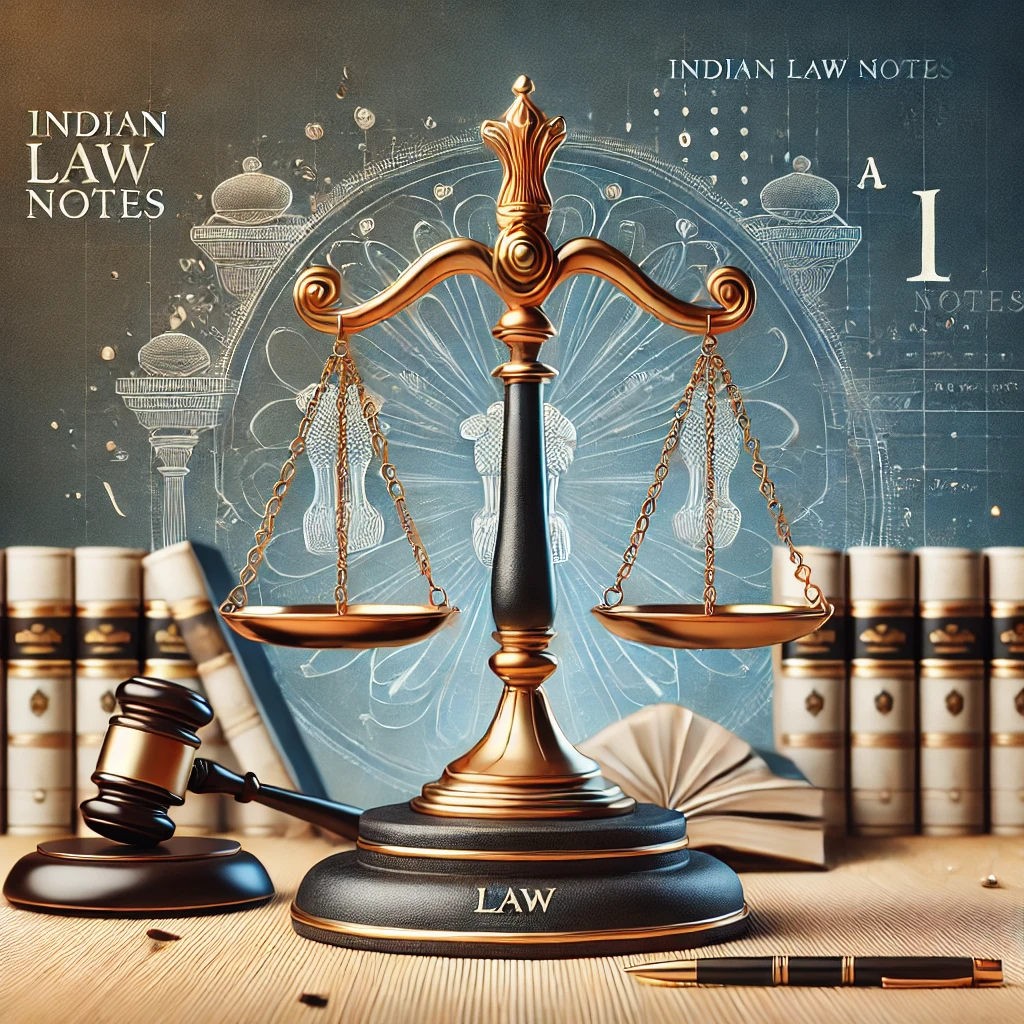बाल स्वास्थ्य और पोषण: कानूनी व नीतिगत पहल
प्रस्तावना
बाल स्वास्थ्य और पोषण किसी भी समाज के विकास के मूलभूत आधार हैं। एक स्वस्थ और पोषित बच्चा न केवल बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण करता है, बल्कि भविष्य में समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी प्रभावी योगदान देता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी चुनौतियाँ—जैसे कुपोषण, संक्रमण, टीकाकरण की कमी, और स्वास्थ्य सेवाओं की असमान पहुंच—अब भी व्यापक रूप से मौजूद हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने कई कानूनी प्रावधान, नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना है।
बाल स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति: एक संक्षिप्त चित्र
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार:
- पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 35% बच्चे कम वजन के हैं।
- 32% बच्चे की लंबाई उनकी उम्र के अनुसार कम है (ठिगनापन)।
- 57% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं।
ये आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि कानूनी और नीतिगत पहल की आवश्यकता केवल कागज़ पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी है।
संवैधानिक प्रावधान
भारत के संविधान में बाल स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कई निर्देश और अधिकार निहित हैं:
- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शामिल है।
- अनुच्छेद 21A – 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएँ और पोषण भी निहित हैं।
- अनुच्छेद 39(e) और 39(f) – बच्चों को स्वास्थ्य और शोषण से बचाने का निर्देश।
- अनुच्छेद 45 – 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था।
- अनुच्छेद 47 – राज्य का कर्तव्य है कि पोषण स्तर और जनस्वास्थ्य को उन्नत करे।
कानूनी प्रावधान
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA)
- धारा 4 – गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण आहार और मातृत्व लाभ।
- धारा 5 – 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उम्र-उपयुक्त मुफ्त भोजन (Anganwadi केंद्रों के माध्यम से)।
- मिड-डे मील योजना को कानूनी दर्जा।
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- संस्थागत देखभाल में बच्चों के लिए उचित स्वास्थ्य, पोषण और चिकित्सा सुविधा की अनिवार्यता।
3. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (संशोधित 2017)
- कार्यरत महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश और मातृत्व लाभ, जिससे नवजात शिशु को शुरुआती छह माह उचित पोषण मिल सके।
4. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- बच्चों के लिए मिलने वाले भोजन और दूध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानक।
5. कोविड-19 और आपदा प्रबंधन के दौरान कानूनी हस्तक्षेप
- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि महामारी के समय बच्चों के लिए मिड-डे मील और पोषण आहार का विकल्प (सूखा राशन/नकद) उपलब्ध कराया जाए।
नीतिगत पहल और सरकारी कार्यक्रम
1. एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), 1975
- आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और शिक्षा।
2. मिड-डे मील योजना
- सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त पौष्टिक भोजन।
- उद्देश्य: विद्यालय उपस्थिति बढ़ाना और पोषण स्तर सुधारना।
3. राष्ट्रीय पोषण मिशन (POSHAN Abhiyaan)
- 2022 तक कुपोषण में कमी लाना (लक्ष्य समय सीमा अब आगे बढ़ाई गई)।
- पोषण ट्रैकर, जनजागरूकता अभियान और डेटा आधारित मॉनिटरिंग।
4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ₹5000 की नकद सहायता, जिससे पोषण आहार में सुधार हो।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
- बच्चों के लिए टीकाकरण (Mission Indradhanush), नवजात देखभाल, और पोषण सुधार कार्यक्रम।
6. अन्नपूर्णा योजना और राशन कार्ड आधारित वितरण
- गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति, जिससे बच्चों के आहार में स्थिरता बनी रहे।
न्यायालय की भूमिका
- People’s Union for Civil Liberties बनाम भारत संघ (2001) – सुप्रीम कोर्ट ने मिड-डे मील योजना को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और सरकार को इसे लागू करने के आदेश दिए।
- Right to Food केस – अदालत ने कहा कि पोषण बच्चों का मौलिक अधिकार है, और राज्य इसका उल्लंघन नहीं कर सकता।
बाल स्वास्थ्य और पोषण सुधार में आने वाली चुनौतियाँ
- कुपोषण और भूख – ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में उच्च स्तर।
- स्वास्थ्य सेवाओं की कमी – प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव।
- अपर्याप्त अवसंरचना – आंगनवाड़ी और विद्यालयों में रसोई और भंडारण की खराब व्यवस्था।
- जागरूकता की कमी – माता-पिता में पोषण संबंधी ज्ञान का अभाव।
- भ्रष्टाचार और आपूर्ति में गड़बड़ी – राशन और मिड-डे मील में गुणवत्ता व मात्रा की समस्या।
सुधार और रोकथाम की रणनीतियाँ
1. कानूनी प्रवर्तन में मजबूती
- NFSA और RTE के प्रावधानों का सख्ती से पालन।
- खाद्य गुणवत्ता मानकों पर नियमित जांच।
2. अवसंरचना सुधार
- आंगनवाड़ी और विद्यालयों में स्वच्छ रसोई, शुद्ध पानी और भंडारण सुविधाएँ।
3. जनजागरूकता अभियान
- गर्भवती महिलाओं और माताओं को पोषण शिक्षा।
- समुदाय आधारित पोषण मेले और स्वास्थ्य शिविर।
4. तकनीकी हस्तक्षेप
- पोषण ट्रैकर और मोबाइल ऐप से बच्चों के स्वास्थ्य डेटा की निगरानी।
- ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली।
5. बहु-क्षेत्रीय समन्वय
- स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग का संयुक्त प्रयास।
- NGOs और सामुदायिक संगठनों की भागीदारी।
निष्कर्ष
बाल स्वास्थ्य और पोषण केवल सामाजिक कल्याण का मुद्दा नहीं, बल्कि यह मौलिक अधिकार है। एक स्वस्थ और पोषित बचपन ही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकता है। भारत ने NFSA, ICDS, POSHAN Abhiyaan और मिड-डे मील जैसी कानूनी और नीतिगत पहल से उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं।
इन पहलों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब कानूनी प्रावधानों का कठोर पालन, पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षित रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।