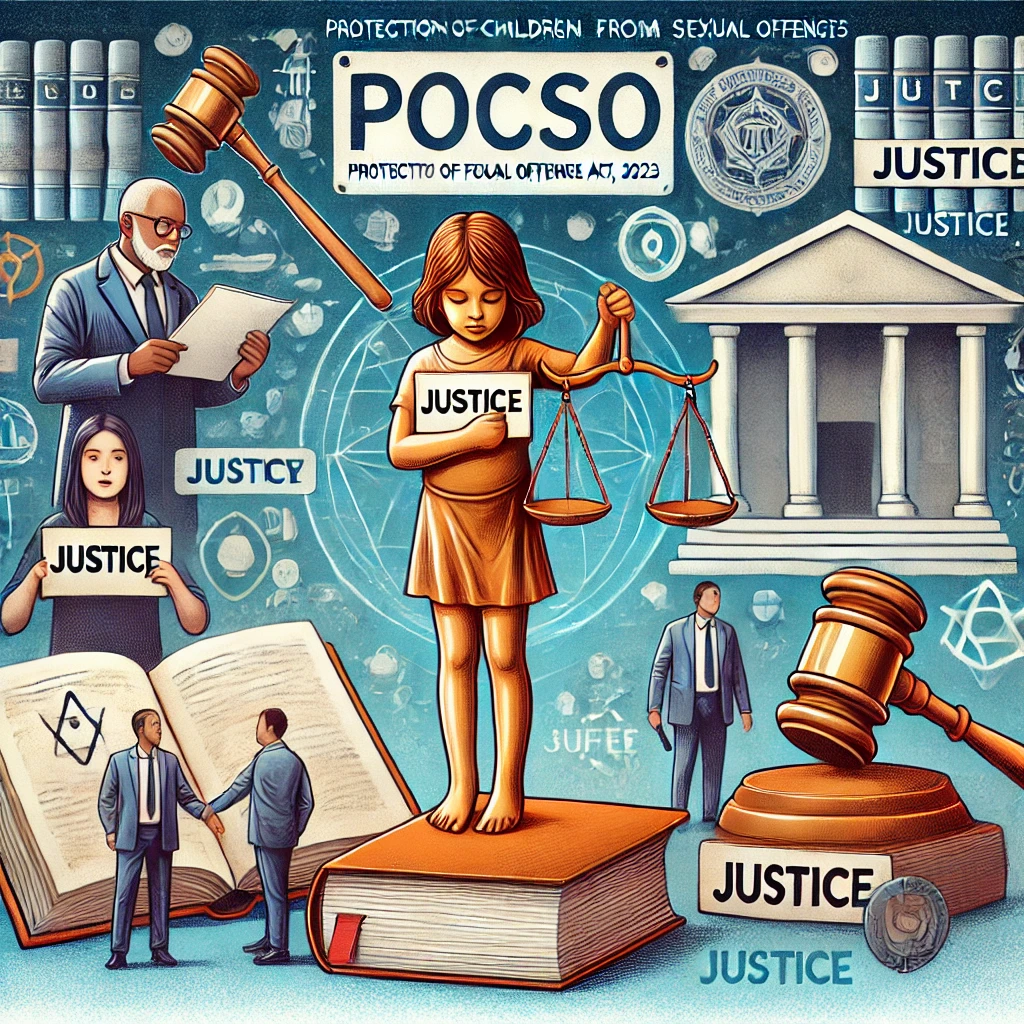बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act 2012) : एक विस्तृत अध्ययन
प्रस्तावना
भारत में बच्चों के प्रति यौन अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में लंबे समय से देखी जाती रही है। बच्चों की असुरक्षा, चुप्पी और समाज का उपेक्षापूर्ण रवैया ऐसे अपराधों को और बढ़ावा देता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने “बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012” (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO Act 2012) लागू किया। यह अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु एक विशेष और सशक्त कानून है।
यह लेख POCSO अधिनियम 2012 की विशेषताओं, प्रावधानों, उद्देश्यों, न्यायिक दृष्टांतों, आलोचनाओं और सुधार की आवश्यकता पर केंद्रित है।
POCSO अधिनियम की आवश्यकता
भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टें लगातार यह दर्शाती रही हैं कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुराने कानून, जैसे भारतीय दंड संहिता (IPC), इन अपराधों को व्यापक रूप से परिभाषित नहीं करते थे। बच्चों की विशेष आवश्यकताओं और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अलग कानून की मांग की जा रही थी।
इस अधिनियम की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि –
- बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में त्वरित और विशेष न्याय की आवश्यकता थी।
- IPC में बच्चों की सहमति से जुड़े मामलों में भ्रम की स्थिति थी।
- यौन अपराधों की परिभाषा सीमित थी और कई तरह के अपराधों को कवर नहीं किया गया था।
- पीड़ित बच्चों की पहचान और गोपनीयता की सुरक्षा पर जोर नहीं था।
POCSO अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ
- बच्चे की परिभाषा – 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा कहलाएगा।
- यौन अपराधों की व्यापक परिभाषा – इसमें Penetrative Sexual Assault, Aggravated Penetrative Sexual Assault, Sexual Assault, Sexual Harassment और Child Pornography को शामिल किया गया।
- लैंगिक तटस्थता (Gender Neutrality) – यह अधिनियम लड़कों और लड़कियों, दोनों की सुरक्षा के लिए है।
- विशेष अदालतें – त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु विशेष अदालतों की स्थापना।
- गोपनीयता का संरक्षण – पीड़ित की पहचान सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध।
- बच्चा-हितैषी प्रक्रिया – पुलिस और अदालतों को निर्देश दिया गया कि वे बच्चों से संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें।
- अनिवार्य रिपोर्टिंग – किसी भी व्यक्ति को यदि बच्चे के प्रति यौन अपराध की जानकारी मिले तो रिपोर्ट करना अनिवार्य है, अन्यथा दंडनीय अपराध।
अधिनियम के अंतर्गत अपराध और दंड
POCSO अधिनियम में कई प्रकार के अपराधों की परिभाषा दी गई है –
- प्रवेशात्मक यौन हमला (Penetrative Sexual Assault) – धारा 3
- बच्चे के शरीर में यौन अंग या वस्तु का प्रवेश करना।
- दंड – न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना।
- गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault) – धारा 5
- जब अपराधी पुलिसकर्मी, शिक्षक, रिश्तेदार, डॉक्टर या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर बच्चे का भरोसा हो।
- दंड – न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर मृत्यु दंड तक।
- यौन हमला (Sexual Assault) – धारा 7
- बच्चे को यौन तरीके से छूना या उसका शारीरिक शोषण करना।
- दंड – न्यूनतम 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
- यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) – धारा 11
- बच्चे से अश्लील बातें करना, उसे अश्लील सामग्री दिखाना, या अश्लील हरकतें करना।
- दंड – अधिकतम 3 वर्ष कारावास और जुर्माना।
- बाल अश्लील सामग्री (Child Pornography) – धारा 13-15
- बच्चे से संबंधित अश्लील चित्र, वीडियो या सामग्री बनाना, प्रसारित करना या रखना।
- दंड – 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना, पुनरावृत्ति पर 7 वर्ष तक की सजा।
विशेष प्रक्रिया
- गोपनीयता – पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध है।
- समयबद्ध सुनवाई – मामले की सुनवाई अधिकतम 1 वर्ष में पूरी होनी चाहिए।
- बच्चा-हितैषी वातावरण – पुलिस पूछताछ बच्चे के घर या परिचित स्थान पर हो सकती है।
- वीडियो रिकॉर्डिंग – बच्चे का बयान वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है।
न्यायिक व्याख्या और दृष्टांत
कई बार अदालतों को यह देखना पड़ा कि किशोर प्रेम संबंधों को भी POCSO के दायरे में अपराध माना जा रहा है।
- केरल हाईकोर्ट (2025) – अदालत ने कहा कि अगर रिश्ता आपसी सहमति का है और लड़की बालिग होने के करीब है, तो युवक पर मुकदमा चलाने से उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है।
- मद्रास हाईकोर्ट (2021) – अदालत ने कहा कि 16-18 वर्ष के किशोरों के प्रेम संबंधों को अपराध की श्रेणी में डालना न्यायसंगत नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कई बार माना है कि POCSO का उद्देश्य शोषण रोकना है, न कि सहमति-आधारित रिश्तों को अपराध घोषित करना।
अधिनियम की आलोचना
- कठोरता और व्यावहारिकता में टकराव – कानून में नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं है, जिससे कई प्रेम संबंधों के मामले भी अपराध बन जाते हैं।
- झूठे मामले – परिवारों द्वारा दबाव में आकर या सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए झूठे मामले दर्ज कर दिए जाते हैं।
- न्यायिक बोझ – अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ गया है।
- बच्चे की मानसिकता पर असर – लंबी कानूनी प्रक्रिया बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है।
सुधार की आवश्यकता
- आयु सीमा पर पुनर्विचार – 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों के सहमति-आधारित संबंधों के लिए अलग प्रावधान होना चाहिए।
- वास्तविक शोषण और सहमति-आधारित मामलों में फर्क – अदालतों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे परिस्थितियों के अनुसार अंतर कर सकें।
- काउंसलिंग और परामर्श – हर मामले में बच्चों और परिवार को मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- जागरूकता अभियान – समाज में POCSO के प्रावधानों की जानकारी और बच्चों को शिक्षित करना बेहद जरूरी है।
POCSO और समाज
यह अधिनियम बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है और अपराधियों को सख्त दंड देता है। लेकिन इसकी सफलता केवल कानून पर निर्भर नहीं है।
- समाज को बच्चों की परवरिश और सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
- अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के साथ खुला संवाद करना चाहिए।
- बच्चों को आत्मरक्षा और अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है।
निष्कर्ष
POCSO अधिनियम 2012 भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। इसने पहली बार बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को व्यापक रूप से परिभाषित किया और सख्त दंड का प्रावधान किया। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हुआ है कि कानून की कठोरता और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
आज आवश्यकता है कि इस कानून की समीक्षा कर सहमति-आधारित किशोर संबंधों और वास्तविक शोषण में अंतर किया जाए। तभी यह अधिनियम अपने वास्तविक उद्देश्य – बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना और उनका उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना – को पूरा कर सकेगा।
1. POCSO अधिनियम, 2012 क्या है?
POCSO अधिनियम 2012 का पूरा नाम Protection of Children from Sexual Offences Act है। इसे बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया। इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना गया है। अधिनियम के तहत यौन शोषण, उत्पीड़न, अश्लीलता, बाल अश्लील चित्रण (Child Pornography) जैसी गतिविधियाँ अपराध मानी जाती हैं। इस कानून की विशेषता यह है कि यह लैंगिक तटस्थ (Gender Neutral) है, अर्थात लड़का और लड़की दोनों समान रूप से इसके तहत संरक्षित हैं। इसके अंतर्गत विशेष अदालतों की स्थापना, गोपनीयता का संरक्षण, और पीड़ित बच्चों के हित में संवेदनशील प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान है।
2. POCSO अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी?
भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध लगातार बढ़ते जा रहे थे। पुराने कानून, जैसे भारतीय दंड संहिता (IPC), बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते थे और कई अपराधों की परिभाषा अधूरी थी। उदाहरण के लिए, यौन उत्पीड़न और बाल पोर्नोग्राफी जैसे अपराध स्पष्ट रूप से IPC में शामिल नहीं थे। साथ ही, बच्चों की पहचान की सुरक्षा और विशेष अदालतों की व्यवस्था का अभाव था। इस कारण बच्चों को न्याय मिलने में देरी होती थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए 2012 में संसद ने POCSO अधिनियम पारित किया ताकि बच्चों को विशेष सुरक्षा दी जा सके और अपराधियों को सख्त दंड मिल सके।
3. POCSO अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
POCSO अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं –
- बच्चों को हर प्रकार के यौन अपराध से सुरक्षा देना।
- अपराध की व्यापक परिभाषा करना ताकि कोई भी अपराध छूट न पाए।
- विशेष अदालतों की स्थापना कर त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।
- पीड़ित बच्चों की पहचान और गोपनीयता की रक्षा करना।
- पुलिस व न्यायिक प्रक्रिया को बच्चा-हितैषी बनाना।
- अनिवार्य रिपोर्टिंग का प्रावधान ताकि कोई भी व्यक्ति अपराध छुपा न सके।
इस प्रकार यह अधिनियम बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और समाज में बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का काम करता है।
4. POCSO अधिनियम में बच्चे की परिभाषा क्या है?
POCSO अधिनियम 2012 की धारा 2(1)(d) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति “बच्चा” माना जाएगा। इस प्रकार, चाहे वह लड़की हो या लड़का, सभी बच्चे इस कानून के अंतर्गत संरक्षित हैं। इस परिभाषा का महत्व इसलिए है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सहमति, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं है। अर्थात, यदि कोई बच्चा यौन संबंध के लिए सहमति भी देता है, तो भी वह संबंध अपराध माना जाएगा। यह प्रावधान बच्चों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने और शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है।
5. POCSO अधिनियम के अंतर्गत मुख्य अपराध कौन-कौन से हैं?
POCSO अधिनियम के अंतर्गत कई अपराध परिभाषित किए गए हैं, जैसे –
- Penetrative Sexual Assault (धारा 3) – बच्चे के शरीर में यौन अंग या वस्तु का प्रवेश करना।
- Aggravated Penetrative Sexual Assault (धारा 5) – जब अपराधी पुलिसकर्मी, शिक्षक, रिश्तेदार, डॉक्टर आदि हो।
- Sexual Assault (धारा 7) – बच्चे को यौन तरीके से छूना।
- Sexual Harassment (धारा 11) – अश्लील बातें करना, अश्लील सामग्री दिखाना।
- Child Pornography (धारा 13-15) – बच्चे की अश्लील सामग्री बनाना, प्रसारित करना।
इन अपराधों पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
6. POCSO अधिनियम में दंड का प्रावधान क्या है?
POCSO अधिनियम में अपराध की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग दंड निर्धारित किए गए हैं –
- Penetrative Sexual Assault – न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास।
- Aggravated Penetrative Sexual Assault – न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर मृत्यु दंड तक।
- Sexual Assault – 3 से 5 वर्ष तक कारावास।
- Sexual Harassment – अधिकतम 3 वर्ष तक कारावास।
- Child Pornography – 5 वर्ष तक की सजा, पुनरावृत्ति पर 7 वर्ष।
इस प्रकार यह अधिनियम अपराधियों पर सख्त दंड थोपकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
7. POCSO अधिनियम में विशेष अदालतों की भूमिका क्या है?
POCSO अधिनियम की धारा 28 में विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है। इन अदालतों का उद्देश्य है कि बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई शीघ्र और संवेदनशील तरीके से हो। अधिनियम के अनुसार, मुकदमों की सुनवाई एक वर्ष के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। विशेष अदालतें बच्चा-हितैषी माहौल में सुनवाई करती हैं, ताकि बच्चा भयभीत न हो और स्वतंत्र रूप से बयान दे सके। इसके अलावा, बच्चे का बयान वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी लिया जा सकता है। इस प्रकार विशेष अदालतें न्याय प्रक्रिया को तेज़ और पीड़ित के अनुकूल बनाती हैं।
8. POCSO अधिनियम में अनिवार्य रिपोर्टिंग क्या है?
POCSO अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को बच्चे के साथ यौन अपराध की जानकारी मिलती है, तो उसका रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इस प्रावधान का उद्देश्य है कि अपराध छिप न पाए और समय रहते बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, इसकी आलोचना भी होती है क्योंकि कई बार परिवार या शिक्षक रिपोर्ट करने से हिचकते हैं और कानूनी कार्यवाही से डरते हैं।
9. POCSO अधिनियम की आलोचना क्यों होती है?
हालांकि POCSO अधिनियम बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएँ भी हैं –
- नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं है, जिससे किशोर प्रेम संबंध भी अपराध माने जाते हैं।
- कई बार झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं।
- अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ गया है।
- लंबी न्यायिक प्रक्रिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है।
इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि अधिनियम में व्यावहारिक संशोधन की आवश्यकता है।
10. POCSO अधिनियम में सुधार की क्या आवश्यकता है?
POCSO अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधार आवश्यक हैं –
- 16-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए अलग प्रावधान होना चाहिए, जहाँ सहमति-आधारित रिश्तों को अपराध न माना जाए।
- वास्तविक शोषण और सहमति-आधारित मामलों में अंतर करने की आवश्यकता है।
- बच्चों और परिवार को मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना चाहिए।
- समाज में जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए।
इन सुधारों से अधिनियम और अधिक व्यावहारिक तथा न्यायसंगत बन सकता है।