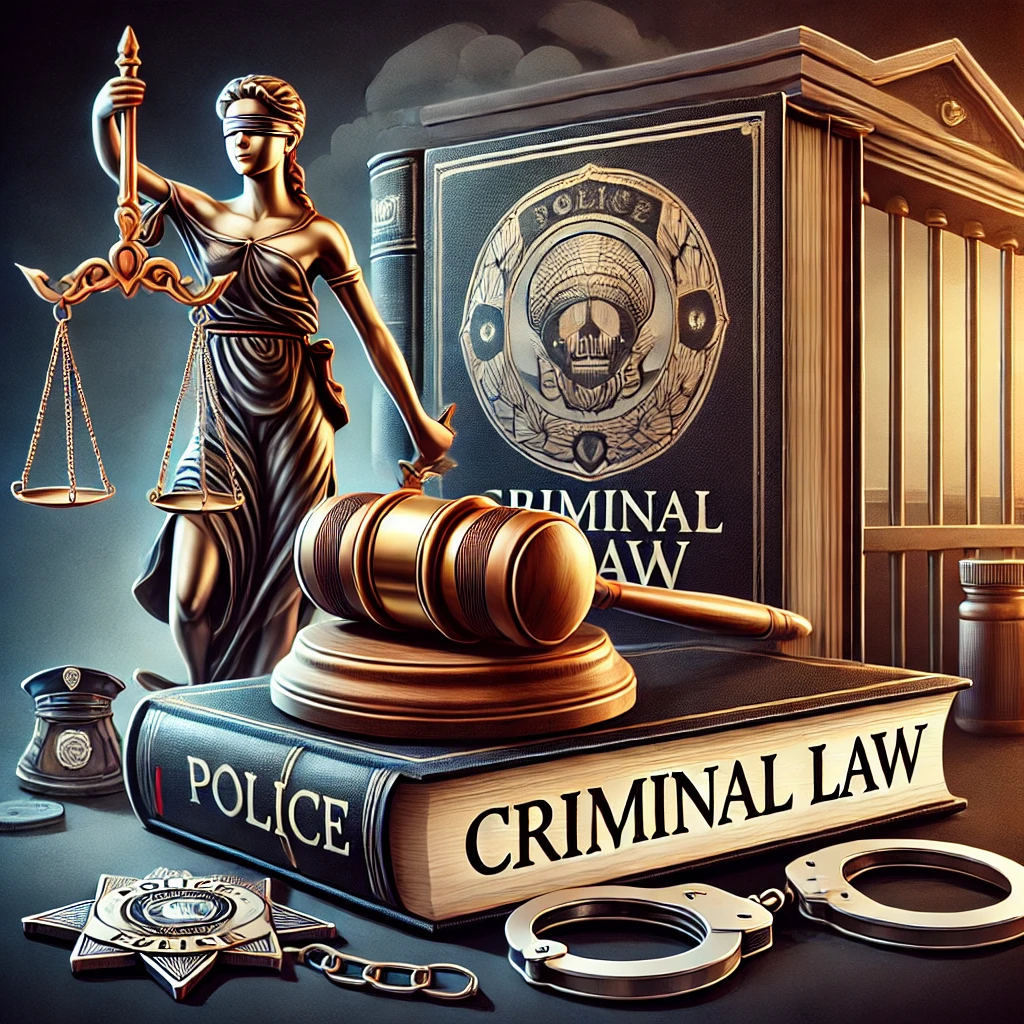बलात्कार कानूनः संशोधन और चुनौतियाँ — एक विश्लेषणात्मक और समसामयिक लेख
प्रस्तावना:
भारत में बलात्कार न केवल एक जघन्य अपराध है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान, गरिमा और मौलिक अधिकारों पर सीधा आघात करता है। लंबे समय तक भारत के बलात्कार कानूनों को रूढ़िगत, संकीर्ण, और पीड़िता विरोधी समझा जाता रहा है। लेकिन समय-समय पर हुए सामाजिक आंदोलनों, जन आक्रोश और न्यायिक हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। फिर भी प्रभावी कार्यान्वयन, पीड़ितों की सुरक्षा, और समाज में बढ़ती लैंगिक हिंसा के संदर्भ में अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
बलात्कार की परिभाषा और कानूनी धारा:
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। इसमें महिला की बिना सहमति या इच्छा के यौन संबंध बनाना या शारीरिक प्रवेश करना बलात्कार माना जाता है। इसकी सजा धारा 376 के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा निर्धारित है।
प्रमुख संशोधन (Amendments) और उनका प्रभाव:
1. 1983 संशोधन:
- पहली बार बलात्कार के मामलों में कस्टोडियल रेप (पुलिस हिरासत में बलात्कार), गैंग रेप, और झूठे आरोपों से सुरक्षा जैसे प्रावधान जोड़े गए।
- बलात्कार मामलों में इन-कैमरा ट्रायल की व्यवस्था की गई।
2. 2013 – निर्भया कांड के बाद ऐतिहासिक संशोधन (Criminal Law Amendment Act, 2013):
- बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाया गया।
- मौखिक, गुदा और वस्तु-प्रवेश भी बलात्कार की श्रेणी में जोड़े गए।
- सात नई धाराएं जोड़ी गईं — जैसे धारा 354-A से 354-D, जिसमें यौन उत्पीड़न, पीछा करना, तेजाब हमला आदि को शामिल किया गया।
- 16 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के लिए न्यूनतम सजा 20 वर्ष निर्धारित की गई।
3. 2018 संशोधन (POCSO & Criminal Law Amendment):
- 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ बलात्कार पर मृत्युदंड की संभावना जोड़ी गई।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना पर बल दिया गया।
बलात्कार कानूनों के समक्ष चुनौतियाँ:
1. कानूनों का क्रियान्वयन और पुलिस व्यवस्था:
- कई मामलों में FIR दर्ज करने में देरी और पीड़िता की उपेक्षा देखी जाती है।
- पुलिस की संवेदनशीलता की कमी और भ्रांत मानसिकता भी न्याय को प्रभावित करती है।
2. न्यायिक देरी:
- कई वर्षों तक केस लंबित रहते हैं, जिससे पीड़िता का मनोबल टूटता है।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और गुणवत्ता अपर्याप्त है।
3. पीड़िता की सामाजिक और मानसिक पीड़ा:
- बलात्कार के बाद पीड़िता को समाज में बदनामी, तिरस्कार और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।
- अक्सर उसे ही दोषी मान लिया जाता है।
4. झूठे मामले और दुरुपयोग की आशंका:
- कुछ मामलों में IPC की धारा 376 का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है, जिससे वास्तविक पीड़िताओं की स्थिति कमजोर हो जाती है।
5. वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) का अपराधीकरण न होना:
- भारत में अभी तक वैवाहिक बलात्कार को IPC की धारा 375 के अपवाद में रखा गया है, जिसे मानवाधिकार और लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से अत्यधिक आलोचना मिल रही है।
समाधान और सुधार की दिशा में सुझाव:
- पुलिस और न्यायपालिका का लैंगिक प्रशिक्षण (Gender Sensitization):
- पुलिस अधिकारियों और न्यायाधीशों को नियमित रूप से यौन हिंसा मामलों की समझ और सहानुभूति पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाना और उनकी निगरानी:
- लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाई जाए।
- साक्ष्य संरक्षण और फोरेंसिक सहायता:
- मेडिकल सबूतों को जल्द और सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करने के लिए सभी अस्पतालों में प्रशिक्षित स्टाफ और किट उपलब्ध कराई जाए।
- पीड़ित सहायता कार्यक्रम (Victim Support Program):
- मानसिक, कानूनी और आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए।
- वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण:
- कानून में जरूरी संशोधन कर पति द्वारा बलपूर्वक यौन संबंध को भी बलात्कार की श्रेणी में लाना चाहिए।
निष्कर्ष:
बलात्कार कानूनों में हुए संशोधन निश्चित रूप से महिला सुरक्षा की दिशा में मजबूत कदम हैं, लेकिन जब तक इनका प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव, और न्यायिक प्रणाली में सुधार नहीं होता, तब तक वास्तविक सुरक्षा की गारंटी संभव नहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां संविधान महिलाओं को समानता, गरिमा और जीवन का अधिकार देता है, वहाँ बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाओं का होना न केवल कानून व्यवस्था की विफलता है, बल्कि सामाजिक चेतना की कमी भी दर्शाता है। कानूनों के साथ-साथ समाज को भी बदलने की आवश्यकता है।