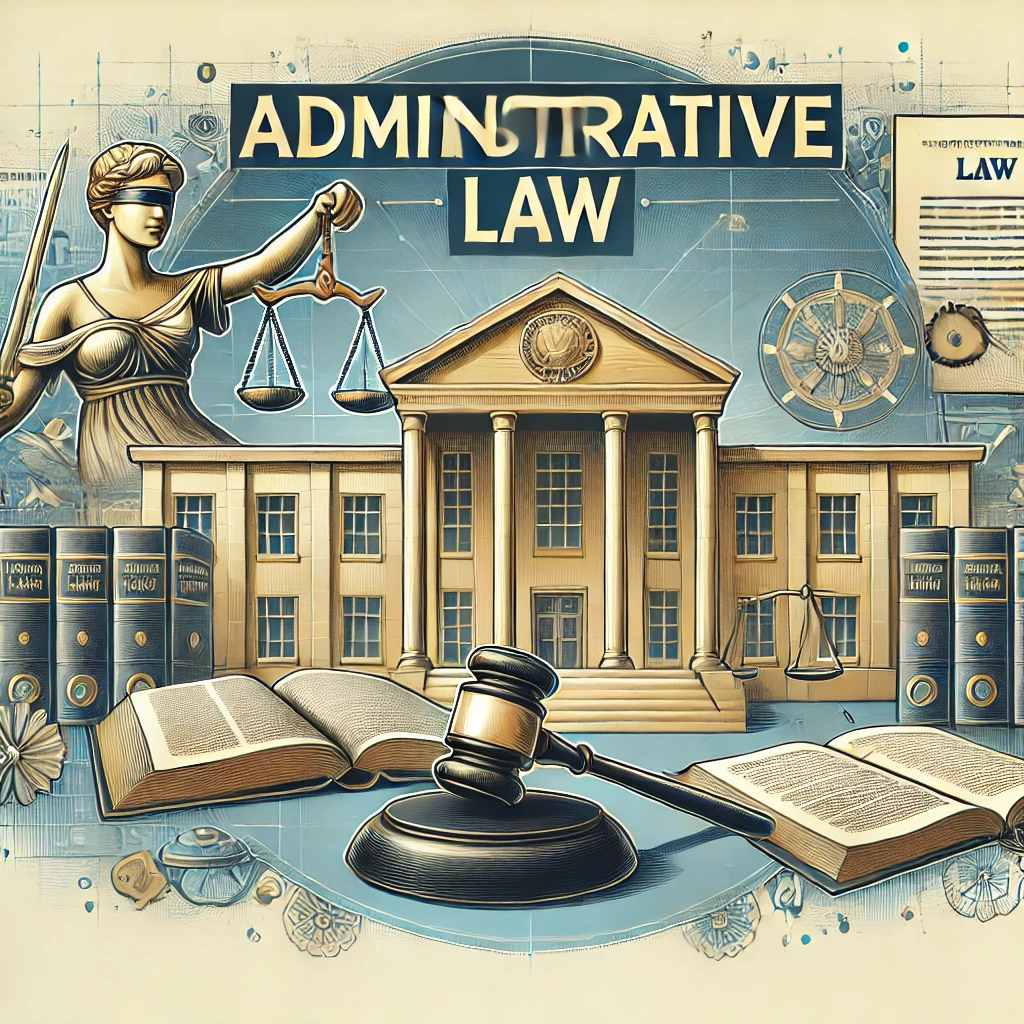प्रशासनिक विधि – शॉर्ट आंसर
1. प्रशासनिक विधि से क्या अभिप्राय है?
प्रशासनिक विधि विधि की वह शाखा है जो राज्य और उसके प्रशासनिक अंगों की शक्तियों, अधिकारों तथा उनके उपयोग पर नियंत्रण का अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका और प्रशासन जनता के अधिकारों का हनन न करें और उनकी कार्यवाही विधि के अधीन हो। प्रशासनिक विधि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखती है। यह विषय विधायिका द्वारा प्रदत्त शक्तियों, प्रशासनिक विवेकाधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन तथा प्राकृतिक न्याय जैसे सिद्धांतों से संबद्ध है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक विधि का महत्व और अधिक बढ़ गया है क्योंकि शासन के अधिकतर कार्य प्रशासनिक अंगों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
2. प्रशासनिक विधि की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
प्रशासनिक विधि की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं—
(1) यह कार्यपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों को नियंत्रित करती है।
(2) यह नागरिकों को मनमानी और दुरुपयोग से बचाती है।
(3) यह न्यायिक पुनरावलोकन और प्राकृतिक न्याय जैसे सिद्धांतों पर आधारित है।
(4) इसका मुख्य स्रोत संविधान और न्यायालयों के निर्णय हैं।
(5) यह एक गतिशील विधि है जो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है।
इस प्रकार प्रशासनिक विधि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रशासन और जनता के बीच न्यायसंगत संतुलन स्थापित करती है।
3. प्रशासनिक विधि के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं?
प्रशासनिक विधि के स्रोत मुख्य रूप से चार प्रकार के हैं—
(1) संविधान – जो सरकार की संरचना और सीमाएँ तय करता है।
(2) विधान (Statute Law) – संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम।
(3) न्यायिक निर्णय – उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय प्रशासनिक विधि को दिशा देते हैं।
(4) प्रथाएँ और परंपराएँ – शासन संबंधी व्यवहार से विकसित मानदंड भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
इसके अतिरिक्त लोकपाल, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आयोग जैसे आधुनिक कानून भी प्रशासनिक विधि के स्रोत माने जाते हैं।
4. प्रशासनिक विधि का महत्व समझाइए।
प्रशासनिक विधि का महत्व इस बात में निहित है कि यह सरकार की शक्तियों और जनता के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करती है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन को व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि इन पर नियंत्रण न हो तो मनमानी और भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। प्रशासनिक विधि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करती है तथा न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा कार्यपालिका की सीमाएँ निर्धारित करती है। इसके माध्यम से पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और विधि का शासन (Rule of Law) स्थापित होता है।
5. ‘Delegated Legislation’ से क्या तात्पर्य है?
Delegated Legislation का अर्थ है कि विधायिका अपनी कुछ विधायी शक्तियों को कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दे, ताकि वे नियम, विनियम और उपविधियाँ बना सकें। आधुनिक समय में यह आवश्यक हो गया है क्योंकि संसद या विधानमंडल हर छोटे-बड़े विषय पर कानून नहीं बना सकता। Delegated Legislation के माध्यम से प्रशासनिक संस्थाएँ तकनीकी और विशिष्ट विषयों पर नियम बना सकती हैं। हालांकि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो, इसके लिए न्यायालय, विधायिका और प्रशासनिक नियंत्रण की व्यवस्था की गई है।
31. प्रशासनिक विवेकाधिकार (Administrative Discretion) क्या है?
प्रशासनिक विवेकाधिकार से अभिप्राय है कि प्रशासनिक अधिकारी किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग कर सके। यह शक्ति प्रशासनिक कार्यों को लचीला और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। किन्तु इस विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। यह केवल विधि के अधीन और न्यायसंगत उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। न्यायालयों ने कहा है कि विवेक का प्रयोग सदैव सार्वजनिक हित और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।
32. Delegated Legislation पर न्यायिक नियंत्रण कैसे होता है?
न्यायालय Delegated Legislation पर नियंत्रण न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के माध्यम से करता है। यदि कोई अधीनस्थ विधान संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। इसी प्रकार यदि नियम या उपविधियाँ मूल अधिनियम से परे हों, मनमाने हों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करें, तो न्यायालय उन्हें निरस्त कर सकता है। यह नियंत्रण प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और विधि का शासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
33. प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Administrative Tribunals) की आवश्यकता क्यों पड़ी?
न्यायालयों पर मामलों का बोझ बहुत अधिक होने के कारण और प्रशासनिक विषयों में विशेषज्ञता की आवश्यकता के कारण प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई। ये न्यायाधिकरण त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करने में सहायक होते हैं। सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा इनमें तकनीकी और विशिष्ट विषयों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति होती है। उदाहरणस्वरूप – केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की स्थापना कर्मचारियों के सेवा विवादों के समाधान हेतु की गई है।
34. प्रशासनिक न्यायाधिकरण और न्यायपालिका में क्या अंतर है?
न्यायाधिकरण विशेष रूप से प्रशासनिक और तकनीकी मामलों की सुनवाई हेतु स्थापित किए जाते हैं, जबकि न्यायालय सामान्य विधिक विवादों का निपटारा करते हैं। न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया लचीली होती है, जबकि न्यायालय कठोर प्रक्रिया का पालन करते हैं। न्यायालय संविधान के अधीन स्वतंत्र निकाय हैं, जबकि न्यायाधिकरण अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं।
35. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) क्या है?
न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। यदि कोई कार्य या कानून संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकते हैं। यह लोकतंत्र और विधि के शासन की रक्षा करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में यह शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है।
36. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या हैं?
प्राकृतिक न्याय के प्रमुख सिद्धांत दो हैं—
(1) Audi Alteram Partem – किसी व्यक्ति को दंडित करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।
(2) Rule Against Bias – कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।
इसके अतिरिक्त निर्णय का कारण बताना भी प्राकृतिक न्याय का हिस्सा माना जाता है। इन सिद्धांतों से निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित होता है।
37. Audi Alteram Partem सिद्धांत का महत्व क्या है?
Audi Alteram Partem का अर्थ है “दूसरी पार्टी को भी सुनो”। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी व्यक्ति को दंड देने या अधिकार से वंचित करने से पहले उसे अपनी बात रखने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया का मूलभूत अंग है। इसके अभाव में लिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण माना जाएगा और न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है।
38. Rule Against Bias क्या है?
इस सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्याय नहीं कर सकता। यदि न्यायाधीश या अधिकारी के पास किसी मामले में व्यक्तिगत हित, पूर्वाग्रह या संबंध हो, तो वह निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकता। अतः ऐसी स्थिति में निर्णय अवैध माना जाता है। यह सिद्धांत प्रशासनिक न्याय और निष्पक्षता की गारंटी देता है।
39. कारण देने का दायित्व क्यों आवश्यक है?
किसी भी प्रशासनिक निर्णय में कारण देना आवश्यक है क्योंकि यह पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाता है। जब निर्णय के पीछे तर्क स्पष्ट होते हैं, तब प्रभावित व्यक्ति अपील या पुनरावलोकन का सहारा ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि बिना कारण दिए गए प्रशासनिक आदेश मनमाने माने जाएंगे और वे न्यायिक समीक्षा के अधीन रद्द किए जा सकते हैं।
40. रिट्स (Writs) कितने प्रकार के होते हैं?
भारत में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पाँच प्रकार की रिट्स जारी कर सकते हैं—
(1) हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) – अवैध निरुद्धि से मुक्ति हेतु।
(2) मैंडेमस (Mandamus) – सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन कराने हेतु।
(3) सर्टियोरारी (Certiorari) – अवैध निर्णय को निरस्त करने हेतु।
(4) प्रोहीबिशन (Prohibition) – न्यायाधिकरण को अपनी अधिकार सीमा से बाहर कार्य करने से रोकने हेतु।
(5) क्वो वारंटो (Quo Warranto) – अवैध रूप से पद पर आसीन व्यक्ति को हटाने हेतु।
41. हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) रिट क्या है?
हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है – “तुम शरीर प्रस्तुत करो”। यह रिट किसी व्यक्ति को अवैध निरुद्धि से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है। यदि किसी नागरिक को बिना वैध कारण अथवा बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में रखा गया है, तो न्यायालय हेबियस कॉर्पस रिट जारी कर उसे तुरंत अदालत में प्रस्तुत करने और उसकी रिहाई सुनिश्चित करने का आदेश देता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रभावी साधन है।
42. मैंडेमस (Mandamus) रिट क्या है?
मैंडेमस रिट का अर्थ है “आदेश देना”। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकरण अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो न्यायालय उसे वह कार्य करने का आदेश देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी नागरिक को वैध अधिकार देने से इंकार कर दे, तो अदालत Mandamus जारी कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपने कर्तव्य से विमुख न हों।
43. प्रोहीबिशन (Prohibition) रिट का उद्देश्य क्या है?
प्रोहीबिशन रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है। इसका उद्देश्य उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना होता है। यदि कोई न्यायाधिकरण अपने वैधानिक अधिकार से अधिक जाकर निर्णय लेने की कोशिश करता है, तो अदालत Prohibition रिट द्वारा उसे रोक देती है।
44. सर्टियोरारी (Certiorari) रिट कब जारी होती है?
सर्टियोरारी रिट किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को निरस्त करने के लिए जारी होती है। यह तब लागू होती है जब निचली अदालत या प्राधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया हो, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया हो या कोई गंभीर विधिक त्रुटि की हो। इससे अवैध आदेश अमान्य हो जाते हैं।
45. क्वो वारंटो (Quo Warranto) रिट का महत्व क्या है?
क्वो वारंटो रिट का अर्थ है “किस अधिकार से”। यह रिट तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर आसीन हो। अदालत यह पूछ सकती है कि वह किस अधिकार से उस पद पर बैठा है। यदि उसके पास वैध अधिकार नहीं है, तो उसे पद से हटा दिया जाता है। यह रिट सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की वैधता की रक्षा करती है।
46. लोकपाल (Ombudsman) की भूमिका क्या है?
लोकपाल नागरिकों की शिकायतों की जांच करने वाला स्वतंत्र प्राधिकरण है। इसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित किया गया जिसके तहत केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की गई। लोकपाल भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग की जांच कर सकता है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।
47. लोकायुक्त (Lokayukta) की शक्तियाँ क्या हैं?
लोकायुक्त राज्यों में स्थापित एक संस्था है जिसका कार्य राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या कदाचार की जांच करना है। यह स्वतंत्र निकाय होता है और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी शक्तियों में शिकायतों की जांच, रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सुधारात्मक सुझाव देना शामिल है। यद्यपि इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, फिर भी यह संस्था प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण है।
48. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य क्या है?
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांग सके। इस कानून के तहत 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह अधिनियम भ्रष्टाचार को रोकने, नागरिकों को सशक्त बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने का महत्वपूर्ण साधन है।
49. जनहित याचिका (PIL) से क्या तात्पर्य है?
जनहित याचिका वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या संस्था, किसी भी सार्वजनिक हित के मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। इसमें याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित होना आवश्यक नहीं है। PIL का उद्देश्य गरीबों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा करना है। न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण, बंधुआ मज़दूरी, प्रदूषण, मानवाधिकार उल्लंघन आदि मामलों में PIL को स्वीकार किया है।
50. भारत में प्रशासनिक विधि के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
भारत में प्रशासनिक विधि का विकास संविधान के साथ जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया, जिससे प्रशासनिक शक्तियों का विस्तार हुआ। न्यायालयों ने कार्यपालिका की मनमानी पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू किया। लोकपाल, सूचना का अधिकार और मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना ने भी प्रशासनिक विधि को मजबूत किया।
51. प्राकृतिक न्याय और संवैधानिक न्याय में अंतर बताइए।
प्राकृतिक न्याय निष्पक्षता, सुनवाई का अवसर और पूर्वाग्रह रहित निर्णय जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। यह लिखित कानून नहीं है बल्कि न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत है। दूसरी ओर संवैधानिक न्याय संविधान में निहित अधिकारों और प्रावधानों से जुड़ा है। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक न्याय है जबकि बिना सुनवाई दंड न देना प्राकृतिक न्याय है।
52. प्रशासनिक कार्यवाही में न्यायिक पुनरावलोकन क्यों आवश्यक है?
प्रशासनिक कार्यवाही में न्यायिक पुनरावलोकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रशासन को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और इनके दुरुपयोग की संभावना रहती है। न्यायालय यह देखता है कि कार्यवाही विधि के अनुरूप है या नहीं। यदि कोई आदेश मनमाना है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। इससे विधि का शासन सुनिश्चित होता है।
53. न्यायालय आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते?
न्यायालय सामान्यतः आर्थिक और वित्तीय नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि ये नीतिगत विषय माने जाते हैं और इनमें विशेषज्ञता तथा विवेक सरकार का क्षेत्र है। जब तक कोई नीति संविधान का उल्लंघन न करे या मनमानी न हो, न्यायालय उसमें दखल नहीं देता। यह सिद्धांत “R.K. Garg v. Union of India” (1981) मामले में स्थापित किया गया।
54. शासकीय संविदात्मक दायित्व (Contractual Liability) क्या है?
जब सरकार या उसके अधिकारी किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध करते हैं, तो वे उसी प्रकार उत्तरदायी होते हैं जैसे कोई निजी व्यक्ति होता है। अनुच्छेद 299 के अनुसार, भारत सरकार और राज्य सरकारों के अनुबंध लिखित और विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। यदि ऐसा अनुबंध वैध रूप से किया गया है और उसका उल्लंघन होता है, तो सरकार पर संविदात्मक दायित्व लागू होता है।
55. शासकीय अपकृत्य दायित्व (Tortious Liability) क्या है?
यदि सरकार या उसके कर्मचारी किसी नागरिक को हानि पहुँचाते हैं, तो सरकार पर अपकृत्य दायित्व लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए सरकारी कर्मचारी की लापरवाही से किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान हो, तो सरकार जिम्मेदार होगी। हालांकि संप्रभु कार्यों (Sovereign Functions) में सरकार को प्रतिरक्षा प्राप्त है, जैसे – युद्ध संचालन या विधि निर्माण।
56. प्रशासनिक विवेकाधिकार पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है?
प्रशासनिक विवेकाधिकार आवश्यक है, परंतु यदि इसका नियंत्रण न हो तो अधिकारी मनमाने और पक्षपातपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। नियंत्रण के लिए न्यायालय यह देखता है कि विवेक का प्रयोग विधि के अनुसार हुआ है या नहीं। यदि निर्णय मनमाना है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है या उद्देश्य से भटका है, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। यह नियंत्रण नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
57. न्यायिक नियंत्रण के अलावा प्रशासनिक नियंत्रण क्या है?
प्रशासनिक नियंत्रण वह है जिसमें उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यवाही की समीक्षा और पर्यवेक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए, विभागीय जाँच, अपील, पुनरीक्षण और रिपोर्टिंग सिस्टम। यह नियंत्रण न्यायालयों से पहले ही प्रशासन में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
58. विधायी नियंत्रण (Legislative Control) क्या है?
विधायी नियंत्रण का अर्थ है कि संसद या राज्य विधानमंडल कार्यपालिका की शक्तियों पर निगरानी रखे। इसमें नियमों और उपविधियों की समीक्षा, प्रश्नकाल, चर्चा और समितियों की रिपोर्ट शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्यपालिका विधायिका द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग न करे।
59. आयोगों की जांच (Commission of Inquiry) का महत्व क्या है?
आयोगों की जांच का उद्देश्य विवादित या महत्वपूर्ण मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच करना है। सरकार किसी मुद्दे की सच्चाई जानने के लिए आयोग नियुक्त करती है। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और सुधार में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, शाह आयोग, मंडल आयोग।
60. मानवाधिकार आयोग की प्रशासनिक विधि में भूमिका क्या है?
मानवाधिकार आयोग नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में प्रताड़ना, अवैध निरुद्धि या भेदभाव का सामना करना पड़े, तो आयोग जांच कर सकता है। यह प्रशासनिक कार्यवाही पर नियंत्रण रखता है और सरकार को सिफारिशें देता है।
61. प्रशासनिक विधि और संविधान का क्या संबंध है?
प्रशासनिक विधि संविधान से प्रेरित और नियंत्रित है। संविधान कार्यपालिका को शक्तियाँ देता है लेकिन साथ ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। प्रशासनिक विधि इन शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है ताकि संविधान का उल्लंघन न हो।
62. भारत में रिट क्षेत्राधिकार किसके पास है?
भारत में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए सक्षम हैं। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और अन्य वैधानिक अधिकारों दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है।
63. Doctrine of Ultra Vires क्या है?
Doctrine of Ultra Vires का अर्थ है – “अधिकार क्षेत्र से बाहर”। यदि कोई प्रशासनिक प्राधिकरण अपनी वैधानिक शक्ति से परे जाकर कोई आदेश पारित करता है, तो वह Ultra Vires कहलाता है और न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। यह सिद्धांत प्रशासनिक कार्यों की वैधता की जांच का प्रमुख साधन है।
64. Rule of Law और प्रशासनिक विधि में क्या संबंध है?
Rule of Law का अर्थ है कि सभी व्यक्ति, संस्था और सरकार विधि के अधीन हैं और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। प्रशासनिक विधि Rule of Law को व्यवहार में लागू करती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक कार्यवाही कानूनी, निष्पक्ष और उत्तरदायी हो।
65. जनहित याचिका और पारंपरिक वाद में अंतर बताइए।
पारंपरिक वाद में केवल वही व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है जो स्वयं पीड़ित हो। जबकि जनहित याचिका में कोई भी व्यक्ति समाज या समुदाय के हित के लिए अदालत में जा सकता है। PIL का उद्देश्य गरीबों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा करना है।
66. Doctrine of Legitimate Expectation क्या है?
इस सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई सरकारी प्राधिकरण किसी नागरिक को कोई सुविधा या लाभ देने की परंपरा बना देता है, तो नागरिक को यह वैध अपेक्षा होती है कि उसे वही लाभ दिया जाएगा। यदि बिना कारण इसे समाप्त कर दिया जाए, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
67. Doctrine of Proportionality क्या है?
Doctrine of Proportionality का अर्थ है कि प्रशासनिक निर्णय तर्कसंगत और आवश्यक सीमा तक ही होना चाहिए। दंड या आदेश का स्वरूप अपराध या परिस्थिति के अनुपात में होना चाहिए। यदि निर्णय अत्यधिक कठोर या अनुचित है, तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है।
68. Doctrine of Malafide क्या है?
यदि कोई प्रशासनिक कार्य या आदेश व्यक्तिगत द्वेष, दुर्भावना या गलत उद्देश्य से किया गया हो, तो उसे Malafide कहा जाता है। ऐसे आदेश न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत शत्रुता के कारण निलंबित करना।
69. Doctrine of Reasonableness क्या है?
इस सिद्धांत के अनुसार, प्रशासनिक आदेश तार्किक और न्यायोचित होना चाहिए। कोई भी मनमाना, असंगत या अनुचित आदेश न्यायालय में चुनौती दी जा सकता है। यह सिद्धांत Rule of Law और प्राकृतिक न्याय की रक्षा करता है।
70. प्रशासनिक विधि की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है?
आज के लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक विधि की प्रासंगिकता अत्यधिक है। प्रशासन नागरिकों के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है – शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार आदि। प्रशासनिक विधि यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी कार्यवाही पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिकों के अधिकारों के अनुरूप हो।