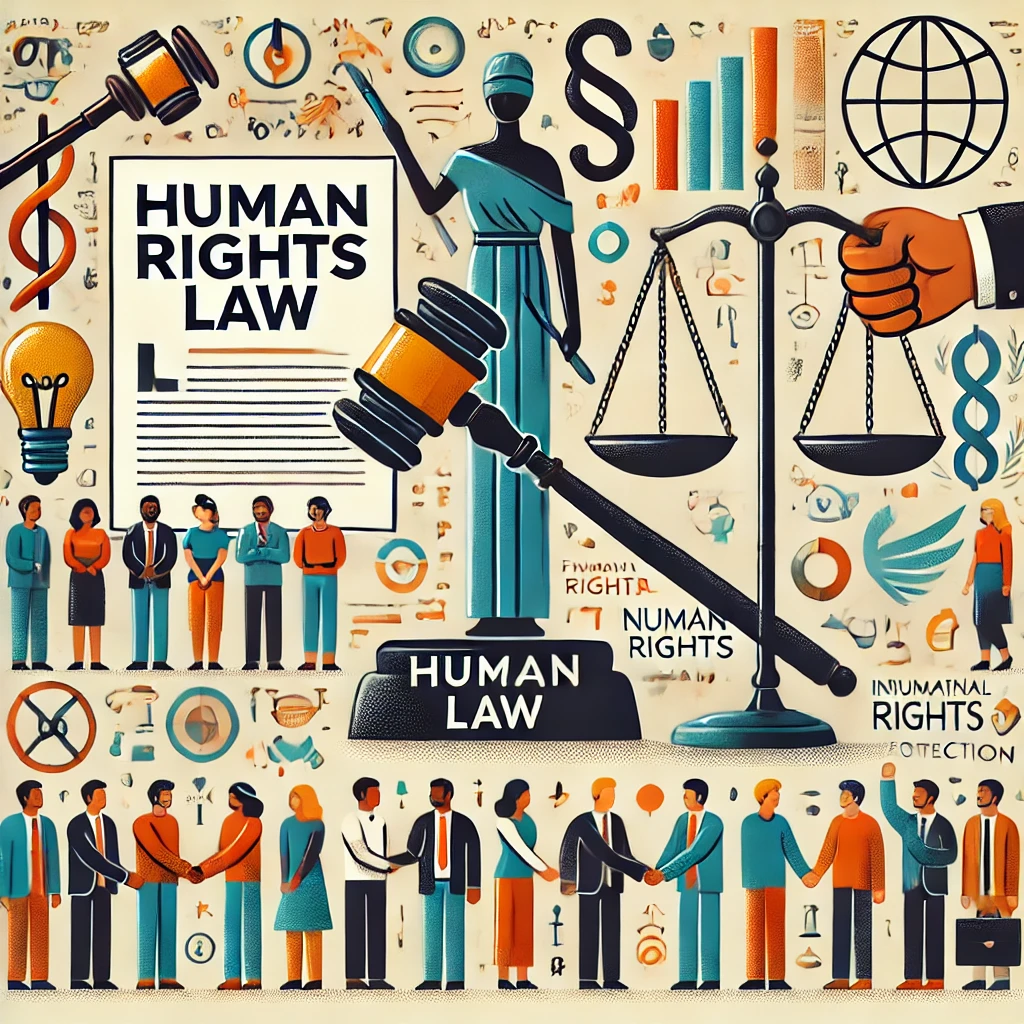लेख शीर्षक: “पुलिस और हिरासत में अत्याचार: संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता”
भूमिका:
भारत में पुलिस व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन जब यही व्यवस्था अत्याचार, हिंसा और अमानवीय व्यवहार की प्रतीक बन जाती है, तो यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। हिरासत में अत्याचार (custodial torture) और मौतें न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हैं, बल्कि ये राज्य की जवाबदेही को भी कठघरे में खड़ा करती हैं।
हिरासत में अत्याचार की परिभाषा और स्वरूप:
हिरासत में अत्याचार वह स्थिति है जब पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसियां किसी आरोपी, संदिग्ध या व्यक्ति को अपनी हिरासत में रखते समय उसके साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से अमानवीय व्यवहार करती हैं। इसमें मारपीट, नींद से वंचित रखना, नग्न करना, यौन हिंसा, और फर्जी मुठभेड़ जैसी घटनाएं शामिल हो सकती हैं।
प्रमुख संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:
- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें ‘जीने का अधिकार’ केवल शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी सम्मिलित है।
- अनुच्छेद 22 – गिरफ्तारी के बाद कानूनी सलाह और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी का अधिकार।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 330 और 331 के अंतर्गत पुलिस द्वारा की गई यातना के लिए सजा का प्रावधान है।
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 – राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) हिरासत में हुई मौतों और अत्याचार की जांच करता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 176 में मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में मौत की जांच का प्रावधान है।
प्रमुख न्यायिक फैसले:
- डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997): सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए 11 दिशानिर्देश जारी किए, जैसे—गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देना, मेडिकल जांच, गिरफ्तारी की रसीद, आदि।
- प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार: पुलिस सुधारों की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए थे ताकि पुलिस राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर कार्य करे।
- नीलगिरी सिंह केस (2000): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में अत्याचार राज्य द्वारा हिंसा का उदाहरण है, जिसके लिए मुआवज़ा आवश्यक है।
हिरासत में अत्याचार के कारण:
- जवाबदेही की कमी और पुलिस सुधारों का अभाव
- राजनैतिक दबाव और लक्ष्यों को पूरा करने की होड़
- न्यायिक प्रणाली की धीमी प्रक्रिया
- आरोपी से कबूलनामे की जबरदस्ती
- पुलिस प्रशिक्षण में मानवाधिकार शिक्षा का अभाव
आंकड़े और वास्तविकता:
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, हर वर्ष दर्जनों हिरासत में मौतें होती हैं, जिनमें अधिकांश मामलों में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। कई बार इन मौतों को आत्महत्या या बीमारी बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है।
समाधान और सुझाव:
- पुलिस अधिकारियों के लिए अनिवार्य मानवाधिकार प्रशिक्षण।
- सीसीटीवी कैमरे और बॉडी कैमरा जैसे निगरानी उपकरणों का अनिवार्य उपयोग।
- स्वतंत्र एजेंसी द्वारा हिरासत में मौत की निष्पक्ष जांच।
- पीड़ितों को शीघ्र और पर्याप्त मुआवज़ा।
- पुलिस में कार्यरत अधिकारियों की नियुक्ति और प्रोन्नति में आचरण की समीक्षा शामिल करना।
- NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाना।
निष्कर्ष:
पुलिस और हिरासत में अत्याचार एक गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौती है। यह न केवल व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद को भी कमजोर करता है। इस समस्या का समाधान केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि व्यावहारिक सुधार, संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने से होगा। पुलिस को अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी बोध कराना और जनता के विश्वास को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।