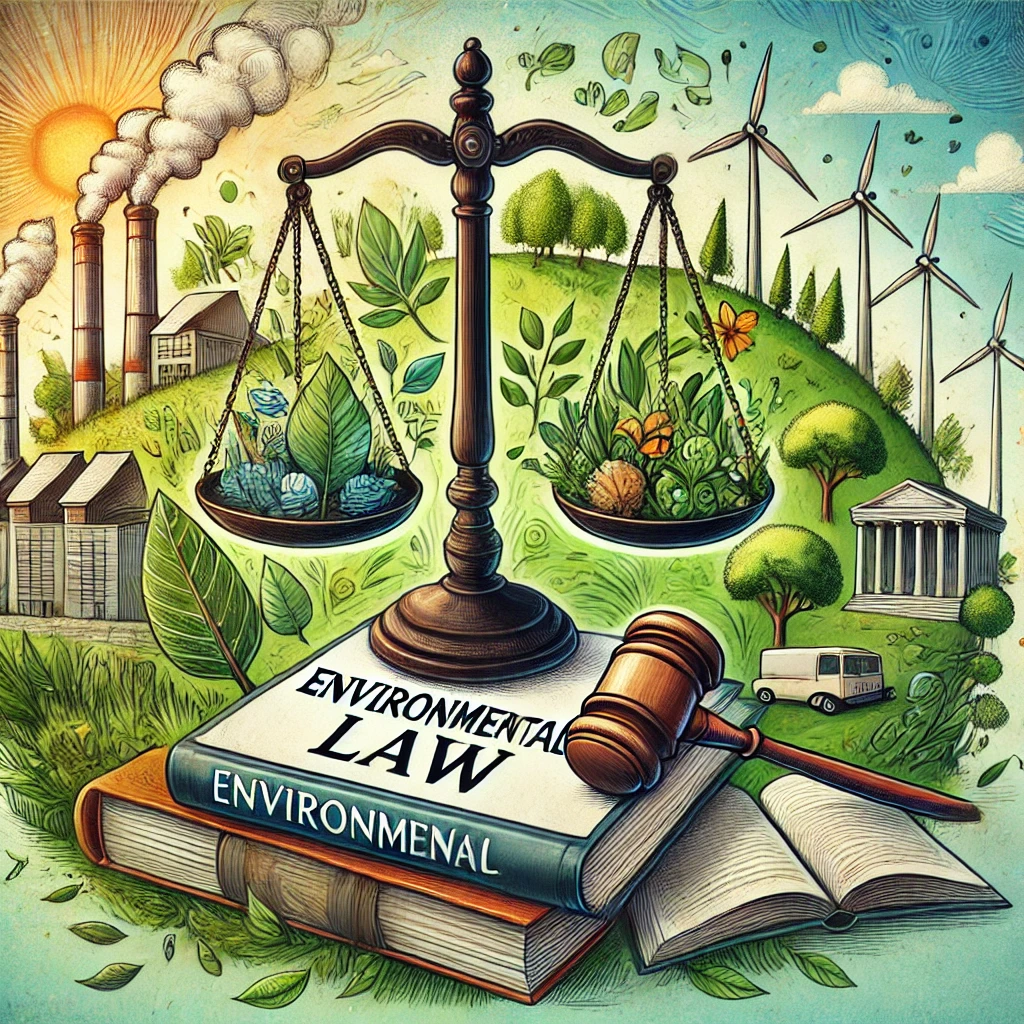लेख शीर्षक:
“पर्यावरण संरक्षण कानून और न्यायपालिका: सतत विकास की संवैधानिक अभिव्यक्ति”
परिचय:
पर्यावरण संरक्षण आज वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जल एवं वायु प्रदूषण जैसे मुद्दे मानव जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और इसे न्यायपालिका के सक्रिय सहयोग से मजबूती मिली है। न्यायपालिका न केवल पर्यावरण कानूनों की व्याख्या करती है बल्कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में निर्णायक भूमिका भी निभाती है।
भारत में पर्यावरण संरक्षण की संवैधानिक पृष्ठभूमि:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A(g) पर्यावरण संरक्षण का दायित्व सरकार और नागरिकों दोनों पर डालते हैं। अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा और वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें।
प्रमुख पर्यावरण संरक्षण कानून:
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 – यह भारत का सबसे व्यापक पर्यावरण संरक्षण कानून है, जो भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाया गया।
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- जैव विविधता अधिनियम, 2002
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
इन अधिनियमों के तहत केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन किया गया है।
न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका:
भारत की न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया और महत्वपूर्ण निर्णय दिए।
महत्वपूर्ण निर्णय:
- MC मेहता बनाम भारत संघ (1987) – गंगा नदी के प्रदूषण पर कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और प्रदूषणकारी कारखानों को बंद करने के निर्देश दिए।
- वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम केस (1996) – सुप्रीम कोर्ट ने सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत को भारतीय कानून का हिस्सा घोषित किया।
- सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) – कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा है।
- टी.एन. गोदावर्मन केस – जंगलों की रक्षा और अवैध कटाई पर रोक लगाने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति की स्थापना की।
जनहित याचिकाओं की भूमिका:
जनहित याचिकाएं (PILs) पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने का प्रभावशाली माध्यम बनी हैं। न्यायपालिका ने ऐसे मामलों में वैज्ञानिक रिपोर्टों, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों के आधार पर निर्णय लिए।
पर्यावरण और आर्थिक विकास में संतुलन:
न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया है कि आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन यह पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। न्यायपालिका ने कई बार विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने पर रोका भी है।
चुनौतियाँ:
- पर्यावरणीय कानूनों का उचित क्रियान्वयन न होना
- भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव
- जन जागरूकता की कमी
- पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी
निष्कर्ष:
भारत की न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रहरी की भूमिका निभाई है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की व्याख्या कर न्यायपालिका ने न केवल सरकार को दिशा दी है, बल्कि आम जनता को भी अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक किया है। आने वाले समय में न्यायपालिका से अपेक्षा है कि वह इस सतत संघर्ष को और अधिक प्रभावशाली बनाए और ‘पर्यावरणीय न्याय’ को सामाजिक न्याय के समकक्ष महत्व दे।
सुझाव:
- पर्यावरणीय कानूनों का कठोर अनुपालन
- न्यायालयों में विशेष ‘ग्रीन ट्रिब्यूनल’ की क्षमता में वृद्धि
- स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाना
- सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पर्यावरणीय निगरानी और संरक्षण