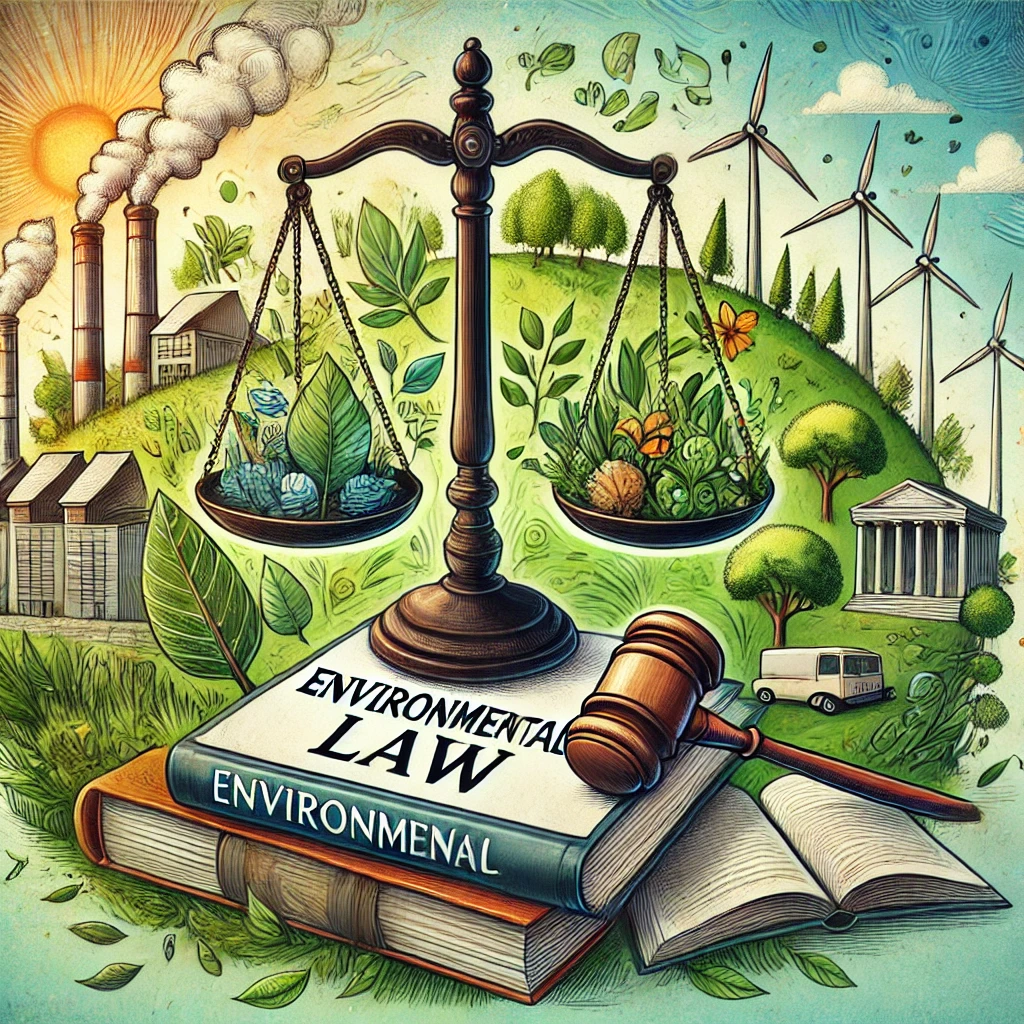लेख शीर्षक:
“पर्यावरण संरक्षण कानून और न्यायपालिकाः संवैधानिक उत्तरदायित्व से न्यायिक सक्रियता तक की यात्रा”
🔸 भूमिका:
पर्यावरण, मानव जीवन के अस्तित्व का आधार है। स्वच्छ हवा, जल, मिट्टी और हरित संसाधनों की सुरक्षा न केवल मानव अधिकारों का हिस्सा है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार का भी अनिवार्य तत्व है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और अनियंत्रित विकास ने पर्यावरण को गंभीर संकट में डाल दिया है। इस संकट से निपटने में जहां विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका सीमित रही, वहीं न्यायपालिका ने सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से पर्यावरणीय न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावशाली कार्य किया है।
🔸 पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक आधार:
- अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निदेशक तत्व) – “राज्य, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा।”
- अनुच्छेद 51A(g) (नागरिकों के मूल कर्तव्य) – “प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे।”
- अनुच्छेद 21 – “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार” को न्यायपालिका ने इस रूप में व्याख्यायित किया कि स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
🔸 प्रमुख पर्यावरणीय कानून:
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 – एक समग्र कानून जो विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करता है।
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- जैव विविधता अधिनियम, 2002
- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (NGT Act)
🔸 न्यायिक सक्रियता और ऐतिहासिक फैसले:
भारतीय न्यायपालिका ने कई बार जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा में हस्तक्षेप किया। इसके माध्यम से न्यायालयों ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन को भी प्रभावित किया।
1. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986 – ओलेम गैस रिसाव मामला):
सुप्रीम कोर्ट ने “Absolute Liability” सिद्धांत को अपनाया और प्रदूषण करने वाली कंपनियों को पूर्ण दायित्व के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया।
2. गंगा प्रदूषण मामले में आदेश:
टैनरी उद्योगों और गंदा जल छोड़ने वाले संस्थानों पर कार्यवाही, जिससे नदियों की स्वच्छता का मुद्दा प्रमुखता में आया।
3. वी. लक्ष्मी बनाम भारत सरकार:
वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े निर्देश जारी किए।
4. गोदावर्मन बनाम भारत संघ (वन संरक्षण का मामला):
सुप्रीम कोर्ट ने वन क्षेत्रों की स्पष्ट परिभाषा दी और वनों के व्यावसायिक दोहन पर रोक लगाई।
5. ताज महल संरक्षण मामला:
ताज ट्रेपेजियम ज़ोन में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण मिला।
🔸 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) की भूमिका:
NGT की स्थापना पर्यावरण से जुड़े मामलों का त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह न्यायाधिकरण अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण, अवैध खनन रोकथाम, और औद्योगिक उत्सर्जन पर निगरानी रखता है।
🔸 न्यायिक सिद्धांत जो विकसित हुए:
- सतत विकास (Sustainable Development)
- प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत (Polluter Pays Principle)
- पूर्व चेतावनी सिद्धांत (Precautionary Principle)
- लोक भागीदारी का अधिकार (Right to Public Participation)
- पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) का महत्व
🔸 चुनौतियाँ:
- न्यायालयों के आदेशों का पालन न होना
- कार्यपालिका की उदासीनता
- पर्यावरणीय मुद्दों का राजनीतिकरण
- जनसंख्या दबाव और अतिक्रमण
- पर्यावरणीय कानूनों के समुचित क्रियान्वयन की कमी
🔸 समाधान और सुझाव:
- पर्यावरण शिक्षा को स्कूल स्तर से अनिवार्य बनाना
- स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त करना
- जन भागीदारी आधारित नीति निर्माण
- NGT और पर्यावरणीय निकायों को और अधिक संसाधन देना
- कठोर दंडात्मक प्रावधानों को लागू करना
🔸 निष्कर्ष:
पर्यावरण संरक्षण न केवल एक कानूनी या प्रशासनिक दायित्व है, बल्कि यह भावी पीढ़ियों के लिए उत्तरदायित्व है। भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में न केवल जागरूकता बढ़ाई, बल्कि उसे एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित भी किया। अब आवश्यकता है कि न्यायालयों के साथ-साथ शासन, प्रशासन और आम नागरिक भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण मिल सके।