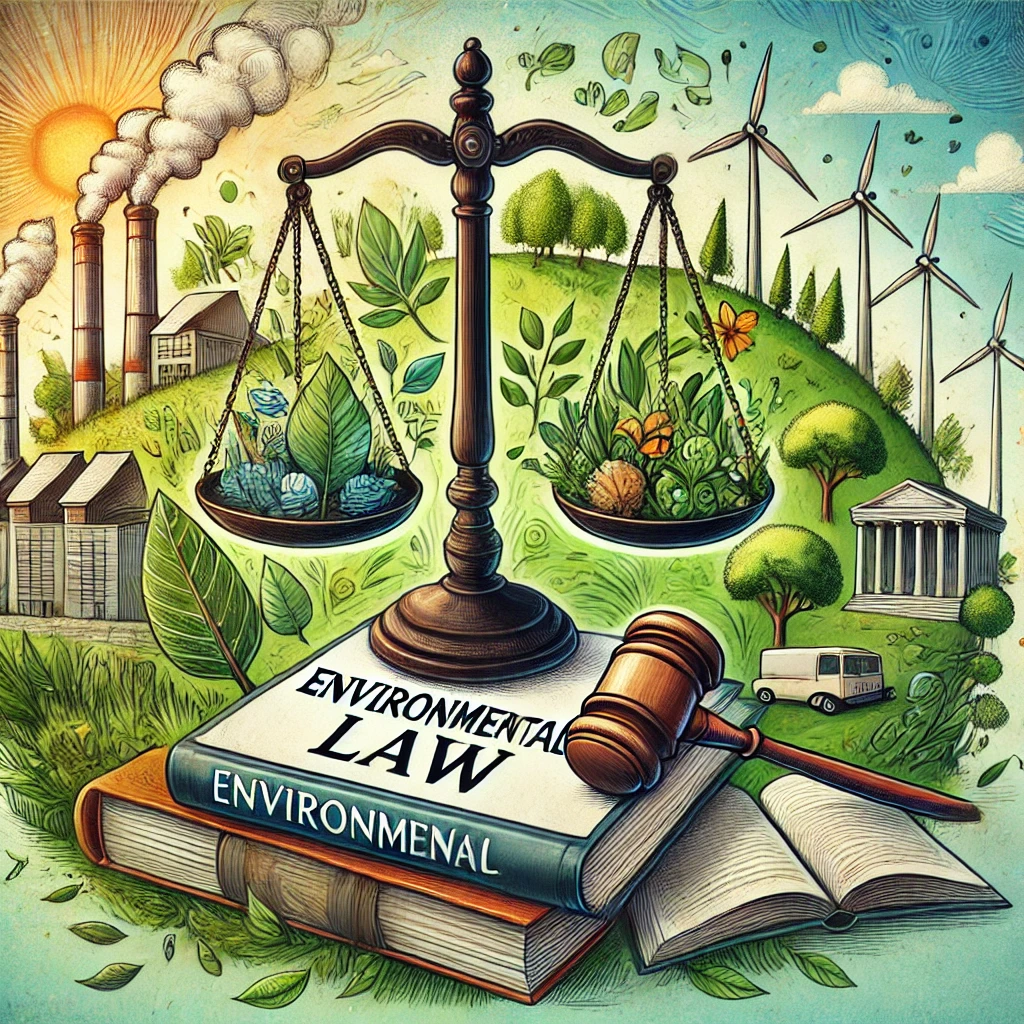पर्यावरण संरक्षण कानून और न्यायपालिकाः संवैधानिक उत्तरदायित्व से न्यायिक सक्रियता तक की यात्रा
प्रस्तावना:
पर्यावरण की रक्षा न केवल नैतिक कर्तव्य है, बल्कि यह एक संवैधानिक आवश्यकता भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A(g) में पर्यावरण संरक्षण को राज्य और नागरिक दोनों की जिम्मेदारी बताया गया है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत में पर्यावरणीय क्षरण तेजी से बढ़ा है, जिससे न केवल पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हुआ है, बल्कि मानव जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में भारतीय न्यायपालिका ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जो पर्यावरणीय न्याय को प्रभावी रूप देने के लिए सक्रिय हुई है।
संवैधानिक प्रावधान और उत्तरदायित्व:
अनुच्छेद 48A राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार के लिए कदम उठाए। अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य देता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करे। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 21 — जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है — को भारतीय न्यायपालिका ने विस्तृत करते हुए “स्वस्थ पर्यावरण में जीवन के अधिकार” के रूप में व्याख्यायित किया है।
प्रमुख पर्यावरणीय कानून:
भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु कई विधायी प्रयास किए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- जैव विविधता अधिनियम, 2002
इन कानूनों ने पर्यावरणीय मानकों, नियंत्रण उपायों, और दंडात्मक प्रावधानों का एक कानूनी ढांचा स्थापित किया है।
न्यायिक सक्रियता और पर्यावरणीय न्याय:
1990 के दशक से भारतीय न्यायपालिका ने “न्यायिक सक्रियता” के माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण में अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई ऐतिहासिक फैसलों में पर्यावरणीय सिद्धांतों को आत्मसात किया है, जैसे —
- सुबाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991):
सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि स्वच्छ और प्रदूषण रहित जल और वायु जीवन के अधिकार का हिस्सा है। - एमसी मेहता बनाम भारत संघ:
इस मामले की विभिन्न श्रृंखलाओं में न्यायालय ने गंगा नदी की सफाई, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, और पर्यावरणीय दायित्व की पुष्टि की। - वेंकटेश मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य (2003):
न्यायालय ने “जनहित याचिका” (PIL) को एक सशक्त उपकरण बनाकर पर्यावरणीय न्याय को जनसामान्य के लिए सुलभ बनाया।
पर्यावरणीय सिद्धांतों का विकास:
न्यायपालिका ने अनेक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में लागू किया, जैसे —
- “सतत विकास का सिद्धांत”
- “प्रदूषक भुगतान करे” (Polluter Pays Principle)
- “पूर्व सतर्कता का सिद्धांत” (Precautionary Principle)
इन सिद्धांतों को न्यायिक निर्णयों में आत्मसात करके पर्यावरणीय नीति को नई दिशा दी गई।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना:
साल 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत NGT की स्थापना की गई, जो पर्यावरणीय मामलों में विशेषज्ञता आधारित न्याय प्रदान करता है। NGT ने अनेक महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय स्वीकृति, और जंगल कटाई में त्वरित और प्रभावी निर्णय दिए हैं।
न्यायपालिका की सीमाएँ और चुनौतियाँ:
हालांकि न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया है, फिर भी कई बार इसके निर्णयों को लागू करने में प्रशासनिक ढिलाई, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव बाधक बना है। इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका के पास वैज्ञानिक संसाधनों की कमी के कारण कुछ निर्णयों में व्यवहारिक समस्याएँ सामने आती हैं।
निष्कर्ष:
भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। संविधान में निहित उत्तरदायित्वों से लेकर न्यायिक सक्रियता तक की यह यात्रा भारतीय लोकतंत्र के सतत विकास की प्रतीक है। भविष्य में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के संयुक्त प्रयास से ही पर्यावरणीय संकटों का समाधान संभव है। हमें यह समझना होगा कि “पर्यावरण की रक्षा करना, जीवन की रक्षा करना है” और यह कार्य केवल कानूनों और न्यायिक निर्णयों से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और नागरिक उत्तरदायित्व से भी संभव होगा।