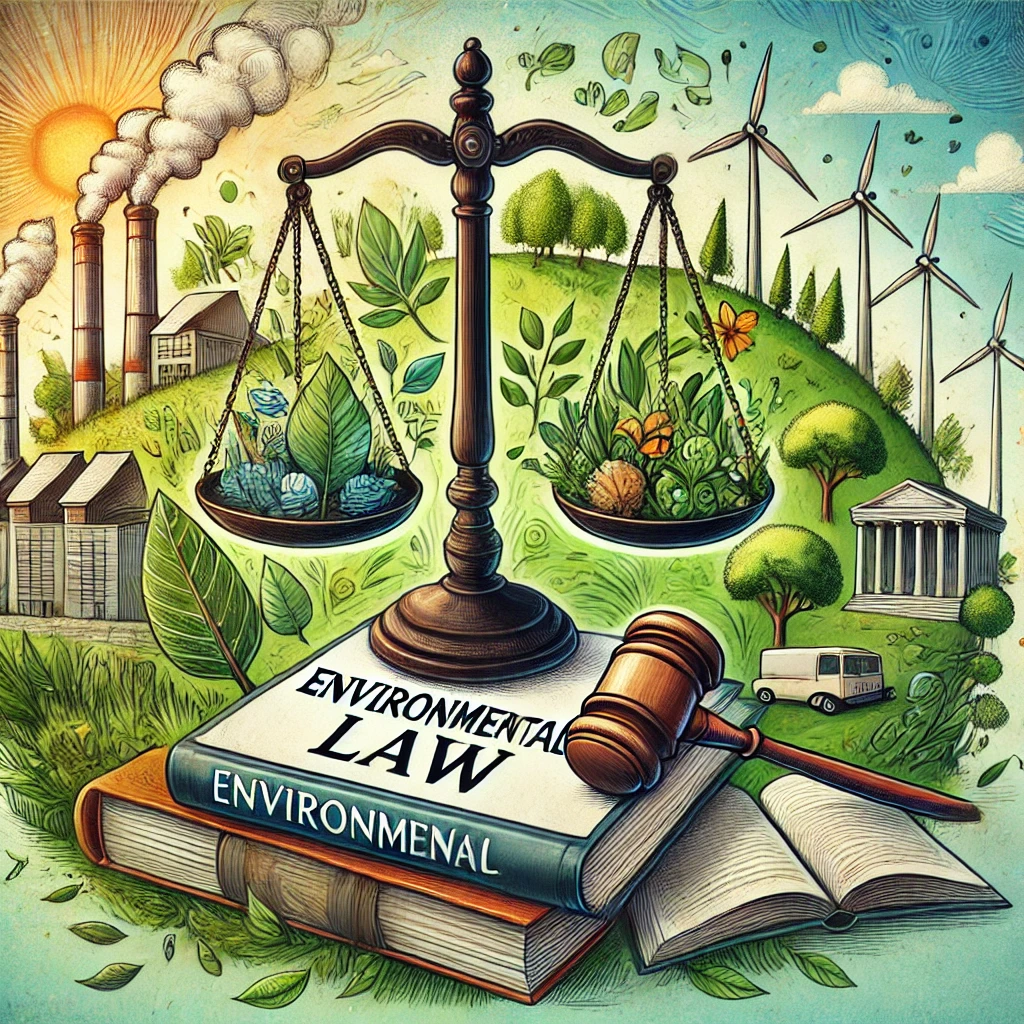पर्यावरण संरक्षण कानून और न्यायपालिका: भारतीय परिप्रेक्ष्य में न्यायिक सक्रियता की संवैधानिक यात्रा
प्रस्तावना:
भारत में औद्योगीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने जहां आर्थिक विकास को गति दी, वहीं पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुँचाई। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के ह्रास जैसे मुद्दे आज हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं। इन परिस्थितियों में पर्यावरण संरक्षण कानूनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होता — इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में भारतीय न्यायपालिका ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।
पर्यावरण संरक्षण कानून का कानूनी ढांचा:
भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न कानून बनाए गए हैं। इनमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 – यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात बना, जो पर्यावरण के समग्र संरक्षण का सबसे प्रमुख कानून है।
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- जैव विविधता अधिनियम, 2002
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 – इसने एक विशिष्ट पर्यावरणीय न्यायालय की स्थापना की।
इन कानूनों के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करना अनिवार्य किया गया है, साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी और मूल्यांकन प्रक्रियाएँ लागू की गई हैं।
संविधान में पर्यावरण संरक्षण का स्थान:
भारतीय संविधान में भी पर्यावरण संरक्षण का स्पष्ट उल्लेख है –
- अनुच्छेद 48A: राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन्य जीवों और वनों की रक्षा और सुधार करे।
- अनुच्छेद 51A(g): प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे।
इन संवैधानिक प्रावधानों को आधार बनाकर न्यायपालिका ने कई बार पर्यावरण संरक्षण हेतु अहम निर्णय दिए हैं।
न्यायपालिका की भूमिका और ऐतिहासिक निर्णय:
भारत की न्यायपालिका, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, ने पर्यावरणीय मामलों में न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) दिखाते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं।
- MC Mehta बनाम यूनियन ऑफ इंडिया – यह पर्यावरणीय न्यायशृंखला का प्रमुख मामला है। इसमें ताजमहल, गंगा नदी, दिल्ली का वायु प्रदूषण जैसे अनेक विषयों पर ऐतिहासिक निर्णय दिए गए।
- सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, जीवन के अधिकार (Article 21) का हिस्सा है।”
- वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया – इसमें “सतत विकास” और “प्रदूषक भुगतान सिद्धांत” को मान्यता दी गई।
- गोधावर्मन बनाम भारत संघ – इसमें वनों की रक्षा के लिए केंद्रीय समिति गठित की गई और वनों की कटाई पर सख्ती बरती गई।
- लाफार्ज यूटेटो सीमेंट मामला – सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और स्थानीय समुदायों की सहभागिता को आवश्यक बताया।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भूमिका:
2010 में स्थापित NGT (National Green Tribunal) पर्यावरणीय न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह तेज, सुलभ और विशेषज्ञता आधारित न्याय प्रदान करता है। NGT ने औद्योगिक प्रदूषण, अवैध निर्माण, नदी प्रदूषण आदि मामलों में कई सख्त निर्णय दिए हैं।
NGT के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय:
- यमुना नदी की सफाई पर निर्देश।
- स्टबल बर्निंग (पराली जलाना) पर सख्ती।
- निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए गाइडलाइंस।
चुनौतियाँ और समाधान:
हालाँकि न्यायपालिका की सक्रियता ने पर्यावरणीय मामलों में चेतना लाई है, फिर भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
- निर्णयों के क्रियान्वयन की कमी
- सरकारी और निजी क्षेत्र की उदासीनता
- जागरूकता की कमी
- भ्रष्टाचार और संसाधनों की कमी
समाधान के उपाय:
- न्यायपालिका के निर्देशों का सख्ती से पालन
- आमजन की भागीदारी
- पर्यावरणीय शिक्षा को प्रोत्साहन
- NGOs और स्थानीय निकायों की सशक्त भूमिका
निष्कर्ष:
भारत में पर्यावरण संरक्षण केवल एक वैधानिक आवश्यकता नहीं बल्कि संवैधानिक कर्तव्य है। न्यायपालिका ने इस दिशा में जो मार्ग प्रशस्त किया है, वह न केवल पर्यावरणीय न्याय की मिसाल है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक आश्वासन भी है। जब संसद और कार्यपालिका चुप हो जाती हैं, तब न्यायपालिका ने ‘पर्यावरण की आवाज़’ बनकर कार्य किया है।
आज आवश्यकता है कि सरकार, न्यायपालिका, उद्योग और नागरिक समाज मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें। यही एक टिकाऊ और स्वस्थ भारत की नींव बन सकती है।