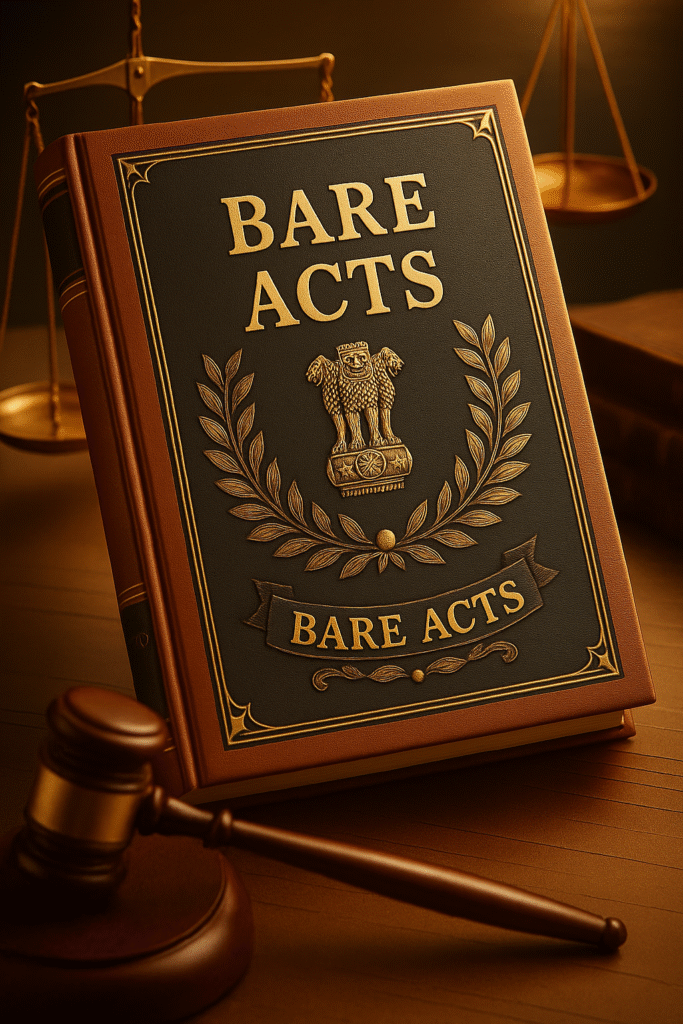पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986)
प्रस्तावना
पर्यावरण मानव जीवन और पृथ्वी के सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वच्छ वायु, जल, मिट्टी, वन और जैव विविधता जीवन को टिकाए रखने का आधार हैं। औद्योगीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने जहाँ एक ओर विकास की गति को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। भारत में भी 1970 के दशक से पर्यावरण संकट गंभीर रूप से सामने आने लगा। इस संदर्भ में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) ने पूरे देश को झकझोर दिया और केंद्र सरकार को एक मजबूत एवं व्यापक पर्यावरणीय कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 अस्तित्व में आया।
अधिनियम की पृष्ठभूमि
- वैश्विक संदर्भ – 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम (Stockholm Conference on Human Environment) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा को लेकर विश्वस्तरीय सहमति बनी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया।
- राष्ट्रीय संदर्भ – भारत में 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस रिसाव की घटना ने हजारों लोगों की जान ली। यह त्रासदी भारत में पर्यावरण और औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित कानूनी खामियों को उजागर करती है।
- संवैधानिक आधार – 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा करने का दायित्व देता है, जबकि अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक पर पर्यावरण की रक्षा का मौलिक कर्तव्य लागू करता है।
अधिनियम का उद्देश्य
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का मुख्य उद्देश्य है:
- पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण को रोकना।
- प्राकृतिक संसाधनों का सतत (Sustainable) उपयोग सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए सरकार को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करना।
- औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रखना।
- जनस्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता की रक्षा करना।
अधिनियम की परिभाषाएँ
अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं, जैसे:
- पर्यावरण (Environment): इसमें जल, वायु, भूमि तथा इनके अंतर्गत आने वाले जीवित और निर्जीव तत्व शामिल हैं।
- पर्यावरण प्रदूषण (Environmental Pollution): किसी भी प्रदूषक तत्व की उपस्थिति जिसके कारण पर्यावरण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- प्रदूषक (Pollutant): कोई भी ठोस, तरल या गैस रूपी पदार्थ जो पर्यावरण में अवांछित रूप से मिलकर उसकी गुणवत्ता को हानि पहुँचाए।
अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ
- केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ – केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए नियम बनाने, मानक तय करने और निगरानी करने का अधिकार है।
- मानकों का निर्धारण – वायु, जल और मिट्टी में प्रदूषण की सीमा तय करने के लिए मानक निर्धारित किए गए।
- औद्योगिक गतिविधियों का नियमन – औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण और उत्सर्जन के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
- परीक्षण और निरीक्षण की शक्ति – सरकार निरीक्षण कर सकती है, नमूने ले सकती है और पर्यावरणीय स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर सकती है।
- दंडात्मक प्रावधान – अधिनियम का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
- पर्यावरणीय आपात स्थिति – सरकार आवश्यकतानुसार किसी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकती है।
अधिनियम के तहत सरकार की शक्तियाँ
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं:
- नियम और मानक बनाना।
- उद्योगों की स्थापना और संचालन पर नियंत्रण।
- किसी गतिविधि को प्रतिबंधित करना।
- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद कराना।
- वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को लागू करना।
दंडात्मक प्रावधान
- अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर पाँच वर्ष तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- यदि अपराध जारी रहता है, तो प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त दंड लगाया जा सकता है।
- यदि पाँच वर्ष से अधिक समय तक अपराध जारी रहता है, तो सात वर्ष तक का कारावास संभव है।
अधिनियम का महत्व
- समग्र पर्यावरण कानून – यह अधिनियम वायु अधिनियम, जल अधिनियम आदि के बीच समन्वय स्थापित करता है।
- औद्योगिक प्रदूषण पर रोक – उद्योगों पर निगरानी और मानक निर्धारित करने से प्रदूषण नियंत्रण संभव हुआ।
- न्यायिक व्याख्या – भारतीय न्यायालयों ने इस अधिनियम को “जीवित रहने के अधिकार” (अनुच्छेद 21) से जोड़कर देखा है।
- सतत विकास की दिशा में कदम – विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन की दिशा में यह अधिनियम एक बड़ा प्रयास है।
अधिनियम की आलोचना
- अत्यधिक केंद्रीयकरण – सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं, राज्यों को सीमित भूमिका दी गई है।
- कठोर प्रवर्तन की कमी – दंड प्रावधान होने के बावजूद उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होता।
- जनसहभागिता का अभाव – कानून में नागरिकों या गैर-सरकारी संगठनों को पर्याप्त भूमिका नहीं दी गई।
- भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय – अधिनियम बनने के बावजूद भोपाल गैस कांड जैसे मामलों में पीड़ितों को उचित मुआवजा और न्याय नहीं मिल पाया।
न्यायालयों की भूमिका
भारतीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की व्याख्या करते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं।
- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987) – ताजमहल क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश।
- भोपाल गैस पीड़ित संघ मामले – पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु व्याख्या।
- वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996) – “सतत विकास” और “प्रदूषक भुगतान सिद्धांत” (Polluter Pays Principle) को मान्यता दी।
निष्कर्ष
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत में पर्यावरणीय कानूनों का आधार स्तंभ है। इसने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय मानकों को लागू करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन और जनसहभागिता की अभी भी आवश्यकता है। बढ़ते औद्योगीकरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए इस अधिनियम को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। पर्यावरण की रक्षा केवल कानून से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के नैतिक दायित्व से भी जुड़ी है। यदि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर कार्य करें तो ही सतत विकास और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित हो सकता है।