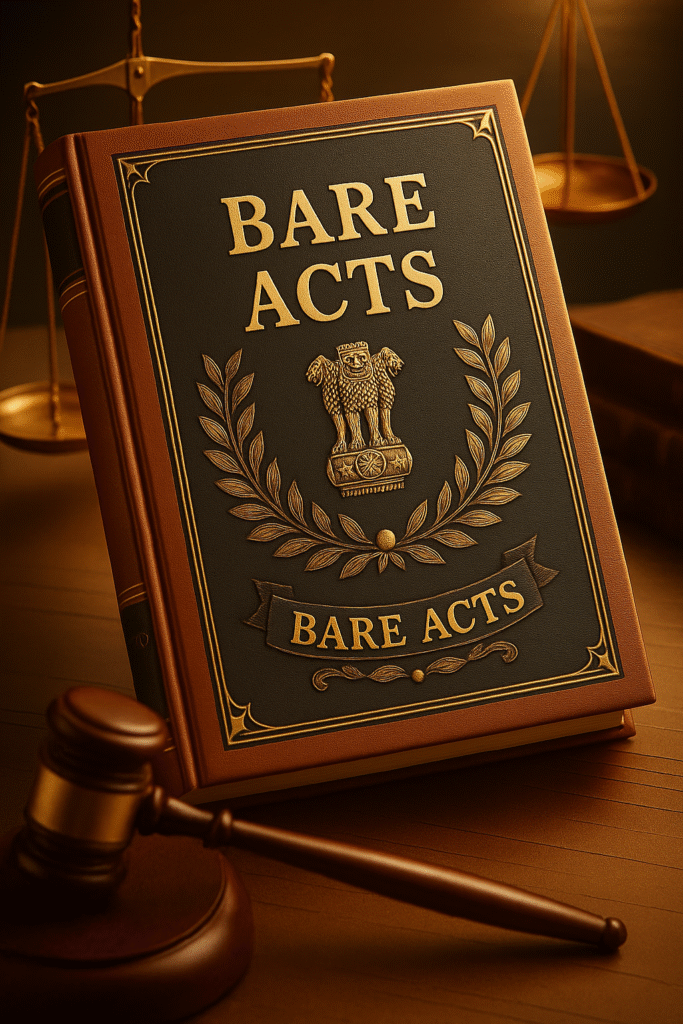न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948) :
प्रस्तावना
भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य था कि श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। उस समय बड़ी संख्या में श्रमिक कम वेतन, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और शोषण का सामना कर रहे थे। इस स्थिति को सुधारने और श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन-स्तर सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 बनाया गया। यह अधिनियम 15 मार्च 1948 को पारित हुआ और उसी वर्ष से लागू कर दिया गया।
उद्देश्य
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके काम के बदले “न्यूनतम वेतन” सुनिश्चित करना है, ताकि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ति कर सकें। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं –
- श्रमिकों को शोषण से बचाना।
- सभी क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन का मानक स्थापित करना।
- कार्य की प्रकृति और क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करना।
- समय-समय पर महंगाई के अनुसार वेतन दरों में संशोधन करना।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- न्यूनतम मजदूरी का विचार सबसे पहले 1929 के व्हाइटली आयोग की सिफारिशों में सामने आया।
- 1936 में लोहे और कोयला उद्योगों में न्यूनतम वेतन तय करने की कोशिश हुई।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ने के कारण श्रमिक आंदोलन तेज हुआ।
- 1948 में स्वतंत्र भारत ने इस अधिनियम को पारित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया।
अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ
1. लागू क्षेत्र (Coverage)
- यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित (Notified) उद्योगों, नियोजनों और व्यवसायों पर लागू होता है।
- यह सभी प्रकार के श्रमिकों—स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक, और संविदा कर्मियों पर लागू हो सकता है, यदि वे अधिसूचित क्षेत्र में कार्यरत हैं।
2. न्यूनतम मजदूरी के घटक
न्यूनतम वेतन में निम्न शामिल हो सकते हैं –
- मूल वेतन (Basic Wages)।
- जीविका भत्ता (Dearness Allowance – DA)।
- अन्य सुविधाएँ जो नकद या वस्तु के रूप में दी जा सकती हैं।
3. मजदूरी तय करने के आधार
- जीवन-यापन की लागत।
- कार्य की प्रकृति (कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल)।
- क्षेत्रीय परिस्थितियाँ।
- महंगाई का स्तर।
4. वेतन की प्रकार
- टुकड़ा दर (Piece Rate) – उत्पादन के आधार पर।
- समय दर (Time Rate) – घंटे, दिन, सप्ताह या महीने के आधार पर।
- गारंटीकृत टुकड़ा दर – न्यूनतम समय दर के साथ उत्पादन पर प्रोत्साहन।
न्यूनतम मजदूरी तय करने की प्रक्रिया
अधिनियम के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने-अपने अधिसूचित क्षेत्रों में मजदूरी दर तय करने के लिए दो विधियाँ अपना सकती हैं –
- समिति पद्धति (Committee Method) – विशेषज्ञों, नियोक्ताओं और श्रमिक प्रतिनिधियों की समिति गठित की जाती है, जो सुझाव देती है।
- अधिसूचना पद्धति (Notification Method) – प्रस्तावित दर को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, और आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं, फिर अंतिम दर तय होती है।
संशोधन और पुनरीक्षण
- अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण कम से कम हर 5 वर्ष में किया जाना चाहिए।
- कई राज्यों में इसे महंगाई भत्ता (DA) से जोड़ दिया गया है, ताकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर स्वतः समायोजन हो सके।
अधिनियम की धाराएँ और मुख्य प्रावधान
- धारा 3 – न्यूनतम मजदूरी दर तय करने की शक्ति।
- धारा 4 – न्यूनतम मजदूरी की संरचना (मूल वेतन + भत्ता)।
- धारा 5 – मजदूरी दर तय करने की प्रक्रिया।
- धारा 12 – न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य।
- धारा 18 – नियोक्ता का रिकॉर्ड रखने का दायित्व।
- धारा 20 – न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान होने पर दावा करने का प्रावधान।
- धारा 22 – उल्लंघन पर दंड।
भुगतान का तरीका और समय
- मजदूरी नकद, चेक या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दी जा सकती है।
- समय पर भुगतान सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के अनुसार वेतन भुगतान की तारीख और अवधि लागू होती है।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और जीवन-निर्वाह मजदूरी
- न्यूनतम मजदूरी – कानून द्वारा तय किया गया वह न्यूनतम वेतन जो नियोक्ता को देना ही होगा।
- जीवन-निर्वाह मजदूरी – ऐसा वेतन जो श्रमिक और उसके परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
- उचित मजदूरी – न्यूनतम और जीवन-निर्वाह मजदूरी के बीच का स्तर, जिसमें कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ भी हों।
न्यायिक व्याख्या और महत्वपूर्ण मामले
- Unichoyi v. State of Kerala (1961) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी भुगतान न करना, श्रमिक को शोषित करने के समान है।
- Hydro (Engineers) Pvt. Ltd. v. Workmen (1969) – न्यूनतम मजदूरी में महंगाई भत्ते को शामिल करने की पुष्टि।
दंड और प्रवर्तन
- न्यूनतम मजदूरी न देना – अधिकतम 6 महीने का कारावास या जुर्माना, या दोनों।
- रिकॉर्ड न रखना – जुर्माना।
- प्रवर्तन अधिकारी (Inspectors) – अधिनियम के पालन की जांच करते हैं और उल्लंघन पर रिपोर्ट दर्ज करते हैं।
अधिनियम के लाभ
- श्रमिकों को न्यूनतम आय की गारंटी।
- असंगठित क्षेत्र में भी कानूनी सुरक्षा।
- महंगाई के अनुसार वेतन संशोधन।
- श्रमिक-नियोक्ता संबंधों में संतुलन।
सीमाएँ और चुनौतियाँ
- कई श्रमिकों को अधिनियम की जानकारी नहीं होती।
- प्रवर्तन तंत्र कमजोर है।
- असंगठित क्षेत्र में निगरानी कठिन।
- अलग-अलग राज्यों में अलग दरें होने से भ्रम।
हालिया सुधार
- वेतन संहिता, 2019 के तहत इस अधिनियम को अन्य वेतन संबंधी कानूनों के साथ मिलाकर एकीकृत किया गया है।
- अब केंद्र सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने की शक्ति रखती है, जिससे राज्यों के बीच बड़े वेतन अंतर को कम किया जा सके।
निष्कर्ष
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ने भारत में श्रमिक अधिकारों की रक्षा और आर्थिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। इसने न केवल शोषण को रोका बल्कि श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार के लिए कानूनी आधार भी प्रदान किया। हालांकि, प्रभावी क्रियान्वयन और समय पर संशोधन ही इसकी सफलता की कुंजी हैं। आने वाले समय में डिजिटल पेरोल सिस्टम, बेहतर निरीक्षण व्यवस्था और श्रमिक जागरूकता अभियानों के जरिए इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।