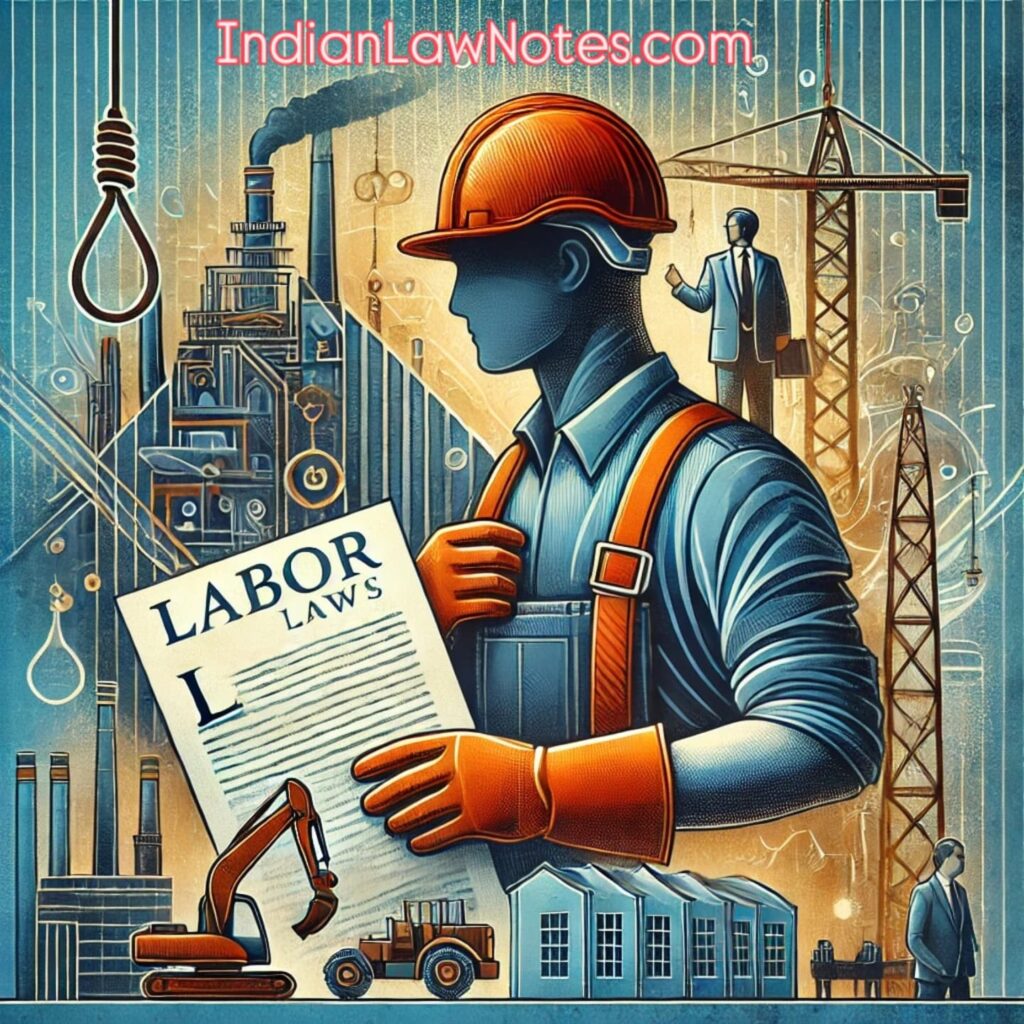शीर्षक: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 : श्रमिकों के जीवन स्तर की गरिमा और न्याय सुनिश्चित करने की संवैधानिक व्यवस्था
परिचय
भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जिनकी आय सीमित, अनिश्चित और कई बार शोषणपूर्ण स्थितियों में होती है। श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, इसके लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू किया। यह अधिनियम श्रमिकों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है जिससे उनके कार्य की न्यूनतम कीमत तय होती है और उन्हें शोषण से सुरक्षा मिलती है।
अधिनियम का उद्देश्य
इस अधिनियम का मूल उद्देश्य निम्नलिखित है:
- श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर सुनिश्चित करना।
- श्रमिकों को शोषण से बचाना।
- समान पारिश्रमिक की भावना को प्रोत्साहित करना।
- श्रमिकों को जीवन यापन योग्य वेतन प्रदान करना।
- देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना।
अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ
- सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी: अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करती हैं।
- अनिवार्य प्रवर्तन: अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम वेतन देना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है।
- समय-समय पर संशोधन: महँगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है।
- कार्य की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण: मजदूरी दर को कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल, प्रशिक्षु जैसे श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
महत्वपूर्ण परिभाषाएँ
- न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages): वह न्यूनतम पारिश्रमिक जो किसी श्रमिक को उसके कार्य के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे वह अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
- अनुसूचित रोजगार (Scheduled Employment): वे रोजगार जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं और जिनके लिए न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की गई है।
न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के आधार
- भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता
- न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं का आकलन
- पारिवारिक आवश्यकताओं का ध्यान
- मुद्रास्फीति (महँगाई दर)
- स्थानीय स्तर पर जीवन-यापन की लागत
अधिनियम के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्य
नियोक्ताओं के कर्तव्य:
- तय न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य।
- समय पर भुगतान करना।
- वेतन रजिस्टर और रिकॉर्ड रखना।
- निरीक्षण में सहयोग करना।
श्रमिकों के अधिकार:
- निर्धारित न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार।
- गलत वेतन या कम वेतन मिलने पर शिकायत करने का अधिकार।
- किसी भी प्रकार की कटौती के विरुद्ध संरक्षण।
प्रवर्तन तंत्र
अधिनियम के तहत मजदूरी निरीक्षक (Labour Inspector) नियुक्त किए जाते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नियोक्ता न्यूनतम मजदूरी का पालन कर रहे हैं। उल्लंघन की स्थिति में मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है।
दंडात्मक प्रावधान
यदि कोई नियोक्ता अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसे—
- ₹5000 तक का जुर्माना, या
- 6 महीने तक की सजा, या
- दोनों हो सकते हैं।
यह प्रावधान श्रमिकों को न केवल हक दिलाते हैं बल्कि नियोक्ताओं को जिम्मेदार भी बनाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय
Reptakos Brett & Co. बनाम वर्कमेन (1992) के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम मजदूरी केवल जीवित रहने की मजदूरी नहीं है, बल्कि उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य मानवीय आवश्यकताओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
कोड ऑन वेजेज, 2019 के अंतर्गत समावेशन
2019 में पारित Code on Wages के अंतर्गत इस अधिनियम को समाहित कर लिया गया है। इस कोड के अनुसार—
- सभी प्रकार के रोजगारों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जा सकता है।
- कार्यस्थलों पर लिंग, प्रकार, क्षेत्र के भेद के बिना समान वेतन की गारंटी दी गई है।
समाज में अधिनियम का महत्व
- गरीबी उन्मूलन में सहायक
- सामाजिक समानता को प्रोत्साहन
- मानव गरिमा की रक्षा
- श्रमिकों का आत्मसम्मान और मनोबल बढ़ाना
- औद्योगिक विवादों में कमी
चुनौतियाँ और सुझाव
चुनौतियाँ:
- अधिनियम के बारे में श्रमिकों में जानकारी की कमी।
- निरीक्षण तंत्र की कमजोरियाँ।
- असंगठित क्षेत्र में प्रवर्तन की कमी।
- कुछ राज्यों में न्यूनतम मजदूरी बहुत कम निर्धारित।
सुझाव:
- जागरूकता अभियान चलाना।
- पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली बनाना।
- न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर करना।
- डिजिटल भुगतान की प्रणाली लागू करना।
निष्कर्ष
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 भारतीय श्रमिकों के लिए न केवल एक कानूनी सुरक्षा कवच है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक दृढ़ कदम भी है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उनके श्रम का सम्मानजनक मूल्य मिले और वे मानव गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकें। श्रम कानूनों के एकीकृत स्वरूप में इसे Code on Wages, 2019 के अंतर्गत लाकर और सशक्त बनाया गया है, जो आने वाले समय में श्रमिक हितों की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।