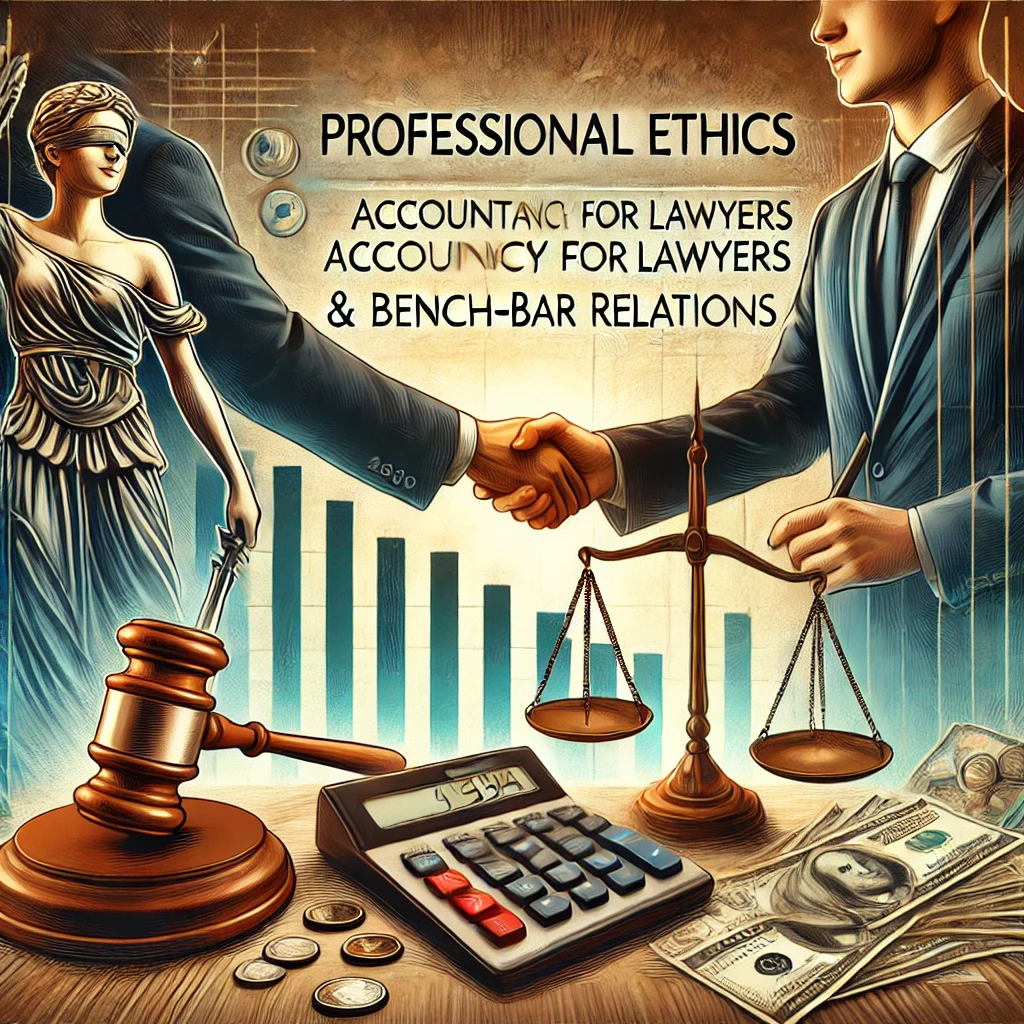प्रश्न: न्यायिक जवाबदेही की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। भारत में न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु अपनाए गए विधिक और संवैधानिक उपायों का विश्लेषण कीजिए।
परिचय:
न्यायपालिका लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है, जिसका मूल उद्देश्य कानून के शासन को लागू करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसलिए, न्यायाधीशों की निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्कलंक छवि बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी संदर्भ में “न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability)” एक ऐसी अवधारणा है जो न्यायपालिका को पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करती है।
न्यायिक जवाबदेही की परिभाषा:
न्यायिक जवाबदेही का तात्पर्य है – न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नैतिकता और विधिक मर्यादा का पालन करना। जब न्यायाधीश किसी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या नैतिक अवनति में लिप्त पाए जाते हैं, तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता:
- लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए
- न्याय में जनविश्वास बनाए रखने हेतु
- न्यायपालिका में पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखने के लिए
- न्यायिक पदों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए
- संविधान की सर्वोच्चता और कानून के शासन को कायम रखने हेतु
भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा विधिक व संवैधानिक उपाय:
1. भारतीय संविधान के प्रावधान:
- अनुच्छेद 124(4): उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल महाभियोग (Impeachment) के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 217(1): उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 235: उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान करता है।
2. महाभियोग की प्रक्रिया:
- न्यायाधीश को केवल “दुराचार या अक्षमता” के आधार पर हटाया जा सकता है।
- इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
- अब तक केवल एक न्यायाधीश – जस्टिस वी. रामास्वामी – के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पारित नहीं हो सका।
3. न्यायिक आचरण की संहिता (Restatement of Values of Judicial Life):
- वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाई गई संहिता।
- इसमें न्यायिक पद की गरिमा बनाए रखने हेतु नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवन में अनुशासन और निष्पक्षता जैसे सिद्धांत शामिल हैं।
4. न्यायिक जवाबदेही और मानक विधेयक (Judicial Standards and Accountability Bill), 2010:
- यह विधेयक न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु लाया गया था।
- इसके प्रमुख प्रावधान थे:
- न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता
- शिकायत निवारण प्रणाली
- शिकायतों की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना
- हालांकि यह विधेयक अभी तक कानून नहीं बन पाया है।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act):
- RTI अधिनियम के अंतर्गत न्यायपालिका को भी उत्तरदायी बनाया गया है।
- हाल के वर्षों में कई न्यायालयों ने अपने प्रशासनिक कार्यों की जानकारी सार्वजनिक करने की दिशा में कदम उठाए हैं।
न्यायिक जवाबदेही की चुनौतियाँ:
- महाभियोग प्रक्रिया की जटिलता – अत्यंत कठिन और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रक्रिया।
- स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही – न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करना एक संतुलन की मांग करता है।
- स्व-नियमन की सीमाएँ – न्यायपालिका द्वारा स्वविवेक से आचार संहिता लागू करना पर्याप्त नहीं है।
- पारदर्शिता की कमी – न्यायिक नियुक्तियों, पदोन्नति, और शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता की कमी।
सुधार के सुझाव:
- न्यायिक जवाबदेही विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू करना।
- न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना।
- न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और सार्वजनिक पहुंच।
- न्यायिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली।
- न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्यों में RTI का समुचित उपयोग।
निष्कर्ष:
न्यायिक जवाबदेही एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की न्याय प्रणाली का आधारभूत तत्व है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन अत्यंत आवश्यक है। जब न्यायपालिका नैतिक, विधिक और संवैधानिक सीमाओं में रहकर कार्य करती है, तभी आमजन का उसमें विश्वास बना रहता है। न्यायाधीशों की उच्च नैतिकता, पारदर्शिता, और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता ही न्यायिक जवाबदेही का वास्तविक अर्थ है।