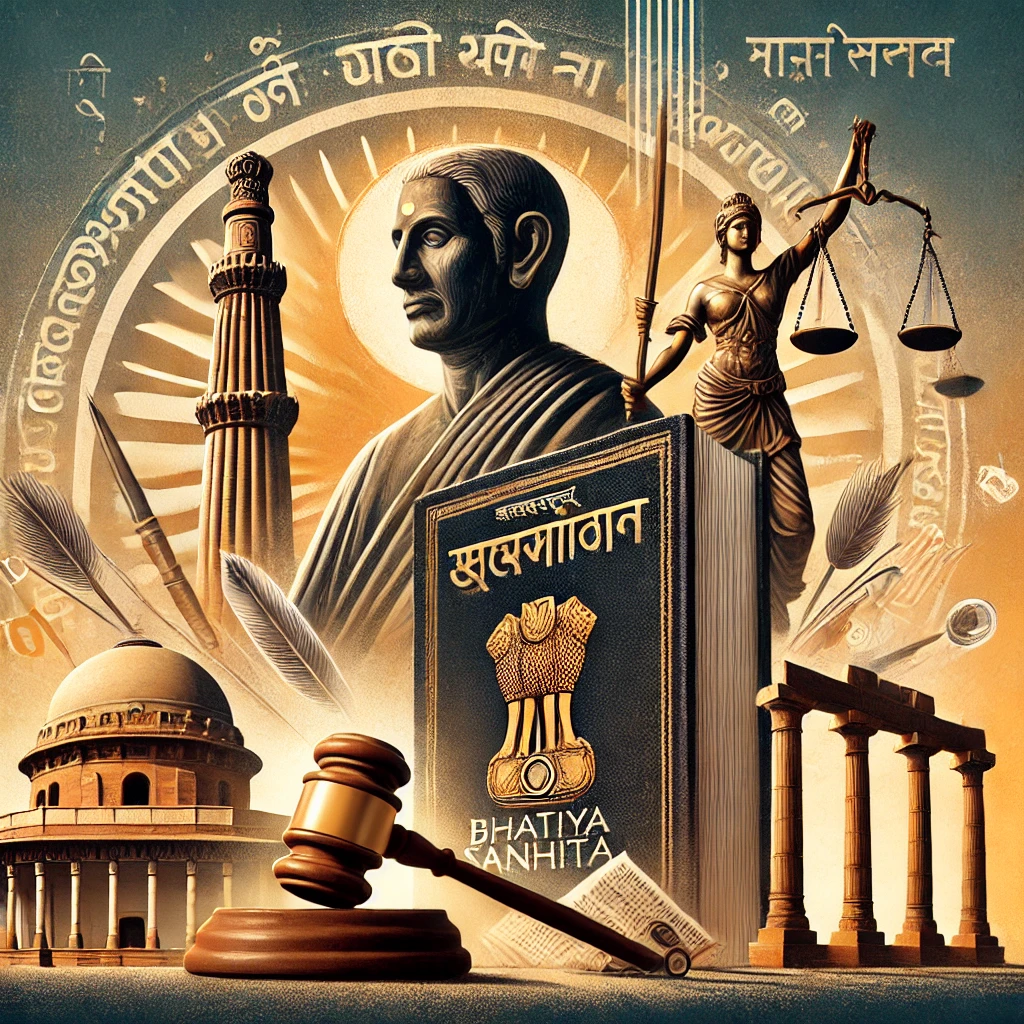नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन कानून: सिद्धांत, ढांचा और प्रभाव (Civil Protection & Disaster Management Law: Principles, Framework and Impact)
परिचय
भारत जैसे विशाल और विविध जलवायु वाले देश में भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा, महामारी, औद्योगिक दुर्घटनाएं और मानव निर्मित आपदाएँ बार-बार आती रहती हैं। इन आपदाओं से जान-माल की क्षति को न्यूनतम करने और प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता प्रदान करने के लिए एक मजबूत नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन कानून की आवश्यकता होती है। भारत में इस दिशा में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एक प्रमुख कानून है, जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है। इसके साथ-साथ नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 भी नागरिकों की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आपदा का अर्थ और प्रकार
आपदा (Disaster) का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो और जिससे निपटने की स्थानीय प्रशासन की क्षमता सीमित हो। इसे मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
1. प्राकृतिक आपदाएं (Natural Disasters):
- भूकंप
- बाढ़
- चक्रवात
- सूखा
- हिमस्खलन
- सुनामी
2. मानवजनित आपदाएं (Man-Made Disasters):
- औद्योगिक दुर्घटनाएं (जैसे भोपाल गैस त्रासदी)
- जैविक/रासायनिक हमला
- रेलवे या विमान दुर्घटना
- आगजनी
- आतंकवादी हमला
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005)
यह अधिनियम भारत में आपदा से निपटने के लिए एक समग्र और संगठित तंत्र प्रदान करता है। इसके मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं:
1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित यह शीर्ष संस्था आपदा नीतियों का निर्धारण करती है, दिशानिर्देश जारी करती है और कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
2. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA):
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यरत यह संस्था राज्य स्तर पर आपदा से निपटने की रणनीति तय करती है।
3. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA):
जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के नेतृत्व में गठित यह संस्था आपदा की स्थानीय योजना और क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है।
4. राष्ट्रीय कार्य बल (NDRF):
आपदा के समय तुरंत राहत पहुंचाने हेतु प्रशिक्षित बल, जिसे NDMA संचालित करता है।
नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (Civil Defence Act, 1968)
इस कानून का उद्देश्य आपदा, युद्ध या किसी आपातकालीन स्थिति में नागरिकों की रक्षा करना है। इसकी प्रमुख बातें:
- यह युद्ध, आक्रमण, आतंकी गतिविधियों और अन्य आपात स्थितियों में नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का प्रावधान करता है।
- आपदा के समय आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति की सुरक्षा हेतु कार्य करता है।
आपदा प्रबंधन में अन्य कानूनों की भूमिका
1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
औद्योगिक या रासायनिक आपदाओं में नियंत्रण और दायित्व तय करता है।
2. कारखाना अधिनियम, 1948
औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करता है।
3. महामारी रोग अधिनियम, 1897
COVID-19 जैसी महामारियों से निपटने में उपयोग किया गया।
4. भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC)
आपदा के समय कानून-व्यवस्था बनाए रखने, झूठी अफवाह फैलाने, लूटपाट रोकने आदि हेतु लागू होते हैं।
आपदा प्रबंधन के चरण (Phases of Disaster Management)
- रोकथाम (Prevention): आपदा आने से पहले सुरक्षा उपाय करना, जैसे बाढ़ नियंत्रण बांध बनाना, निर्माण में भूकंपरोधी तकनीक अपनाना।
- तैयारी (Preparedness): आपदा की आशंका में संसाधनों का जुटाव, आपदा पूर्वाभ्यास, आमजन को जागरूक बनाना।
- प्रतिक्रिया (Response): आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य, चिकित्सा सेवा, शरण और खाद्य आपूर्ति।
- पुनर्वास और पुनर्निर्माण (Recovery & Rehabilitation): प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण, आर्थिक सहायता, रोजगार, और मानसिक परामर्श।
COVID-19 और आपदा कानून की भूमिका
कोरोना महामारी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम की प्रासंगिकता को पुनः उजागर किया। NDMA ने लॉकडाउन और स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यों और जिलों ने स्थानीय लॉकडाउन, अस्पताल व्यवस्था और टीकाकरण रणनीति को लागू किया।
भारत में आपदा प्रबंधन की चुनौतियाँ
- संसाधनों की कमी और बुनियादी ढांचे की अक्षमता
- शहरीकरण और अनियोजित निर्माण कार्य
- जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी
- जलवायु परिवर्तन और उसका अप्रत्याशित प्रभाव
- आपातकालीन सेवाओं में समन्वय की कमी
प्रस्तावित समाधान और सुधार
- प्रशिक्षण और जन-जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार।
- स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियाँ और संसाधन देना।
- तकनीकी उन्नयन जैसे GIS, Remote Sensing और Early Warning Systems का उपयोग।
- स्कूलों, कॉलेजों में आपदा प्रबंधन शिक्षा को अनिवार्य बनाना।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का समन्वय बढ़ाना।
निष्कर्ष
भारत में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन कानून समय की मांग और आवश्यकता को देखते हुए अस्तित्व में आया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के माध्यम से एक संगठित और जिम्मेदार तंत्र की स्थापना की गई है। किन्तु चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए नीति निर्माताओं, प्रशासन, समुदाय और प्रत्येक नागरिक को मिलकर प्रयास करना होगा। जब तक आपदा से पहले तैयारी नहीं की जाएगी, तब तक उसकी भयावहता को कम करना संभव नहीं होगा।