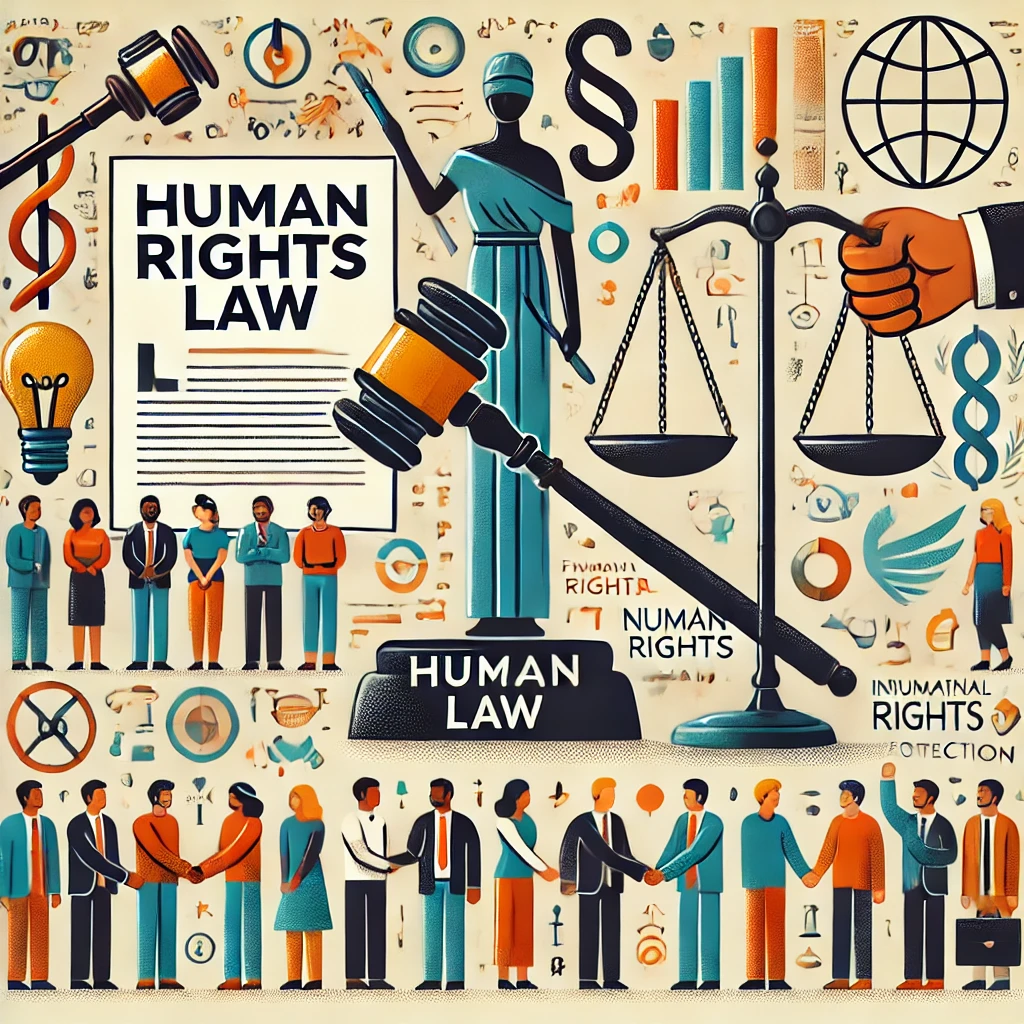लेख शीर्षक:
“नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकार हनन: विकास, संघर्ष और राज्य की जिम्मेदारी का द्वंद्व”
🔸 भूमिका:
भारत के कुछ आदिवासी और पिछड़े इलाके वर्षों से नक्सलवाद की चपेट में हैं। नक्सली आंदोलन मूलतः भूमि, संसाधनों और अधिकारों के लिए उत्पन्न हुआ था, लेकिन समय के साथ यह सशस्त्र संघर्ष में परिवर्तित हो गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आम नागरिक, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय, दोहरी मार झेलते हैं — एक ओर माओवादी हिंसा और दूसरी ओर राज्य की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मानवाधिकारों का हनन। यह स्थिति भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और मानवाधिकारों की रक्षा के दावे को चुनौती देती है।
🔸 नक्सलवाद की पृष्ठभूमि:
नक्सल आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई। इसका उद्देश्य सामाजिक अन्याय, भूमि पर अधिकार और शोषण के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना था। धीरे-धीरे यह आंदोलन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फैल गया।
🔸 मानवाधिकार हनन के दो रूप:
1. माओवादी समूहों द्वारा:
- आम नागरिकों की हत्या या अपहरण
- स्कूलों और अस्पतालों को नष्ट करना
- जबरन बच्चों की भर्ती (बाल सैनिक)
- विकास कार्यों का विरोध और धमकी
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालना (जैसे चुनाव बहिष्कार)
2. राज्य द्वारा (सुरक्षा बलों के माध्यम से):
- फर्जी मुठभेड़ (fake encounters)
- बलात्कार और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार
- आदिवासियों को माओवादी बताकर गिरफ्तार करना
- गांवों का जबरन विस्थापन
- नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश
- जनसुनवाई और मीडिया की पहुंच में बाधा
🔸 प्रमुख घटनाएं और रिपोर्टें:
- सालवा जुडूम आंदोलन (छत्तीसगढ़): 2005 में सरकार समर्थित यह मिलिशिया आंदोलन आदिवासियों को नक्सलियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन इसके तहत व्यापक स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन हुए।
- सोनी सोरी केस: छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला शिक्षक को माओवादी संपर्क के शक में यातनाएं दी गईं, जिससे मानवाधिकार संगठनों में भारी आक्रोश फैला।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने भी कई बार रिपोर्ट के माध्यम से सुरक्षा बलों द्वारा की गई ज्यादतियों को उजागर किया है।
🔸 कानूनी और संवैधानिक प्रावधान:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता
- अनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- अफस्पा (AFSPA) जैसे कानूनों का दुरुपयोग भी आलोचना का विषय बना है
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा सालवा जुडूम को असंवैधानिक ठहराना (2011)
🔸 कारण और चुनौतियाँ:
- दशकों से उपेक्षित आदिवासी इलाके
- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की भारी कमी
- खनिज संसाधनों का दोहन, लेकिन स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं
- नक्सलियों द्वारा भय का माहौल
- सरकार का अति-आक्रामक सुरक्षा दृष्टिकोण, बिना संवाद या पुनर्वास नीति के
🔸 आंकड़े और वर्तमान स्थिति:
- गृह मंत्रालय के अनुसार, 70 से अधिक जिलों को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया है।
- हजारों लोग मुठभेड़ों और विस्फोटों में जान गंवा चुके हैं।
- ग्रामीण इलाकों में आज भी भय और असुरक्षा का माहौल है।
- बड़ी संख्या में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित (Internally Displaced Persons – IDPs) बन चुके हैं।
🔸 समाधान और सुझाव:
- सुरक्षा के साथ-साथ संवाद और पुनर्वास नीति अपनाना
- विकास योजनाओं का निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन
- स्वतंत्र जांच एजेंसियों द्वारा मानवाधिकार हनन की निगरानी
- स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना
- शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार पर प्राथमिकता
- सुरक्षा बलों को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षण देना
🔸 निष्कर्ष:
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकार हनन एक गंभीर लोकतांत्रिक और नैतिक संकट है। केवल बंदूक से नक्सलवाद का समाधान संभव नहीं है; इसके लिए राज्य को संवाद, विकास और न्याय के रास्ते अपनाने होंगे। जब तक आम लोगों का विश्वास शासन प्रणाली में बहाल नहीं होता, तब तक न तो शांति आएगी और न ही स्थायी समाधान संभव होगा। सशक्त लोकतंत्र की नींव तभी मजबूत होगी जब हर नागरिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या जाति से हो, अपने अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान महसूस करेगा।