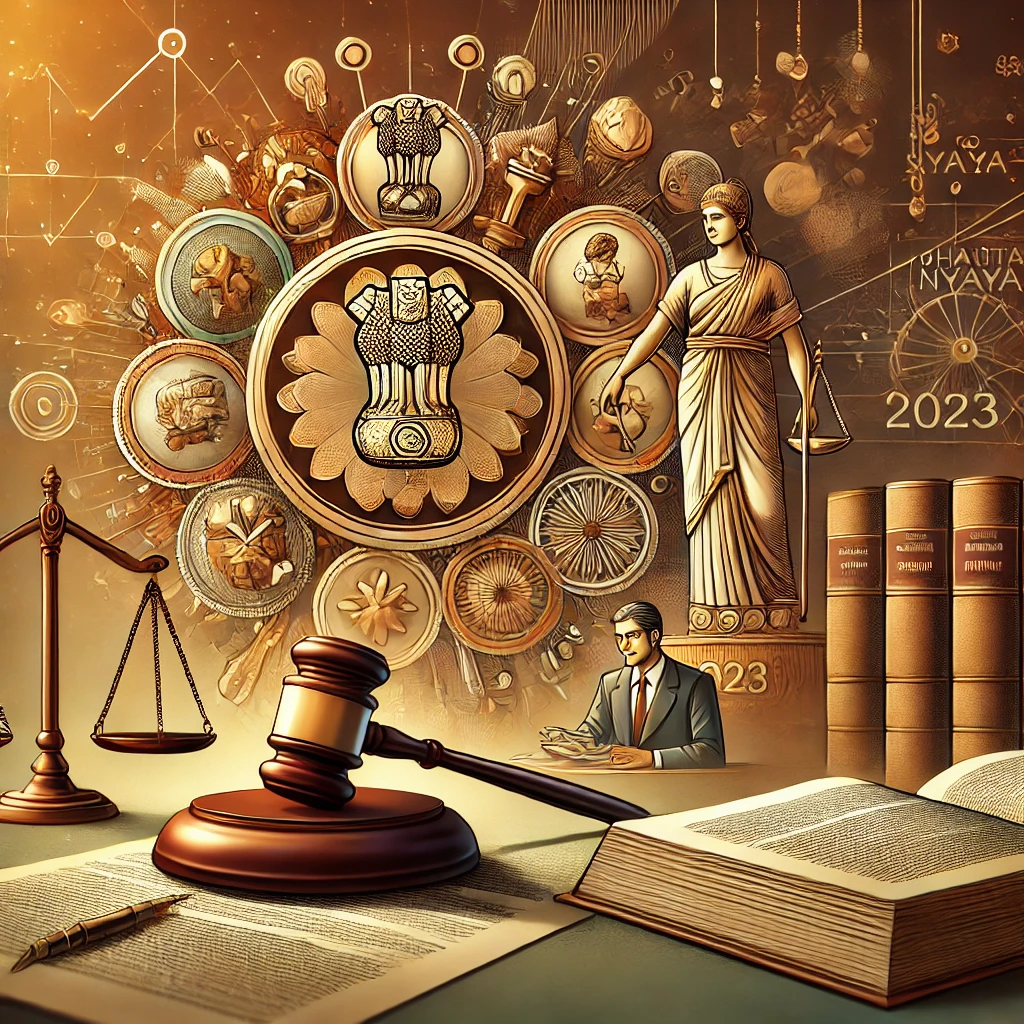धारा 279 – अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति या मृत्यु : विस्तृत विवेचना
भूमिका
भारतीय न्याय व्यवस्था में अभियोगकर्ता (Complainant) का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी दंड प्रक्रिया में अभियोगकर्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी अपराध के घटित होने की जानकारी देता है और न्यायालय में जाकर अपने बयान के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रस्तुत करता है। परंतु कई बार अभियोगकर्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाता – या तो बीमारी, मृत्यु, डर, असमर्थता अथवा अन्य कारणों से। ऐसे समय में न्यायालय को यह तय करना होता है कि क्या मुकदमा आगे बढ़े या अभियुक्त को मुक्त कर दिया जाए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) में धारा 279 का प्रावधान किया गया है, जो अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति या मृत्यु की स्थिति में न्यायालय की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।
इस लेख में हम धारा 279 का उद्देश्य, इसकी प्रक्रिया, न्यायालय की भूमिका, अभियुक्त के अधिकार, अभियोगकर्ता के दायित्व, तथा व्यावहारिक मामलों में इसके प्रयोग को विस्तार से समझेंगे।
धारा 279 का सार
धारा 279 उन परिस्थितियों से संबंधित है जब अभियोगकर्ता अदालत में तय तिथि पर उपस्थित नहीं होता, और न ही उसका कोई अधिवक्ता या अभियोजन अधिकारी उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हो। यदि अदालत यह मानती है कि अभियोगकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो वह उचित प्रक्रिया अपनाकर मामला आगे बढ़ा सकती है या अभियुक्त को बरी कर सकती है।
धारा 279 मुख्यतः निम्न बिंदुओं पर आधारित है:
- अभियोगकर्ता तय तिथि पर उपस्थित नहीं है।
- अभियोगकर्ता का कोई अधिवक्ता या अभियोजन अधिकारी अदालत में उपस्थित नहीं है।
- न्यायालय को यह संतोष होना चाहिए कि अभियोगकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- न्यायालय अभियोगकर्ता को 30 दिनों का नोटिस देकर अंतिम अवसर देता है।
- नोटिस का पालन न होने पर न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है या मुकदमा आगे बढ़ा सकता है।
- अभियोगकर्ता की मृत्यु होने पर भी यह प्रक्रिया लागू होती है।
धारा 279 का उद्देश्य
इस प्रावधान का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा होने से रोकना है। कई बार अभियोगकर्ता बार-बार अनुपस्थित रहता है, जिससे मुकदमों में देरी होती है और अभियुक्त को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती है। साथ ही, न्यायालय को यह विवेक दिया गया है कि यदि अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति से मुकदमा बेवजह लंबा हो रहा हो और अदालत यह मानती हो कि अभियोगकर्ता की उपस्थिति से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, तो मामला समाप्त किया जा सकता है।
धारा 279 का उद्देश्य निम्नलिखित है:
- न्यायालय का समय बचाना।
- अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करना।
- न्याय प्रक्रिया को प्रभावी और समयबद्ध बनाना।
- अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति में मामला अनिश्चित काल तक लंबित न रखना।
- अभियोगकर्ता की मृत्यु की स्थिति में प्रक्रिया का स्पष्ट मार्ग प्रदान करना।
प्रक्रिया : चरण दर चरण
(1) अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति की पुष्टि
न्यायालय को यह देखना होता है कि अभियोगकर्ता निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं है। यदि उसका कोई अधिवक्ता या अभियोजन अधिकारी उपस्थित नहीं है, तो न्यायालय अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति को दर्ज करता है।
(2) व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है – न्यायालय का विचार
न्यायालय यह विचार करता है कि अभियोगकर्ता की उपस्थिति से मुकदमे में कोई विशेष लाभ या आवश्यकता तो नहीं। यदि मामला दस्तावेज़ों पर आधारित है, गवाह उपलब्ध हैं, या अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति से अभियुक्त का अधिकार प्रभावित नहीं होता, तो न्यायालय आगे की प्रक्रिया कर सकता है।
(3) 30 दिनों का नोटिस
न्यायालय अभियोगकर्ता को अंतिम अवसर देने के लिए नोटिस जारी करता है। नोटिस की अवधि न्यूनतम 30 दिन होती है। नोटिस में अभियोगकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पक्ष रखे।
(4) अनुपस्थिति की स्थिति में निर्णय
यदि अभियोगकर्ता नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय के पास दो विकल्प होते हैं:
- अभियुक्त को दोषमुक्त (Acquit) कर देना।
- मुकदमा आगे बढ़ाना, यदि अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति से कोई गंभीर असर नहीं पड़ता।
(5) अभियोगकर्ता की मृत्यु होने पर
यदि अभियोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो न्यायालय अभियोग की प्रकृति, अन्य गवाहों की उपलब्धता, और अभियुक्त के अधिकारों को देखते हुए मुकदमा आगे बढ़ा सकता है या समाप्त कर सकता है।
न्यायालय की जिम्मेदारी
धारा 279 न्यायालय को केवल अधिकार नहीं देती, बल्कि उसे सावधानी से कार्य करने का दायित्व भी देती है। न्यायालय को:
- अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति का वास्तविक कारण जांचना चाहिए।
- नोटिस उचित समय पर देना चाहिए।
- अभियुक्त के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।
- न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखना चाहिए।
- आवश्यक होने पर अन्य गवाहों से बयान लेकर मुकदमा आगे बढ़ा सकता है।
अभियुक्त के अधिकार
धारा 279 अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करती है। अभियुक्त को यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है कि उसके खिलाफ मामला केवल अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति के कारण लंबित न रहे। यदि अभियोगकर्ता आवश्यक नहीं है, तो मुकदमा समाप्त कर दिया जाता है जिससे अभियुक्त को बेवजह परेशान नहीं किया जाता।
इसके अतिरिक्त:
- अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत होने का अधिकार मिलता है।
- अभियुक्त को सुनवाई का अवसर मिलता है।
- अभियुक्त की बेगुनाही या दोष सिद्ध करने के आधार पर उचित निर्णय लिया जाता है।
अभियोगकर्ता के अधिकार और दायित्व
हालांकि धारा 279 अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति की स्थिति में न्यायालय को कार्रवाई करने का अधिकार देती है, फिर भी अभियोगकर्ता को निम्नलिखित दायित्व निभाने चाहिए:
- समय पर अदालत में उपस्थित होना।
- प्रतिनिधि नियुक्त करना यदि स्वयं उपस्थित न हो सके।
- न्यायालय को अनुपस्थिति का उचित कारण बताना।
- मुकदमे को आगे बढ़ाने में सहयोग करना।
यदि अभियोगकर्ता बार-बार अनुपस्थित रहता है, तो न्यायालय उसके पक्ष को समाप्त कर सकता है। इस तरह अभियोगकर्ता पर भी एक जिम्मेदारी आती है कि वह न्याय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाए।
व्यावहारिक उदाहरण
उदाहरण 1 – अनुपस्थिति पर मामला समाप्त
रमेश नामक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के खिलाफ सार्वजनिक उपद्रव का मामला दर्ज कराया। अदालत में तीन बार समन जारी हुआ लेकिन रमेश उपस्थित नहीं हुआ। न कोई वकील आया न कोई प्रतिनिधि। न्यायालय ने अभियोगकर्ता को 30 दिनों का नोटिस देकर अंतिम अवसर दिया। कोई जवाब नहीं आया तो अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।
उदाहरण 2 – मृत्यु पर मामला आगे बढ़ा
सीमा नामक महिला ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया। अदालत में दो बार उपस्थित नहीं हो सकी। तीसरे समन से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने उसके बयान, चिकित्सा रिपोर्ट और अन्य गवाहों के आधार पर मामला आगे बढ़ाया क्योंकि अपराध की प्रकृति गंभीर थी।
उदाहरण 3 – व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं
किसी ट्रैफिक उल्लंघन के मामले में अभियोगकर्ता एक अधिकारी था। उसके न आने पर न्यायालय ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई जारी रखी क्योंकि अभियोगकर्ता की उपस्थिति केवल औपचारिकता थी।
धारा 279 का न्यायिक महत्व
धारा 279 न्यायपालिका को व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है। इससे:
- न्यायालय का समय बचता है।
- अभियुक्त को बेवजह अभियोग का सामना नहीं करना पड़ता।
- न्याय प्रक्रिया समय पर पूरी होती है।
- अभियोगकर्ता को जिम्मेदारी का एहसास होता है।
- मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है।
धारा 279 और अन्य प्रावधानों का संबंध
धारा 279 अकेला प्रावधान नहीं है। यह दंड प्रक्रिया की अन्य धाराओं के साथ मिलकर न्याय प्रक्रिया को संतुलित करती है। उदाहरण के लिए:
- धारा 528 BNSS के तहत न्यायालय कुछ मामलों में संज्ञान लेने के बाद भी अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति में उचित कदम उठा सकता है।
- धारा 173 में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा आगे बढ़ सकता है।
- धारा 304 में गवाहों के अनुपस्थिति पर निर्णय दिया जा सकता है।
इस प्रकार धारा 279 न्यायालय को विवेक प्रदान करती है, परंतु इसे सावधानी से लागू करना आवश्यक है।
धारा 279 लागू करते समय न्यायालय की सावधानियां
- नोटिस भेजना आवश्यक है – अन्यथा न्यायालय की कार्रवाई अनुचित मानी जा सकती है।
- अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति के वास्तविक कारण की जाँच करनी चाहिए।
- अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए।
- मामला समाप्त करने से पहले अदालत को संतोष होना चाहिए कि अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति न्याय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर रही।
- मृत्यु की स्थिति में गवाहों और दस्तावेज़ों का समुचित परीक्षण करना चाहिए।
धारा 279 का आलोचनात्मक विश्लेषण
धारा 279 न्याय की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका भी रहती है। यदि अदालत जल्दबाजी में बिना उचित कारण के अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति मानकर मामला समाप्त कर देती है, तो न्याय प्रभावित हो सकता है। इसलिए:
- न्यायालय को पर्याप्त कारण दर्ज करना चाहिए।
- अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति को औपचारिकता न मानकर गंभीरता से जांचना चाहिए।
- अभियुक्त और अभियोगकर्ता दोनों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
निष्कर्ष
धारा 279 भारतीय न्याय संहिता, 2023 का एक ऐसा प्रावधान है जो अभियोगकर्ता की अनुपस्थिति या मृत्यु की स्थिति में न्याय प्रक्रिया को स्पष्टता और दिशा देता है। यह प्रावधान न्यायालय को यह विवेक देता है कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए, साथ ही अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा की जा सके। उचित नोटिस, संतुलित निर्णय, और पारदर्शिता के साथ इसका प्रयोग न्याय प्रणाली को प्रभावी, समयबद्ध और न्यायसंगत बनाता है।
इस प्रावधान से यह संदेश भी मिलता है कि न्याय केवल विधिक अधिकारों का प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रक्रिया की जिम्मेदारी और सक्रिय भागीदारी का भी विषय है। न्यायालय, अभियोगकर्ता और अभियुक्त – तीनों की भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए धारा 279 भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और व्यावहारिक बनाती है।