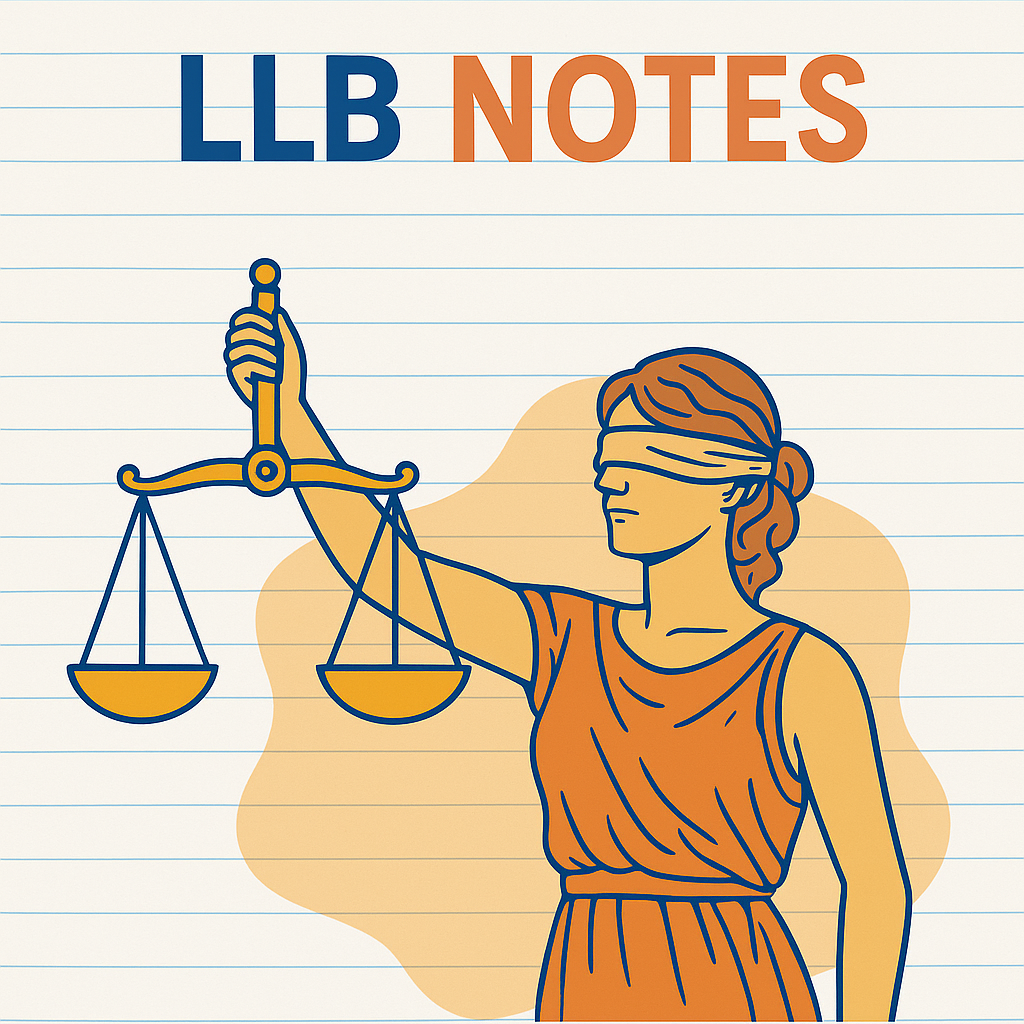दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunction) और अंतरिम आदेश (Interim Orders)
I. प्रस्तावना
दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code – CPC) के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतरिम आदेश न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले ऐसे आदेश हैं, जिनका उद्देश्य वाद के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखना और पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करना है। ये आदेश न्याय की अंतरिम सुरक्षा के लिए होते हैं, ताकि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी पक्ष को अपूरणीय हानि न हो।
II. अस्थायी निषेधाज्ञा की परिभाषा (Temporary Injunction – Definition)
Order XXXIX Rules 1 & 2 CPC के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा वह आदेश है, जिसके द्वारा न्यायालय किसी पक्ष को कोई कार्य करने या न करने का निर्देश देता है, ताकि वाद के अंतिम निपटारे तक पक्षकारों के अधिकार सुरक्षित रहें।
III. अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की परिस्थितियां (Grounds under Order 39 Rule 1 & 2)
A. Rule 1 – सामान्य परिस्थितियां
न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है यदि –
- प्रतिवादी द्वारा वादी की संपत्ति को नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने या बेचने का खतरा हो।
- प्रतिवादी वादी के कब्जे से संपत्ति हटाने का प्रयास कर रहा हो।
- प्रतिवादी वादी की अचल संपत्ति में अतिक्रमण कर रहा हो।
B. Rule 2 – संविदात्मक या अन्य अधिकारों का उल्लंघन
यदि यह सिद्ध हो कि प्रतिवादी वादी के संविदात्मक या अन्य विधिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या करने की धमकी दे रहा है, तो न्यायालय उसे रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकता है।
IV. अस्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए न्यायिक सिद्धांत (Judicial Principles)
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने अस्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए निम्न तीन आवश्यक तत्व तय किए हैं –
- Prima Facie Case – वादी का प्रथम दृष्टया एक वैधानिक अधिकार और उस पर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण का खतरा होना चाहिए।
- Balance of Convenience – सुविधाओं का संतुलन वादी के पक्ष में होना चाहिए, अर्थात निषेधाज्ञा न देने पर वादी को अधिक नुकसान होगा।
- Irreparable Loss – यदि निषेधाज्ञा न दी गई तो वादी को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई केवल हर्जाने (Damages) से नहीं हो सकेगी।
केस लॉ:
- Dalpat Kumar v. Prahlad Singh, (1992) 1 SCC 719 – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्थायी निषेधाज्ञा देना न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसे उपरोक्त तीन शर्तों के आधार पर ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
V. अंतरिम आदेश (Interim Orders)
A. परिभाषा
अंतरिम आदेश ऐसे आदेश हैं, जिन्हें न्यायालय वाद के लंबित रहने के दौरान जारी करता है, ताकि वाद का अंतिम निर्णय प्रभावी और न्यायसंगत हो सके।
B. प्रकार
- अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunction) – Order 39 के तहत।
- अस्थायी नियुक्ति (Appointment of Receiver) – Order 40 के तहत।
- संपत्ति का संरक्षण या अभिरक्षा (Preservation of Property) – Order 38 के तहत जब्त (Attachment) का आदेश।
- अंतरिम भरण-पोषण (Interim Maintenance) – पारिवारिक मामलों में।
C. उद्देश्य
- यथास्थिति बनाए रखना।
- अंतिम निर्णय को प्रभावी बनाना।
- न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित रखना।
VI. क्या न्यायालय इन्हें स्वेच्छा से जारी कर सकता है?
A. सामान्य नियम
- सामान्यतः अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतरिम आदेश आवेदन (Application) पर ही दिए जाते हैं।
- CPC के तहत न्यायालय का अधिकार विवेकाधीन (Discretionary) है, और इसे न्यायसंगत कारणों से ही प्रयोग किया जा सकता है।
B. अपवाद
- यदि परिस्थितियां अत्यंत तात्कालिक हैं और न्यायालय को यह लगता है कि बिना आवेदन के आदेश न देने से न्याय में विफलता होगी, तो न्यायालय Suo Motu (स्वप्रेरणा से) आदेश जारी कर सकता है, बशर्ते कि –
- ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण रिकॉर्ड पर हों, और
- पक्षकारों को बाद में सुनवाई का अवसर दिया जाए।
केस लॉ:
- Manohar Lal Chopra v. Rai Bahadur Rao Raja Seth Hiralal, AIR 1962 SC 527 – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CPC के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा न्यायालय अपने अंतर्निहित अधिकार (Inherent Powers – Section 151 CPC) का प्रयोग कर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।
- Padam Sen v. State of U.P., AIR 1961 SC 218 – न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 151 CPC का प्रयोग न्याय की रक्षा के लिए किया जा सकता है, परंतु इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
VII. निषेधाज्ञा के उल्लंघन के परिणाम
- Order 39 Rule 2A CPC – उल्लंघन करने वाले पक्ष को दंडस्वरूप हिरासत या संपत्ति की कुर्की की सजा दी जा सकती है।
- यह न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) भी मानी जा सकती है।
VIII. निष्कर्ष
अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतरिम आदेश, न्यायालय द्वारा न्याय की अंतरिम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय हैं।
- ये न केवल पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि वाद के अंतिम निर्णय को प्रभावी और सार्थक बनाते हैं।
- न्यायालय इन्हें सामान्यतः पक्षकार के आवेदन पर देता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में अपने अंतर्निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्वेच्छा से भी जारी कर सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट के दृष्टांतों से यह सिद्ध होता है कि ऐसे आदेश न्याय के हित में, विवेकपूर्ण और पारदर्शी ढंग से ही दिए जाने चाहिए।