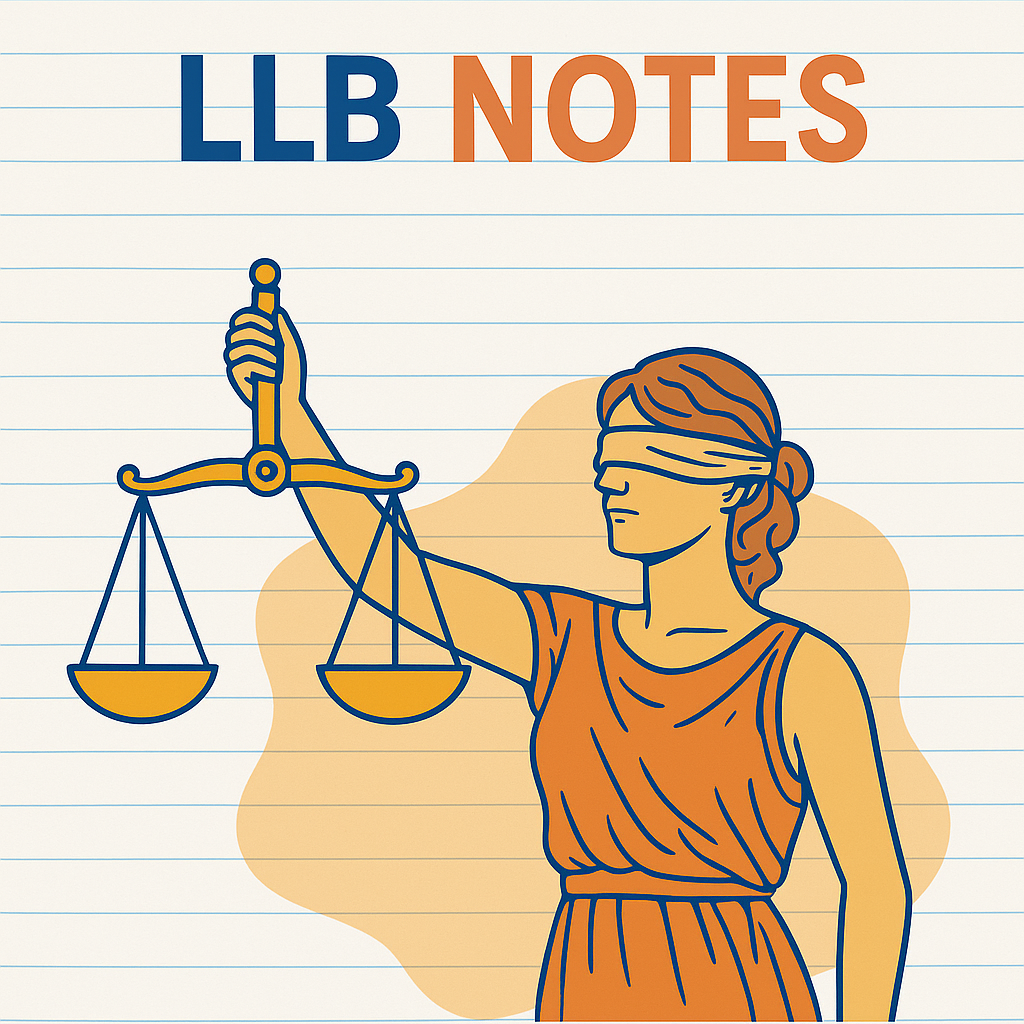दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 का उद्देश्य और क्षेत्राधिकार (Object and Scope)
भूमिका
दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code – CPC) भारत में दीवानी न्यायालयों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला प्रमुख अधिनियम है। यह संहिता एक व्यापक और सुव्यवस्थित विधिक ढांचा प्रदान करती है, जिसके माध्यम से नागरिक मामलों में न्यायालय कार्यवाही, दावे, वाद, अपील, वाद का निर्णय, आदेश, निष्पादन आदि को संचालित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक वादों में निष्पक्ष, त्वरित और एकसमान न्याय सुनिश्चित करना है।
I. CPC का उद्देश्य (Object of CPC)
दीवानी प्रक्रिया संहिता के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –
- न्यायिक प्रक्रिया में एकरूपता (Uniformity in Civil Proceedings)
- CPC पूरे भारत में दीवानी कार्यवाही के लिए एक समान नियम प्रदान करती है ताकि न्यायालयों में भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएं न अपनाई जाएं।
- न्याय की निष्पक्षता और सुविधा (Fairness and Convenience in Justice)
- यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और सबूत देने का पूरा अवसर मिले।
- त्वरित निपटान (Speedy Disposal of Cases)
- लंबे समय तक मुकदमेबाजी से बचाने के लिए इसमें ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा हो सके।
- न्यायिक संसाधनों का कुशल उपयोग (Efficient Use of Judicial Resources)
- CPC में वाद की सुनवाई, साक्ष्य की प्रस्तुति और आदेश के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिससे न्यायालय का समय बच सके।
- अधिकारों का संरक्षण (Protection of Rights)
- यह पक्षकारों के वैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा करते हुए न्याय दिलाने का माध्यम बनती है।
II. CPC का क्षेत्राधिकार (Scope of CPC)
दीवानी प्रक्रिया संहिता का क्षेत्राधिकार व्यापक है, जो निम्न प्रकार से समझा जा सकता है –
1. भौगोलिक क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction)
- CPC पूरे भारत में लागू है, सिवाय जम्मू-कश्मीर राज्य (जहाँ पर कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग प्रावधान लागू थे, जो अब 2019 के बाद भारतीय कानूनों के अंतर्गत आ चुके हैं)।
2. विषयगत क्षेत्राधिकार (Subject Matter Jurisdiction)
- यह केवल दीवानी मामलों पर लागू होती है, आपराधिक मामलों पर नहीं।
- उदाहरण: संपत्ति विवाद, अनुबंध विवाद, वसूली, वैवाहिक वाद, उत्तराधिकार आदि।
3. संरचनात्मक क्षेत्राधिकार (Structural Scope)
- CPC के दो भाग हैं:
- भाग 1 – आदेश एवं नियम (Orders & Rules) – प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत प्रावधान।
- भाग 2 – अनुसूचियां (Schedules) – विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं और फार्मेट का विवरण।
4. प्रक्रियात्मक क्षेत्राधिकार (Procedural Scope)
- CPC में वाद की शुरुआत से लेकर निर्णय और उसके क्रियान्वयन तक की संपूर्ण प्रक्रिया दी गई है।
III. CPC: केवल प्रक्रियात्मक कानून या मौलिक अधिकारों का प्रावधान?
CPC मूलतः प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) है, क्योंकि यह यह निर्धारित करती है कि न्यायालय में दीवानी मामले कैसे दायर, सुने और निपटाए जाएंगे। यह स्वयं में कोई नया अधिकार (Substantive Right) प्रदान नहीं करती, बल्कि मौलिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है।
A. CPC का प्रक्रियात्मक स्वरूप
- किसी व्यक्ति का संपत्ति पर अधिकार या अनुबंध से उत्पन्न अधिकार substantive right है, लेकिन उसका प्रवर्तन (enforcement) कैसे होगा, यह CPC बताती है।
- उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति का अनुबंध के तहत धन वसूलने का अधिकार है, तो वह CPC के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा दायर करेगा।
B. कुछ प्रावधानों का अर्ध-मौलिक स्वरूप (Quasi-Substantive Nature)
हालांकि CPC प्रक्रियात्मक कानून है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान पक्षकारों के अधिकारों को सीधे प्रभावित करते हैं। उदाहरण:
- धारा 9 – यह बताती है कि सभी दीवानी वादों का न्यायालय में विचार होगा, जब तक कि वे स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हों। यह व्यक्तियों को न्यायालय में जाने का अधिकार देती है।
- धारा 11 (Res Judicata) – एक ही वाद को दोबारा लाने पर रोक लगाती है। यह अधिकार के प्रयोग को सीमित करती है।
- धारा 80 – सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने से पहले नोटिस देना आवश्यक है।
इन प्रावधानों का प्रभाव सीधा substantive rights पर पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्ध-मौलिक माना जा सकता है।
IV. न्यायिक दृष्टांत (Judicial Precedents)
- State of Punjab v. Shamlal Murari, AIR 1976 SC 1177
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि CPC एक प्रक्रियात्मक कानून है, जिसका उद्देश्य न्याय की सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, न कि अधिकार प्रदान करना।
- Sushil Kumar Mehta v. Gobind Ram Bohra, (1990) 1 SCC 193
- न्यायालय ने कहा कि CPC का मूल उद्देश्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया और विधिक सिद्धांतों को स्पष्ट करना है, ताकि मुकदमों का निष्पक्ष निपटान हो सके।
- Bhagwati Developers Pvt. Ltd. v. Peerless General Finance & Investment Co. Ltd., (2013) 5 SCC 455
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि CPC के कुछ प्रावधान अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य चरित्र प्रक्रियात्मक ही है।
- Mulla’s Commentary on CPC
- मल्ला के अनुसार CPC न्याय का एक साधन है, न कि स्वयं न्याय। इसका उद्देश्य विधिक अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करना है।
V. निष्कर्ष
दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 भारत के नागरिक न्यायिक तंत्र की रीढ़ है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में एकरूप, निष्पक्ष और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया स्थापित करना है। यह मूलतः एक प्रक्रियात्मक कानून है, जो यह तय करता है कि नागरिक अधिकारों का प्रवर्तन कैसे होगा।
यद्यपि इसके कुछ प्रावधान पक्षकारों के substantive rights को प्रभावित करते हैं, फिर भी इसका प्रमुख स्वरूप प्रक्रियात्मक ही है। न्यायिक दृष्टांतों से भी यह स्पष्ट होता है कि CPC अधिकार नहीं देती, बल्कि उन्हें लागू करने का मार्ग प्रदान करती है।
अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि CPC का उद्देश्य न्याय की सुव्यवस्थित, त्वरित और निष्पक्ष प्रक्रिया प्रदान करना है, तथा इसका क्षेत्राधिकार व्यापक है, जो भारत के सभी दीवानी न्यायालयों में लागू होता है।