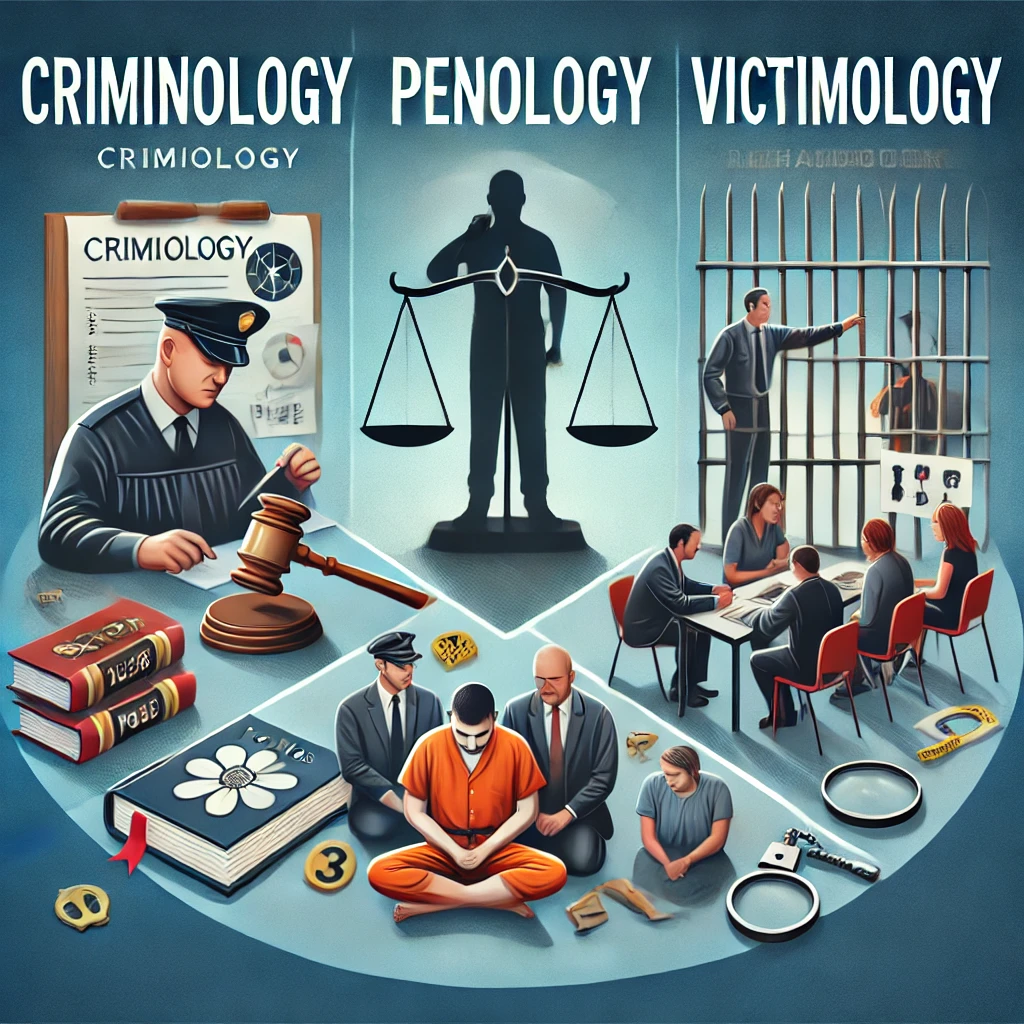-
अपराध को परिभाषित कीजिए।
अपराध वह कार्य है, जो कानून द्वारा अवैध घोषित किया गया है और जिस पर दंड या दंडात्मक कार्रवाई निर्धारित है। - अपराध शास्त्र को परिभाषित कीजिए।
अपराध शास्त्र वह अध्ययन है, जो अपराध, अपराधी और समाज पर इसके प्रभावों का अध्ययन करता है, तथा अपराधों के कारण, परिहार और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। - अपराधशास्त्र के महत्व को बताइये।
अपराधशास्त्र समाज में अपराध की पहचान, कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपायों को समझने में मदद करता है। यह अपराध की रोकथाम के लिए प्रभावी नीतियों का निर्माण करने में सहायक होता है। - अपराधशास्त्र के सन्दर्भ में समाजशास्त्री विचारधारा।
समाजशास्त्रियों के अनुसार अपराध समाज की संरचना, सांस्कृतिक मान्यताओं और सामाजिक स्थितियों से प्रभावित होता है। वे यह मानते हैं कि अपराध का कारण सामाजिक असमानताएँ, गरीबी, शिक्षा का अभाव और पारिवारिक समस्याएँ होती हैं। - आपराधिक विधि के उद्देश्य।
आपराधिक विधि का उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना, समाज में न्याय की स्थापना करना, और अपराध की रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों का निर्माण करना है। - दुराशय क्या है?
दुराशय (Mens Rea) वह मानसिक स्थिति है, जब अपराधी किसी अपराध को करने का इरादा रखता है। यह अपराध के दोषी होने के मानसिक तत्व को दर्शाता है। - अपराध की कारणता का शास्त्रीय सिद्धान्त।
शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार, अपराध के कारण व्यक्ति का स्वार्थ और स्वतंत्र इच्छा होती है। इसे बेकलर और बेकन द्वारा समर्थित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों को समझने और पूर्वानुमान करने में सक्षम होता है। - सफेदपोश अपराध से आप क्या समझते हैं?
सफेदपोश अपराध (White-collar crime) उच्च पदस्थ व्यक्तियों द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों को कहा जाता है, जो आमतौर पर धोखाधड़ी, कर चोरी, और वित्तीय अनियमितताओं के रूप में होते हैं। - “उपचार से निवारण बेहतर होता है।” विवेचना कीजिए।
यह कथन इस बात को दर्शाता है कि किसी समस्या या अपराध के होने से पहले उसका निवारण करना अधिक प्रभावी है, बजाय इसके कि बाद में उस पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाए। निवारण से समाज में अपराध की दर को कम किया जा सकता है। - दण्डशास्त्र से आप क्या समझते हैं?
दण्डशास्त्र (Penology) वह शास्त्र है, जो दंड, जेल, सुधारात्मक उपायों और सजा की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, और यह समाज में अपराधियों के पुनर्वास और उनके सुधार के तरीकों पर केंद्रित है। - दण्ड को परिभाषित कीजिए।
दण्ड वह कार्रवाई है, जिसे किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए सजा देने के उद्देश्य से लागू किया जाता है। यह शारीरिक, मानसिक या वित्तीय हो सकता है। - दण्ड के क्या औचित्य हैं?
दण्ड के औचित्य में अपराधी को सुधारना, समाज में न्याय की स्थापना करना, अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना, और समाज को यह संदेश देना कि अपराधियों को दंडित किया जाएगा, शामिल हैं।
- एकान्त परिरोध
एकान्त परिरोध (Solitary Confinement) वह स्थिति है, जिसमें अपराधी को अन्य कैदियों से अलग करके अकेले रखा जाता है। इसका उद्देश्य अपराधी को मानसिक और शारीरिक रूप से दंडित करना होता है, हालांकि इसे अत्यधिक नहीं अपनाया जाता क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। - मृत्युदण्ड से आप क्या समझते हैं?
मृत्युदण्ड (Death Sentence) वह सजा है, जिसमें अपराधी को उसकी अपराधों के लिए जीवनभर की सजा के बजाय मृत्यु तक दंडित किया जाता है। यह सजा गंभीर अपराधों के लिए लागू की जाती है, जैसे हत्या, आतंकवाद, और अन्य गंभीर अपराध। - “मृत्यु अन्वेषण रिपोर्ट” से क्या अभिप्राय है? इसकी विधिक एवं साक्ष्यीय उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।
मृत्यु अन्वेषण रिपोर्ट (Inquest Report) एक सरकारी अधिकारी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच का विवरण होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होती है। इसका उद्देश्य मृत्यु के कारणों का पता लगाना होता है। यह रिपोर्ट न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है और इसकी विधिक उपयोगिता होती है क्योंकि यह मृत्यु के कारणों का प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करती है। - इच्छा मृत्यु क्या है?
इच्छा मृत्यु (Euthanasia) एक प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी गंभीर बीमारी या असहनीय दर्द से मुक्ति देने के लिए चिकित्सकीय रूप से मृत्यु दी जाती है। इसे “मृत्यु का दया” भी कहा जाता है, और इसे कुछ देशों में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। - दण्ड कितने प्रकार के होते हैं?
दण्ड मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं:- शारीरिक दण्ड: जैसे सजा, जेल, बन्धन आदि।
- आर्थिक दण्ड: जैसे जुर्माना।
- मानसिक दण्ड: जैसे अपमान, समाज से बहिष्कार।
- दण्ड को निलम्बित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
दण्ड को निलम्बित करने का मुख्य उद्देश्य अपराधी को एक दूसरे अवसर देना होता है, ताकि वह अपने सुधार और पुनर्वास के लिए कार्य कर सके। यह एक प्रकार का लचीला दण्ड है, जिसका उद्देश्य सुधारात्मक उपायों पर जोर देना होता है। - प्राचीन एवं वर्तमान दण्ड विधियों की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए।
प्राचीन दण्ड विधियों में शारीरिक दण्ड जैसे फांसी, शारीरिक उत्पीड़न, और उत्पीड़न के अन्य तरीके सामान्य थे। वर्तमान दण्ड विधियों में सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। आजकल, मृत्यु दण्ड कम प्रयोग में आता है और जेलों में सुधारात्मक कार्यक्रमों की अधिकता है। - आदर्श दण्ड नीति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
आदर्श दण्ड नीति की विशेषताएँ हैं:- न्यायसंगतता: दण्ड को अपराध के गंभीरता के अनुसार उचित रूप से निर्धारित किया जाए।
- समाज सुधार: दण्ड का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि अपराधी को समाज में वापस सुधारकर लाना होना चाहिए।
- मानवीयता: दण्ड को अत्यधिक कठोर और अमानवीय नहीं होना चाहिए।
- संवेदनशीलता: दण्ड प्रक्रिया में पीड़ितों और अपराधियों दोनों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
- ‘दण्ड के प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त’ को संक्षिप्त रूप से समझाइए।
प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त (Retributive Theory of Punishment) के अनुसार, दण्ड का उद्देश्य केवल अपराधी को उसके अपराध का बदला देना है, न कि सुधार या निवारण। यह सिद्धान्त मानता है कि अपराध करने वाले को उसी के अपराध के अनुरूप सजा मिलनी चाहिए। - अपराध-शास्त्र एवं दण्डशास्त्र के बीच सम्बन्धों की विवेचना करें।
अपराधशास्त्र और दण्डशास्त्र दोनों का उद्देश्य समाज में अपराध की रोकथाम और दंडात्मक उपायों का निर्धारण करना है। अपराधशास्त्र अपराधों और उनके कारणों का अध्ययन करता है, जबकि दण्डशास्त्र अपराधियों के लिए सजा और सुधारात्मक उपायों का अध्ययन करता है। दोनों में जुड़ा हुआ तत्व यह है कि वे समाज को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाए रखने के लिए काम करते हैं। - आत्महत्या
आत्महत्या (Suicide) एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपनी जीवनलीला समाप्त करने की क्रिया है। यह मानसिक तनाव, अवसाद या अन्य मानसिक समस्याओं के कारण हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। - धन्धेबाजी (बलाद्गहण)
धन्धेबाजी (Racketeering) एक अवैध व्यापार या गतिविधि है, जिसमें अपराधियों द्वारा अवैध तरीकों से धन अर्जित करने के लिए धोखाधड़ी, जबरन वसूली, या अन्य अपराधिक गतिविधियाँ की जाती हैं। - अनियत दण्डादेश से आप क्या समझते हैं?
अनियत दण्डादेश (Indeterminate Sentence) वह सजा होती है, जिसमें अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसे एक न्यूनतम और अधिकतम समय के बीच सजा दी जाती है, और यह उसकी आचरण के आधार पर बदल सकती है।
- पुलिस को परिभाषित करें।
पुलिस एक सरकारी संगठन है, जिसका कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना, और समाज में सुरक्षा प्रदान करना है। - राष्ट्रीय पुलिस आयोग।
राष्ट्रीय पुलिस आयोग (National Police Commission) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग है, जिसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था में सुधार करना और इसे अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिकों के प्रति जिम्मेदार बनाना है। - महिला पुलिस।
महिला पुलिस वह पुलिसकर्मी होती हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों की जांच, रोकथाम और सुधार कार्य में कार्यरत होती हैं। वे संवेदनशील मुद्दों पर विशेष ध्यान देती हैं, जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, आदि। - इन्टरपोल।
इंटरपोल (Interpol) एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। यह सदस्य देशों के बीच सूचना का आदान-प्रदान और सहयोग बढ़ाने में मदद करता है। - दण्ड न्यायालयों से आप क्या समझते हैं?
दण्ड न्यायालय (Criminal Courts) वे न्यायालय होते हैं, जो अपराधों के मामलों की सुनवाई करते हैं और अपराधियों को दंडित करने का निर्णय लेते हैं। इन न्यायालयों का उद्देश्य अपराधी को दंडित करना और न्याय स्थापित करना है। - किशोर अपराधिता को परिभाषित कीजिए।
किशोर अपराधिता (Juvenile Delinquency) वह स्थिति है, जिसमें किशोर (आमतौर पर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति) अपराध करते हैं। यह अपराध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चोरी, हिंसा, ड्रग्स की तस्करी आदि। - परिवीक्षा को परिभाषित कीजिए।
परिवीक्षा (Probation) एक सुधारात्मक व्यवस्था है, जिसमें अपराधी को कारागार भेजने के बजाय उसे एक पर्यवेक्षक (परिवीक्षा अधिकारी) के तहत अपनी आचरण सुधारने का मौका दिया जाता है। इसका उद्देश्य अपराधियों का पुनर्वास करना है। - परिवीक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
परिवीक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं:- अपराधियों का सुधार और पुनर्वास
- अपराधी को समाज में पुनः शामिल करना
- जेलों की भीड़ को कम करना
- समाज में अपराध दर को कम करना।
- परिवीक्षा अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं?
परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य हैं:- परिवीक्षित अपराधी की निगरानी करना
- उसे सुधारात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना
- उसके व्यवहार का मूल्यांकन करना
- न्यायालय को परिवीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- अपराधी के सुधार के लिए योजना बनाना और उसे लागू करना।
- परिवीक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं?
परिवीक्षा प्रणाली एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें अपराधी को सजा के रूप में जेल भेजने के बजाय उसे अपनी आचरण सुधारने और पुनर्वास करने का मौका दिया जाता है, और यह एक पर्यवेक्षक द्वारा नियंत्रित होता है। - परिवीक्षा और निलम्बित दण्ड में विभेद कीजिए।
- परिवीक्षा: अपराधी को जेल भेजने के बजाय उसे पुनर्वास के लिए एक पर्यवेक्षक के तहत छोड़ा जाता है।
- निलम्बित दण्ड: अपराधी को एक निश्चित समय तक दण्डित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वह शर्तों का उल्लंघन करता है, तो सजा को लागू किया जा सकता है।
- पैरोल से आप क्या समझते हैं?
पैरोल (Parole) एक सुधारात्मक व्यवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी सजा का कुछ हिस्सा पूरी करने के बाद अच्छे आचरण के कारण समय से पहले रिहा किया जाता है। यह रिहाई एक शर्तों के तहत होती है, जिसमें अपराधी को अनुशासन का पालन करना होता है। - पैरोल और फर्मों में विभेद कीजिए।
- पैरोल: यह एक ऐसा सुधारात्मक उपाय है, जिसमें व्यक्ति को उसकी सजा पूरी करने से पहले शर्तों के साथ रिहा किया जाता है।
- फर्मों: यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें अपराधी को अस्थायी रूप से जेल से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है, जैसे कि परिवार से मिलने या इलाज के लिए।
- कारागार को परिभाषित कीजिए।
कारागार (Jail) वह संस्थान है, जहां अपराधियों को उनकी सजा भुगतने के लिए रखा जाता है। यह जेल, सुधार गृह या कारागार के रूप में हो सकता है और इसका उद्देश्य अपराधियों को सुधारना और उन्हें समाज में वापस लाना है। - कारागार सुधार।
कारागार सुधार (Prison Reformation) वह प्रक्रिया है, जिसके तहत जेलों में रह रहे अपराधियों को उनके आचरण में सुधार करने, शिक्षा प्राप्त करने, और समाज में पुनः शामिल होने के लिए उपयुक्त अवसर और कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।
- भारत में खुले कारागार शिविर।
भारत में खुले कारागार शिविर एक सुधारात्मक व्यवस्था है, जिसमें कैदी को जेल के दीवारों से बाहर कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। यहां कैदी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। इसका उद्देश्य अपराधियों को सुधारने और उन्हें समाज में पुनः शामिल करने के लिए अवसर प्रदान करना है। - आदर्श कारागार।
आदर्श कारागार एक ऐसा कारागार होता है, जिसमें अपराधियों को सुधारने के लिए बेहतर शर्तें और पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। यह कैदियों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, और मानसिक सुधार के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है। - बोर्टल प्रणाली क्या है?
बोर्टल प्रणाली (Borstal Home System) एक सुधारात्मक प्रणाली है, जो विशेष रूप से किशोर अपराधियों के लिए होती है। इसमें किशोरों को सुधारने के लिए विशेष पुनर्वास कार्यक्रम और शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे भविष्य में समाज में पुनः शामिल हो सकें। - भारत में जेल प्रणाली।
भारत में जेल प्रणाली का उद्देश्य अपराधियों को सजा देना, उनके सुधार के लिए उपयुक्त कार्यक्रम देना और समाज में पुनः शामिल करने के लिए उन्हें तैयार करना है। जेलों में विभिन्न सुधारात्मक उपाय जैसे शिक्षा, कार्य, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। - पुलिस-जनता का सम्बन्ध।
पुलिस-जनता का सम्बन्ध (Police-Public Relations) उस पारस्परिक विश्वास और सहयोग को दर्शाता है, जो पुलिस और जनता के बीच होना चाहिए। यह अच्छे कानून-व्यवस्था की स्थापना और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। - जेल संहिता।
जेल संहिता (Prison Code) एक कानूनी दस्तावेज़ है, जो जेलों में अपराधियों के प्रबंधन, सजा और सुधार की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह जेलों में रहने वाले कैदियों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। - प्राचीर विहीन कारागार।
प्राचीर विहीन कारागार (Wall-less Prison) एक प्रकार का सुधारात्मक केंद्र है, जिसमें कैदी को सुरक्षा के अन्य उपायों के साथ एक खुले वातावरण में रखा जाता है, बिना दीवारों के। यह उनके पुनर्वास और सुधार के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। - जेल सहायता।
जेल सहायता (Prison Aid) वह सहायता होती है, जो जेलों में कैदियों के सुधार और उनके पुनर्वास के लिए प्रदान की जाती है। इसमें शैक्षिक कार्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, और अन्य सुधारात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं। - ब्रेन मैपिग।
ब्रेन मैपिग (Brain Mapping) एक वैज्ञानिक तकनीक है, जिसका उपयोग मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसे अपराध विज्ञान में अपराधियों के मानसिक स्थिति और अपराध के कारणों को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। - अपराधशास्त्र में निठारी काण्ड का महत्व।
निठारी काण्ड अपराधशास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह समाज में अपराधों की जटिलताओं और अपराधियों के मानसिक दृष्टिकोण को उजागर करता है। इस काण्ड ने अपराधशास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया है, जैसे मनोवैज्ञानिक तत्व और समाज पर अपराधों के प्रभाव। - खुले जेल की परिभाषा दीजिए।
खुले जेल (Open Jail) एक सुधारात्मक व्यवस्था है, जिसमें कैदी को कुछ स्वतंत्रता दी जाती है और उन्हें काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और समाज में पुनः शामिल होने के अवसर दिए जाते हैं। इसमें कैदी को जेल की दीवारों से बाहर कार्य करने की अनुमति होती है, लेकिन उन पर निगरानी रखी जाती है। - दण्ड नीति में परिवीक्षा का क्या स्थान है?
दण्ड नीति में परिवीक्षा का स्थान सुधारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो अपराधियों को जेल भेजने के बजाय उन्हें सुधारने और समाज में पुनः शामिल करने का अवसर देता है। यह एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे अपराधियों के पुनर्वास की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। - मृत्युदण्ड के कार्यान्वयन में विलम्ब का क्या प्रभाव होता है?
मृत्युदण्ड के कार्यान्वयन में विलम्ब का प्रभाव यह हो सकता है कि अपराधी की मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, और न्याय प्रक्रिया पर जनता का
- लोक हित वाद क्या है?
लोक हित वाद (Public Interest Litigation – PIL) एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक हित में न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यह याचिका आमतौर पर उन मामलों में दायर की जाती है, जिनमें समाज के एक बड़े हिस्से के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो या जब किसी महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर न्याय की आवश्यकता हो। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करना है। - न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं?
न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) वह अवधारणा है, जिसमें न्यायालय अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, केवल विवादों के निपटारे तक सीमित न रहते हुए, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है। यह न्यायालयों का यह दायित्व मानता है कि वे समाज की समस्याओं पर ध्यान दें और आवश्यकतानुसार सरकार और अन्य संस्थाओं को दिशा-निर्देश और आदेश प्रदान करें। न्यायिक सक्रियता अक्सर सार्वजनिक नीति, मानवाधिकार, और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने में दिखती है।
- कारागार शिक्षा पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए।
कारागार शिक्षा (Prison Education) एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य कैदियों को जेल में रहते हुए शिक्षा और कौशल प्रदान करना है। यह उन्हें समाज में पुनः समाहित करने के लिए तैयार करता है। कारागार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कैदियों के मानसिक सुधार के साथ-साथ उनके पेशेवर कौशलों को बढ़ाना है, ताकि वे जेल से रिहा होने के बाद अपराध से बच सकें और समाज में अपने योगदान दे सकें। इस प्रकार, यह पुनर्वास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद करती है। - जेल का क्या उद्देश्य है?
जेल का प्रमुख उद्देश्य अपराधियों को सजा देना, उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करना, और समाज से खतरनाक तत्वों को अलग करना है। यह न्याय व्यवस्था का हिस्सा है, जो अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराती है। साथ ही, जेल सुधारात्मक उपायों जैसे शिक्षा, कार्य, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से अपराधियों का पुनर्वास करती है। इसके द्वारा समाज में सुरक्षा और न्याय का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। - पुलिस हिरासत में दी जाने वाली यातनाओं की संवैधानिकता पर टिप्पणी कीजिए।
पुलिस हिरासत में यातना देना संविधान और मानवाधिकारों के खिलाफ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, और यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में रखने से नहीं छीना जा सकता। पुलिस हिरासत में यातना देना, न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का भी उल्लंघन है। इस प्रकार की यातनाएं न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यह न्यायपालिका और पुलिस के बीच विश्वास को भी कमजोर करती हैं। - पुलिस रिपोर्ट की व्याख्या कीजिए।
पुलिस रिपोर्ट (Police Report) एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसे पुलिस किसी अपराध की जांच के दौरान तैयार करती है। इसमें अपराध के विवरण, सबूतों की स्थिति, गवाहों के बयान, और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का संक्षेप में वर्णन होता है। यह रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाती है और अदालत को मामले की स्थिति पर निर्णय लेने में सहायता करती है। पुलिस रिपोर्ट का उद्देश्य मामले की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करना और मामले की आगे की कार्यवाही के लिए दिशा-निर्देश देना होता है। - प्रतिकर प्रदान करने की न्यायालय की शक्ति की विवेचना कीजिए।
न्यायालय को प्रतिकर (Compensation) प्रदान करने की शक्ति संविधान और कानून द्वारा दी गई है। जब किसी व्यक्ति को अपराध के कारण मानसिक, शारीरिक या वित्तीय नुकसान होता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को उचित प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। यह शक्ति विशेष रूप से आपराधिक मामलों, महिला उत्पीड़न, मानवाधिकार उल्लंघन, और दुर्घटनाओं के मामलों में लागू होती है। इसका उद्देश्य पीड़ित को उसके नुकसान का मुआवजा देना और न्याय की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। - प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रतिकर (Compensation): यह एक वित्तीय भुगतान है जो अपराधी या संबंधित पक्ष द्वारा पीड़ित व्यक्ति को उसके नुकसान के बदले में दिया जाता है। यह एक तात्कालिक और एकमुश्त मुआवजा होता है।
- पुनर्वासन अनुदान (Rehabilitation Grant): यह वित्तीय सहायता है जो अपराध या दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को समाज में पुनः शामिल होने के लिए दी जाती है। यह लंबे समय तक जारी रह सकती है और इसका उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक पुनर्वास को बढ़ावा देना होता है।
- साइबर अपराधी।
साइबर अपराधी वे व्यक्ति होते हैं जो इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपराध करते हैं। ये अपराध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हैकिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर स्टॉकिंग, और मैलवेयर वितरण। साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होती है क्योंकि ये अपराध पारंपरिक अपराधों से कहीं अधिक जटिल और वैश्विक होते हैं। - किशोर अपराधी।
किशोर अपराधी वे व्यक्ति होते हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के होते हुए अपराध करते हैं। इन अपराधियों को विशेष रूप से किशोर न्याय प्रणाली के तहत न्यायिक उपचार मिलता है, जिसमें सुधारात्मक उपायों, पुनर्वास और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किशोर अपराधियों के लिए सजा देने के बजाय उन्हें सुधारने और समाज में पुनः समाहित करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। - घरेलू हिंसा।
घरेलू हिंसा (Domestic Violence) एक प्रकार का शारीरिक, मानसिक, या यौन उत्पीड़न होता है, जो परिवार के सदस्य (जैसे पति-पत्नी, बच्चों, या अन्य रिश्तेदारों) के बीच होता है। यह एक गंभीर अपराध है और इसे रोकने के लिए विभिन्न कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005। घरेलू हिंसा के मामलों में कानूनी सहायता, शरण और पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जाती है। - अपराध निवारण।
अपराध निवारण (Crime Prevention) वह प्रक्रिया है, जिसमें अपराधों के होने से पहले उनकी रोकथाम की जाती है। इसमें सामुदायिक भागीदारी, पुलिस कार्यवाही, शिक्षा, और जागरूकता अभियानों का योगदान होता है। अपराध निवारण के उपायों में सुरक्षा बढ़ाना, अपराधियों की पहचान करना, और समाज में सुरक्षा की भावना का निर्माण करना शामिल है। - सशर्त अभिमुक्ति।
सशर्त अभिमुक्ति (Conditional Release) एक प्रक्रिया है, जिसमें अपराधी को उसकी सजा के एक हिस्से की अवधी पूरी करने के बाद रिहा किया जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें अपराधी को पालन करना होता है। यदि वह शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी रिहाई को रद्द किया जा सकता है और उसे शेष सजा भुगतनी पड़ती है। - पुलिस में भ्रष्टाचार।
पुलिस में भ्रष्टाचार (Corruption in Police) तब होता है जब पुलिसकर्मी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और किसी मामले में रिश्वत, घूस या अन्य अवैध साधनों से लाभ प्राप्त करते हैं। यह कानून व्यवस्था को कमजोर करता है और समाज में असंतोष उत्पन्न करता है। पुलिस में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़े कानून और निगरानी की आवश्यकता होती है। - पीत पत्रकारिता का आपराधिक न्याय प्रशासन पर प्रभाव।
पीत पत्रकारिता (Yellow Journalism) समाचारों को सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे जनता में भ्रम और गलत सूचना फैल सकती है। यह आपराधिक न्याय प्रशासन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है क्योंकि यह मामलों की निष्पक्षता और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। पत्रकारिता के इस प्रकार के रूप से सामाजिक विश्वास और न्याय की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- पेशेवर अपराधी।
पेशेवर अपराधी वे व्यक्ति होते हैं जो अपराध को अपनी आजीविका का मुख्य साधन बनाते हैं। ये अपराधियों का एक समूह होते हैं, जो नियमित रूप से अपराध करते हैं और अपराधों में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। पेशेवर अपराधियों के अपराधों में चोरी, लूट, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर अपराध शामिल हो सकते हैं। इनका अपराध एक व्यवस्थित और योजना के तहत किया जाता है, और वे अधिकतर कानून की पकड़ से बचने में सफल रहते हैं। - अश्लील साहित्य।
अश्लील साहित्य (Pornography) वह सामग्री है जो यौन उत्तेजना उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रकाशित, प्रस्तुत या प्रसारित की जाती है। इसमें चित्र, वीडियो, लेख, या अन्य सामग्री हो सकती है जो यौन गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। अश्लील साहित्य को अक्सर समाज में नैतिक रूप से अनुशासनहीन माना जाता है और यह कुछ देशों में कानूनी प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है, विशेष रूप से यदि यह बच्चों या अप्राकृतिक यौन कृत्यों से संबंधित हो। - पुलिस के लिए नीति मूलक सिद्धान्त।
पुलिस के लिए नीति मूलक सिद्धांत (Principles of Policing) वह बुनियादी सिद्धांत हैं, जो पुलिस कार्यों को दिशा देने में मदद करते हैं। इनमें शामिल हैं:- न्याय की निष्पक्षता: पुलिस को हर नागरिक के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए।
- कानून का पालन: पुलिस को कानून का पालन करना और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिक कानून का पालन करें।
- सामुदायिक विश्वास: पुलिस को समाज के साथ विश्वास और सहयोग बनाए रखने की आवश्यकता है।
- कर्मचारी प्रशिक्षण: पुलिस अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना ताकि वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया: पुलिस को किसी भी आपातकालीन स्थिति का तत्परता से समाधान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- पुलिस के पाँच मुख्य विधिक कार्यों का उल्लेख कीजिए।
पुलिस के पाँच मुख्य विधिक कार्यों में शामिल हैं:- अपराध की रोकथाम: पुलिस का प्रमुख कार्य अपराधों की रोकथाम करना है।
- अपराधियों का गिरफ्तार करना: अपराधी और संदिग्धों को गिरफ्तार करना और उन्हें न्यायालय में पेश करना।
- जांच करना: पुलिस अपराधों की जांच करती है, ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और साक्ष्य एकत्र किए जा सकें।
- कानून व्यवस्था बनाए रखना: सार्वजनिक स्थानों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना।
- सामाजिक सुरक्षा: समाज में अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- अपराध की रोकथाम हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिए।
अपराध की रोकथाम के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:- शिक्षा का प्रसार: बच्चों और युवाओं में नैतिक शिक्षा और जीवन कौशल सिखाना।
- सामाजिक जागरूकता: समाज में अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- कानून का सख्त पालन: अपराधियों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान लागू करना और प्रभावी ढंग से उनका पालन कराना।
- सुरक्षा उपकरणों का उपयोग: कैमरे, सीसीटीवी और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना।
- सामुदायिक पुलिसिंग: पुलिस और जनता के बीच सहयोग बढ़ाना और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देना।
- उत्पीड़नशास्त्र की परिभाषा दीजिए।
उत्पीड़नशास्त्र (Victimology) वह शास्त्र है, जो अपराध पीड़ितों के अध्ययन से संबंधित है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से व्यक्तियों को अपराध का शिकार होना पड़ता है, इसके परिणाम क्या होते हैं, और समाज और कानून प्रणाली द्वारा उन्हें कौन सी सहायता प्राप्त होती है। उत्पीड़नशास्त्र अपराधों के पीड़ितों की मानसिक, शारीरिक, और सामाजिक स्थिति का भी अध्ययन करता है। - द्वितीयक अपराध पीड़ित व्यक्ति से क्या अभिप्राय है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए।
द्वितीयक अपराध पीड़ित व्यक्ति (Secondary Crime Victims) वे लोग होते हैं जो सीधे अपराध के शिकार नहीं होते, लेकिन अपराध के परिणामस्वरूप प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो हत्या का शिकार हुआ है, उसके परिवार के सदस्य द्वितीयक अपराध पीड़ित होते हैं क्योंकि वे अपराध से मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। -
“पीड़ित अवक्षेपण का सिद्धान्त” पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
पीड़ित अवक्षेपण का सिद्धांत (Victim Precipitation Theory) यह सिद्धांत है कि कुछ अपराधी परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए पीड़ित व्यक्ति के अपने कार्यों या व्यवहार के कारण अपराध का शिकार बनते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, अपराध पीड़ितों का कुछ कृत्य या व्यवहार अपराध के होने में योगदान कर सकता है। हालांकि, यह सिद्धांत विवादास्पद है और सभी मामलों में लागू नहीं होता, क्योंकि यह पीड़ित की जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कई बार अन्यायपूर्ण हो सकता है।