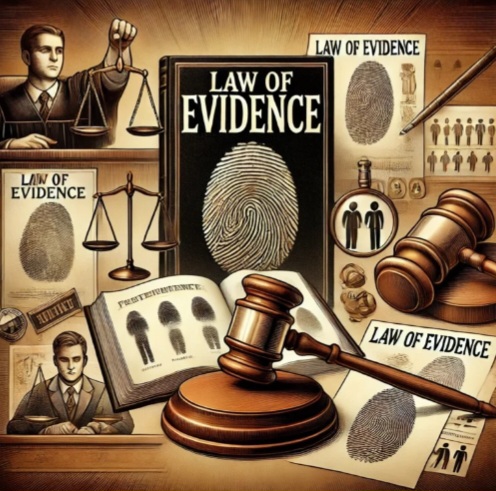डिजिटल एविडेंस की वैधता: भारतीय न्यायालयों का दृष्टिकोण
भूमिका:
डिजिटल तकनीक के बढ़ते प्रयोग ने साक्ष्य संग्रहण और प्रस्तुति की विधियों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब अपराधों का पता लगाने, उनके विश्लेषण और अभियोजन में डिजिटल एविडेंस (Digital Evidence) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मोबाइल कॉल डिटेल, ईमेल, सोशल मीडिया चैट्स, सीसीटीवी फुटेज, हार्ड ड्राइव डेटा आदि न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। परंतु, इनकी वैधता को लेकर भारतीय न्यायालयों का दृष्टिकोण तकनीकी, विधिक और संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है।
डिजिटल एविडेंस की परिभाषा और प्रकृति:
डिजिटल एविडेंस वह जानकारी है जो डिजिटल प्रारूप में होती है और जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ से एकत्र किया जाता है। यह कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट नेटवर्क, कैमरा या अन्य डिजिटल माध्यमों से उत्पन्न होता है। इसकी प्रकृति अस्थायी, संशोधित किए जा सकने योग्य और तकनीकी जांच योग्य होती है, जिससे इसकी वैधता पर संदेह की संभावनाएं बनी रहती हैं।
भारतीय कानून में डिजिटल एविडेंस की वैधता:
1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:
यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इसकी धारा 4, 5 और 65B भारतीय न्याय प्रणाली में डिजिटल एविडेंस को मान्यता प्रदान करने का आधार हैं।
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संशोधित):
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के पश्चात भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी संशोधन किया गया। इसके अनुसार:
- धारा 65B: यह विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता से संबंधित है। इसके अंतर्गत जब डिजिटल साक्ष्य की एक प्रिंटेड कॉपी, सीडी, पेन ड्राइव आदि को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके साथ एक प्रमाणपत्र (certificate) अनिवार्य होता है, जो यह सिद्ध करता है कि वह रिकॉर्ड एक वैध प्रक्रिया से निकाला गया है।
प्रमुख न्यायिक निर्णय:
1. अंजू चौधरी बनाम सीबीआई (2013):
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब तक डिजिटल साक्ष्य के स्रोत की प्रमाणिकता प्रमाणपत्र द्वारा नहीं दी जाती, तब तक उसकी वैधता संदेहास्पद मानी जा सकती है।
2. अनवर पी. वी बनाम पी. के. बशीर (2014):
इस ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता तभी दी जा सकती है जब वह धारा 65B के अंतर्गत आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. अरुणा सेन बनाम राज्य (2020, दिल्ली हाईकोर्ट):
कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा कि जब तक मूल चैट डिवाइस की वैधता की पुष्टि नहीं होती, तब तक इसे निर्णायक नहीं माना जा सकता।
4. अमिताभ ठाकुर बनाम भारत सरकार (2023):
कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि डिजिटल साक्ष्य की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह साक्ष्य किस प्रकार एकत्रित और प्रस्तुत किया गया है। न्यायालयों को तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता लेने की सलाह दी गई।
डिजिटल एविडेंस की स्वीकार्यता की शर्तें:
- प्रमाणपत्र (Certificate under Section 65B): आवश्यक है जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी प्रस्तुत की जाती है।
- प्रामाणिकता (Authenticity): साक्ष्य से छेड़छाड़ न हुई हो।
- स्रोत की वैधता: रिकॉर्ड जिस डिवाइस से लिया गया है, वह यथावत और नियंत्रित हो।
- समय और तारीख का सत्यापन: डिजिटल साक्ष्य में समय-सीमा और लोकेशन का भी महत्व होता है।
- चेन ऑफ कस्टडी (Chain of Custody): यह स्पष्ट होना चाहिए कि साक्ष्य किस-किस के पास रहा है।
चुनौतियाँ और समस्याएँ:
- साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना।
- तकनीकी विशेषज्ञता की कमी न्यायालयों में।
- प्रमाणपत्र (65B) का दुरुपयोग या अनुपलब्धता।
- डेटा गोपनीयता और व्यक्ति की निजता का उल्लंघन।
- विदेशों से प्राप्त डिजिटल साक्ष्य (जैसे – Google, Facebook) के प्रमाणीकरण में बाधा।
आधुनिक समाधान और सुधार की आवश्यकता:
- न्यायाधीशों और वकीलों को साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण।
- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं।
- न्यायालयों में डिजिटल साक्ष्य विशेषज्ञों की नियुक्ति।
- साक्ष्य संग्रहण की प्रक्रियाओं का मानकीकरण।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए साइबर कानून संधियाँ।
निष्कर्ष:
डिजिटल एविडेंस आधुनिक न्याय प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, किंतु इसकी वैधता भारतीय न्यायालयों में तकनीकी प्रमाणिकता और विधिक प्रमाणपत्रों पर निर्भर करती है। भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर अपने निर्णयों से इसकी दिशा स्पष्ट की है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में आवश्यक है कि न्यायिक प्रणाली तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बने, ताकि डिजिटल युग में न्याय की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रह सके।