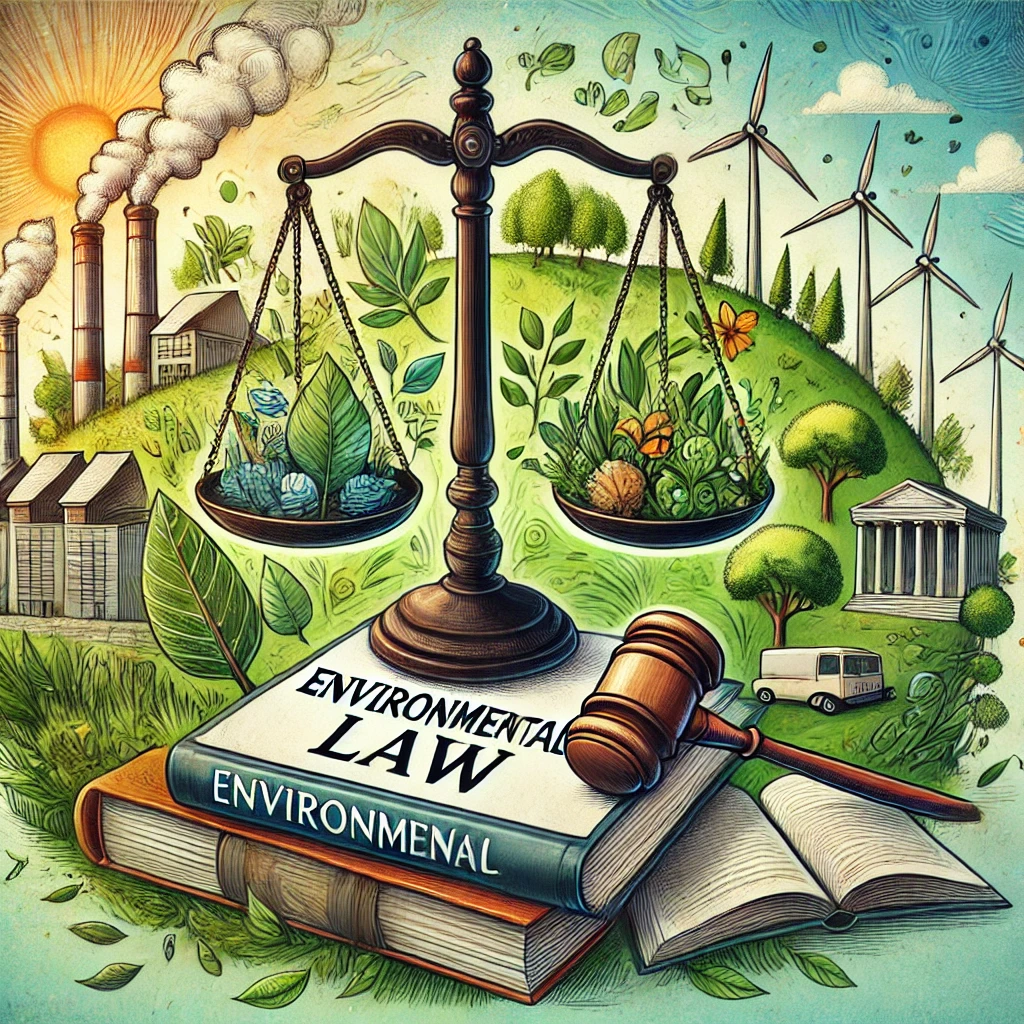जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974: स्वच्छ जल की संवैधानिक गारंटी और कानूनी रूपरेखा
प्रस्तावना:
जल मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, परंतु औद्योगीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल स्रोतों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जल की गुणवत्ता में गिरावट से न केवल मानव स्वास्थ्य, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है। इसी संकट से निपटने हेतु भारत सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को लागू किया, जो देश का पहला प्रमुख पर्यावरणीय कानून है जिसका उद्देश्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना है।
अधिनियम की पृष्ठभूमि:
1972 में स्टॉकहोम में आयोजित ‘मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन’ के बाद भारत ने पर्यावरण से जुड़े कानूनों पर गंभीरता से विचार किया। इसका पहला परिणाम था — जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, जिसे संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत राज्यों की सहमति से संसद द्वारा पारित किया गया।
मुख्य उद्देश्य:
- नदियों, तालाबों, झीलों आदि में औद्योगिक, घरेलू और कृषि अपशिष्ट के निर्वहन को नियंत्रित करना।
- प्रदूषण फैलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- जल की गुणवत्ता की निगरानी और संरक्षण हेतु संस्थागत ढांचा विकसित करना।
प्रमुख प्रावधान:
- केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना, जिन्हें जल निकायों की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण का कार्य सौंपा गया।
- किसी उद्योग को अपशिष्ट जल का निस्तारण करने से पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- प्रदूषित जल स्रोतों की पहचान कर उन्हें स्वच्छ करने के लिए योजना तैयार करना।
- नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान।
न्यायिक व्याख्या और सक्रियता:
भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर जल प्रदूषण से संबंधित मामलों में जनहित याचिकाओं के आधार पर कड़े आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने ‘जल का अधिकार’ को जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा माना है। उदाहरणस्वरूप, वेंकटेश विरुद्ध राज्य सरकार जैसे मामलों में न्यायालय ने औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए।
वर्तमान चुनौतियाँ:
- कई क्षेत्रों में जल बोर्ड संसाधनों और तकनीकी क्षमता की कमी से जूझ रहे हैं।
- कानून के क्रियान्वयन में सुस्ती और भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और निगरानी की कमी।
समाधान और सुझाव:
- ‘पोल्यूटर पेय’ सिद्धांत को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- औद्योगिक इकाइयों को आधुनिक अपशिष्ट शोधन तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- आम जनता की सहभागिता और पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- बोर्डों की स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
निष्कर्ष:
जल अधिनियम, 1974 देश में जल प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि इसकी सफलता कानून के साथ-साथ जन जागरूकता, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और न्यायिक सक्रियता पर भी निर्भर करती है। जल संसाधनों की रक्षा करना केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। स्वच्छ जल का अधिकार केवल कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि जीवन का आधार है जिसे संरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।