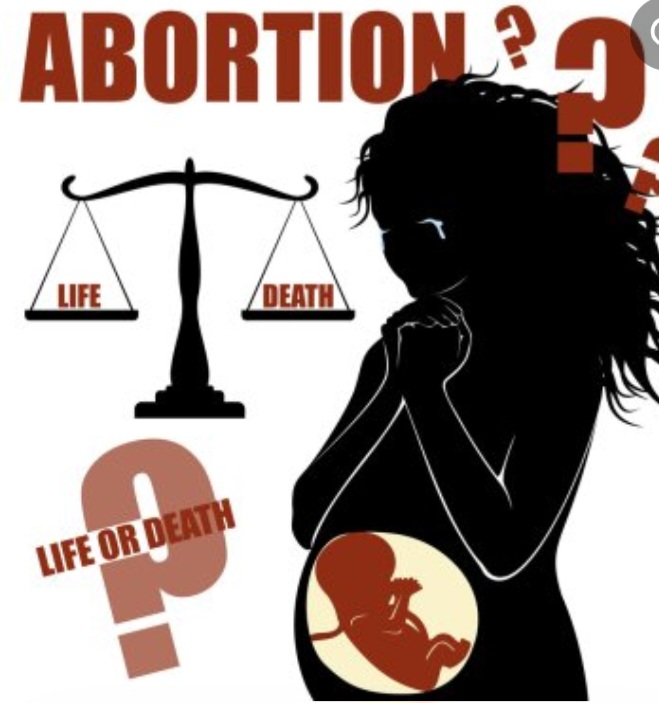गर्भपात पर सामाजिक कलंक और कानूनी समाधान
गर्भपात (Abortion) एक जटिल और संवेदनशील विषय है, जो न केवल महिला के प्रजनन स्वास्थ्य और उसके शारीरिक अधिकारों से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी अत्यधिक विवादास्पद रहा है। भारत में कानूनी रूप से गर्भपात को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (MTP Act) के तहत अनुमति दी गई है, परंतु वास्तविकता में महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण और पारंपरिक समाज में, गर्भपात कराने वाली महिलाओं को गंभीर सामाजिक कलंक (Social Stigma) का सामना करना पड़ता है। यह कलंक उन्हें न केवल मानसिक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि कानूनी और चिकित्सकीय सुविधाओं तक उनकी पहुँच को भी बाधित करता है। इस लेख में हम गर्भपात से जुड़े सामाजिक कलंक के स्वरूप, उसके कारण, प्रभाव और कानूनी समाधान पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
1. गर्भपात से जुड़ा सामाजिक कलंक – स्वरूप और कारण
गर्भपात को लेकर सामाजिक दृष्टिकोण मुख्यतः नैतिकता, धर्म, पारंपरिक संस्कृति और लिंग-भूमिकाओं की धारणाओं से निर्मित होता है। कई समाजों में यह माना जाता है कि गर्भपात “अप्राकृतिक” या “पाप” है, जिससे यह धारणा बनती है कि गर्भपात कराने वाली महिलाएँ नैतिक रूप से दोषी हैं।
मुख्य कारण –
- धार्मिक मान्यताएँ – अनेक धर्म जीवन को गर्भधारण के क्षण से ही पवित्र मानते हैं, और गर्भपात को हत्या के समान समझते हैं।
- पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ – महिला की भूमिका को ‘माँ’ के रूप में देखने वाली मानसिकता, गर्भपात को इस भूमिका से “विचलन” मानती है।
- अज्ञानता और गलत जानकारी – गर्भपात के कानूनी प्रावधानों और चिकित्सकीय सुरक्षा के बारे में जानकारी की कमी से भ्रांतियाँ फैलती हैं।
- लिंग आधारित भेदभाव – कुछ मामलों में यह धारणा भी बन जाती है कि गर्भपात कराने वाली महिलाएँ “चरित्रहीन” हैं, विशेषकर अविवाहित या किशोर माताओं के मामले में।
2. सामाजिक कलंक का प्रभाव
गर्भपात से जुड़े कलंक का असर महिलाओं के जीवन के कई पहलुओं पर पड़ता है—
- स्वास्थ्य पर प्रभाव – कलंक के डर से महिलाएँ गर्भपात के लिए सुरक्षित चिकित्सकीय केंद्रों की बजाय असुरक्षित और अवैध तरीकों का सहारा लेती हैं, जिससे उनकी जान को खतरा होता है।
- मानसिक स्वास्थ्य पर असर – अपराधबोध, शर्म और समाज के नकारात्मक व्यवहार से महिलाएँ अवसाद, चिंता और आघात (Trauma) से गुजरती हैं।
- कानूनी अधिकारों तक पहुँच में बाधा – कलंक और डर के कारण महिलाएँ MTP Act के तहत उपलब्ध कानूनी सुविधाओं का उपयोग करने से कतराती हैं।
- सामाजिक अलगाव – गर्भपात कराने वाली महिलाएँ परिवार, समुदाय या कार्यस्थल से अलग-थलग की जा सकती हैं।
3. भारतीय कानूनी प्रावधान – गर्भपात का अधिकार
भारत में MTP Act, 1971 और इसके संशोधन (2021) के तहत गर्भपात की अनुमति दी गई है—
- 20 सप्ताह तक गर्भपात के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक की अनुमति पर्याप्त है।
- 20 से 24 सप्ताह तक कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात किया जा सकता है, जैसे—बलात्कार, नाबालिग गर्भावस्था, भ्रूण में गंभीर असामान्यता।
- महिला की सहमति अनिवार्य है; अविवाहित और विवाहित दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं।
- गोपनीयता का अधिकार – चिकित्सक को महिला की पहचान गोपनीय रखनी होती है।
लेकिन समस्या यह है कि कानून होने के बावजूद सामाजिक कलंक के कारण कई महिलाएँ कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश करती हैं।
4. कलंक को कम करने के लिए कानूनी समाधान
- कानूनी जागरूकता अभियान – महिलाओं, परिवारों और समुदायों को MTP Act और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जागरूक करना।
- गोपनीयता और सुरक्षा की गारंटी – अस्पताल और क्लीनिक में महिला की पहचान और रिकॉर्ड को पूरी तरह गोपनीय रखना, ताकि कलंक और सामाजिक बहिष्कार का डर न रहे।
- भेदभाव विरोधी कानून का सख्त प्रवर्तन – गर्भपात कराने वाली महिलाओं के साथ भेदभाव, उत्पीड़न या हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई।
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता – कानूनी प्रावधानों में यह सुनिश्चित किया जाए कि गर्भपात कराने वाली महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श (Counseling) की सुविधा मिले।
- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सुरक्षित सेवाओं का विस्तार – सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित चिकित्सकों और सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना।
- सामुदायिक संवाद और शिक्षा – पंचायत, स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठनों के माध्यम से संवाद कर भ्रांतियाँ दूर करना।
5. अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और सीख
कई देशों ने गर्भपात के कलंक को कम करने के लिए प्रगतिशील नीतियाँ अपनाई हैं—
- कनाडा में गर्भपात पूरी तरह कानूनी और स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा है, जिससे कलंक काफी हद तक कम हुआ है।
- दक्षिण अफ्रीका ने Choice on Termination of Pregnancy Act के तहत न केवल गर्भपात को कानूनी किया, बल्कि सामुदायिक शिक्षा और गोपनीय सेवाओं पर जोर दिया।
- नेपाल में गर्भपात के अपराधीकरण को खत्म करने के साथ ही व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ उपलब्ध हुईं।
भारत इन उदाहरणों से सीख लेकर नीतियों को और अधिक सामाजिक संवेदनशील बना सकता है।
6. निष्कर्ष
गर्भपात केवल एक चिकित्सकीय या कानूनी विषय नहीं है, बल्कि यह महिला के स्वायत्तता, गरिमा और समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सामाजिक कलंक के कारण महिलाएँ न केवल अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं, बल्कि उनकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि कानून केवल कागज़ पर न रहकर जमीनी स्तर पर लागू हो, और साथ ही समाज में ऐसी सोच विकसित हो जो महिला के निर्णय का सम्मान करे।
सामाजिक कलंक को समाप्त करने के लिए कानूनी सुधार, जन-जागरूकता, गोपनीयता की सुरक्षा, और मानसिक स्वास्थ्य सहायता का एक साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तभी हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहाँ गर्भपात को अपराध या शर्म का कारण नहीं, बल्कि महिला का वैधानिक और मानवीय अधिकार माना जाए।