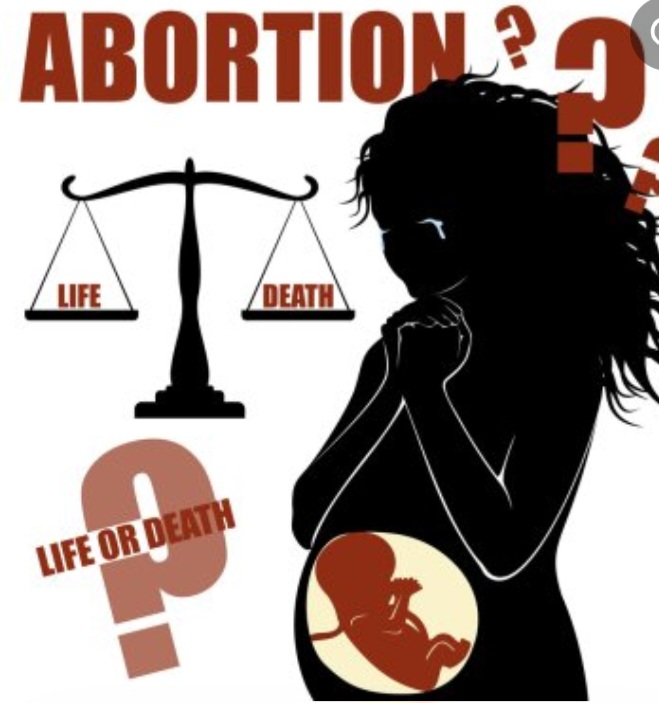शीर्षक:
“गर्भपात कानून में संशोधन: महिला अधिकार, स्वास्थ्य और न्याय की नई दिशा”
भूमिका
गर्भपात (Medical Termination of Pregnancy – MTP) से जुड़ा कानून भारत में 1971 में लागू हुआ था। उस समय यह कानून महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन समाज, चिकित्सा तकनीक, और महिलाओं की भूमिका में समय के साथ आए बदलावों ने इस कानून में संशोधन की आवश्यकता पैदा की।
वर्ष 2021 में भारत सरकार ने MTP (Amendment) Act, 2021 लागू किया, जिसने न केवल गर्भपात की समयसीमा बढ़ाई बल्कि महिला की गरिमा, प्रजनन अधिकार और गोपनीयता को भी अधिक महत्व दिया। इस संशोधन ने भारत को महिला प्रजनन अधिकारों के मामले में एक प्रगतिशील राष्ट्र की श्रेणी में ला खड़ा किया।
1. पुराने कानून की सीमाएँ
1971 के कानून में कुछ ऐसी शर्तें थीं जो महिलाओं के लिए गर्भपात को कठिन बना देती थीं—
- समयसीमा केवल 20 सप्ताह – इस सीमा के कारण कई बलात्कार पीड़िताएँ या भ्रूण में गंभीर विकृति पाए जाने वाली महिलाएँ गर्भपात नहीं करा पाती थीं।
- केवल विवाहित महिलाओं पर केंद्रित – अविवाहित या विधवा महिलाओं के लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान का अभाव था।
- डॉक्टर की अनुमति – 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर, और कई मामलों में दो डॉक्टरों की अनुमति आवश्यक थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्रिया जटिल हो जाती थी।
- गोपनीयता की कमी – कई बार महिला की पहचान उजागर हो जाती थी, जिससे सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता था।
2. 2021 संशोधन के मुख्य प्रावधान
2.1 गर्भपात की समयसीमा में वृद्धि
- पहले सीमा 20 सप्ताह थी, अब इसे 24 सप्ताह कर दिया गया।
- यह विशेष रूप से बलात्कार पीड़िताओं, नाबालिगों, और असाधारण परिस्थितियों वाली महिलाओं पर लागू होता है।
2.2 ‘विशेष श्रेणी’ की महिलाओं के लिए लचीलापन
- नाबालिग, बलात्कार पीड़िता, विधवा, तलाकशुदा, शारीरिक/मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाएँ, और आपदा या आपातकालीन परिस्थितियों में फँसी महिलाएँ।
2.3 डॉक्टर की राय में बदलाव
- 20 सप्ताह तक – एक पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर की राय पर्याप्त।
- 20 से 24 सप्ताह – दो पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों की राय आवश्यक।
2.4 मेडिकल बोर्ड का गठन
- 24 सप्ताह से अधिक गर्भावस्था के मामलों में गर्भपात के लिए राज्य या केंद्र सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की अनुमति आवश्यक।
- मेडिकल बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट और अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
2.5 गोपनीयता का अधिकार
- धारा 5A के तहत महिला की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य। उल्लंघन करने वाले पर दंड का प्रावधान।
3. महिला अधिकार और प्रजनन स्वतंत्रता
संशोधित कानून ने महिला के शारीरिक स्वायत्तता (Bodily Autonomy) और प्रजनन अधिकार (Reproductive Rights) को कानूनी मान्यता दी।
- महिला को यह अधिकार है कि वह अपने गर्भ को जारी रखे या समाप्त करे।
- यह अधिकार न्यायपालिका द्वारा भी कई मामलों में मौलिक अधिकार (Fundamental Right) के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है (जैसे Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration, 2009)।
4. न्यायिक दृष्टिकोण
- X v. Union of India (2022) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाएँ भी 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं।
- Murugan Nayakkar v. Union of India (2017) – 13 वर्षीय पीड़िता को 32 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भपात की अनुमति दी गई, क्योंकि यह उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था।
- Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) – निजता का अधिकार (Right to Privacy) मौलिक अधिकार घोषित, जो गर्भपात के संदर्भ में भी लागू है।
5. व्यावहारिक चुनौतियाँ
5.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा की कमी
- विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल बोर्ड की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है।
5.2 सामाजिक कलंक और दबाव
- अविवाहित महिलाओं को गर्भपात के लिए अधिक मानसिक दबाव और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
5.3 समयसीमा से जुड़ी देरी
- भ्रूण में विकृति अक्सर 20 सप्ताह के बाद सामने आती है, और तब तक मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
5.4 POCSO और नाबालिग मामले
- नाबालिग गर्भधारण के मामलों में पुलिस रिपोर्टिंग की अनिवार्यता से गोपनीयता प्रभावित होती है।
6. अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण
- कनाडा – कोई समयसीमा नहीं, निर्णय पूरी तरह महिला और डॉक्टर पर।
- यूके – 24 सप्ताह तक गर्भपात, विशेष परिस्थितियों में उसके बाद भी अनुमति।
- अमेरिका – Dobbs v. Jackson (2022) के बाद कई राज्यों में कड़ा प्रतिबंध, लेकिन कुछ राज्यों में महिला का पूर्ण अधिकार।
7. आगे की राह – सुधार के सुझाव
- गर्भपात के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट मान्यता।
- मेडिकल बोर्ड की त्वरित उपलब्धता – जिला स्तर पर बोर्ड गठन।
- गोपनीयता सुरक्षा तंत्र – अस्पताल और पुलिस में पहचान उजागर करने वालों पर कठोर दंड।
- ग्रामीण स्वास्थ्य ढाँचे में सुधार – गर्भपात की सुरक्षित और कानूनी सुविधा हर महिला तक पहुँचे।
- यौन शिक्षा और जागरूकता – ताकि महिलाएँ समय पर निर्णय ले सकें।
निष्कर्ष
गर्भपात कानून में 2021 का संशोधन महिलाओं के स्वास्थ्य, अधिकार और गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल महिला को अपनी प्रजनन पसंद चुनने का अधिकार देता है, बल्कि चिकित्सा तकनीक और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप भी है। फिर भी, प्रावधानों के क्रियान्वयन, जागरूकता, और सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि यह कानून वास्तव में महिलाओं को सशक्त बना सके।