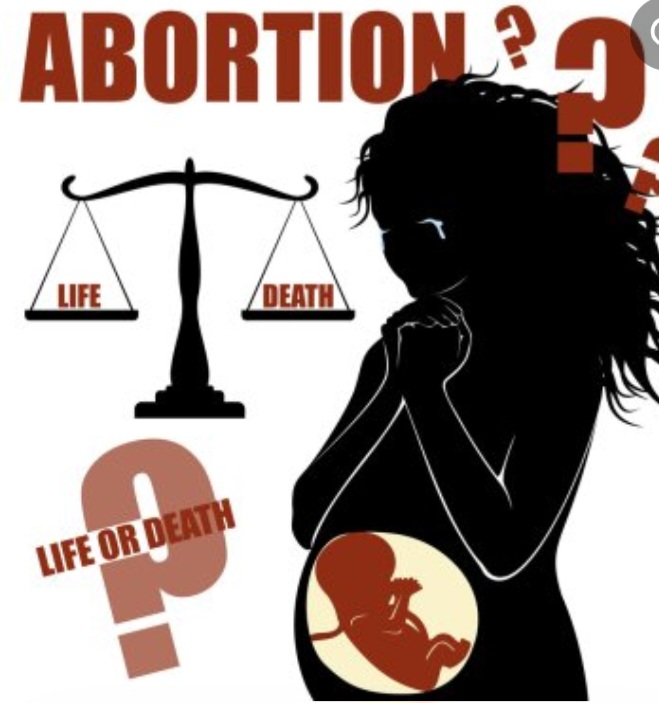गर्भपात कानून: एक कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण
(Abortion Law: A Legal and Ethical Perspective)
परिचय
गर्भपात या एबॉर्शन एक ऐसा संवेदनशील विषय है जो न केवल महिलाओं के शरीर और उनके प्रजनन अधिकारों से जुड़ा है, बल्कि इसका गहरा संबंध नैतिक, सामाजिक, धार्मिक और कानूनी विमर्श से भी है। भारत जैसे विविधता भरे देश में जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष जारी है, वहां गर्भपात का मुद्दा जटिल हो जाता है। यह लेख गर्भपात कानून की कानूनी और नैतिक दृष्टियों का विश्लेषण करता है, साथ ही महिलाओं के अधिकार, राज्य की भूमिका और सामाजिक सोच की भी पड़ताल करता है।
भारत में गर्भपात कानून का विकास
1. प्रारंभिक स्थिति
भारत में गर्भपात पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 312 से 316 के तहत अपराध माना गया था। गर्भपात को ‘मिसकैरेज’ कहा गया और यह संज्ञेय, गैर-जमानती अपराध था। इसका अपवाद केवल तब था जब माँ की जान को खतरा हो।
2. चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 – MTP Act)
1971 में भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चिकित्सा गर्भपात अधिनियम पारित किया, जिससे कुछ परिस्थितियों में गर्भपात को वैधता मिली। इसके अनुसार:
- गर्भपात 20 सप्ताह तक किया जा सकता था, यदि:
- माँ की जान को खतरा हो,
- भ्रूण में कोई गंभीर असामान्यता हो,
- गर्भ बलात्कार का परिणाम हो,
- या अविवाहित/अवांछित गर्भधारण हो।
3. MTP संशोधन अधिनियम, 2021
समाज में बदलती संवेदनाओं और महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 में MTP अधिनियम में संशोधन किया गया:
- गर्भावधि सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई, कुछ विशेष वर्गों के लिए (बलात्कार पीड़िता, नाबालिग, आदि)।
- भ्रूण की गंभीर असामान्यता के मामलों में मेडिकल बोर्ड की अनुमति से 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात संभव।
- विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव समाप्त किया गया।
कानूनी दृष्टिकोण से गर्भपात
1. संविधानिक परिप्रेक्ष्य
भारतीय संविधान में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) महिलाओं को अपनी शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration (2009) केस में कहा कि महिला को यह तय करने का अधिकार है कि वह माँ बने या नहीं।
2. न्यायिक दृष्टांत
- X v. Union of India (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने 24 सप्ताह की सीमा पार होने के बाद भी गर्भपात की अनुमति दी, जब भ्रूण में गंभीर असामान्यता पाई गई।
- 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट किया गया कि अविवाहित महिलाएं भी विवाहितों की तरह गर्भपात का अधिकार रखती हैं।
3. सीमाएँ और विवाद
- मेडिकल बोर्ड की मंजूरी में देरी से महिलाओं की हालत बिगड़ सकती है।
- 24 सप्ताह की सीमा के बाद की अनुमति एक विशेष प्रक्रिया से जुड़ी है, जो ग्रामीण इलाकों में असंभव सी हो जाती है।
नैतिक दृष्टिकोण से गर्भपात
1. भ्रूण का जीवन बनाम महिला का अधिकार
यह बहस सदियों पुरानी है — क्या भ्रूण को एक “जीवित व्यक्ति” माना जाए, जिसका जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना महिला का?
- प्रो-लाइफ दृष्टिकोण कहता है कि गर्भधारण के क्षण से भ्रूण को जीवन का अधिकार मिल जाना चाहिए।
- प्रो-चॉइस दृष्टिकोण कहता है कि महिला को अपने शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जिसमें गर्भपात का अधिकार भी शामिल है।
2. धार्मिक और सांस्कृतिक विचार
- हिंदू धर्म आमतौर पर गर्भपात को अधर्म मानता है, जब तक कि यह माँ के जीवन के लिए आवश्यक न हो।
- इस्लाम गर्भपात को सीमित परिस्थितियों में वैध मानता है (आमतौर पर 120 दिन से पहले)।
- ईसाई धर्म भ्रूण को जन्म से पहले ही जीव मानता है और गर्भपात को पाप मानता है।
3. सामाजिक नैतिकता और लिंग आधारित भेदभाव
भारत में लिंग चयन के कारण भ्रूण हत्या (female foeticide) एक गंभीर समस्या रही है। इससे सामाजिक असंतुलन और लिंग अनुपात में गिरावट आई। यही कारण है कि Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, 1994 के तहत लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाया गया।
गर्भपात के सामाजिक आयाम
1. ग्रामीण और शहरी विभाजन
शहरी क्षेत्रों में कानूनी जानकारी और मेडिकल सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षित गर्भपात की घटनाएं अधिक हैं। इसके चलते मातृ मृत्यु दर बढ़ती है।
2. सामाजिक कलंक
गर्भपात विशेष रूप से अविवाहित महिलाओं के लिए सामाजिक कलंक का कारण बनता है। इससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक आघात भी पहुंचता है।
3. पुरुष भागीदारी की कमी
बहुत बार पुरुष गर्भपात के फैसले से दूर रहते हैं या इसका समर्थन नहीं करते, जिससे महिला पर अकेले निर्णय का दबाव आता है।
वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ
1. सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच
- भारत में प्रति वर्ष हजारों महिलाएं असुरक्षित गर्भपात के कारण जान गंवाती हैं।
- कानूनी ढांचे के बावजूद प्रशिक्षित चिकित्सकों और उपकरणों की कमी एक गंभीर बाधा है।
2. कानून की व्याख्या में अस्पष्टता
कई बार डॉक्टर और अस्पताल कानूनी दायरे के डर से गर्भपात करने से इंकार कर देते हैं, जिससे महिला को अवैध या असुरक्षित विकल्प चुनना पड़ता है।
3. डिजिटल गोपनीयता और डेटा सुरक्षा
टेलीमेडिसिन और डिजिटल परामर्श के बढ़ते चलन के साथ महिलाओं के मेडिकल डेटा की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है।
समाधान और सुझाव
- कानूनी जागरूकता – महिलाओं और चिकित्सकों दोनों को MTP Act की जानकारी दी जानी चाहिए, विशेष रूप से संशोधित कानून के संदर्भ में।
- सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं – ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित गर्भपात की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए।
- मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान – गर्भपात के बाद महिलाओं को काउंसलिंग और मानसिक सहायता मिलनी चाहिए।
- पितृत्व और नैतिक शिक्षा – पुरुषों को भी प्रजनन स्वास्थ्य और निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
- गोपनीयता संरक्षण – डिजिटल डेटा के उपयोग में महिलाओं की निजता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
निष्कर्ष
गर्भपात कानून न केवल एक कानूनी मुद्दा है बल्कि यह नैतिकता, स्वास्थ्य, मानवाधिकार और सामाजिक संरचना का सम्मिलित विषय है। भारत ने MTP अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को कुछ हद तक अधिकार तो प्रदान किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी प्रभावशीलता अभी भी चुनौतियों से घिरी है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज, कानून और चिकित्सा प्रणाली मिलकर महिलाओं को न केवल गर्भपात का कानूनी अधिकार दें, बल्कि एक सुरक्षित, सुलभ और संवेदनशील वातावरण भी प्रदान करें।