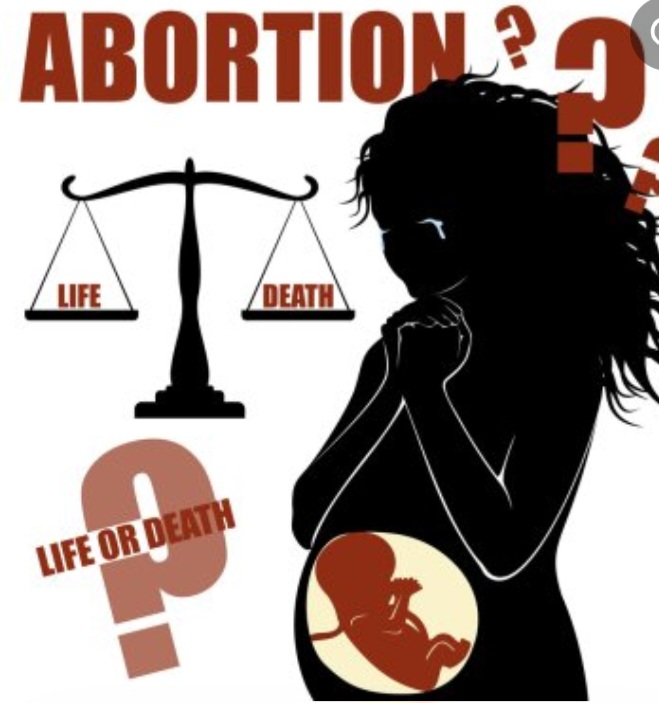क्या भारत को गर्भपात के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करना चाहिए?
प्रस्तावना
गर्भपात का मुद्दा केवल चिकित्सा या व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की स्वायत्तता, गरिमा, गोपनीयता और समानता से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत में गर्भपात को Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (MTP Act) के तहत नियंत्रित किया जाता है, जिसमें 2021 में संशोधन के बाद कई प्रगतिशील बदलाव किए गए हैं। इसके बावजूद, गर्भपात का अधिकार अभी भी एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत को इसे संविधान के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा देना चाहिए, ताकि यह महिला के अपने शरीर और जीवन पर नियंत्रण के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बन सके।
1. गर्भपात का मौजूदा कानूनी ढांचा
भारत में गर्भपात केवल कुछ निर्धारित परिस्थितियों में ही वैध है—
- गर्भावस्था 20 से 24 सप्ताह तक (विशेष मामलों में) चिकित्सकीय कारणों से।
- महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा होने पर।
- भ्रूण में गंभीर असामान्यता होने पर।
- बलात्कार या यौन शोषण के मामलों में।
हालाँकि, कानून में संशोधन के बावजूद, यह अधिकार “शर्तों पर आधारित” है, न कि महिला की स्वतंत्र पसंद पर।
2. मौलिक अधिकार का अर्थ और महत्व
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, नागरिकों को राज्य के हस्तक्षेप से बचाने और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। यदि गर्भपात का अधिकार मौलिक अधिकार बनता है, तो—
- इसे अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सकता है।
- राज्य की नीतियाँ और कानून महिला की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा करने के लिए बाध्य होंगे।
- किसी भी प्रकार के भेदभाव या अत्यधिक कानूनी अड़चनों को संवैधानिक रूप से चुनौती दी जा सकेगी।
3. न्यायिक दृष्टिकोण
भारतीय न्यायपालिका ने कई बार गर्भपात और प्रजनन अधिकारों को Article 21 से जोड़ा है—
- Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration (2009): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रजनन विकल्प का अधिकार महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है।
- X v. NCT of Delhi (2022): कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं के लिए भी 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी और इसे समानता व गरिमा के अधिकार से जोड़ा।
इसके बावजूद, ये निर्णय कानूनी ढांचे के भीतर सीमित हैं और सभी परिस्थितियों में स्वतंत्र गर्भपात का अधिकार नहीं देते।
4. गर्भपात को मौलिक अधिकार बनाने के पक्ष में तर्क
(i) शारीरिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत गरिमा
महिला को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। गर्भधारण और प्रसव एक गहरा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अनुभव है, जिसे जबरन थोपना अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन है।
(ii) स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा
गर्भपात पर कठोर प्रतिबंध या देरी से अनुमति देने के कारण कई महिलाएं असुरक्षित और गैर-कानूनी तरीकों का सहारा लेती हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर बढ़ती है। WHO के अनुसार, सुरक्षित गर्भपात की उपलब्धता महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
(iii) समानता का अधिकार
शहरी और शिक्षित महिलाएं अपेक्षाकृत आसानी से कानूनी रास्ते अपना सकती हैं, जबकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं सामाजिक कलंक और कानूनी पेचीदगियों में फंस जाती हैं। मौलिक अधिकार का दर्जा इन असमानताओं को कम कर सकता है।
(iv) गोपनीयता का संवैधानिक संरक्षण
Puttaswamy v. Union of India (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। प्रजनन निर्णय, जिसमें गर्भपात भी शामिल है, महिला की निजी स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है।
5. गर्भपात को मौलिक अधिकार बनाने के खिलाफ तर्क
(i) नैतिक और धार्मिक विरोध
कुछ लोग मानते हैं कि जीवन गर्भाधान से ही शुरू होता है और भ्रूण के जीवन का भी संवैधानिक संरक्षण होना चाहिए। ऐसे में गर्भपात को मौलिक अधिकार बनाना भ्रूण के जीवन के अधिकार से टकरा सकता है।
(ii) दुरुपयोग की संभावना
बिना चिकित्सकीय आधार के गर्भपात की स्वतंत्रता, भ्रूण-लिंग चयन जैसे अपराधों को बढ़ावा दे सकती है, खासकर भारत जैसे देशों में जहां लिंगानुपात पहले से ही असंतुलित है।
(iii) चिकित्सकीय दृष्टिकोण की अनदेखी
कुछ चिकित्सक मानते हैं कि गर्भपात का निर्णय केवल महिला की इच्छा पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा मानकों पर आधारित होना चाहिए।
6. अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
- अमेरिका: Roe v. Wade (1973) ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार माना, लेकिन Dobbs v. Jackson (2022) में इसे उलट दिया गया।
- कनाडा: गर्भपात पूरी तरह से अपराधमुक्त है और इसे महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाता है।
- आयरलैंड: 2018 में जनमत संग्रह के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध हटाया गया।
इन उदाहरणों से पता चलता है कि गर्भपात के अधिकार का संवैधानिक दर्जा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
7. व्यवहारिक चुनौतियाँ
गर्भपात को मौलिक अधिकार बनाने के बाद भी यह तभी प्रभावी होगा जब—
- ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।
- डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को कानूनी प्रावधानों और महिला के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।
- लिंगानुपात सुधारने के लिए PCPNDT Act (लिंग चयन निषेध अधिनियम) का सख्ती से पालन हो।
8. संभावित कानूनी समाधान
- संवैधानिक संशोधन: अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से प्रजनन अधिकार और गर्भपात का अधिकार जोड़ा जा सकता है।
- गाइडलाइन्स का सरलीकरण: MTP Act में महिला की स्वायत्तता को प्राथमिक आधार बनाया जाए, न कि केवल चिकित्सकीय राय को।
- सुरक्षा और गोपनीयता की गारंटी: कानूनी रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि गर्भपात का निर्णय और प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय हो।
- जागरूकता अभियान: महिलाओं और समाज को गर्भपात के कानूनी अधिकारों और सुरक्षित प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करना।
9. निष्कर्ष
गर्भपात को मौलिक अधिकार बनाने का प्रश्न केवल कानूनी सुधार का नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता और समानता की पहचान का प्रश्न है। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जीवन देना है, और यह तभी संभव है जब महिला को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण मिले। हालांकि, इसके साथ-साथ भ्रूण-लिंग चयन और अन्य संभावित दुरुपयोग पर सख्त निगरानी आवश्यक है।
अतः, भारत को गर्भपात के अधिकार को संविधानिक स्तर पर स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देनी चाहिए, ताकि यह केवल कानून की उदारता पर नहीं, बल्कि महिला के अटल संवैधानिक अधिकार पर आधारित हो।