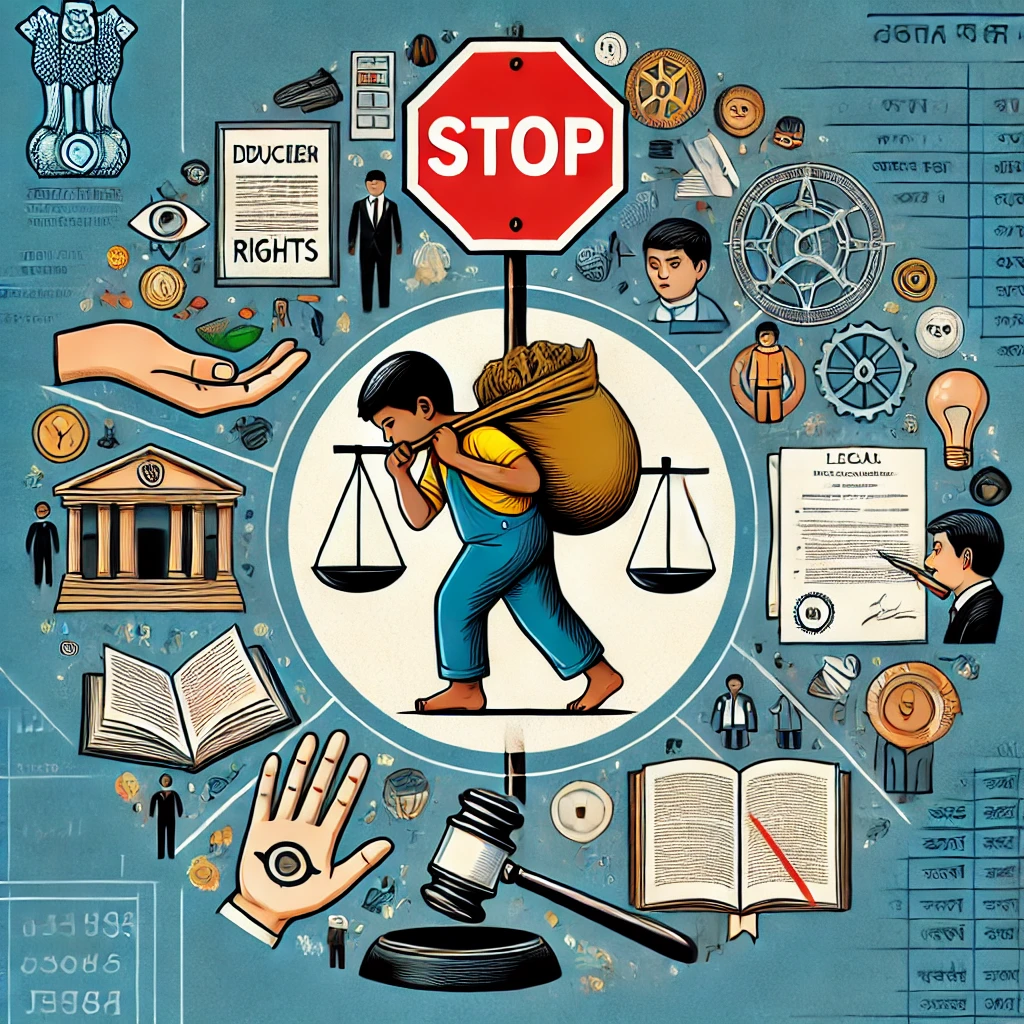किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015: बाल न्याय प्रणाली का एक व्यापक स्वरूप
(Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015: A Comprehensive Framework of Juvenile Justice System)
प्रस्तावना:
भारत में बच्चों के संरक्षण और उनके अपराधों से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पहले यह जिम्मेदारी किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत निभाई जाती थी, लेकिन निर्भया कांड (2012) के बाद देश में किशोरों द्वारा गंभीर अपराधों में संलिप्तता को देखते हुए एक नए, सख्त और व्यावहारिक कानून की जरूरत महसूस की गई। इसी पृष्ठभूमि में किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 अस्तित्व में आया, जिसने किशोर अपराधों के प्रति दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित किया।
अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:
- किशोर की परिभाषा: अधिनियम के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति ‘किशोर’ (Juvenile) या ‘बालक’ (Child) की श्रेणी में आता है। यह परिभाषा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) के अनुरूप है।
- गंभीर अपराधों के लिए अपवाद: अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि 16 से 18 वर्ष की आयु का किशोर कोई गंभीर या जघन्य अपराध (heinous offence) करता है, तो किशोर न्याय बोर्ड यह तय करेगा कि उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए या नहीं।
- तीन प्रकार की अपराध श्रेणियाँ: अधिनियम अपराधों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:
- छोटे अपराध (Petty offences)
- गंभीर अपराध (Serious offences)
- जघन्य अपराध (Heinous offences)
- बाल संरक्षण की व्यवस्था: अधिनियम उन बच्चों के लिए भी संरचना प्रदान करता है जो अपराध नहीं करते लेकिन लावारिस, अनाथ या शोषण के शिकार होते हैं। ऐसे बच्चों को “देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक” (Children in Need of Care and Protection) की श्रेणी में रखा जाता है।
संस्थागत ढाँचा:
- किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board – JJB): यह बोर्ड उन किशोरों के मामलों की सुनवाई करता है जिन्होंने कोई अपराध किया हो। इसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें से कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है।
- बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee – CWC): इस समिति का कार्य देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना होता है।
- बालगृह, निरीक्षण गृह और विशेष गृह: इन संस्थानों में विभिन्न प्रकार के बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार रखा जाता है — जैसे कि निराश्रित, अपराधी, पीड़ित या पुनर्वास की प्रतीक्षा में।
दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया:
अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण (Adoption) की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority – CARA) की भूमिका को वैधानिक मान्यता दी गई है। इस प्राधिकरण के माध्यम से दत्तक ग्रहण की पारदर्शिता और वैधानिकता सुनिश्चित की जाती है।
बाल अधिकारों का संरक्षण:
यह अधिनियम न केवल किशोर अपराधियों से संबंधित है, बल्कि उन बच्चों के हितों की भी रक्षा करता है जो किसी न किसी रूप में उपेक्षा, शोषण या अपराध के शिकार हुए हैं। इनमें बाल विवाह, बाल श्रम, तस्करी, यौन शोषण आदि के पीड़ित शामिल हैं।
विशेष प्रावधान:
- बच्चों को हिरासत में रखने की अंतिम व्यवस्था सुधार गृहों में ही की जाती है, जेलों में नहीं।
- किशोर को वयस्क अपराधी घोषित करने से पहले उसकी मानसिक परिपक्वता, अपराध की प्रकृति और उसके इरादों का आकलन किया जाता है।
- पुनर्वास और पुनर्संवेशन (Rehabilitation and Reintegration) पर विशेष ध्यान दिया गया है।
आलोचना और बहस:
अधिनियम के अंतर्गत किशोरों को वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाए जाने की संभावना को लेकर व्यापक बहस हुई है। आलोचकों का मानना है कि इससे किशोरों के सुधारात्मक पहलू की उपेक्षा हो सकती है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि यह प्रावधान जघन्य अपराधों को रोकने और न्याय की भावना को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
न्यायपालिका की भूमिका:
भारत के न्यायालयों ने समय-समय पर इस अधिनियम की व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के अधिकारों और प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए हैं। ‘एक्स बनाम भारत संघ’ जैसे मामलों में यह स्पष्ट किया गया कि किशोर की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन वैज्ञानिक विधियों से होना चाहिए।
निष्कर्ष:
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एक आधुनिक, संतुलित और बालहितैषी कानून है जो बच्चों के संरक्षण और अपराधियों के सुधार दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अधिनियम भारत की न्याय प्रणाली को मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण से सशक्त बनाता है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में अब भी कई चुनौतियाँ हैं — जैसे संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण की आवश्यकता और सामाजिक जागरूकता की कमी — परंतु यह कानून बाल अधिकारों और न्याय के क्षेत्र में एक मजबूत आधारशिला प्रस्तुत करता है।