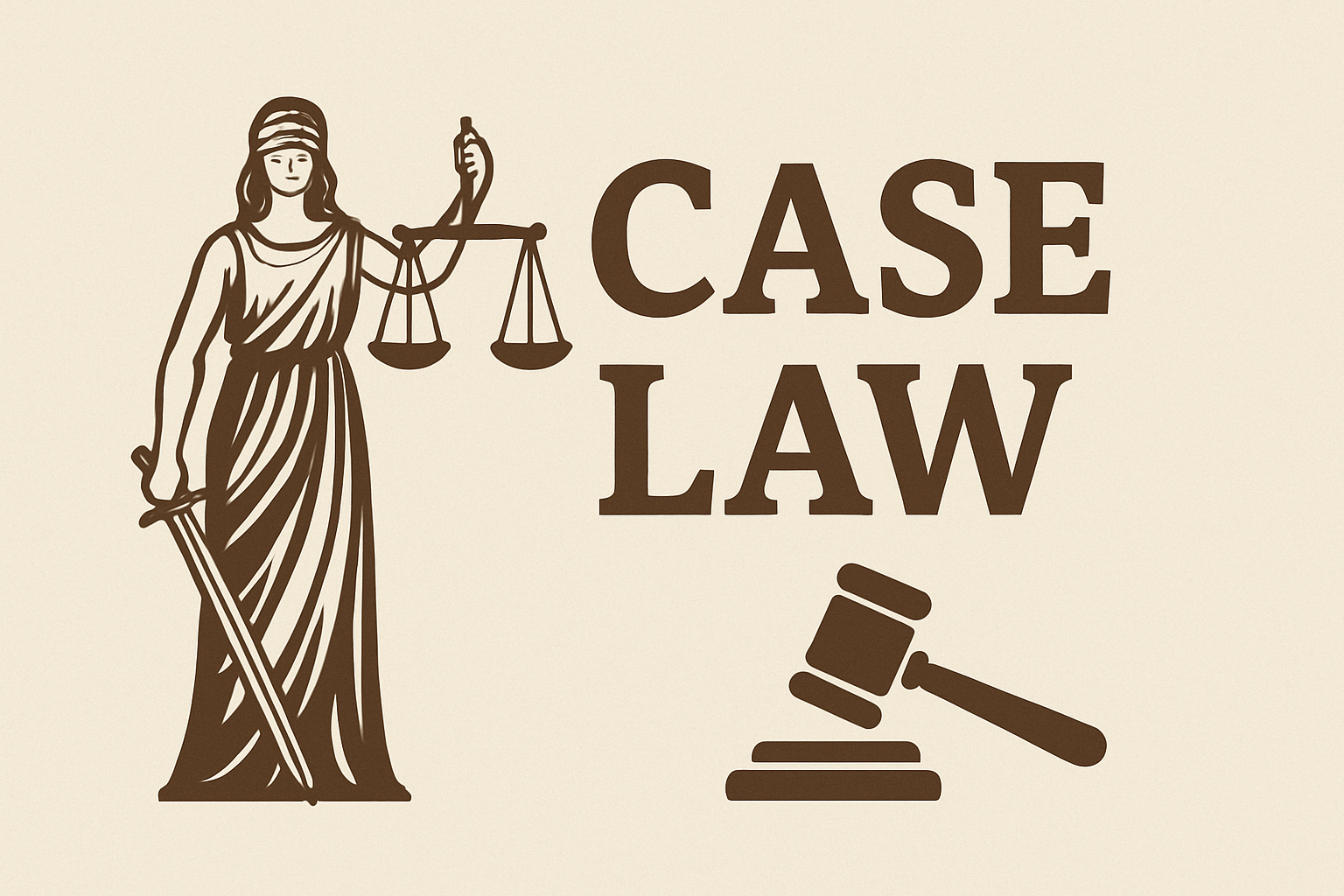“कंवर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (AIR 1954 SC 207): पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकृति को सर्वोच्च न्यायालय ने ठहराया अमान्य”
प्रस्तावना
भारतीय दंड प्रक्रिया में स्वीकृति (Confession) को एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है। परंतु यह तभी स्वीकार्य होती है जब वह पूरी तरह स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव या भय के की गई हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24, 25 और 26 इस सिद्धांत की रक्षा करती हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि यदि स्वीकृति किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष या पुलिस हिरासत में दी गई है, तो वह न्यायालय में प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कंवर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (AIR 1954 SC 207) के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसने न्यायिक निष्पक्षता और अभियुक्त के मौलिक अधिकारों की रक्षा को मजबूत किया।
मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case)
कंवर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान उसने पुलिस अधिकारियों के समक्ष एक कथित स्वीकृति दी थी जिसमें अपराध स्वीकार करने का उल्लेख था। पुलिस ने इस स्वीकृति को आधार बनाकर अभियोजन चलाया और इसे साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। निचली अदालत ने भी इस स्वीकृति को प्रमाण मानते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया।
हालाँकि, कंवर सिंह ने उच्च न्यायालय और तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में यह अपील की कि उसकी स्वीकृति दबाव और पुलिस हिरासत के दौरान भय के वातावरण में दी गई थी। अतः यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।
मुख्य विधिक प्रश्न (Legal Issue Involved)
मुख्य प्रश्न यह था कि —
क्या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई स्वीकृति को न्यायालय में प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है?
या क्या ऐसी स्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अमान्य ठहराई जाएगी?
संबंधित विधिक प्रावधान (Relevant Legal Provisions)
- धारा 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 – यदि स्वीकृति किसी भय, दबाव, प्रलोभन या वादे के कारण की गई हो, तो वह न्यायालय में अमान्य मानी जाएगी।
- धारा 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 – “किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकृति को किसी अपराध के अभियोजन में प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।”
- धारा 26, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 – यदि अभियुक्त पुलिस हिरासत में है, तो उसकी कोई भी स्वीकृति तब तक मान्य नहीं होगी जब तक वह मजिस्ट्रेट के समक्ष न दी गई हो।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (Supreme Court’s Decision)
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि —
“किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई कोई भी स्वीकृति न्यायिक रूप से अस्वीकार्य है, चाहे वह सत्य हो या झूठी।”
न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को पुलिस के दबाव या प्रताड़ना के भय से झूठी स्वीकृति देने के लिए मजबूर न किया जाए। इसलिए, भले ही अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया हो, यदि वह स्वीकारोक्ति पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई है, तो वह कानूनी रूप से साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि केवल वह स्वीकृति मान्य होगी जो किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक अधिकारी — अर्थात् मजिस्ट्रेट — के समक्ष दी गई हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्वीकृति स्वेच्छा से और बिना किसी बाहरी प्रभाव के की गई है।
न्यायालय के तर्क (Court’s Reasoning)
- मानवाधिकार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की रक्षा:
पुलिस के समक्ष दी गई स्वीकृति को अस्वीकार करना अभियुक्त के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। - दबाव और भय की संभावना:
पुलिस हिरासत में व्यक्ति मनोवैज्ञानिक दबाव में होता है, जिससे सत्यता का निर्धारण कठिन हो जाता है। - निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया का संरक्षण:
न्यायालय ने कहा कि किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों पर निर्भर करती है। - विधायी उद्देश्य का सम्मान:
साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 का उद्देश्य पुलिस अत्याचार को रोकना और अभियुक्त को झूठे अपराध-स्वीकार से बचाना है।
मामले का प्रभाव (Impact of the Judgment)
इस निर्णय ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक मजबूत मिसाल स्थापित की। इसके बाद से यह सिद्धांत दृढ़ हुआ कि —
- पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई स्वीकृति कभी भी साक्ष्य नहीं बन सकती।
- केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई स्वेच्छिक स्वीकृति ही मान्य है।
- इस निर्णय ने पुलिस की जांच प्रणाली पर नियंत्रण और पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
अन्य संबंधित निर्णय (Related Judgments)
- प्यारे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (AIR 1962 SC 690): न्यायालय ने कहा कि स्वीकृति तभी मान्य होगी जब वह स्वेच्छा से और बिना भय या प्रलोभन के की गई हो।
- राजा राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1970 CriLJ 960): पुलिस हिरासत में दी गई स्वीकृति को अस्वीकार्य ठहराया गया।
- केदारनाथ बनाम दिल्ली प्रशासन (AIR 1953 SC 18): पुलिस हिरासत में स्वीकारोक्ति की वैधता पर समान विचार रखे गए।
विचार और विश्लेषण (Critical Analysis)
यह निर्णय न केवल साक्ष्य अधिनियम की भावना की रक्षा करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल पुलिस के बयानों या दबाव में दिए गए कथनों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
इससे भारतीय न्याय प्रणाली में “presumption of innocence” का सिद्धांत और भी सशक्त हुआ — अर्थात् जब तक अपराध सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा।
इसके अतिरिक्त, इस निर्णय ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया का विश्वास जनता के बीच बना रहे।
निष्कर्ष (Conclusion)
कंवर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (AIR 1954 SC 207) का निर्णय भारतीय साक्ष्य कानून में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई कोई भी स्वीकृति न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। यह निर्णय मानवाधिकारों की सुरक्षा, प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह मामला हमें याद दिलाता है कि न्याय केवल अपराध के विरुद्ध नहीं, बल्कि व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए भी होता है। पुलिस द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण और संविधान-सम्मत तरीके से किया जाना चाहिए ताकि कानून का शासन (Rule of Law) समाज में दृढ़ बना रहे।