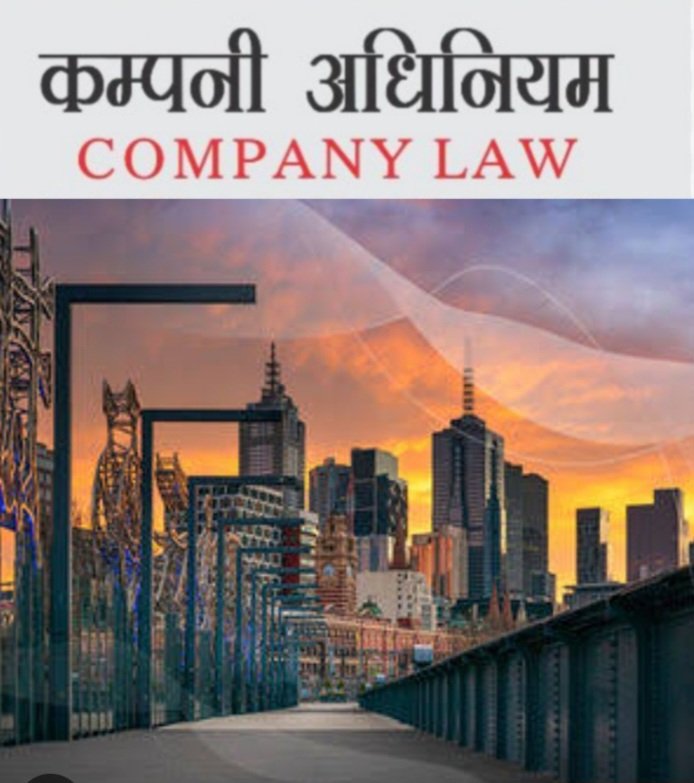प्रश्न 1. कंपनी की परिभाषा एवं विशेषताएँ (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार)
परिभाषा
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) के अनुसार,
“कंपनी वह कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person) है, जिसे विधि द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसका एक पृथक अस्तित्व होता है, जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है और जिसकी अपनी एक सार्वमुद्रा (Common Seal) होती है।”
ब्रिटिश न्यायालय ने Salomon v. Salomon & Co. Ltd. (1897) मामले में स्पष्ट किया कि कंपनी एक पृथक कानूनी इकाई (Separate Legal Entity) होती है, जो अपने सदस्यों से भिन्न होती है।
कंपनी की विशेषताएँ
- कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (Artificial Legal Person)
कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, जिसे कानून द्वारा निर्मित किया जाता है। यह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अधिकार और कर्तव्य रखती है, लेकिन इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। - पृथक कानूनी अस्तित्व (Separate Legal Entity)
कंपनी के शेयरधारक और कंपनी दो अलग-अलग इकाइयाँ होती हैं। किसी सदस्य की व्यक्तिगत देनदारियाँ कंपनी को प्रभावित नहीं करतीं। - अविच्छिन्न उत्तराधिकार (Perpetual Succession)
कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन या हटने से प्रभावित नहीं होता। यह तब तक बनी रहती है जब तक इसे कानून के तहत भंग नहीं किया जाता। - सीमित दायित्व (Limited Liability)
कंपनी के शेयरधारकों की देनदारी केवल उनके निवेश तक सीमित होती है। यदि कंपनी को हानि होती है, तो इसके निदेशक या सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते। - सार्वमुद्रा (Common Seal)
पहले, कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती थी, जो उसके आधिकारिक दस्तावेजों और अनुबंधों पर लगाई जाती थी। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 में इसे अनिवार्य नहीं रखा गया है। - संविदा करने की क्षमता (Capacity to Contract)
कंपनी एक स्वतंत्र इकाई होने के कारण अपने नाम से अनुबंध कर सकती है और अपने हितों की रक्षा के लिए न्यायालय में मुकदमा कर सकती है। - संपत्ति का स्वामित्व (Ownership of Property)
कंपनी स्वयं अपनी संपत्तियों की मालिक होती है, न कि उसके शेयरधारक। इसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से कंपनी की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते। - हस्तांतरणीयता (Transferability of Shares)
एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयरों का स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण किया जा सकता है, जिससे पूंजी का प्रवाह बना रहता है। - कानूनी नियंत्रण (Statutory Regulation)
कंपनी को अपने कार्यों का संचालन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार करना होता है और विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। - मुकदमा करने और मुकदमा झेलने की क्षमता (Right to Sue and Be Sued)
कंपनी अपने नाम पर किसी अन्य व्यक्ति पर मुकदमा कर सकती है और किसी भी कानूनी विवाद में उसे भी मुकदमा झेलना पड़ सकता है।
निष्कर्ष
कंपनी एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति है, जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है। इसके निर्माण, संचालन और समाप्ति की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों द्वारा निर्धारित होती है। इसकी विशेषताएँ इसे अन्य व्यावसायिक संगठनों, जैसे एकल स्वामित्व (Sole Proprietorship) और साझेदारी (Partnership) से अलग बनाती हैं।
प्रश्न 2. “कम्पनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व, अनिच्छित उत्तराधिकार एवं सार्वमुद्रा होती है।’ इस कथन को समझाइये तथा कम्पनी की आधारभूत विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
यह कथन कंपनी की प्रकृति और उसकी कानूनी पहचान को स्पष्ट करता है। इसे निम्नलिखित भागों में समझा जा सकता है—
1. कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person)
कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून द्वारा निर्मित किया जाता है। यह मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेती, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अस्तित्व में आती है। हालांकि यह स्वयं कार्य नहीं कर सकती, बल्कि इसके निदेशक और अधिकारी इसके लिए कार्य करते हैं।
2. पृथक अस्तित्व (Separate Legal Entity)
कंपनी का अस्तित्व इसके मालिकों (शेयरधारकों) से अलग होता है। अर्थात, कंपनी स्वयं अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, मुकदमा कर सकती है और उस पर मुकदमा किया जा सकता है। शेयरधारकों की मृत्यु या परिवर्तन का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
3. अनिच्छित उत्तराधिकार (Perpetual Succession)
कंपनी का जीवनकाल असीमित होता है। इसके सदस्य बदल सकते हैं, लेकिन कंपनी तब तक चलती रहती है जब तक कि इसे कानूनी रूप से समाप्त नहीं किया जाता।
4. सार्वमुद्रा (Common Seal)
कंपनी की अपनी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती, इसलिए वह अपनी स्वीकृति और निर्णयों को प्रमाणित करने के लिए एक सार्वमुद्रा (कॉमन सील) का उपयोग करती है। यह सील कंपनी के अधिकृत दस्तावेजों पर लगाई जाती है।
कंपनी की आधारभूत विशेषताएँ
- कानूनी अस्तित्व – कंपनी को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और यह एक स्वतंत्र इकाई होती है।
- सीमित देयता – शेयरधारकों की देनदारी उनके निवेश तक सीमित होती है।
- पृथक स्वामित्व और प्रबंधन – कंपनी के मालिक (शेयरधारक) और प्रबंधन (निदेशक मंडल) अलग-अलग होते हैं।
- अनिश्चितकालीन जीवनकाल – यह शेयरधारकों की मृत्यु या निकासी से प्रभावित नहीं होती।
- संविदा करने की शक्ति – कंपनी स्वयं के नाम पर अनुबंध कर सकती है।
- मुकदमा करने और मुकदमा झेलने की क्षमता – कंपनी अपने नाम से न्यायालय में मुकदमा कर सकती है और उस पर भी मुकदमा किया जा सकता है।
निष्कर्ष
कंपनी एक कृत्रिम कानूनी इकाई है, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यह स्थायी होती है और इसके शेयरधारकों के जीवन पर निर्भर नहीं करती। इसके सभी कार्य कानून के अनुसार होते हैं, और यह अपनी सार्वमुद्रा का उपयोग करके निर्णयों को प्रमाणित करती है।
प्रश्न 3. “एक कम्पनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है।’ इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा कम्पनी की आधारभूत विशेषताओं को वताइए।
परिचय
कंपनी एक कृत्रिम (Artificial) व्यक्ति है जिसे कानून द्वारा निर्मित किया जाता है। यह एक स्वतंत्र कानूनी इकाई (Legal Entity) होती है, जिसका अस्तित्व इसके मालिकों (शेयरधारकों) से अलग होता है। इसका संचालन निदेशक मंडल (Board of Directors) द्वारा किया जाता है और यह अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, अनुबंध कर सकती है, तथा न्यायालय में मुकदमा कर सकती है।
“एक कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है” – इस कथन की व्याख्या
1. कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person)
कंपनी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन यह कोई प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होती। यह स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती, बल्कि इसके निदेशक और अधिकारी इसके लिए कार्य करते हैं।
2. राजनियम द्वारा निर्मित (Created by Law)
कंपनी की स्थापना कानून द्वारा की जाती है। इसका निर्माण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकरण (Registration) द्वारा किया जाता है। यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक कानूनी इकाई होती है।
3. पृथक कानूनी अस्तित्व (Separate Legal Entity)
एक कंपनी का अस्तित्व इसके मालिकों (शेयरधारकों) से अलग होता है। इसका मतलब है कि यदि कंपनी पर कोई कर्ज है या कोई कानूनी मामला है, तो इसके लिए व्यक्तिगत रूप से शेयरधारक जिम्मेदार नहीं होते।
4. स्थायी उत्तराधिकार (Perpetual Succession)
कंपनी की निरंतरता बनी रहती है, चाहे इसके शेयरधारकों या निदेशकों की मृत्यु हो जाए या वे बदल जाएं। जब तक इसे कानूनी रूप से भंग नहीं किया जाता, यह बनी रहती है।
कंपनी की आधारभूत विशेषताएँ
- स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व (Independent Legal Entity) – कंपनी का अपना अलग कानूनी अस्तित्व होता है, जो इसके सदस्यों से अलग होता है।
- सीमित देयता (Limited Liability) – शेयरधारकों की जिम्मेदारी केवल उनके द्वारा निवेशित राशि तक सीमित होती है।
- स्थायी उत्तराधिकार (Perpetual Succession) – कंपनी तब तक चलती रहती है जब तक कि इसे कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जाता।
- मुकदमा करने और मुकदमा झेलने की क्षमता – कंपनी अपने नाम पर न्यायालय में मुकदमा कर सकती है और उस पर भी मुकदमा किया जा सकता है।
- स्वतंत्र संपत्ति अधिकार (Right to Own Property) – कंपनी स्वयं के नाम से संपत्ति खरीद, बेच और रख सकती है।
- संविदा करने की शक्ति (Power to Contract) – कंपनी अपने नाम से अनुबंध कर सकती है।
- सार्वमुद्रा (Common Seal) – कंपनी के नाम से जारी किए गए दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए एक आधिकारिक मोहर (कॉमन सील) का उपयोग किया जाता है।
निष्कर्ष
कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जो कानून द्वारा निर्मित होती है और उसका एक स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व होता है। यह अपने सदस्यों से अलग होकर कार्य करती है और इसका अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक इसे कानूनी रूप से समाप्त नहीं किया जाता। इसकी सीमित देयता, स्थायी उत्तराधिकार, तथा स्वतंत्र संपत्ति अधिकार इसे एक मजबूत व्यावसायिक इकाई बनाते हैं।
प्रश्न 4. “कम्पनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जो ठीक एक व्यक्ति की तरह है, किन्तु जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है।’ पूर्ण रूप से समझाइए।
परिचय:
कम्पनी कानून के अनुसार, एक कम्पनी (Company) एक कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person) होती है, जिसे कानून द्वारा निर्मित किया जाता है। यह एक स्वतंत्र कानूनी इकाई (Legal Entity) होती है, जो अपने सदस्यों (Members) से अलग होती है। यद्यपि यह कानूनी रूप से एक व्यक्ति की तरह अधिकार और कर्तव्य रखती है, लेकिन इसका कोई भौतिक (Physical) अस्तित्व नहीं होता, जैसे कि मनुष्यों का होता है।
कम्पनी को कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा जाता है?
कम्पनी को कृत्रिम व्यक्ति कहने के पीछे निम्नलिखित कारण हैं:
- कानूनी अस्तित्व (Legal Existence):
- कम्पनी का निर्माण कानूनी प्रक्रिया (Lawful Process) द्वारा होता है, और यह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है।
- इसे व्यक्ति की तरह करार (Contracts) करने, संपत्ति रखने, और मुकदमे करने का अधिकार होता है।
- स्वतंत्र इकाई (Separate Legal Entity):
- कम्पनी अपने संस्थापकों (Founders) या शेयरधारकों (Shareholders) से अलग होती है।
- कम्पनी के कर्ज और देनदारियों के लिए उसके शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते।
- कोई भौतिक अस्तित्व नहीं (No Physical Existence):
- कम्पनी सिर्फ कागजों और दस्तावेजों में होती है, इसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता।
- यह केवल अपने निदेशकों (Directors) और अधिकारियों (Officers) के माध्यम से कार्य करती है।
- स्थायित्व (Perpetual Succession):
- कम्पनी की स्थायी उत्तराधिकारिता (Perpetual Succession) होती है, यानी इसके सदस्य मर सकते हैं, लेकिन कम्पनी तब भी चलती रहती है।
- इसका अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक इसे कानूनन भंग (Dissolve) नहीं किया जाता।
- मुकदमा करने और करार करने की शक्ति (Right to Sue & Enter into Contracts):
- कम्पनी अपने नाम से किसी पर मुकदमा कर सकती है और उस पर मुकदमा भी किया जा सकता है।
- यह व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं के साथ अनुबंध (Contract) कर सकती है।
निष्कर्ष:
“कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता” – इस कथन का अर्थ है कि कम्पनी कानूनी रूप से एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। यह एक कानूनी कल्पना (Legal Fiction) पर आधारित होती है और अपने शेयरधारकों व निदेशकों से अलग अस्तित्व रखती है।
प्रश्न 5. कम्पनी की परिभाषा दीजिए। कम्पनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
कम्पनी की परिभाषा
कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person) होती है, जिसे कानून द्वारा निर्मित किया जाता है। यह एक अलग कानूनी अस्तित्व (Separate Legal Entity) रखती है, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करना होता है। कम्पनी को उसके शेयरधारकों (Shareholders) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इसके कार्यों का संचालन निदेशक मंडल (Board of Directors) करता है।
कुछ प्रमुख परिभाषाएँ:
- लॉर्ड जस्टिस लिंडले:
“कम्पनी व्यक्तियों का एक ऐसा संघ है, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है और जिसे कानून द्वारा एक कृत्रिम व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है।” - भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार:
“एक कम्पनी वह संघ है जो इस अधिनियम के तहत गठित की जाती है या पूर्व कम्पनी अधिनियम के तहत गठित की गई थी।”
कम्पनी की विशेषताएँ
- कृत्रिम कानूनी व्यक्ति (Artificial Legal Person):
कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, जिसे कानून द्वारा मान्यता दी जाती है। यह अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, अनुबंध कर सकती है और कानूनी कार्यवाही कर सकती है। - अलग कानूनी अस्तित्व (Separate Legal Entity):
कम्पनी का अस्तित्व उसके मालिकों (शेयरधारकों) से अलग होता है। यानी, अगर कम्पनी पर कोई ऋण होता है, तो उसके शेयरधारकों की व्यक्तिगत संपत्ति प्रभावित नहीं होती। - सीमित देयता (Limited Liability):
कम्पनी के शेयरधारकों की देयता केवल उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों तक सीमित होती है। यदि कम्पनी को नुकसान होता है, तो शेयरधारकों को अपने व्यक्तिगत धन से इसकी भरपाई नहीं करनी पड़ती। - स्थायी अस्तित्व (Perpetual Succession):
कम्पनी का अस्तित्व उसके सदस्यों के जीवन या मृत्यु पर निर्भर नहीं करता। सदस्यों के बदलने के बावजूद कम्पनी चलती रहती है। - स्थानांतरित करने योग्य शेयर (Transferability of Shares):
सार्वजनिक कम्पनी के शेयरधारक अपने शेयर आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, जिससे निवेशकों को सुविधा मिलती है। हालांकि, निजी कम्पनी के शेयरों के हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं। - सामूहिक स्वामित्व और प्रबंधन (Collective Ownership and Management):
कम्पनी के मालिक इसके शेयरधारक होते हैं, लेकिन प्रबंधन निदेशक मंडल (Board of Directors) द्वारा किया जाता है, जिसे शेयरधारकों द्वारा चुना जाता है। - कानूनी विनियमन (Legal Regulation):
कम्पनी को भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के नियमों का पालन करना होता है और उसे सरकार के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। - संपत्ति रखने की क्षमता (Right to Own Property):
कम्पनी अपने नाम से संपत्ति खरीद, बेच और धारित कर सकती है। कम्पनी की संपत्ति उसके मालिकों (शेयरधारकों) की व्यक्तिगत संपत्ति से अलग होती है।
निष्कर्ष
कम्पनी एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्था होती है, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यह सीमित देयता, स्थायी उत्तराधिकार, अलग कानूनी पहचान और संपत्ति रखने की क्षमता जैसी विशेषताओं के कारण व्यापार संचालन के लिए एक प्रभावी संरचना प्रदान करती है।
प्रश्न 6. “कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण कानून द्वारा किया जाता है, यह एक पृथक अस्तित्व रखती है, इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है तथा इसकी एक सार्वमुद्रा होती है।’ उक्त कथन की व्याख्या कीजिए।
परिचय
कम्पनी एक कृत्रिम (Artificial) और विधि द्वारा निर्मित (Legal Entity) संस्था होती है, जिसका एक स्वतंत्र अस्तित्व (Separate Legal Entity) होता है। यह न केवल अपने नाम से व्यापार कर सकती है, बल्कि अपनी संपत्ति भी रख सकती है, अनुबंध कर सकती है और कानूनी कार्यवाही में भाग ले सकती है। इस परिभाषा में निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया गया है:
- कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है
- कम्पनी का पृथक (अलग) अस्तित्व होता है
- अविच्छिन्न उत्तराधिकार (Perpetual Succession) प्राप्त है
- कम्पनी की एक सार्वमुद्रा (Common Seal) होती है
अब इन चारों विशेषताओं की व्याख्या करते हैं।
1. कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है
कम्पनी को कानून द्वारा एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है, जिसका निर्माण कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, लेकिन यह अपने सदस्यों से अलग होती है। यह प्राकृतिक व्यक्ति (Natural Person) की तरह कार्य कर सकती है, जैसे:
- अपने नाम से संपत्ति खरीद और बेच सकती है।
- करार (Contracts) कर सकती है।
- मुकदमा कर सकती है और उस पर मुकदमा चल सकता है।
हालांकि, कम्पनी स्वयं कोई शारीरिक कार्य नहीं कर सकती, इसलिए उसके निर्णय निदेशक मंडल (Board of Directors) द्वारा लिए जाते हैं।
उदाहरण: टाटा समूह या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसी कम्पनियाँ अपने नाम से संपत्ति रखती हैं, सौदे करती हैं और कानूनी कार्यवाही में भाग ले सकती हैं।
2. कम्पनी का पृथक अस्तित्व होता है (Separate Legal Entity)
कानूनी दृष्टि से, कम्पनी का अस्तित्व उसके मालिकों (शेयरधारकों) से अलग होता है। इसका मतलब है कि:
- अगर कम्पनी किसी ऋण (Debt) में डूब जाती है, तो उसके शेयरधारकों की व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान नहीं होगा।
- कम्पनी के शेयरधारक बदल सकते हैं, लेकिन कम्पनी का अस्तित्व बना रहता है।
- कम्पनी स्वयं कर का भुगतान करती है और उसके लाभ और हानि का असर सीधे उसके शेयरधारकों पर नहीं पड़ता।
न्यायिक उदाहरण: Salomon v. Salomon & Co. Ltd. (1897) में इंग्लैंड की अदालत ने यह सिद्ध किया कि कम्पनी अपने मालिकों से अलग एक स्वतंत्र इकाई होती है।
3. अविच्छिन्न उत्तराधिकार (Perpetual Succession)
कम्पनी का अस्तित्व उसके सदस्यों के जीवन या मृत्यु से प्रभावित नहीं होता। यदि किसी कम्पनी के सभी शेयरधारकों की मृत्यु हो जाए या वे कम्पनी छोड़ दें, तो भी कम्पनी का अस्तित्व बना रहता है।
- कम्पनी का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक इसे कानूनन समाप्त (Wound Up) नहीं किया जाता।
- इसके निदेशक और शेयरधारक बदलते रहते हैं, लेकिन कम्पनी का संचालन चलता रहता है।
उदाहरण: कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ (जैसे IBM, Microsoft) दशकों से कार्यरत हैं, जबकि उनके संस्थापक या शुरुआती निदेशक बदल चुके हैं।
4. कम्पनी की एक सार्वमुद्रा (Common Seal) होती है
चूंकि कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए इसे मान्यता देने के लिए सार्वमुद्रा (Common Seal) का उपयोग किया जाता है।
- कम्पनी के सभी आधिकारिक दस्तावेजों, अनुबंधों और महत्वपूर्ण पत्रों पर इसकी मुहर लगाई जाती है।
- यह प्रमाण होता है कि उस दस्तावेज को कम्पनी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किया गया है।
हालांकि, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 में कम्पनी के लिए सार्वमुद्रा अनिवार्य नहीं रखी गई है, लेकिन कुछ कानूनी मामलों में इसका महत्व बना रहता है।
निष्कर्ष
कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका पृथक अस्तित्व होता है, यह अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त करती है और इसे अपनी पहचान के लिए एक सार्वमुद्रा की आवश्यकता होती है। ये विशेषताएँ कम्पनी को एक प्रभावी व्यावसायिक संगठन बनाती हैं, जिससे यह दीर्घकाल तक कार्य कर सकती है और कानूनी सुरक्षा का लाभ उठा सकती है।
प्रश्न 7. “कम्पनी एक विधिक व्यक्ति है।’ उचित वादों की सहायता से इसकी विवेचना कीजिए।
परिचय
कंपनी को एक “विधिक व्यक्ति” (Legal Person) कहा जाता है, क्योंकि यह कानून द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र इकाई होती है। इसका अर्थ यह है कि कंपनी स्वयं कानूनी अधिकार और दायित्वों वाली एक अलग इकाई होती है, जो इसके सदस्यों (अंशधारकों) से भिन्न होती है। इसे कानून द्वारा एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जो अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकती है, करार कर सकती है, और कानूनी मामलों में पक्षकार बन सकती है।
उचित वादों के आधार पर विवेचना
कंपनी के विधिक व्यक्ति होने की अवधारणा को समझाने के लिए कई न्यायिक वाद (केस लॉ) महत्वपूर्ण हैं:
1. सालोमॉन बनाम सालोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड (Salomon v. Salomon & Co. Ltd., 1897)
- यह मामला कंपनी कानून का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें यह स्थापित किया गया कि कंपनी एक अलग विधिक व्यक्ति होती है।
- न्यायालय ने यह घोषित किया कि कंपनी और उसके सदस्य (शेयरधारक) दो अलग-अलग इकाइयाँ हैं।
- इस निर्णय ने “पृथक कानूनी अस्तित्व” (Separate Legal Entity) के सिद्धांत को स्थापित किया।
2. ली बनाम ली’स एयर फार्मिंग लिमिटेड (Lee v. Lee’s Air Farming Ltd., 1961)
- इस मामले में, श्री ली अपनी ही कंपनी में निदेशक और कर्मचारी दोनों थे।
- न्यायालय ने यह माना कि कंपनी एक अलग विधिक व्यक्ति है, इसलिए श्री ली कंपनी के कर्मचारी माने गए और उनके परिवार को क्षतिपूर्ति का अधिकार मिला।
- यह मामला यह दर्शाता है कि कंपनी अपने संस्थापक से अलग होती है और उसके अपने अधिकार एवं दायित्व होते हैं।
3. मैक्सवेल बनाम डोड्सवेल (Macwell v. Dodwell, 1917)
- इस मामले में न्यायालय ने पुनः इस तथ्य की पुष्टि की कि एक कंपनी अपने सदस्यों से अलग होती है और यह अपनी संपत्ति की मालिक हो सकती है।
कंपनी के विधिक व्यक्ति होने के परिणाम
- पृथक कानूनी अस्तित्व (Separate Legal Entity)
- कंपनी अपने सदस्यों से अलग एक कानूनी इकाई होती है।
- सीमित दायित्व (Limited Liability)
- शेयरधारकों की देनदारी केवल उनके निवेश तक सीमित होती है।
- अपने नाम पर संपत्ति रखने का अधिकार
- कंपनी स्वयं संपत्ति खरीद और बेच सकती है।
- अनुबंध करने की स्वतंत्रता
- कंपनी अपने नाम से कानूनी अनुबंध कर सकती है।
- कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है और वह भी मुकदमा कर सकती है
- एक कंपनी पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और वह भी अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा दायर कर सकती है।
- निरंतरता (Perpetual Succession)
- कंपनी अपने सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफे से समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक इसे कानूनन बंद न किया जाए।
निष्कर्ष
“कंपनी एक विधिक व्यक्ति है”—यह सिद्धांत विभिन्न न्यायिक वादों के माध्यम से स्थापित हो चुका है। कंपनी का अस्तित्व उसके संस्थापकों और शेयरधारकों से अलग होता है। इसका पृथक कानूनी अस्तित्व, सीमित देयता और स्थायित्व इसे व्यापार और निवेश के लिए एक आदर्श इकाई बनाते हैं।
प्रश्न 8. “एक कम्पनी एक विधिक व्यक्ति है जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से पृथक होता है।’ उपयुक्त वादों का उल्लेख करते हुए विवेचना कीजिए।
परिचय
कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत, कम्पनी को एक विधिक (कानूनी) व्यक्ति माना जाता है, जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों (शेयरधारकों) से अलग होता है। इसका अर्थ यह है कि कम्पनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, करार कर सकती है, मुकदमा कर सकती है और उस पर मुकदमा किया जा सकता है। भले ही कम्पनी के मालिक (शेयरधारक) और प्रबंधक बदल जाएं, फिर भी कम्पनी का अस्तित्व बना रहता है।
कम्पनी का पृथक अस्तित्व (Separate Legal Entity)
किसी भी कम्पनी के गठन के बाद वह एक स्वतंत्र कानूनी इकाई बन जाती है। इस सिद्धांत को विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा पुष्टि दी गई है, जिनमें कुछ प्रमुख वाद निम्नलिखित हैं:
(1) सलीमन बनाम सलीमन एंड कंपनी लिमिटेड (Salomon v. Salomon & Co. Ltd. (1897))
तथ्य:
- मिस्टर सलीमन ने अपनी जूते की व्यवसाय को एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत कराया और कम्पनी के अधिकांश शेयर स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के नाम कर दिए।
- कम्पनी ने सलीमन से व्यापार खरीदा और उन्हें कुछ रकम कंपनी के ऋणपत्रों (Debentures) के रूप में दे दी।
- कम्पनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया, और लेनदारों ने दावा किया कि सलीमन को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए।
निर्णय:
- हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह निर्णय दिया कि कम्पनी एक पृथक विधिक इकाई है और सलीमन व्यक्तिगत रूप से कम्पनी के ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
महत्व:
- इस वाद ने कम्पनी के पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को स्थापित किया।
(2) ली बनाम ली एअर फार्मिंग लिमिटेड (Lee v. Lee’s Air Farming Ltd. (1961))
तथ्य:
- श्री ली ने एक कम्पनी बनाई और स्वयं को इसका प्रबंध निदेशक नियुक्त किया।
- वे कम्पनी के एकमात्र शेयरधारक भी थे और कम्पनी के लिए पायलट के रूप में कार्य करते थे।
- एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी पत्नी ने श्रमिक मुआवजा दावा किया।
निर्णय:
- न्यायालय ने निर्णय दिया कि कम्पनी और श्री ली दो अलग-अलग इकाइयाँ थीं, इसलिए श्री ली कम्पनी के कर्मचारी माने जाएंगे, और उनकी पत्नी को मुआवजा मिलेगा।
महत्व:
- इस निर्णय ने कम्पनी के पृथक अस्तित्व को पुनः प्रमाणित किया और यह स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति कम्पनी का मालिक होने के साथ-साथ उसका कर्मचारी भी हो सकता है।
(3) मैकएडम बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Macadam v. Exide Industries Ltd.)
तथ्य:
- यह मामला निदेशकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी से संबंधित था।
- कम्पनी के कर्जों के लिए व्यक्तिगत रूप से निदेशकों को उत्तरदायी ठहराने की माँग की गई।
निर्णय:
- न्यायालय ने कहा कि कम्पनी अपने निदेशकों से अलग इकाई होती है, इसलिए निदेशक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे, जब तक कि कोई धोखाधड़ी या अन्य अवैध गतिविधि न की गई हो।
महत्व:
- कम्पनी के पृथक अस्तित्व को एक बार फिर मान्यता दी गई और निदेशकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सीमित कर दिया गया।
निष्कर्ष
“एक कम्पनी एक विधिक व्यक्ति है जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से पृथक होता है।” यह सिद्धांत कम्पनी कानून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यह न केवल शेयरधारकों और निदेशकों को व्यक्तिगत जोखिम से बचाता है, बल्कि व्यापार को एक स्थायी और स्वतंत्र पहचान भी प्रदान करता है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों ने इसे बार-बार सिद्ध किया है कि एक बार कम्पनी स्थापित हो जाने के बाद, उसका अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है और उसे एक स्वतंत्र कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दी जाती है।
प्रश्न 9. कम्पनी अधिनियम, 2013 का प्रशासन किन-किन एजेन्सीज द्वारा चलाया जाता है?
कम्पनी अधिनियम, 2013 का प्रशासन मुख्य रूप से निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाता है:
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs – MCA)
- यह मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन, नियमों के निर्माण और निगरानी का कार्य करता है।
- रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ (Registrar of Companies – ROC)
- यह हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत होता है और कंपनियों का पंजीकरण, अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal – NCLT)
- यह कंपनी मामलों से जुड़े विवादों, दिवालियापन और पुनर्गठन के मामलों की सुनवाई करता है।
- राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal – NCLAT)
- यह NCLT के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने के लिए कार्यरत है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India – SEBI)
- सूचीबद्ध कंपनियों और उनके प्रतिभूति बाजार से जुड़े मामलों की निगरानी करता है।
- सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (Serious Fraud Investigation Office – SFIO)
- यह गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी और कॉर्पोरेट गड़बड़ियों की जांच करता है।
ये सभी एजेंसियां मिलकर कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू और प्रभावी बनाती हैं।
प्रश्न 10. कम्पनी के निगमित होने पर प्राप्त लाभ एवं हानि का विस्तार से वर्णन कीजिए।
कम्पनी के निगमित होने पर प्राप्त लाभ एवं हानि
किसी भी कम्पनी के निगमित (Incorporation) होने का अर्थ है कि उसे एक कानूनी पहचान मिल जाती है। इसका सीधा प्रभाव कम्पनी के संचालन, उत्तरदायित्व, कराधान और कानूनी अधिकारों पर पड़ता है। निगमित होने के कई लाभ होते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ हानियाँ भी जुड़ी होती हैं।
1. कम्पनी के निगमित होने के लाभ
(i) पृथक कानूनी अस्तित्व (Separate Legal Entity)
कम्पनी का अपना अलग कानूनी अस्तित्व होता है, जो उसके मालिकों या शेयरधारकों से अलग होता है। इसका मतलब यह है कि कम्पनी स्वयं मुकदमा कर सकती है और उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(ii) सीमित उत्तरदायित्व (Limited Liability)
शेयरधारकों की व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षित रहती है क्योंकि उनका उत्तरदायित्व केवल उनके निवेश तक सीमित होता है। यदि कम्पनी को घाटा होता है या दिवालिया हो जाती है, तो शेयरधारकों की निजी संपत्ति पर असर नहीं पड़ता।
(iii) पूंजी जुटाने में आसानी (Ease of Raising Capital)
निगमित कम्पनी शेयर, डिबेंचर और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से पूंजी जुटाने में सक्षम होती है, जिससे व्यापार के विस्तार में सहायता मिलती है।
(iv) स्थायित्व (Perpetual Succession)
कम्पनी का अस्तित्व उसके मालिकों या निदेशकों की मृत्यु या हटने से समाप्त नहीं होता। यह तब तक चलती रहती है जब तक इसे कानूनी रूप से भंग (dissolve) नहीं किया जाता।
(v) कर लाभ (Tax Benefits)
कुछ देशों में निगमित कम्पनियों को कर में छूट मिलती है या व्यक्तिगत व्यवसायों की तुलना में कम कर दर लागू होती है।
(vi) पेशेवर प्रबंधन (Professional Management)
कम्पनी में निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम होते हैं, जो व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं।
(vii) कानूनी सुरक्षा (Legal Protection)
कम्पनी की संपत्ति, बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) और व्यावसायिक हित कानूनी रूप से सुरक्षित होते हैं।
2. कम्पनी के निगमित होने की हानियाँ
(i) अधिक कानूनी औपचारिकताएँ (More Legal Formalities)
निगमन (Incorporation) की प्रक्रिया जटिल होती है और इसमें कई कानूनी दस्तावेज, लाइसेंस और मंजूरी की आवश्यकता होती है।
(ii) अधिक लागत (Higher Cost)
कम्पनी को पंजीकृत करने, लेखांकन, कानूनी सेवाओं और सरकारी शुल्कों में अधिक खर्च करना पड़ता है।
(iii) कर बोझ (Tax Burden)
कुछ मामलों में, निगमित कम्पनियों पर अधिक कर लगाया जा सकता है, विशेष रूप से यदि वे छोटे व्यवसायों की तुलना में अधिक लाभ कमा रही हों।
(iv) गोपनीयता में कमी (Lack of Privacy)
निगमित कम्पनियों को अपने वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल की जानकारी और वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होती है, जिससे उनकी गोपनीयता प्रभावित होती है।
(v) स्वायत्तता में कमी (Less Personal Control)
यदि कम्पनी के शेयर कई लोगों के पास हैं, तो संस्थापक को अपने निर्णयों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति लेनी पड़ सकती है, जिससे उनका नियंत्रण सीमित हो सकता है।
(vi) अधिक नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance)
कम्पनियों को सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे उनका संचालन जटिल हो सकता है।
निष्कर्ष
कम्पनी के निगमित होने के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं, जैसे सीमित उत्तरदायित्व, पूंजी जुटाने की क्षमता और स्थायित्व। हालांकि, इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं, जैसे अधिक कानूनी जटिलताएँ, खर्च और गोपनीयता में कमी। इसलिए, निगमित होने से पहले किसी व्यवसाय को अपने उद्देश्यों और आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना चाहिए।
प्रश्न 11. निजी कम्पनी क्या है ? कम्पनी विधान के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी को प्राप्त विशेषाधिकार और छूटों की व्याख्या कीजिए।
निजी कंपनी क्या है?
निजी कंपनी (Private Company) एक प्रकार की कंपनी होती है जिसे निजी स्वामित्व में रखा जाता है और इसके शेयर आम जनता को नहीं बेचे जाते। भारत में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(68) के अनुसार, एक निजी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें—
- सदस्यों की संख्या—न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं।
- शेयर स्थानांतरण पर प्रतिबंध—इसके शेयरधारकों के बीच शेयरों के हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध होते हैं।
- न्यूनतम पूंजी—2015 के संशोधन के बाद, निजी कंपनी के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है।
- ‘प्राइवेट लिमिटेड’ (Pvt. Ltd.)—इस प्रकार की कंपनियों के नाम के अंत में “Private Limited” (Pvt. Ltd.) लिखा जाता है।
निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार और छूटें
निजी कंपनियों को सार्वजनिक कंपनियों की तुलना में कुछ कानूनी छूटें और विशेषाधिकार दिए गए हैं, जो उनके संचालन को सरल और अधिक लचीला बनाते हैं। ये छूट निम्नलिखित हैं—
1. न्यूनतम निदेशक (Directors) की संख्या
- सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 3 निदेशक आवश्यक होते हैं, जबकि निजी कंपनी में सिर्फ 2 निदेशक ही आवश्यक होते हैं।
2. स्वतंत्र निदेशक (Independent Director) की बाध्यता नहीं
- सार्वजनिक कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, लेकिन निजी कंपनियों को इससे छूट दी गई है।
3. वैधानिक सभा (Statutory Meeting) की आवश्यकता नहीं
- सार्वजनिक कंपनियों को अपनी स्थापना के बाद वैधानिक सभा बुलानी होती है, लेकिन निजी कंपनियों को इससे छूट दी गई है।
4. शेयरों का स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण प्रतिबंधित
- सार्वजनिक कंपनियों के विपरीत, निजी कंपनियां अपने शेयरधारकों के बीच शेयरों के स्थानांतरण पर नियंत्रण रख सकती हैं।
5. न्यूनतम चुकता पूंजी की कोई बाध्यता नहीं
- पहले, निजी कंपनी के लिए न्यूनतम 1 लाख रुपये की चुकता पूंजी अनिवार्य थी, लेकिन 2015 में इसे हटा दिया गया।
6. निदेशकों की भागीदारी (Participation in Board Meetings)
- निजी कंपनियों के निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से बैठक में भाग ले सकते हैं, जिससे प्रबंधन अधिक लचीला बनता है।
7. ऋण और निवेश पर कम प्रतिबंध
- सार्वजनिक कंपनियों के लिए कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत कड़े नियम होते हैं, लेकिन निजी कंपनियों को इनमें से कुछ नियमों से छूट दी गई है।
8. निदेशकों के वेतन पर कोई सीमा नहीं
- सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकों को दिए जाने वाले वेतन पर कुछ सीमाएँ होती हैं, जबकि निजी कंपनियों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती।
9. ऑडिट आवश्यकताओं में राहत
- कुछ विशेष परिस्थितियों में, निजी कंपनियों को आंतरिक ऑडिट से छूट मिल सकती है।
निष्कर्ष
निजी कंपनियों को कई कानूनी छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जो उनके संचालन को अधिक सरल और प्रभावी बनाते हैं। ये विशेषाधिकार मुख्य रूप से शेयरधारकों की संख्या, ऑडिट आवश्यकताओं, निदेशक मंडल के नियमों, पूंजी आवश्यकताओं और विनियामक अनुपालन से संबंधित होते हैं। इन छूटों के कारण निजी कंपनियां कम औपचारिकताओं और अधिक लचीलेपन के साथ कार्य कर सकती हैं।
प्रश्न 12. निजी कम्पनी की परिभाषा दीजिए। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें कौन-कौन • से विशेषाधिकार एवं छूटें प्राप्त हैं ?
निजी कंपनी की परिभाषा
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(68) के अनुसार, निजी कंपनी (Private Company) वह कंपनी होती है जो अपने अनुच्छेदों द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंध लगाती है:
- शेयर स्थानांतरण पर प्रतिबंध – इसके शेयरधारकों को अपने शेयर स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं होती।
- सदस्यों की सीमा – इसमें न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं (एकल सदस्य वाली निजी कंपनी के लिए एक व्यक्ति भी सदस्य हो सकता है)।
- न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं – अब किसी न्यूनतम पूंजी की बाध्यता नहीं है।
- जनता से पूंजी या डिपॉजिट स्वीकार करने पर प्रतिबंध – यह किसी भी प्रकार से जनता से पूंजी नहीं जुटा सकती।
निजी कंपनियों को प्राप्त विशेषाधिकार एवं छूटें
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निजी कंपनियों को निम्नलिखित विशेषाधिकार एवं छूटें प्रदान की गई हैं:
- न्यूनतम निदेशकों की संख्या – सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक आवश्यक होते हैं, जबकि निजी कंपनी में केवल 2 निदेशक पर्याप्त होते हैं।
- स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता नहीं – निजी कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती।
- वार्षिक आम बैठक (AGM) – यदि निजी कंपनी में एक ही सदस्य है, तो उसे वार्षिक आम बैठक बुलाने की जरूरत नहीं होती।
- निदेशकों की सेवानिवृत्ति – सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकों को निश्चित अवधि के बाद सेवानिवृत्त करना आवश्यक होता है, लेकिन निजी कंपनियों पर यह नियम लागू नहीं होता।
- शेयर पूंजी की आवश्यकता – पहले निजी कंपनियों के लिए न्यूनतम 1 लाख रुपये की पूंजी आवश्यक थी, लेकिन अब यह अनिवार्यता हटा दी गई है।
- निदेशकों की भागीदारी – निदेशक अपने रिश्तेदारों के साथ वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं, बशर्ते यह हितों के टकराव (Conflict of Interest) के नियमों के अनुसार हो।
- लेन-देन में सरलता – निजी कंपनियों को संबद्ध पक्षों (Related Party Transactions) के मामलों में सार्वजनिक कंपनियों की तुलना में कम कठोर नियमों का पालन करना होता है।
- शेयर जारी करने की प्रक्रिया आसान – निजी कंपनियों को अपने शेयर जारी करने और आवंटन करने में अपेक्षाकृत कम औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता है।
इन विशेषाधिकारों और छूटों के कारण निजी कंपनियां भारत में छोटे और मध्यम व्यापारिक उपक्रमों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं।
प्रश्न 13. एक निजी कम्पनी को परिभाषित कीजिए। निजी कम्पनी को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कौन-कौन सी विशेष सुविधाएँ तथा छूटें प्राप्त हैं ?
निजी कम्पनी की परिभाषा
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(68) के अनुसार, निजी कम्पनी (Private Company) वह कम्पनी होती है जो अपने अनुच्छेदों द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंध लगाती है—
- शेयर हस्तांतरण पर प्रतिबंध – इसके शेयरधारक अपने शेयरों को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित नहीं कर सकते।
- न्यूनतम सदस्यता – इसमें न्यूनतम 2 सदस्य (shareholders) होने आवश्यक हैं।
- अधिकतम सदस्यता – इसमें अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं (एकमात्र कर्माचारी शेयरधारकों को छोड़कर)।
- न्यूनतम पूँजी – कम्पनी अधिनियम, 2013 में न्यूनतम पूँजी की कोई बाध्यता नहीं है।
- ‘प्राइवेट लिमिटेड’ नाम अनिवार्य – हर निजी कम्पनी को अपने नाम के अंत में “Private Limited” लगाना आवश्यक होता है।
निजी कम्पनी को मिलने वाली विशेष सुविधाएँ एवं छूटें
निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनियों की तुलना में कुछ विशेष सुविधाएँ और छूट प्राप्त होती हैं, जिससे इसका संचालन सरल हो जाता है। ये छूटें निम्नलिखित हैं—
1. न्यूनतम पूँजी की कोई बाध्यता नहीं
निजी कम्पनियों के लिए न्यूनतम चुकता पूँजी की कोई अनिवार्यता नहीं है, जबकि पहले यह सीमा निर्धारित थी।
2. निदेशकों की न्यूनतम संख्या
निजी कम्पनी में न्यूनतम 2 निदेशक (Directors) होने आवश्यक हैं, जबकि सार्वजनिक कम्पनी में कम से कम 3 निदेशक अनिवार्य होते हैं।
3. शेयर हस्तांतरण पर नियंत्रण
निजी कम्पनी अपने शेयरों को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की बाध्यता से मुक्त होती है, जिससे अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता।
4. पब्लिक डिपॉजिट पर कोई रोक नहीं
निजी कम्पनियाँ अपने निदेशकों, सदस्यों या उनके रिश्तेदारों से बिना कोई अतिरिक्त औपचारिकताएँ पूरी किए ऋण (Loan) ले सकती हैं।
5. कंपनी सचिव नियुक्त करने की अनिवार्यता नहीं
अगर किसी निजी कम्पनी की चुकता पूँजी ₹10 करोड़ से कम है, तो उसे पूर्णकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती।
6. कम कानूनी अनुपालन
- निदेशकों की बैठकें कम बार आयोजित करनी पड़ती हैं।
- वार्षिक आम बैठक (AGM) को लेकर सख्त नियम नहीं होते।
- प्रॉस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं होती।
7. निदेशकों की योग्यता में छूट
- एक निजी कम्पनी में केवल 1 निदेशक भी 100% शेयरधारिता रख सकता है।
- स्वतंत्र निदेशक (Independent Director) रखने की कोई अनिवार्यता नहीं होती।
8. सार्वजनिक निर्गम (Public Issue) की अनिवार्यता नहीं
निजी कम्पनियाँ अपने शेयर या डिबेंचर आम जनता को जारी नहीं कर सकतीं, जिससे उन्हें SEBI और अन्य नियामक प्रक्रियाओं का पालन करने की जरूरत नहीं होती।
9. कम रिपोर्टिंग एवं ऑडिट अनिवार्यता
- निजी कम्पनियों के लिए वैधानिक ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ सार्वजनिक कम्पनियों की तुलना में सरल होती हैं।
- कुछ मामलों में गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है।
निष्कर्ष
निजी कम्पनी का स्वरूप छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें कानूनी औपचारिकताएँ कम होती हैं और संचालन अधिक लचीला होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत इसे कई विशेष सुविधाएँ और छूट दी गई हैं, जिससे यह व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनती है।
प्रश्न 14. एक निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी में बदलने की कार्यविधि को संक्षेप में वताइये।
एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में बदलने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है:
1. निदेशक मंडल की स्वीकृति:
- कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की जाती है।
- निजी से सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया जाता है।
- आवश्यक संशोधन (नाम, लेख व संघ पत्र) को मंजूरी दी जाती है।
2. संवैधानिक दस्तावेजों में संशोधन:
- संघ पत्र (MOA) और लेख पत्र (AOA) में संशोधन किया जाता है।
- निजी कंपनी से संबंधित प्रतिबंध (जैसे शेयर ट्रांसफर की पाबंदी, न्यूनतम सदस्य सीमा आदि) हटाए जाते हैं।
3. विशेष प्रस्ताव (Special Resolution) पास करना:
- शेयरधारकों की आम बैठक (General Meeting) बुलाई जाती है।
- निजी से सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है।
4. नाम परिवर्तन और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार करना:
- कंपनी के नाम में “Private Limited” हटाकर “Limited” जोड़ा जाता है।
- निदेशकों व शेयरधारकों की सूची तैयार की जाती है।
5. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) में आवेदन:
- फॉर्म MGT-14 (Special Resolution के लिए) और INC-27 (संशोधन के लिए) दाखिल किया जाता है।
- आवश्यक शुल्क जमा किया जाता है।
6. प्रमाण पत्र प्राप्त करना:
- ROC द्वारा सभी दस्तावेजों की समीक्षा के बाद, कंपनी को नया प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) जारी किया जाता है।
- इसके बाद, कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में कार्य कर सकती है।
7. अन्य अनुपालन (Compliances):
- न्यूनतम निदेशकों (3) और सदस्यों (7) की संख्या सुनिश्चित करना।
- शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के लिए SEBI नियमों का पालन करना (यदि आवश्यक हो)।
- वैधानिक ऑडिट और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना।
इस प्रकार, इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में बदल सकती है।
प्रश्न 15. सरकारी कम्पनी क्या होती है? इसके विशेष लक्षण वताइए। कम्पनी अधिनियम, 2013 कहाँ तक इसे शासित करता है ?
सरकारी कम्पनी वह कम्पनी होती है जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थात सरकार का उस कम्पनी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह कम्पनी भारतीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाती है, और इसके अधिकतर शेयर सरकार के पास होते हैं।
सरकारी कम्पनी के विशेष लक्षण:
- स्वामित्व: सरकारी कम्पनी में सरकार का कम से कम 51% शेयर होता है।
- नियंत्रण: सरकारी कम्पनी के संचालन और निर्णय सरकार के नियंत्रण में होते हैं।
- लाभ और उद्देश्य: इसका उद्देश्य न केवल लाभ अर्जित करना होता है, बल्कि सार्वजनिक सेवा और राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना भी होता है।
- कानूनी स्थिति: सरकारी कम्पनी एक कानूनी व्यक्तित्व (legal entity) होती है, जो कि अपने स्वयं के नाम से कानूनी कार्य कर सकती है।
- वित्तपोषण: सरकारी कम्पनी के लिए पूंजी का स्रोत सरकार होती है या सरकारी वित्तीय संस्थानों से होती है।
- नियामक प्राधिकरण: यह कम्पनी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत काम करती है, लेकिन इसमें सरकार के लिए विशेष प्रावधान होते हैं।
- सरकार का प्रतिनिधित्व: इसका संचालन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सरकार के प्रतिनिधि होते हैं।
कम्पनी अधिनियम, 2013 और सरकारी कम्पनी:
कम्पनी अधिनियम, 2013 सरकारी कंपनियों को भी शासित करता है, लेकिन सरकारी कंपनियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान होते हैं। जैसे कि:
- धारा 2(45) में सरकारी कम्पनी की परिभाषा दी गई है।
- धारा 46 में सरकारी कंपनियों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिसमें कम्पनी की गठन, निदेशक मंडल, और अन्य प्रशासनिक कार्यों के बारे में नियम निर्धारित हैं।
- धारा 47 सरकारी कंपनियों के लिए शेयरholding की संरचना को स्पष्ट करती है, जिसमें सरकार का स्वामित्व 51% से अधिक होना चाहिए।
सरकारी कंपनियाँ कम्पनी अधिनियम के सामान्य नियमों का पालन करती हैं, लेकिन इनमें सरकार का विशेष नियंत्रण होता है, और इसके संचालन पर अतिरिक्त सरकारी नियम लागू होते हैं।