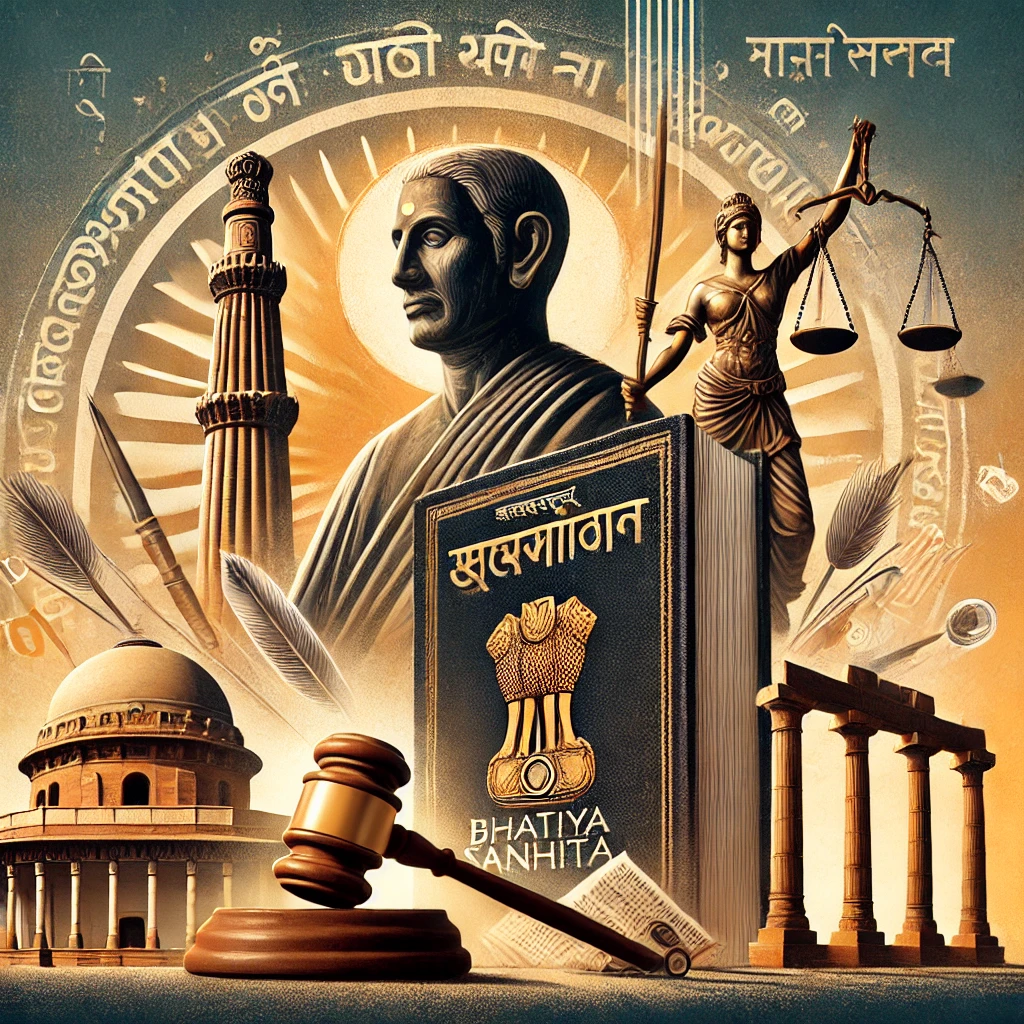शीर्षक:
‘एक्टिविज़्म’ और ‘ओवररीच’: क्या न्यायपालिका की सीमाएं लांघी जा रही हैं?
प्रस्तावना:
भारत के संवैधानिक ढांचे में न्यायपालिका को सर्वोच्च प्रहरी माना गया है जो विधायिका और कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर नजर रखती है। परंतु हाल के वर्षों में न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) के नाम पर न्यायपालिका द्वारा ऐसे निर्णय दिए गए हैं जिन्हें कई बार ‘न्यायिक अतिक्रमण’ (Judicial Overreach) कहा गया है। यह लेख न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के मध्य बारीक अंतर, उनके लाभ-हानि तथा लोकतांत्रिक ढांचे पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करता है।
न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति और आवश्यकता:
न्यायिक सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय सामाजिक और सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में पहल करता है, विशेष रूप से तब जब अन्य दो अंग — विधायिका और कार्यपालिका — निष्क्रिय प्रतीत होते हैं। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आवश्यक साधन बना, जैसे कि मनeka Gandhi मामला (1978) या विशाखा केस (1997), जहां न्यायपालिका ने आगे बढ़कर दिशा-निर्देश तय किए।
न्यायिक अतिक्रमण (Overreach) क्या है?
जब न्यायालय कानून बनाने या नीति निर्धारण जैसी विधायिका की भूमिका में हस्तक्षेप करता है, तो इसे ‘न्यायिक अतिक्रमण’ कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट द्वारा योजनाओं का संचालन, नियुक्तियों में दखल या संसद द्वारा पारित कानूनों की व्याख्या के दौरान सीमा से अधिक हस्तक्षेप देखा गया है।
मुख्य अंतर: एक्टिविज़्म बनाम ओवररीच
- Judicial Activism: जब न्यायपालिका संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर निष्क्रियता के कारण हस्तक्षेप करती है।
- Judicial Overreach: जब न्यायपालिका अन्य अंगों की संवैधानिक सीमाओं में दखल देती है या अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ती है।
यह अंतर सूक्ष्म होते हुए भी लोकतंत्र के संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रसिद्ध उदाहरण:
- एक्टिविज़्म: सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वच्छता, पर्यावरण, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा से जुड़े कई मामलों में दिशा-निर्देश देना।
- ओवररीच: NEET परीक्षा पर तमिलनाडु की विशेष छूट को रोकना, या नीति निर्माण में निर्देश देना जिसे आमतौर पर कार्यपालिका का क्षेत्र माना जाता है।
लोकतंत्र पर प्रभाव:
एक मजबूत न्यायपालिका लोकतंत्र की आत्मा है। किंतु जब न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका की सीमाएं पार करती है, तब यह शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकती है। न्यायपालिका की निष्पक्षता, सार्वजनिक विश्वास और पारदर्शिता तभी बनी रह सकती है जब वह अपनी सीमाओं में रहते हुए काम करे।
विधायिका की प्रतिक्रिया:
कई बार संसद या कार्यपालिका ने न्यायालयों पर ‘लोकतंत्र में अति हस्तक्षेप’ का आरोप लगाया है। यह तकरार तब और बढ़ जाती है जब न्यायपालिका नीति निर्धारण में घुसपैठ करती है, जिससे संविधान में निहित ‘प्रत्येक अंग की स्वायत्तता’ प्रभावित होती है।
क्या संतुलन संभव है?
संविधान के तीनों अंगों — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — को अपनी-अपनी सीमाओं का आदर करते हुए आपसी सामंजस्य से काम करना चाहिए। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग केवल आवश्यक और संविधान-सम्मत स्थितियों में किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष:
‘न्यायिक सक्रियता’ जहां लोकतंत्र की रक्षा का मजबूत औजार बन सकती है, वहीं ‘न्यायिक अतिक्रमण’ उसकी नींव को कमजोर कर सकता है। न्यायपालिका को जनहित के मामलों में हस्तक्षेप अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह हस्तक्षेप संविधान की मर्यादा के भीतर ही होना चाहिए। लोकतंत्र तभी फल-फूल सकता है जब तीनों अंग परस्पर विश्वास और संतुलन के साथ कार्य करें।
समसामयिक प्रासंगिकता:
आज जब कई सामाजिक और संवैधानिक प्रश्नों पर न्यायालय स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, यह जरूरी हो जाता है कि एक्टिविज़्म और ओवररीच की सीमा स्पष्ट बनी रहे। अन्यथा, यह न केवल नीति निर्माण को प्रभावित करेगा, बल्कि आम जनमानस में न्यायिक विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकता है।