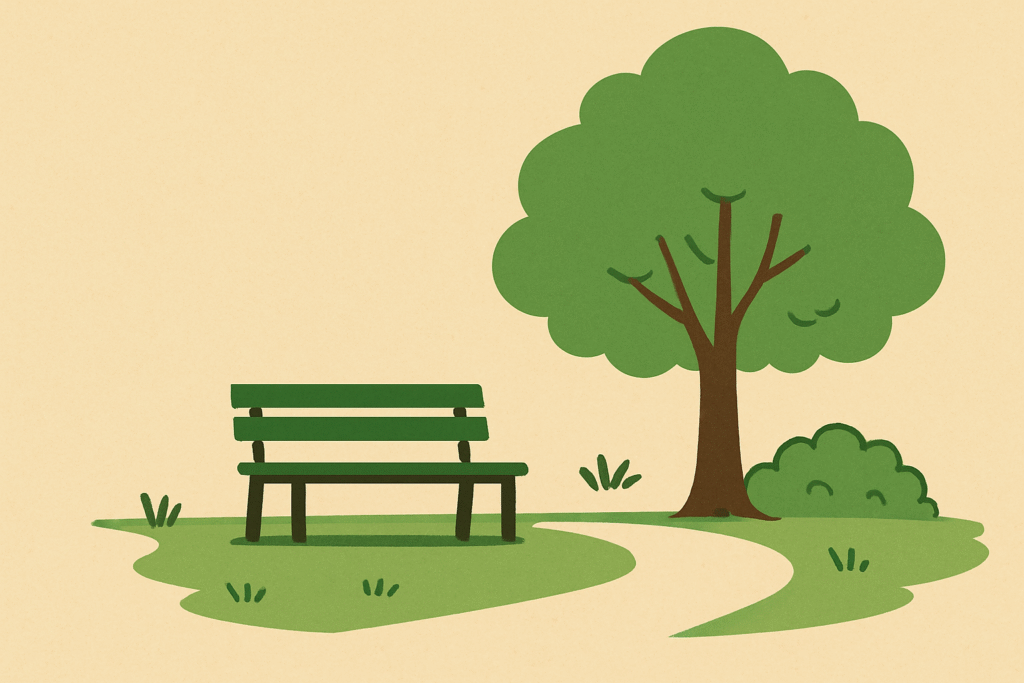उद्यान और पार्क कानून — विस्तृत दीर्घ उत्तर
1. भूमिका (Introduction):
उद्यान और पार्क किसी भी विकसित समाज के आवश्यक अंग होते हैं। वे न केवल शहरों और कस्बों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि लोगों को मानसिक शांति, सामाजिक संवाद, व्यायाम और प्राकृतिक वातावरण प्रदान करते हैं। इनकी रक्षा, विकास और सुव्यवस्थित संचालन हेतु कई कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। भारत में बढ़ती शहरीकरण की प्रक्रिया के चलते उद्यान और पार्कों का संरक्षण अब और भी अधिक आवश्यक हो गया है।
2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
भारत में मुग़ल काल से ही बगीचों और पार्कों की परंपरा रही है। बाबर द्वारा बनवाया गया रामबाग (आगरा) इसका प्रमुख उदाहरण है। ब्रिटिश काल में पार्कों को शहरी नियोजन का भाग बनाया गया, जैसे कि लोधी गार्डन (दिल्ली), हॉग मार्केट के आसपास का हरी क्षेत्र (कोलकाता) आदि।
स्वतंत्रता के बाद, शहरी विकास के साथ-साथ हरित क्षेत्रों को योजना का अंग बनाया गया, जिसे कानूनी रूप भी दिया गया।
3. उद्यान और पार्कों से संबंधित प्रमुख कानून (Major Laws Related to Parks and Gardens):
(क) नगर निकाय कानून (Municipal Acts):
हर राज्य का नगर निगम या नगर पालिका अधिनियम होता है, जिसमें स्थानीय निकायों को सार्वजनिक पार्कों के प्रबंधन और रख-रखाव की जिम्मेदारी दी जाती है। उदाहरण:
- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916
- दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957
- महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम
इन कानूनों के अंतर्गत:
- पार्क की भूमि को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।
- पार्क में कूड़ा फैलाना, अतिक्रमण, अवैध निर्माण दंडनीय अपराध हैं।
- नगर निकाय पार्कों की सफाई, पौधारोपण, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाते हैं।
(ख) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:
इस कानून के तहत सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम बनाए और लागू करे। पार्कों को हरित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इनका संरक्षण आवश्यक होता है।
(ग) वृक्ष संरक्षण कानून (Tree Protection Acts):
जैसे – दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक पार्क में पेड़ काटने, नुकसान पहुँचाने या हटाने के लिए वन विभाग से पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
(घ) शहरी और ग्रामीण भूमि नियोजन कानून:
जैसे – Town and Country Planning Act, जो तय करता है कि किस भू-भाग का किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाएगा। पार्कों के लिए आरक्षित भूमि पर निर्माण अवैध माना जाता है।
(ङ) भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 के अंतर्गत धाराएँ:
- धारा 268: सार्वजनिक उपद्रव (जैसे पार्क में अवैध गतिविधियाँ)
- धारा 431: सार्वजनिक रास्ते या पार्क को नुकसान पहुँचाना
- धारा 427: पार्क की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना
4. न्यायिक दृष्टिकोण (Judicial Interpretation):
भारतीय न्यायपालिका ने उद्यानों और पार्कों की रक्षा हेतु अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं:
(i) M.C. Mehta बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1987):
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और हरित क्षेत्र की रक्षा को नागरिकों के मौलिक अधिकार (जीवन के अधिकार, अनुच्छेद 21) से जोड़ा।
(ii) Bangalore Medical Trust बनाम बी.एस. मुत्तैया (1991):
इस केस में कोर्ट ने कहा कि किसी पार्क की भूमि को अस्पताल या अन्य निर्माण के लिए बदलना अवैध है। पार्कों की जमीन जनता की “Public Trust” मानी जाती है, जिसे बदला नहीं जा सकता।
5. आधुनिक नीतियाँ और पहल (Modern Policies and Initiatives):
(i) स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission):
इस योजना में हरित क्षेत्र, खुले स्थान और स्मार्ट पार्किंग, पर्यावरणीय स्थायित्व को प्राथमिकता दी गई है।
(ii) अमृत योजना (AMRUT):
इस योजना के अंतर्गत शहरों में हरित क्षेत्र और बच्चों के खेलने की जगहें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
(iii) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA):
पार्क क्षेत्र के पास किसी भी निर्माण कार्य के लिए EIA रिपोर्ट आवश्यक होती है।
6. चुनौतियाँ (Challenges):
- अतिक्रमण: पार्कों पर अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं।
- रखरखाव की कमी: सफाई, पौधों की कटाई-छंटाई और उपकरणों की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जाता।
- राजनीतिक हस्तक्षेप: कई बार नेताओं द्वारा वोट बैंक के लिए पार्कों की जमीन का व्यावसायिक उपयोग।
- जन भागीदारी का अभाव: स्थानीय लोगों की भागीदारी कम होती है, जिससे संरक्षण मुश्किल होता है।
7. समाधान और सुझाव (Solutions and Suggestions):
- सख्त कानून का पालन: मौजूदा कानूनों का कठोरता से क्रियान्वयन किया जाए।
- पार्क समितियों का गठन: स्थानीय निवासियों को शामिल कर ‘Park User Committees’ बनाई जाएँ।
- जन जागरूकता: स्कूलों, कॉलेजों, और समाज में पर्यावरण और पार्क संरक्षण के लिए अभियान चलाए जाएँ।
- CSR भागीदारी: कंपनियों को अपने CSR फंड के तहत पार्कों के रखरखाव हेतु प्रेरित किया जाए।
8. निष्कर्ष (Conclusion):
पार्क और उद्यान किसी भी समाज की “हरित आत्मा” होते हैं। ये केवल प्राकृतिक संपदा ही नहीं, बल्कि जनजीवन की गुणवत्ता के संवाहक भी हैं। इनका संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि नागरिकों का भी नैतिक कर्तव्य है। उचित कानूनों, न्यायिक निर्णयों और जनसहभागिता से ही हम इन हरित धरोहरों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रख सकते हैं।