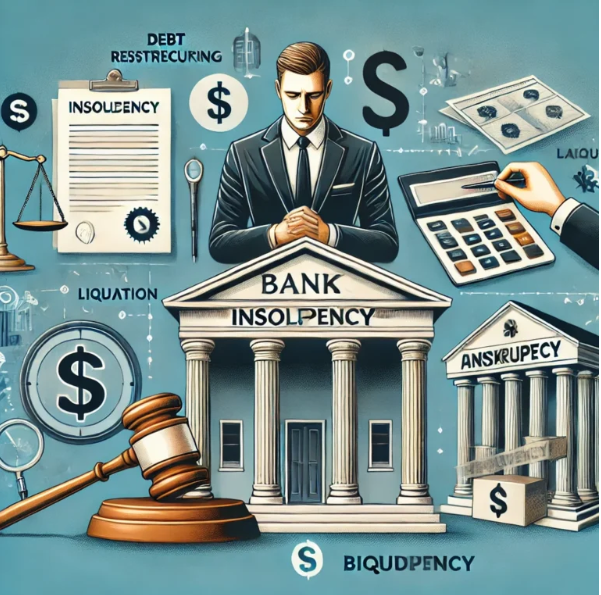इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) बनाम SARFAESI अधिनियम: सम्पूर्ण विश्लेषण
प्रस्तावना
भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण की वसूली और बैंकों की स्थिरता हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। लंबे समय तक SARFAESI अधिनियम, 2002 और Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI Act) जैसे कानूनों के माध्यम से बैंकों को ऋण की वसूली का अधिकार दिया गया। लेकिन ये कानून मुख्यतः secured assets तक ही सीमित थे और ऋणग्रस्त कंपनियों या व्यक्तिगत दिवालियापन की समस्या का समग्र समाधान नहीं दे पाते थे।
इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) लागू किया। यह एक व्यापक कानून है जो केवल secured assets तक सीमित न रहकर पूरी कंपनी या व्यक्ति की इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया को कवर करता है। IBC का मुख्य उद्देश्य है – समयबद्ध तरीके से ऋण पुनर्गठन (Resolution) और दिवालियापन (Bankruptcy) की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना।
इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि SARFAESI अधिनियम और IBC में क्या अंतर है, दोनों की कार्यप्रणाली कैसी है और क्यों IBC को अधिक व्यापक और प्रभावी माना जाता है।
1. SARFAESI अधिनियम, 2002 का परिचय
SARFAESI (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) मुख्यतः बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह अधिकार देता है कि यदि कोई उधारकर्ता ऋण चुकाने में असफल हो, तो वे उसकी secured assets (जैसे – संपत्ति, बंधक या गिरवी रखी संपत्ति) को जब्त कर नीलाम कर सकें।
मुख्य विशेषताएँ:
- धारा 13(2) – डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस।
- धारा 13(4) – नोटिस के बाद भी भुगतान न होने पर संपत्ति पर कब्ज़ा।
- Asset Reconstruction Companies (ARCs) को NPAs बेचने की सुविधा।
- बिना कोर्ट की अनुमति के संपत्ति की नीलामी का अधिकार।
सीमा: यह केवल secured assets तक ही लागू है और कंपनी की कुल वित्तीय स्थिति या व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी को संबोधित नहीं करता।
2. IBC, 2016 का परिचय
Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 एक व्यापक आर्थिक सुधार कानून है, जो कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तिगत व्यक्तियों की इन्सॉल्वेंसी और दिवालियापन से संबंधित है।
मुख्य उद्देश्य:
- समयबद्ध तरीके से ऋण वसूली और पुनर्गठन।
- बैंकों और निवेशकों का विश्वास बढ़ाना।
- व्यवसायों को पुनर्जीवित करना या आवश्यकता पड़ने पर दिवालियापन घोषित करना।
- एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करना।
मुख्य प्रावधान:
- कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) – कंपनियों के लिए।
- व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस।
- दिवालियापन का प्रबंधन करने के लिए Insolvency Professionals और Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) का गठन।
- समय सीमा – 180 दिन (90 दिन की अतिरिक्त अवधि संभव)।
3. SARFAESI बनाम IBC: प्रमुख अंतर
| पहलू | SARFAESI अधिनियम, 2002 | IBC, 2016 |
|---|---|---|
| लागू क्षेत्र | केवल secured assets पर लागू | कंपनी, LLP, व्यक्तिगत और साझेदारी पर लागू |
| प्रक्रिया | संपत्ति की जब्ती और नीलामी | समयबद्ध पुनर्गठन या दिवालियापन प्रक्रिया |
| नियंत्रण | बैंक स्वयं कार्रवाई करते हैं | NCLT (National Company Law Tribunal) की निगरानी |
| उद्देश्य | बकाया ऋण की वसूली | व्यवसाय को पुनर्जीवित करना और आर्थिक स्थिरता |
| समय सीमा | निश्चित समय सीमा नहीं | 180-270 दिन |
| प्रभाव | केवल ऋण वसूली पर केंद्रित | व्यापक समाधान – वसूली, पुनर्गठन और दिवालियापन |
4. IBC की कार्यप्रणाली
(i) कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (CIRP):
- यदि कंपनी ऋण चुकाने में असफल रहती है, तो लेनदार (Financial या Operational Creditor) NCLT में आवेदन कर सकता है।
- एक Insolvency Resolution Professional (IRP) नियुक्त किया जाता है।
- कंपनी का नियंत्रण प्रबंधन से निकलकर IRP के पास चला जाता है।
- Committee of Creditors (CoC) एक Resolution Plan तैयार करती है।
- यदि Resolution Plan असफल होता है, तो कंपनी को दिवालिया घोषित कर Liquidation किया जाता है।
(ii) व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया:
- व्यक्तिगत उधारकर्ता और साझेदारी फर्मों पर लागू।
- ऋण के पुनर्गठन या दिवालियापन की प्रक्रिया IBC के अंतर्गत होती है।
5. IBC बनाम SARFAESI: न्यायिक दृष्टिकोण
- Innoventive Industries Ltd. v. ICICI Bank (2017) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IBC का उद्देश्य समयबद्ध समाधान है और यह विशेष कानून होने के कारण अन्य कानूनों (जैसे SARFAESI) पर प्राथमिकता रखता है।
- Swiss Ribbons Pvt. Ltd. v. Union of India (2019) – कोर्ट ने IBC को संवैधानिक ठहराया और इसे अर्थव्यवस्था सुधारने वाला बताया।
- Essar Steel Case (2019) – सुप्रीम कोर्ट ने Committee of Creditors (CoC) के निर्णय को सर्वोच्च माना और Resolution Plan की महत्ता को स्वीकार किया।
6. IBC का आर्थिक प्रभाव
- NPAs में कमी – IBC ने बैंकों को तेजी से ऋण वसूली का रास्ता दिया।
- Ease of Doing Business – भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ।
- निवेशकों का विश्वास – विदेशी और घरेलू निवेशकों का भरोसा बढ़ा।
- कंपनियों का पुनर्जीवन – कई कंपनियाँ दिवालियापन से बाहर निकलीं।
- बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधरी – ऋण पुनर्प्राप्ति आसान हुई।
7. IBC की सीमाएँ
- कई मामलों में 180 दिन की समय सीमा का पालन नहीं हो पाता।
- NCLT पर मामलों का अत्यधिक बोझ।
- छोटे उधारकर्ताओं और MSMEs के लिए प्रक्रिया जटिल।
- Resolution Professionals की गुणवत्ता और निष्पक्षता पर प्रश्न।
8. SARFAESI और IBC का पारस्परिक संबंध
- SARFAESI अधिनियम मुख्यतः secured creditors के लिए है, जबकि IBC सभी creditors को शामिल करता है।
- IBC लागू होने के बाद SARFAESI अधिनियम गौण हो गया है, लेकिन अभी भी बैंकों के लिए उपयोगी है जब वे केवल गिरवी रखी संपत्ति से वसूली करना चाहते हैं।
- यदि कंपनी या व्यक्ति की समग्र इन्सॉल्वेंसी की बात हो तो IBC ही प्राथमिक कानून है।
9. भविष्य की दिशा
IBC ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत किया है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए:
- NCLT और NCLAT की क्षमता बढ़ानी होगी।
- छोटे व्यवसायों के लिए विशेष प्रावधान बनाने होंगे।
- Resolution Professionals के प्रशिक्षण और नियमन को सुदृढ़ करना होगा।
- SARFAESI और IBC के बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा।
निष्कर्ष
SARFAESI अधिनियम, 2002 बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने उन्हें बिना अदालत की अनुमति के secured assets जब्त करने का अधिकार दिया। लेकिन यह केवल संपत्ति आधारित वसूली तक ही सीमित रहा। दूसरी ओर, IBC, 2016 एक व्यापक कानून है जो पूरी कंपनी या व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का समाधान करता है और समयबद्ध पुनर्गठन एवं दिवालियापन की प्रक्रिया प्रदान करता है।
आज की परिस्थितियों में IBC को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह सिर्फ वसूली नहीं, बल्कि व्यवसायों को पुनर्जीवित करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में सहायक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहाँ SARFAESI अधिनियम एक आंशिक समाधान था, वहीं IBC 2016 एक समग्र समाधान है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान की है।
1. प्रश्न: SARFAESI अधिनियम, 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
SARFAESI अधिनियम, 2002 का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग़ैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) से राहत दिलाना है। इस अधिनियम ने बैंकों को यह शक्ति दी कि वे बिना न्यायालय की अनुमति के secured assets पर कब्ज़ा कर सकें और उसकी नीलामी करके बकाया ऋण वसूल सकें। इससे पहले बैंकों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिससे वसूली में सालों लग जाते थे। SARFAESI अधिनियम ने इस समस्या का त्वरित समाधान प्रदान किया। हालाँकि, यह अधिनियम केवल secured loans तक सीमित है और उधारकर्ता की समग्र वित्तीय स्थिति या दिवालियापन को कवर नहीं करता।
2. प्रश्न: IBC, 2016 लागू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
उत्तर:
SARFAESI और अन्य पुराने कानून केवल आंशिक समाधान देते थे, जिससे ऋण वसूली प्रभावी ढंग से नहीं हो पाती थी। बैंकों के NPAs बढ़ते जा रहे थे और कंपनियों का पुनर्गठन असंभव हो गया था। इस स्थिति में सरकार ने Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 लागू किया। IBC एक समग्र कानून है, जो कंपनियों, LLPs, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों की इन्सॉल्वेंसी और दिवालियापन की प्रक्रिया को कवर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है – ऋण वसूली को समयबद्ध और पारदर्शी बनाना, व्यवसायों का पुनर्जीवन करना और निवेशकों का विश्वास बढ़ाना।
3. प्रश्न: SARFAESI और IBC में सबसे बड़ा अंतर क्या है?
उत्तर:
सबसे बड़ा अंतर इनके लागू क्षेत्र में है। SARFAESI अधिनियम केवल secured assets की जब्ती और नीलामी तक सीमित है। यह मुख्यतः बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए उपयोगी है। दूसरी ओर, IBC, 2016 एक व्यापक ढाँचा है जो पूरी कंपनी, LLP, साझेदारी या व्यक्तिगत उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति को संबोधित करता है। IBC केवल वसूली पर नहीं बल्कि ऋण पुनर्गठन (Resolution) और दिवालियापन (Bankruptcy) पर भी ध्यान देता है। इसीलिए IBC को अधिक प्रभावी और प्राथमिक कानून माना जाता है।
4. प्रश्न: IBC के अंतर्गत Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) कैसे कार्य करता है?
उत्तर:
CIRP IBC की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब कोई कंपनी ऋण चुकाने में असफल होती है, तो लेनदार NCLT में आवेदन कर सकता है। इसके बाद एक Insolvency Resolution Professional (IRP) नियुक्त होता है, जो कंपनी का नियंत्रण संभालता है। फिर Committee of Creditors (CoC) का गठन होता है, जो एक Resolution Plan तैयार करती है। यदि योजना सफल रहती है, तो कंपनी का पुनर्जीवन होता है। लेकिन यदि योजना असफल होती है, तो कंपनी को दिवालिया घोषित कर Liquidation प्रक्रिया शुरू की जाती है।
5. प्रश्न: IBC में NCLT और NCLAT की क्या भूमिका है?
उत्तर:
NCLT (National Company Law Tribunal) IBC के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मंच है, जहाँ कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी के सभी मामले दर्ज होते हैं। यह आवेदन स्वीकार करता है, Insolvency Professionals नियुक्त करता है और Resolution Plan की मंजूरी देता है। यदि किसी पक्ष को NCLT के निर्णय से असहमति होती है, तो वह NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) में अपील कर सकता है। इस प्रकार, NCLT और NCLAT IBC की पूरी प्रक्रिया को न्यायिक ढाँचे के भीतर नियंत्रित और सुव्यवस्थित करते हैं।
6. प्रश्न: IBC का बैंकों और निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर:
IBC लागू होने के बाद बैंकों और निवेशकों का विश्वास काफी बढ़ा। पहले बैंकों को वर्षों तक ऋण वसूली के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन IBC ने 180–270 दिन की समयसीमा तय कर दी। इससे NPAs कम हुए और बैंकों की बैलेंस शीट सुधरी। विदेशी और घरेलू निवेशकों का भरोसा भारतीय वित्तीय प्रणाली पर बढ़ा। कई कंपनियाँ दिवालियापन से बचकर पुनर्जीवित हुईं। इससे Ease of Doing Business Index में भारत की रैंकिंग में भी सुधार हुआ।
7. प्रश्न: SARFAESI अधिनियम की सीमाएँ क्या हैं?
उत्तर:
SARFAESI अधिनियम केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर लागू होता है और यह सिर्फ secured loans तक सीमित है। इसका उपयोग कृषि ऋणों पर नहीं किया जा सकता। इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह केवल संपत्ति जब्ती और नीलामी की अनुमति देता है, लेकिन कंपनी या व्यक्ति की समग्र वित्तीय स्थिति का समाधान नहीं करता। कई बार छोटे उधारकर्ताओं और किसानों को भी परेशानी होती है क्योंकि उनकी संपत्ति पर कब्ज़ा किया जा सकता है। इसलिए SARFAESI को आंशिक समाधान माना जाता है।
8. प्रश्न: IBC की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
उत्तर:
यद्यपि IBC ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को मजबूती दी है, फिर भी इसमें कई चुनौतियाँ हैं। कई मामलों में 180 दिन की समयसीमा का पालन नहीं हो पाता और NCLT पर मामलों का अत्यधिक बोझ बढ़ गया है। छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए IBC की प्रक्रिया जटिल है। Insolvency Professionals की संख्या और उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। इसके अलावा Resolution Plan को लागू करने में देरी होती है। इन चुनौतियों के बावजूद, IBC अब भी सबसे व्यापक और प्रभावी कानून माना जाता है।
9. प्रश्न: IBC को न्यायपालिका ने किस प्रकार वैध ठहराया?
उत्तर:
सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण मामलों में IBC की वैधता और महत्व को स्वीकार किया। Innoventive Industries Ltd. v. ICICI Bank (2017) में कहा गया कि IBC समयबद्ध समाधान हेतु विशेष कानून है और यह अन्य कानूनों पर प्राथमिकता रखता है। Swiss Ribbons Pvt. Ltd. v. Union of India (2019) में कोर्ट ने IBC को संवैधानिक ठहराया और कहा कि इसका उद्देश्य केवल वसूली नहीं बल्कि व्यवसायों का पुनर्जीवन भी है। Essar Steel Case (2019) में कोर्ट ने Committee of Creditors के निर्णय को सर्वोच्च माना।
10. प्रश्न: IBC और SARFAESI का आपसी संबंध क्या है?
उत्तर:
SARFAESI और IBC दोनों ही ऋण वसूली से जुड़े कानून हैं, लेकिन उनका दायरा अलग है। SARFAESI केवल secured assets तक सीमित है और बैंकों को सीधे संपत्ति जब्त करने की शक्ति देता है। दूसरी ओर, IBC कंपनी, LLP, साझेदारी और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की समग्र इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया को कवर करता है। यदि कोई कंपनी या व्यक्ति गंभीर वित्तीय संकट में हो, तो IBC ही प्राथमिक कानून है। दोनों कानून मिलकर भारतीय बैंकिंग प्रणाली को स्थिरता प्रदान करते हैं, लेकिन IBC को अधिक व्यापक और प्रभावी माना जाता है।