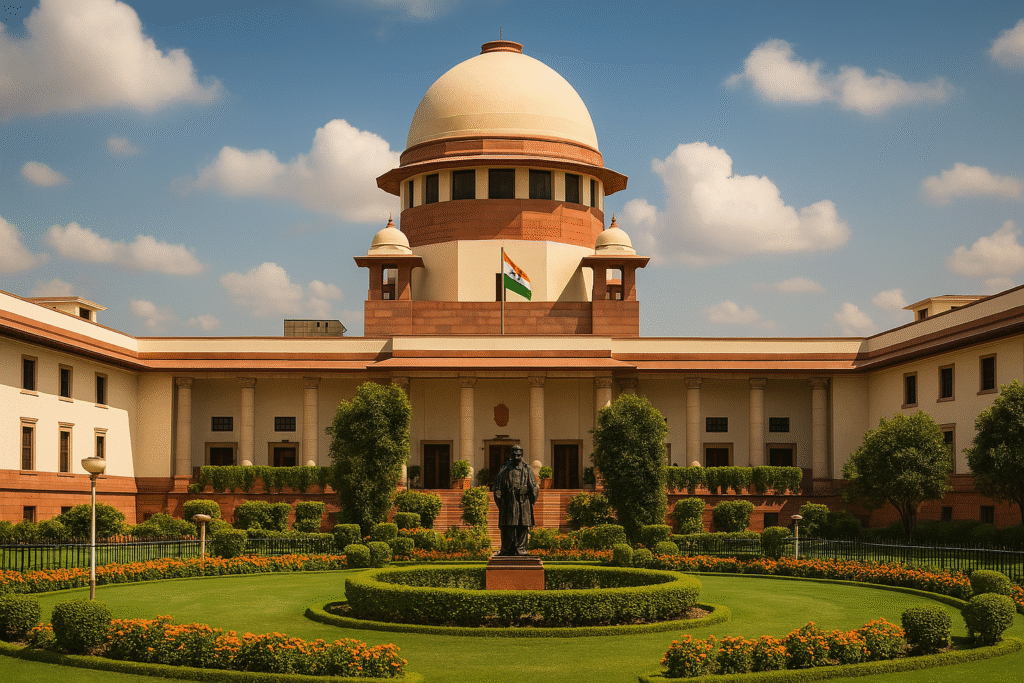इंद्रा शर्मा बनाम वी. के. वी. शर्मा (2013): सुप्रीम कोर्ट द्वारा “घरेलू संबंध” की परिभाषा का ऐतिहासिक विस्तार
प्रस्तावना
भारतीय समाज में विवाह संस्था को अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन समय के साथ-साथ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन के कारण लिव-इन रिलेशनशिप, सीमित वैवाहिक संबंध तथा अन्य पारिवारिक व्यवस्थाएं भी उभर कर सामने आई हैं। इस बदलते सामाजिक परिदृश्य में, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना भारतीय न्यायपालिका की एक बड़ी चुनौती बन गई है।
इसी संदर्भ में वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय — इंद्रा शर्मा बनाम वी. के. वी. शर्मा, भारतीय सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसमें न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2(f) में दी गई “घरेलू संबंध” (domestic relationship) की परिभाषा का व्यापक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विस्तार किया।
मामले की पृष्ठभूमि
- याचिकाकर्ता इंद्रा शर्मा एक निजी कंपनी में कार्यरत थीं और वहीं उनके सहकर्मी वी.के.वी. शर्मा के साथ उनका संबंध विकसित हुआ।
- दोनों ने लगभग 5 वर्षों तक एक साथ सहजीवन (cohabitation) में रहना शुरू किया, और अपने परिवारों तथा समाज के समक्ष खुद को पति-पत्नी के रूप में प्रस्तुत भी किया।
- वी.के.वी. शर्मा पहले से विवाहित थे, लेकिन उन्होंने इंद्रा को यह झूठ बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया है।
समय के साथ जब वी.के.वी. शर्मा ने इंद्रा को त्याग दिया और उसे मानसिक उत्पीड़न देने लगे, तब इंद्रा ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत राहत की मांग की।
कानूनी प्रश्न
क्या ऐसी महिला, जो विवाहित पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही है, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत घरेलू संबंध में शामिल मानी जा सकती है और संरक्षण की अधिकारी है?
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की पीठ ने इस मामले में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए:
1. घरेलू संबंध की व्याख्या (Section 2(f), DV Act):
अधिनियम में “घरेलू संबंध” की परिभाषा में ऐसा संबंध जो विवाह के समान हो (relationship in the nature of marriage) को शामिल किया गया है।
अतः यदि कोई महिला लंबे समय तक एक पुरुष के साथ रहती है, और उनके बीच पारिवारिक, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक संबंध हैं, तो वह ‘घरेलू संबंध’ के अंतर्गत आती है।
2. लिव-इन रिलेशनशिप को पूरी तरह से अवैध नहीं ठहराया जा सकता:
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप अब कोई “वर्जित” या “अवैध” व्यवस्था नहीं है, यदि वह दीर्घकालिक, स्थायी और विश्वास आधारित हो।
3. ‘विवाह के समान संबंध’ को परिभाषित करने के मानक तय किए:
न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप को ‘विवाह-समान संबंध’ मानने के लिए निम्नलिखित मानदंड (tests) सुझाए:
- दोनों व्यक्तियों ने स्वयं को पति-पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया हो।
- संबंध दीर्घकालिक, स्थायी, और सामाजिक रूप से मान्य हो।
- महिला को यह विश्वास हो कि वह विधिक रूप से पत्नी है।
- पुरुष ने महिला को धोखे में रखकर संबंध नहीं बनाया हो।
4. धोखे से बने संबंध को भी संरक्षण की आवश्यकता:
यदि कोई पुरुष जानबूझकर महिला को धोखे में रखकर विवाह या तलाक का झूठा वादा करके उसके साथ संबंध बनाए, और महिला ने उसे विवाह-समान मानकर जीवन बिताया, तो वह महिला भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण की पात्र मानी जाएगी।
निर्णय का सारांश
- इंद्रा शर्मा को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत राहत नहीं मिली, क्योंकि अदालत ने यह पाया कि यद्यपि संबंध दीर्घकालिक था, लेकिन महिला को यह जानकारी थी कि पुरुष विवाहित है, और फिर भी उसने सहमति से यह संबंध जारी रखा।
- हालांकि, कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप की वैधानिकता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी, और यह कहा कि “सभी लिव-इन रिलेशनशिप अवैध नहीं होतीं, परंतु हर लिव-इन रिलेशनशिप को संरक्षण नहीं मिल सकता।”
इस निर्णय का महत्व
- लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए “विवाह-समान संबंध” की अवधारणा को विधिक ढांचे में सम्मिलित किया गया।
- घरेलू हिंसा अधिनियम की व्याख्या को लचीला और व्यावहारिक बनाया गया, जिससे असुरक्षित महिलाओं को न्याय मिल सके।
- फर्जी और धोखे पर आधारित लिव-इन संबंधों से बचने हेतु महिला की जानकारी और समझ की भूमिका को भी केंद्र में रखा गया।
निष्कर्ष
इंद्रा शर्मा बनाम वी. के. वी. शर्मा (2013) का यह ऐतिहासिक निर्णय भारतीय न्यायिक परंपरा में लिव-इन रिलेशनशिप और घरेलू संबंधों की वैधानिक समझ का विस्तार करता है।
यह फैसला यह भी स्पष्ट करता है कि न्याय केवल विधिक शब्दों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि सामाजिक यथार्थ, महिला अधिकारों और नैतिक जिम्मेदारियों के सुसंतुलन से ही पूर्ण न्याय संभव है।