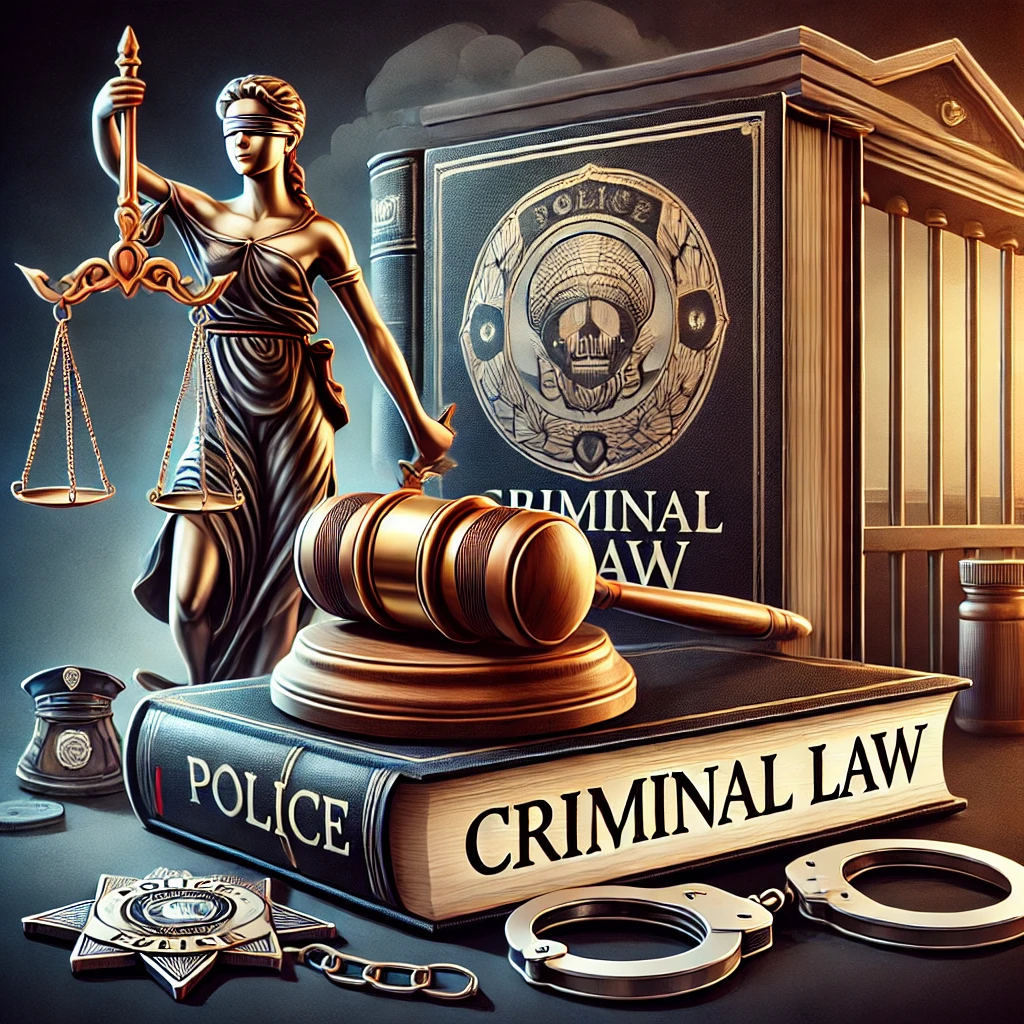1. संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराधों पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:
- संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence): ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ही गिरफ्तारी कर सकती है, संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। ये अपराध आमतौर पर गंभीर होते हैं, जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार आदि।
- असंज्ञेय अपराध (Non-Cognizable Offence): ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है, असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। ये अपराध कम गंभीर होते हैं, जैसे मानहानि, गाली-गलौज आदि।
2. परिवाद को परिभाषित कीजिए। उसके आवश्यक तत्व बताइये।
उत्तर:
- परिभाषा: दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 2(डी) के अनुसार, “परिवाद” वह शिकायत होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष इस उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है कि वह अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करे।
- आवश्यक तत्व:
- यह किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
- मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- इसमें किसी अपराध का उल्लेख होता है।
- इसमें कार्यवाही करने की प्रार्थना की जाती है।
3. अन्वेषण एवं जाँच में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
- अन्वेषण (Investigation): पुलिस द्वारा अपराध के संबंध में की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें साक्ष्य संग्रह, गवाहों से पूछताछ, और अपराधी की पहचान शामिल होती है।
- जाँच (Enquiry): यह न्यायिक प्रक्रिया का भाग होती है, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच की जाती है ताकि यह तय किया जा सके कि मुकदमा चलाया जाए या नहीं।
4. अन्वेषण एवं विचारण में अन्तर स्पष्ट करें।
उत्तर:
- अन्वेषण (Investigation): यह प्रारंभिक प्रक्रिया है, जिसमें पुलिस या अन्य एजेंसियां अपराध की छानबीन करती हैं।
- विचारण (Trial): यह न्यायालय द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय लिया जाता है।
5. (क) पुलिस रिपोर्ट (Police Report)
उत्तर:
पुलिस रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जो पुलिस द्वारा अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाती है। यह धारा 173(2) CrPC के अंतर्गत आती है।
(ख) पुलिस स्टेशन (Police Station)
उत्तर:
पुलिस स्टेशन वह स्थान है जिसे सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, जहां पुलिस अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करती है और कानून-व्यवस्था बनाए रखती है।
6. समन एवं वारण्ट में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
- समन (Summon): यह एक लिखित आदेश होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
- वारंट (Warrant): यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है, जिसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया जाता है।
7. (क) न्यायिक कार्यवाही को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:
न्यायिक कार्यवाही से आशय न्यायालय द्वारा की जाने वाली किसी भी विधिक प्रक्रिया से है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई और निर्णय दिया जाता है।
(ख) “पीड़ित” को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:
CrPC की धारा 2(वा) के अनुसार, “पीड़ित” वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अपराध के कारण प्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंची हो।
8. परिवाद एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्तर कीजिए।
उत्तर:
- परिवाद (Complaint): यह मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जाता है और इसमें किसी अपराध की सूचना दी जाती है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR): यह पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर दर्ज की जाती है। यह CrPC की धारा 154 के अंतर्गत आती है।
9. (क) जमानतीय तथा गैर जमानतीय अपराध में अन्तर को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
- जमानतीय अपराध (Bailable Offence): इसमें अभियुक्त को जमानत लेने का कानूनी अधिकार होता है। जैसे—साधारण मारपीट।
- गैर-जमानतीय अपराध (Non-Bailable Offence): इनमें जमानत मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करती है। जैसे—हत्या, बलात्कार।
(ख) महानगरीय क्षेत्र (Metropolitan Area)
उत्तर:
CrPC की धारा 8 के अनुसार, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को महानगरीय क्षेत्र कहा जाता है, जहां विशेष प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं लागू होती हैं।
10. वारंट मामला (Warrant Case)
उत्तर:
वारंट मामला वह होता है जिसमें अपराध की गंभीरता अधिक होती है और सजा दो वर्ष से अधिक की हो सकती है। इन मामलों में पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किया जाता है।
11. आरोप क्या है? आरोप के अवयवों को इंगित कीजिए।
उत्तर:
- परिभाषा: आरोप (Charge) वह विधिक सूचना है जिसमें किसी व्यक्ति पर लगाए गए अपराध का विवरण होता है। यह CrPC की धारा 211-214 में परिभाषित है।
- अवयव:
- अपराध की प्रकृति और विवरण
- अपराध का समय और स्थान
- अभियुक्त का नाम
- कानून की वह धारा जिसके अंतर्गत अपराध हुआ है
12. संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अन्तर बताइये।
उत्तर:
| आधार | संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) | असंज्ञेय अपराध (Non-Cognizable Offence) |
|———–|———————————|———————————–|
| गंभीरता | गंभीर अपराध | कम गंभीर अपराध |
| पुलिस की शक्ति | पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी कर सकती है | पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है |
| उदाहरण | हत्या, डकैती, बलात्कार | मानहानि, गाली-गलौज |
13. जाँच एवं विचारण में अन्तर बताइये।
उत्तर:
- जाँच (Inquiry): न्यायालय द्वारा किसी अपराध से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।
- विचारण (Trial): वह प्रक्रिया जिसमें न्यायालय अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय लेता है।
14. न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता की विवेचना कीजिए।
उत्तर:
CrPC की धारा 6-15 के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता उनके नियुक्त क्षेत्र तक सीमित होती है। वे केवल अपने अधिकार क्षेत्र में घटित अपराधों पर सुनवाई कर सकते हैं, जब तक कि विशेष अनुमति न दी जाए।
15. लोक अभियोजक (Public Prosecutor)
उत्तर:
लोक अभियोजक सरकार द्वारा नियुक्त एक विधि अधिकारी होता है, जो राज्य की ओर से आपराधिक मामलों में अभियोजन करता है।
16. लोक अभियोजक के अधिकारों तथा नियुक्ति की अर्हता का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
- अर्हताएँ:
- कम से कम 7 वर्षों का विधि व्यवसाय का अनुभव।
- सरकार द्वारा नियुक्ति।
- अधिकार:
- अभियोजन का संचालन करना।
- न्यायालय में सबूत प्रस्तुत करना।
- मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना।
17. (क) जमानतीय अपराध (Bailable Offence)
उत्तर:
ऐसे अपराध जिनमें अभियुक्त को जमानत लेने का कानूनी अधिकार होता है, जैसे—साधारण चोरी, मारपीट।
(ख) गैर-जमानतीय अपराध (Non-Bailable Offence)
उत्तर:
वे अपराध जिनमें जमानत मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करती है, जैसे—हत्या, बलात्कार।
18. एक सम्यक् विचारण के आवश्यक अवयव (Essentials of a Fair Trial)
उत्तर:
- निष्पक्ष न्यायालय
- अभियुक्त का सुनवाई का अधिकार
- स्वतंत्र गवाहों की जाँच
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन
- निष्पक्ष निर्णय
19. किन परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी कर सकता है?
उत्तर:
CrPC की धारा 43 के अनुसार, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में गिरफ्तारी कर सकता है:
- यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता हुआ पाया जाए।
- यदि किसी व्यक्ति पर घोषित वारंट हो।
- यदि कोई अपराधी पुलिस से बचकर भाग रहा हो।
20. जमानत एवं पैरोल में अन्तर कीजिए।
उत्तर:
| आधार | जमानत (Bail) | पैरोल (Parole) |
|———–|—————–|—————–|
| अवधि | मुकदमे के दौरान दी जाती है | सजा के दौरान अस्थायी रूप से रिहाई |
| लक्ष्य | अभियुक्त को अस्थायी स्वतंत्रता देना | अच्छे आचरण के आधार पर अस्थायी रिहाई |
| प्रक्रिया | न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है | जेल प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाती है |
21. प्रथम सूचना रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? समझाइये।
उत्तर:
- परिभाषा: CrPC की धारा 154 के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) वह रिपोर्ट होती है, जो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर दर्ज की जाती है।
- महत्व:
- यह न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत करता है।
- पुलिस को अपराध की जाँच करने का आधार देता है।
- अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त हो सकता है।
22. प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्यिक महत्व (Evidentiary Value of FIR)
उत्तर:
- FIR प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होती, लेकिन इसका उपयोग विवेचना (investigation) में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में किया जाता है।
- इसका प्रयोग अभियुक्त के बचाव या अभियोजन पक्ष की पुष्टि के लिए किया जा सकता है।
- इसे स्वतः सत्य माना नहीं जाता, लेकिन विरोधाभास या समर्थन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
23. सर्च वारण्ट से क्या तात्पर्य है? (What is meant by Search Warrant?)
उत्तर:
सर्च वारंट एक न्यायिक आदेश है, जिसके माध्यम से पुलिस या अन्य अधिकृत अधिकारी किसी स्थान की तलाशी ले सकते हैं और आपत्तिजनक सामग्री को जब्त कर सकते हैं। यह CrPC की धारा 93-98 के अंतर्गत आता है।
24. फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की की प्रक्रिया कब प्रारम्भ होती है?
उत्तर:
- यदि कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध के लिए वांछित है और गिरफ्तारी से बच रहा है, तो CrPC की धारा 82 और 83 के तहत उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है।
- न्यायालय द्वारा “फरारी घोषित” करने के बाद उसकी चल-अचल संपत्ति को जब्त किया जाता है।
25. जाँच एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्तर समझाइए।
उत्तर:
| आधार | जाँच (Inquiry) | प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) |
|———|——————|———————|
| अर्थ | न्यायालय द्वारा प्रारंभिक जांच | पुलिस द्वारा अपराध की प्रारंभिक सूचना दर्ज करना |
| प्रक्रिया | न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा | पुलिस जांच का प्रारंभिक चरण |
| लक्ष्य | यह तय करना कि मुकदमा चलाया जाए या नहीं | अपराध की जांच शुरू करना |
26. दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार (Rights of an Arrested Person as per CrPC)
उत्तर:
CrPC की धारा 41D, 50, 50A, 54, 57, 167 आदि के अंतर्गत गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं—
- गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार।
- जमानत लेने का अधिकार (यदि अपराध जमानतीय है)।
- वकील से मिलने का अधिकार।
- 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार।
- चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार।
27. कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा लोक न्यूसेन्स हटाने हेतु आदेश
उत्तर:
CrPC की धारा 133 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह किसी सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance) को रोकने या हटाने के लिए आदेश पारित कर सकता है। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब—
- कोई सार्वजनिक स्थान बाधित हो।
- कोई गतिविधि जनहित के लिए हानिकारक हो।
- कोई संरचना सार्वजनिक खतरा उत्पन्न कर रही हो।
28. धारा 125 के अंतर्गत पत्नी एवं बच्चों के भरण-पोषण के अधिकार
उत्तर:
CrPC की धारा 125 के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति भरण-पोषण के हकदार होते हैं—
- पत्नी (यदि वह स्वयं निर्वाह करने में असमर्थ हो)।
- नाबालिग संतान (चाहे वैध हो या अवैध)।
- असमर्थ माता-पिता।
- यदि पुत्र वयस्क है लेकिन शारीरिक या मानसिक विकलांगता से ग्रस्त है, तो वह भी भरण-पोषण का अधिकारी है।
29. संज्ञेय अपराधों के निवारण हेतु पुलिस की शक्तियाँ (Powers of Police to Prevent Cognizable Offence)
उत्तर:
CrPC की धारा 149-153 के तहत पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होती हैं—
- संभावित अपराध को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना।
- संदेहास्पद व्यक्तियों से पूछताछ करना।
- संदिग्ध वस्तुओं को जब्त करना।
- गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करना।
- आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी करना।
30. पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
CrPC की धारा 161 के अनुसार, पुलिस को साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार होता है। इसमें—
- गवाहों के बयान लेना।
- अभियुक्त के विरुद्ध सबूत जुटाना।
- अपराध स्थल पर गवाहों से जानकारी प्राप्त करना।
- मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्षी के बयान को दर्ज कराना (धारा 164)।
31. (क) विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार (Powers of Special Executive Magistrate)
उत्तर:
विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को CrPC की धारा 21 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है और निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं—
- सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए आदेश देना।
- भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- कानून व्यवस्था के उल्लंघन पर कार्रवाई करना।
- आपराधिक मामलों में विशेष कार्यवाही करना।
(ख) महानगरीय मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate)
उत्तर:
- CrPC की धारा 16-19 के तहत महानगरीय मजिस्ट्रेट 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं।
- वे संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं।
- ये मुख्य रूप से प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं और बड़े शहरी क्षेत्रों में न्यायिक प्रक्रिया का संचालन करते हैं।
32. क्या माता-पिता अपने भरण-पोषण का दावा अपनी संतान पर कर सकते हैं?
उत्तर:
हाँ, माता-पिता अपनी संतान से भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। CrPC की धारा 125 के अनुसार, यदि माता-पिता असमर्थ हैं और स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, तो वे अपनी संतान (पुत्र या पुत्री) से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं।
33. भरण-पोषण को परिभाषित कीजिए। (Explain Maintenance)
उत्तर:
भरण-पोषण का अर्थ किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन या सहायता प्रदान करना है। CrPC की धारा 125 के अंतर्गत, यह आश्रितों जैसे पत्नी, नाबालिग संतान और असहाय माता-पिता को दिया जाता है।
34. (क) मजिस्ट्रेटों को दंड देने की शक्तियाँ (Powers of Magistrate regarding Punishment)
उत्तर:
CrPC की धारा 29 के अनुसार, मजिस्ट्रेटों की दंड देने की शक्तियाँ इस प्रकार हैं—
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) – अधिकतम 7 वर्ष की सजा दे सकते हैं।
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट – अधिकतम 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं।
- द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट – अधिकतम 1 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं।
(ख) कार्यकारी मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate)
उत्तर:
कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, धारा 144 लागू करने, और लोक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं।
35. (क) गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? (Arrest How Made?)
उत्तर:
CrPC की धारा 46 के अनुसार, गिरफ्तारी निम्नलिखित प्रकार से की जाती है—
- पुलिस अधिकारी अभियुक्त को स्पर्श करके या उसे नियंत्रित करके गिरफ्तार करता है।
- यदि अभियुक्त गिरफ्तारी से बचता है, तो बल प्रयोग किया जा सकता है।
- महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए विशेष नियम होते हैं (रात में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती)।
(ख) स्थानीय क्षेत्राधिकार (Local Jurisdiction)
उत्तर:
स्थानीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि किसी न्यायालय या पुलिस थाने की कानूनी शक्ति किस भौगोलिक क्षेत्र में लागू होती है।
36. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिये जाने वाले दण्डादेश (Sentences by High Court and Sessions Judges under Section 28 of CrPC)
उत्तर:
- उच्च न्यायालय (High Court) – कोई भी प्रकार की सजा दे सकता है, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है।
- सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge) –
- सत्र न्यायाधीश – मृत्युदंड दे सकता है (परंतु उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है)।
- अपर सत्र न्यायाधीश – अधिकतम 10 वर्ष की सजा और जुर्माना लगा सकता है।
37. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। (Objects of Section 144 of CrPC)
उत्तर:
धारा 144 का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। इसके तहत—
- लोक अशांति, दंगे और अवैध जमाव को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जाती है।
- जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट चार या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा सकता है।
- किसी विशेष क्षेत्र में हथियार ले जाने या इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
38. अन्वेषण (Investigation)
उत्तर:
अन्वेषण एक प्रक्रिया है, जिसमें पुलिस अधिकारी किसी अपराध से जुड़े तथ्यों की जांच करता है। इसमें—
- अपराध स्थल की जांच
- गवाहों और अभियुक्तों से पूछताछ
- साक्ष्यों का संग्रह और विश्लेषण
- न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करना (चार्जशीट) शामिल है।
39. अन्तरिम भरण-पोषण (Interim Maintenance)
उत्तर:
जब भरण-पोषण का अंतिम निर्णय लंबित होता है, तब अदालत अस्थायी रूप से भरण-पोषण देने का आदेश देती है, जिसे अंतरिम भरण-पोषण कहा जाता है। यह आमतौर पर CrPC की धारा 125(1) के तहत दिया जाता है।
40. संस्वीकृति (Confession)
उत्तर:
संस्वीकृति का अर्थ होता है, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार करना। यह दो प्रकार की होती है—
- न्यायिक संस्वीकृति (Judicial Confession) – मजिस्ट्रेट के सामने की गई।
- पुलिस के समक्ष संस्वीकृति (Extra-judicial Confession) – पुलिस या अन्य व्यक्ति के सामने की गई।
41. संक्षिप्त विचारण (Summary Trial)
उत्तर:
संक्षिप्त विचारण का अर्थ है, छोटे और साधारण मामलों की सुनवाई को शीघ्रता से पूरा करना। CrPC की धारा 260-265 के तहत, कुछ मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं।
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट – 2 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों के लिए।
- द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट – 6 महीने तक की सजा वाले अपराधों के लिए।
- इसमें साक्ष्यों की लिखित रिकॉर्डिंग संक्षिप्त होती है और प्रक्रिया को तेजी से निपटाया जाता है।
42. क्या साक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने पर दण्डित किया जा सकता है? (Can a witness be punished for not attending the Court?)
उत्तर:
हां, यदि साक्षी न्यायालय में उपस्थित होने से इनकार करता है, तो उसे CrPC की धारा 174 के तहत आदेश के बावजूद उपस्थित न होने पर दंडित किया जा सकता है। यदि साक्षी न्यायालय के सम्मन के बावजूद अनुपस्थित रहता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
43. अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति का उल्लेख कीजिए (Explain the power to examine the accused)
उत्तर:
CrPC की धारा 313 के तहत, न्यायालय को अभियुक्त से उसकी रक्षा के लिए कोई भी सवाल पूछने का अधिकार है। यह सवाल अभियुक्त के अपराध से संबंधित होते हैं और उसे अपनी सफाई में उत्तर देने का अवसर दिया जाता है। इसका उद्देश्य अभियुक्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना होता है।
44. अभिवाक् सौदेबाजी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए (Write short notes on Plea Bargaining)
उत्तर:
अभिवाक् सौदेबाजी (Plea Bargaining) एक प्रक्रिया है, जिसमें अभियुक्त आरोप स्वीकार करने के बदले में आरोपों के हल्के दंड के लिए सहमत होता है। यह प्रक्रिया CrPC की धारा 265A-265L के तहत 2005 में लागू की गई थी, और यह मुख्य रूप से छोटे अपराधों के लिए होती है। इसके लाभों में समय और संसाधन की बचत और जल्दी निर्णय प्राप्त करना शामिल है।
45. विचारण क्या है? विचारण एवं जाँच में क्या अन्तर है? (What is Trial? What is difference between Trial and Enquiry?)
उत्तर:
- विचारण (Trial): यह एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय द्वारा किसी अपराध के आरोपी के खिलाफ सबूतों और गवाहों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसमें साक्षी और अन्य सामग्री का परीक्षण किया जाता है।
- जांच (Enquiry): यह एक प्रारंभिक प्रक्रिया है, जिसमें अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जाती है, ताकि यह तय किया जा सके कि मामले में विचारण (Trial) होना चाहिए या नहीं।
अंतर:
- विचारण न्यायालय में होता है, जबकि जांच पुलिस या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाती है।
- विचारण में अभियुक्त का बचाव और अभियोजन पक्ष प्रस्तुत होते हैं, जबकि जांच मुख्य रूप से प्रारंभिक तथ्यों के संग्रहण तक सीमित होती है।
46. आदेशिका जारी करने की प्रक्रिया (Procedure for issue of process)
उत्तर:
CrPC की धारा 204 के अनुसार, न्यायालय द्वारा आदेशिका (process) तब जारी की जाती है जब उसे लगता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध की स्थिति बनती है।
- न्यायालय साक्ष्य और तथ्यों का मूल्यांकन करता है।
- अगर मामला दर्ज करने योग्य लगता है, तो वह अभियुक्त को सम्मन या वारंट जारी कर सकता है।
47. सत्र न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए (Describe the procedure for a trial before a Court of Session)
उत्तर:
सत्र न्यायालय में विचारण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है:
- आरोप निर्धारण: पहले सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त पर आरोप तय किए जाते हैं।
- साक्ष्य प्रस्तुत करना: अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी पेश किए जाते हैं और उनका परीक्षण किया जाता है।
- अभियुक्त का बयान: फिर अभियुक्त से उसका बयान लिया जाता है।
- निर्णय: यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है, तो सत्र न्यायालय दंड निर्धारित करता है।
48. परिवाद का संज्ञान (Cognizance of Complaint)
उत्तर:
CrPC की धारा 190 के अनुसार, न्यायालय द्वारा परिवाद का संज्ञान तब लिया जाता है जब—
- कोई व्यक्ति न्यायालय में लिखित शिकायत प्रस्तुत करता है।
- न्यायालय को लगता है कि उस शिकायत में अपराध का तात्पर्य है।
- न्यायालय पहले से उपलब्ध जानकारी के आधार पर भी संज्ञान ले सकता है।
49. निर्देश से क्या अभिप्राय है? (What is meant by reference?)
उत्तर:
निर्देश (Reference) का अर्थ होता है, किसी मामले को उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय को भेजना। यह CrPC की धारा 395 के तहत होता है, जब निचली अदालत किसी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर निर्णय नहीं ले पाती है और उच्च न्यायालय से मार्गदर्शन प्राप्त करती है।
50. पुनरीक्षण से क्या तात्पर्य है? पुनरीक्षण का प्रयोग कौन न्यायालय कर सकता है? स्पष्ट करें (What is meant by revision? Which Court can exercise it?)
उत्तर:
पुनरीक्षण (Revision) का अर्थ है, किसी उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के द्वारा निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करना।
- कौन कर सकता है: उच्च न्यायालय (CrPC की धारा 401) और सत्र न्यायालय (CrPC की धारा 399) पुनरीक्षण की शक्ति रखते हैं।
- यह प्रक्रिया तब होती है जब निचली अदालत का निर्णय कानूनी दृष्टिकोण से गलत, अनुचित या असंगत होता है।
51. अभियुक्त को उन्मोचित करने की प्रक्रिया (Process for the discharge of an accused)
उत्तर:
CrPC की धारा 227 और 239 के तहत, यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो वह उसे उन्मोचित कर सकता है।
- इसमें न्यायालय अभियुक्त को आरोप से मुक्त करने का आदेश देता है।
- यह प्रक्रिया आमतौर पर प्रारंभिक चरणों में होती है, जब कोई साक्ष्य या तथ्य नहीं होते हैं।
52. निर्देश या पुनरीक्षण में अन्तर कीजिए (Distinguish between Reference and Revision)
उत्तर:
| आधार | निर्देश (Reference) | पुनरीक्षण (Revision) |
|———-|———————-|————————–|
| अर्थ | उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा निचली अदालत से मार्गदर्शन लेना। | निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करना।
| अधिकार | यह न्यायालय द्वारा स्वयं प्राप्त किया जाता है। | यह पक्षकार द्वारा दाखिल किया जाता है।
| प्रभाव | न्यायालय नए आदेश के लिए संदर्भित करता है। | निर्णय में सुधार, संशोधन या रद्द किया जा सकता है।
53. दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुधार हेतु चार सुझाव दीजिए (Give four suggestions for reforming Code of Criminal Procedure)
उत्तर:
- त्वरित न्याय: जमानत और विचारण की प्रक्रिया को त्वरित किया जाए ताकि मामले लंबित न रहें।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: डिजिटल रिकॉर्डिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में साक्षियों का परीक्षण किया जा सकता है।
- साक्षी संरक्षण: साक्षियों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधान बनाए जाएं ताकि वे गवाही देने से डरें नहीं।
- अधिकारों का संरक्षण: गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान आरोपी के अधिकारों को सख्ती से सुनिश्चित किया जाए।
54. सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण शक्तियाँ (Revisional Powers of Session’s Judge)
उत्तर:
सेशन न्यायाधीश के पास पुनरीक्षण की शक्ति होती है, जो उसे CrPC की धारा 399 और 400 के तहत दी जाती है। यह शक्ति उसे निचली अदालतों के आदेशों की समीक्षा और सुधार करने का अधिकार देती है। सेशन न्यायाधीश पुनरीक्षण के दौरान न्यायालय के आदेशों, फैसलों, या फैसलों में कोई त्रुटि पाए जाने पर उन्हें सही कर सकता है।
55. उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय की जमानत सम्बन्धी शक्तियों के विषय में आप क्या जानते हैं? (What do you know about the powers of the High Court and Session Court regarding bail?)
उत्तर:
उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों के पास जमानत देने की शक्ति होती है।
- सत्र न्यायालय: CrPC की धारा 439 के तहत, सत्र न्यायालय के पास किसी भी आरोपी को जमानत पर रिहा करने का अधिकार है। यह शक्ति अपील करने वाले मामलों में भी काम आती है।
- उच्च न्यायालय: CrPC की धारा 439 के तहत, उच्च न्यायालय किसी आरोपी को जमानत देने की शक्ति रखता है, खासकर जब सत्र न्यायालय ने जमानत से इनकार किया हो।
56. अपील एवं पुनरीक्षण में अन्तर बताइये (Distinguish between Appeal and Revision)
उत्तर:
| आधार | अपील (Appeal) | पुनरीक्षण (Revision) |
|———-|——————-|————————–|
| अर्थ | अपील एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करने की प्रक्रिया है। | पुनरीक्षण, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा निचली अदालत के आदेशों की त्रुटियों की समीक्षा करने की प्रक्रिया है।
| प्रवृत्ति | अपील की प्रक्रिया का उद्देश्य एक नई सुनवाई होती है। | पुनरीक्षण में केवल पहले से पारित आदेश की समीक्षा की जाती है।
| न्यायिक स्थिति | अपील एक कानूनी अधिकार है। | पुनरीक्षण न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है।
57. मिच्या साक्ष्य देने पर विचारण करने की संक्षिप्त प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए (Explain the brief procedure of trial for giving false evidence)
उत्तर:
मिच्या साक्ष्य (False Evidence) देने पर अपराधी के खिलाफ CrPC की धारा 191 और 192 के तहत विचारण किया जाता है। इस प्रक्रिया में:
- साक्षी को आरोपित किया जाता है कि उसने झूठा बयान दिया।
- अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं।
- यदि साक्ष्य झूठे पाए जाते हैं, तो न्यायालय साक्षी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।
- मिच्या साक्ष्य देने पर सजा भी हो सकती है, जैसे कि IPC की धारा 193 के तहत दो साल तक की सजा।
58. सेशन न्यायालय (Court of Session)
उत्तर:
सेशन न्यायालय उच्चतम न्यायालय का हिस्सा होता है और यह CrPC की धारा 9 के तहत सजा देने और अपराधों के विचारण का कार्य करता है। यह विशेष रूप से गंभीर अपराधों (जैसे हत्या, बलात्कार आदि) के मामलों का निपटारा करता है। सेशन न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य सुनने के बाद सजा सुनाई जाती है।
59. भूल का प्रभाव (Effect of Errors)
उत्तर:
भूल (Errors) का प्रभाव एक न्यायिक प्रक्रिया में हो सकता है, जैसे:
- साक्ष्य से जुड़ी भूलें: यदि किसी साक्ष्य को गलत तरीके से स्वीकार किया गया है, तो उसे निरस्त किया जा सकता है।
- प्रक्रियागत भूलें: यदि किसी आदेश या प्रक्रिया में तकनीकी भूल होती है, तो उसे संशोधित किया जा सकता है।
- सजा की भूल: यदि सजा में कोई भूल होती है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उसे सुधार सकता है।
60. पुलिस के उच्च अधिकारियों की शक्तियाँ (Powers of superior officers of Police)
उत्तर:
पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास CrPC की धारा 36 के तहत कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं:
- उन्हें किसी अपराध के संदर्भ में जांच और साक्ष्य एकत्र करने का अधिकार है।
- वे किसी भी स्थान पर तलाशी ले सकते हैं और जब आवश्यक हो तो गिरफ्तारी कर सकते हैं।
- वे अपनी शक्ति का प्रयोग करके सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं।
61. कब जमानत की माँग अधिकार स्वरूप की जा सकती है? (When demand of Bail can be exercised as right)
उत्तर:
CrPC की धारा 437 और 438 के तहत, जमानत की मांग अधिकार स्वरूप तब की जा सकती है जब:
- बेलाय जमानत अपराध: यदि अपराध जमानत योग्य है और आरोपी पर गंभीर आरोप नहीं हैं।
- अवसर का प्रमाण: आरोपी पहले से निर्दोष पाया गया है या उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
62. उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ बतलाइये? (State the inherent powers of the High Court)
उत्तर:
उच्च न्यायालय के पास CrPC की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, जो उसे किसी भी मामले में न्याय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार देती हैं। इनमें:
- मामलों को निपटाने के लिए गैर-स्थायी आदेश जारी करना।
- आदेशों और निर्णयों को रद्द करना जो किसी त्रुटि की वजह से गलत हो।
- जनहित में कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार रखना।
63. अग्रिम जमानत से आप क्या समझते हैं? (What do you understand by Anticipatory Bail?)
उत्तर:
अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) एक प्रकार की जमानत है जो व्यक्ति को अपराधी बनने से पहले ही मिल सकती है, ताकि वह गिरफ्तार न हो। यह CrPC की धारा 438 के तहत दी जाती है और तब होती है जब किसी व्यक्ति को यह डर हो कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और वह गिरफ्तारी से पहले न्यायालय से जमानत की मांग करता है।
64. शमन एवं समझौते के अभिवचन पर टिप्पणी कीजिए (Comment on ‘Compounding’ and Concept of Plea Bargaining)
उत्तर:
- शमन (Compounding): यह तब होता है जब अपराध के पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता हो जाता है और वे मामले को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं। कुछ अपराधों में शमन किया जा सकता है, जैसे कि द्वाराचार या चोटें।
- प्ली बARGेनिंग (Plea Bargaining): यह एक समझौता प्रक्रिया है जिसमें अभियुक्त आरोप स्वीकार कर लेता है और बदले में हल्की सजा या अपराध को कम करने की संभावना होती है। यह प्रक्रिया CrPC की धारा 265A-265L के तहत स्थापित की गई है।
65. वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता की चार प्रमुख कमियाँ (Four major shortcomings of present Code of Criminal Procedure)
उत्तर:
- विलंबित न्याय: न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण अभियुक्तों और पीड़ितों को लंबा इंतजार करना पड़ता है।
- साक्षी सुरक्षा की कमी: साक्षियों के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे वे अपने बयान देने में डरते हैं।
- संवेदनशीलता का अभाव: महिला अपराधों और बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता की कमी है।
- प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त उपयोग: न्यायिक प्रक्रिया में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं होने के कारण प्रक्रिया धीमी होती है।