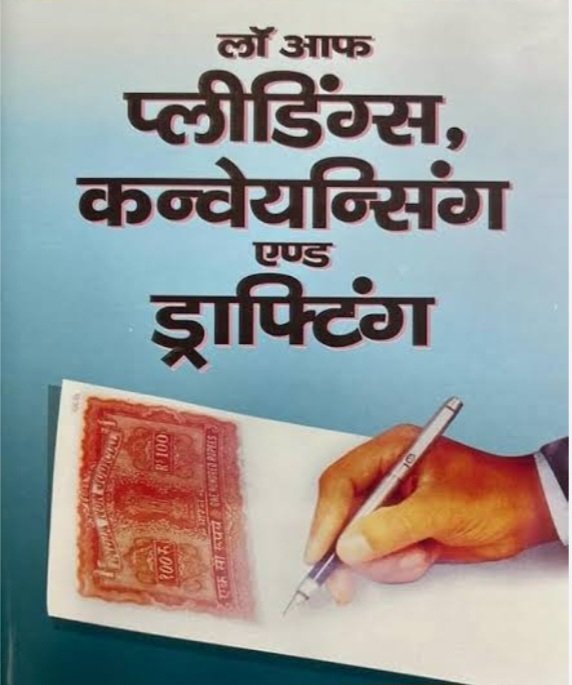-
अभिवचन (Pleading) का अर्थ, विकास एवं मुख्य उद्देश्य:
अभिवचन का अर्थ है, किसी कानूनी विवाद में पक्षकारों द्वारा न्यायालय में अपनी स्थिति और तर्क प्रस्तुत करना। यह प्रायः लिखित रूप में होता है, जिसमें तथ्यों और कानूनी आधारों का उल्लेख किया जाता है। अभिवचन के मुख्य उद्देश्य में शामिल हैं:
- न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करना।
- दोनों पक्षों के बीच विवाद के मुद्दों को निर्धारित करना।
- न्यायालय को उचित निर्णय लेने में सहायता देना।
विकास:
प्रारंभ में, अभिवचन का विकास बहुत सीमित था, और केवल मौखिक दावों पर आधारित था। समय के साथ, इसकी विधि और प्रक्रिया में सुधार हुआ, और इसे लिखित रूप में दर्ज किया जाने लगा, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो सकी। - अभिवचन के आधारभूत नियम एवं उनके विशेष नियम:आधारभूत नियम:
- सारांश तथ्य (Material Facts): प्रत्येक अभिवचन में केवल सारांश तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- साक्ष्य के रूप में नहीं: अभिवचन में साक्ष्य (Evidence) का उल्लेख नहीं किया जाता, केवल तथ्यों का उल्लेख होता है।
- स्पष्टता: अभिवचन में शब्दों का चयन और उनकी प्रस्तुति इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि न्यायालय आसानी से समझ सके।
विशेष नियम:
- अभिवचन में जटिलताओं से बचते हुए, केवल आवश्यक और महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- प्रक्रिया में उल्लंघन करने पर उस अभिवचन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- अभिवचन के निर्वचन (Interpretation of Pleadings):
अभिवचन का निर्वचन, अदालत द्वारा अभिवचन के शब्दों और उनके संदर्भ की व्याख्या करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभिवचन में उल्लिखित तथ्यों और कानूनी मुद्दों का सही अर्थ समझा जाए। इसके अंतर्गत यह देखना होता है कि क्या अभिवचन में दिए गए तथ्य और उनके आधार उचित और वैध हैं। - (i) ‘प्रत्येक अभिवचन में तथ्यों का अभिकथन किया जाना चाहिए, न कि विधि का’:
इस नियम का अर्थ है कि अभिवचन में केवल घटनाओं और तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि उनसे संबंधित कानून या कानूनी सिद्धांतों का। विधि या कानून का उल्लेख अदालत द्वारा किया जाएगा, न कि अभिवचन में।
अपवाद:- यदि कानून का आवेदन सीधे तौर पर किसी तथ्य से संबंधित है, तो उसका उल्लेख अभिवचन में किया जा सकता है, जैसे कि किसी विशेष कानून के तहत अधिकार का उल्लंघन।
(ii) ‘प्रत्येक अभिवचन में सब सारवान् तथ्यों तथा केवल सारवान् तथ्यों का अभिकथन किया जाना चाहिए’:
इसका मतलब है कि अभिवचन में उन तथ्यों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए जो मुकदमे के फैसले के लिए महत्वपूर्ण हैं। केवल वे तथ्य जो कानूनी विवाद को प्रभावित करते हैं, उन्हें ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
अपवाद:- कभी-कभी कुछ परिधीय तथ्य या संदर्भ देने की आवश्यकता हो सकती है जो किसी मुख्य तथ्य को समझाने के लिए आवश्यक हो।
- अभिवचन और प्रमाण में भिन्नता:अभिवचन और प्रमाण में मुख्य भिन्नता यह है कि अभिवचन केवल तथ्यों की प्रस्तुति होती है, जबकि प्रमाण में उन तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अभिवचन में आरोपित तथ्य होते हैं, जबकि प्रमाण में उनका समर्थन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है।नियम:
- अभिवचन में केवल तथ्यों का उल्लेख किया जाता है, साक्ष्य नहीं। प्रमाण का कार्य अदालत द्वारा किया जाता है, न कि पक्षकारों द्वारा।
घातक नहीं होना:
इस नियम का मतलब है कि हर छोटी सी भिन्नता अभिवचन और प्रमाण के बीच न तो निर्णय को प्रभावित करती है, और न ही मुकदमा नष्ट करती है। यह जरूरी नहीं कि हर भिन्नता कानूनी प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे।
- विशिष्टियाँ (Particulars) का अर्थ और आवश्यकताएँ:विशिष्टियाँ या विवरण उन विशेष तथ्यों, घटनाओं, या परिस्थितियों को कहा जाता है जो किसी दावे या प्रतिवाद को स्पष्ट और समझने योग्य बनाने के लिए अभिवचन में शामिल किए जाते हैं। यह आमतौर पर तब आवश्यक होती हैं जब किसी पक्ष द्वारा दावा किया गया तथ्य पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होता, या जब अदालत को विवादित मुद्दों को समझने के लिए और जानकारी की आवश्यकता होती है।विशिष्टियों का दिया जाना आवश्यक है जब:
- किसी दावा में असमान्य या जटिल तथ्य शामिल हों।
- किसी पक्ष द्वारा पेश किए गए तथ्यों में अस्पष्टता या कमी हो।
- किसी कानून के तहत किसी विशेष घटना के विवरण की आवश्यकता हो।
- अभिवचनों का संशोधन (Amendment of Pleadings):अभिवचन का संशोधन तब किया जाता है जब पक्षकार को अपनी दलीलों में सुधार, जोड़, या हटाने की आवश्यकता हो। यह प्रक्रिया उस समय आवश्यक होती है जब किसी पक्षकार को महसूस हो कि अभिवचन में कुछ गलत या अधूरी जानकारी दी गई है या अगर नई जानकारी या दलील को जोड़ने की आवश्यकता हो।अभिवचनों में संशोधन के प्रकार:
- सिद्धांत संशोधन: जब किसी तथ्य या तर्क को जोड़ने की आवश्यकता होती है।
- प्रासंगिकता का संशोधन: जब किसी तथ्य को हटाने या बदलने की आवश्यकता होती है।
- साक्ष्य में बदलाव: यदि साक्ष्य में कोई नया तथ्य सामने आता है।
संशोधन के लिए सामान्य सिद्धांत:
- संशोधन की अनुमति तभी दी जाती है जब यह मुकदमा में उचित है और न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आती।
- यह केवल उन मामलों में अनुमत है जहाँ बिना किसी अन्य पक्ष को नुकसान पहुँचाए न्याय की प्राप्ति हो सके।
- विधिक प्रावधानों के तहत, यह समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।
- अभिवचनों के संशोधन की अनुमति न देने की परिस्थितियाँ:अभिवचन में संशोधन की अनुमति तब नहीं दी जाती जब:
- यह मुकदमे को अनावश्यक रूप से विलंबित करता है।
- संशोधन से किसी पार्टी को अनावश्यक नुकसान या नुकसान पहुँच सकता है।
- यदि संशोधन मूल रूप से एक नया दावा या विवाद उत्पन्न करता है, जो मुकदमे के मौजूदा मुद्दों से बाहर हो।
निर्णीत वादों के हवाले से:
- Order 6 Rule 17, CPC के तहत संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती यदि यह मुकदमे की प्रक्रिया को अव्यवस्थित या अन्य पक्ष को असमान रूप से प्रभावित करता हो।
- Nathulal v. State of Madhya Pradesh में न्यायालय ने यह माना कि यदि कोई संशोधन न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है तो इसे अस्वीकार किया जा सकता है।
- वैकल्पिक एवं असंगत दलीलें (Alternative and Inconsistent Pleas):वैकल्पिक दलीलें वे होती हैं जो किसी एक तर्क पर निर्भर नहीं होतीं, बल्कि विभिन्न संभावित परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत की जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक पक्ष एक दावे को साबित करने के लिए दो अलग-अलग सिद्धांतों का पालन कर सकता है। असंगत दलीलें वह होती हैं जो एक-दूसरे के विपरीत होती हैं और एक समय में दोनों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।निर्णीत वादों के हवाले से:
- S. Ramaswamy v. K. S. Ramaswamy में न्यायालय ने वैकल्पिक दलीलों को स्वीकार किया और कहा कि जब तक वे असंगत न हों, तब तक उनका कोई विरोध नहीं है।
- असंगत दलीलें नहीं स्वीकार की जाती हैं, क्योंकि वे पक्षकार की स्थिति में भ्रम उत्पन्न कर सकती हैं।
- वाद-पत्र (Plaint) की परिभाषा और उसके विभिन्न भाग:
वाद-पत्र (Plaint) वह लिखित दस्तावेज होता है जिसे कोई पक्षकार न्यायालय में किसी मामले को दायर करने के लिए प्रस्तुत करता है। इसमें उस पक्षकार द्वारा दावा किए गए तथ्यों और कानूनी आधारों का विवरण होता है।
वाद-पत्र के विभिन्न भाग:
- शीर्षक और विवरण: इसमें मुकदमे का नाम, पक्षकारों के विवरण और न्यायालय का नाम होता है।
- दावों का विवरण: इसमें उन दावों का विस्तार से वर्णन होता है जो पक्षकार न्यायालय से चाहता है।
- तथ्यों का वर्णन: इसमें वे सभी तथ्य और घटनाएँ होती हैं जो दावे को समर्थन देने के लिए पेश की जाती हैं।
- कानूनी आधार: यह उस कानून का उल्लेख करता है जिस पर दावे का आधार है।
- समाप्ति: इसमें पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर और तारीख का उल्लेख किया जाता है।
- लिखित कथन (Written Statement) का अर्थ और अनिवार्यताएँ:
7. लिखित कथन (Written Statement) वह दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी पक्ष अपनी स्थिति और दावे का उत्तर देता है। इसमें वह सभी तथ्यों और कानूनी आधारों का उल्लेख करता है, जिनका वह समर्थन करता है या विरोध करता है।
लिखित कथन की अनिवार्यताएँ:
- प्रतिवादी को सभी आरोपों का स्पष्ट उत्तर देना आवश्यक है।
- यदि प्रतिवादी को किसी तथ्यों पर आपत्ति है, तो उसे उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।
- प्रतिवादी को यह भी उल्लेख करना चाहिए कि उसके पास क्या साक्ष्य है, जो उसकी स्थिति को सही साबित कर सके।
12.
(अ) बकाया किराये की वसूली और किरायेदार को बेदखल करने के लिए वाद-पत्र (Plaint) का प्रारूप:
वाद-पत्र का प्रारूप:
मुहम्मदाबाद न्यायालय
विवाद संख्या: _______
दिनांक: ___________
वादी:
मन्नू लाल, निवासी [पता] (मकान मालिक)
प्रतिवादी:
मायाराम, निवासी [पता] (किरायेदार)
विषय: बकाया किराए की वसूली और किरायेदार की बेदखली के लिए वाद
मान्य न्यायालय के समक्ष,
समान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है:
- वादी मन्नू लाल एक मकान का स्वामी है, जिसका पता [पता] है।
- प्रतिवादी मायाराम उक्त मकान के एक हिस्से में किराये पर निवास करता है, और यह किरायेदारी [समझौता दिनांक] को प्रारंभ हुई थी।
- प्रतिवादी ने पिछले 10 महीने से किराया अदा नहीं किया है, जिससे वादी को कुल बकाया किराया [राशि] रुपये बन चुका है।
- वादी ने कई बार प्रतिवादी से किराया वसूलने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिवादी ने भुगतान करने से इंकार कर दिया।
- वादी के पास किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार है क्योंकि वह किराया अदा नहीं कर रहा है।
- वादी ने प्रतिवादी को नोटिस भेजा था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
अतः वादी निवेदन करता है कि न्यायालय:
- प्रतिवादी से बकाया किराया [राशि] रुपये वसूल करने का आदेश दे।
- प्रतिवादी को मकान से तत्काल बेदखल करने का आदेश दे।
- अन्य उचित आदेश जारी करने की कृपा करें।
वादी का नाम: मन्नू लाल
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
(ब) प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित कथन (Written Statement) का प्रारूप:
मुहम्मदाबाद न्यायालय
विवाद संख्या: _______
दिनांक: ___________
प्रतिवादी:
मायाराम, निवासी [पता]
वादी:
मन्नू लाल, निवासी [पता]
विषय: बकाया किराये की वसूली और किरायेदार की बेदखली पर प्रतिवादी का लिखित कथन
मान्य न्यायालय के समक्ष,
प्रतिवादी, मायाराम, निम्नलिखित लिखित कथन प्रस्तुत करता है:
- प्रतिवादी ने वादी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है।
- प्रतिवादी मानता है कि वह किरायेदार है, लेकिन बकाया किराया वसूलने के लिए वादी की ओर से भेजे गए नोटिस में तथ्यों की ग़लत व्याख्या की गई है।
- प्रतिवादी ने समय पर किराया अदा किया है और इसके बावजूद कुछ भुगतान वादियों द्वारा आरोपित किया गया है।
- प्रतिवादी ने समय समय पर वादी से किराया की समस्याओं के बारे में संवाद किया था।
- प्रतिवादी यह भी दावा करता है कि वादी की ओर से भेजे गए नोटिस का कोई वैध आधार नहीं है।
अतः प्रतिवादी निवेदन करता है कि न्यायालय:
- वादी के दावे को खारिज करे।
- वादी के खिलाफ उचित निर्देश जारी करे।
- अन्य उचित आदेश जारी करने की कृपा करें।
प्रतिवादी का नाम: मायाराम
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
(स) वाद-बिन्दुओं की रचना:
- क्या वादी का दावा सही है कि प्रतिवादी ने 10 महीने से किराया नहीं अदा किया है?
- क्या वादी का नोटिस वैध था और क्या यह निर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी को किराया का भुगतान करना चाहिए था?
- क्या प्रतिवादी की ओर से उठाए गए आरोप सही हैं कि उसने समय पर किराया अदा किया है?
- क्या वादी को प्रतिवादी को बेदखल करने का अधिकार है?
13. तीव्र और उपेक्षापूर्ण वाहन चालन के कारण पहुँची चोटों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु वाद-पत्र (Plaint) का प्रारूप:
मुहम्मदाबाद न्यायालय
विवाद संख्या: _______
दिनांक: ___________
वादी:
[नाम], निवासी [पता]
प्रतिवादी:
[नाम], निवासी [पता] (वाहन चालक)
विषय: तीव्र और उपेक्षापूर्ण वाहन चालन के कारण हुई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली
मान्य न्यायालय के समक्ष,
- वादी [तारीख] को प्रतिवादी द्वारा चलाए गए वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
- प्रतिवादी ने गाड़ी तेज गति से चलाने के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था, जिससे वादी को गंभीर चोटें आईं।
- वादी को चिकित्सीय इलाज की आवश्यकता पड़ी, और उपचार पर खर्च हुए पैसे की वसूली वादी अब करना चाहता है।
- प्रतिवादी की लापरवाही और उपेक्षापूर्ण वाहन चालन के कारण वादी की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति पर भारी असर पड़ा है।
अतः वादी निवेदन करता है कि न्यायालय:
- प्रतिवादी से वादी को क्षतिपूर्ति [राशि] रुपये देने का आदेश दे।
- अन्य उचित आदेश जारी करने की कृपा करें।
वादी का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
14. प्रोनोट के आधार पर उधार दिये गये धन की वसूली हेतु वाद-पत्र (Plaint) का प्रारूप:
मुहम्मदाबाद न्यायालय
विवाद संख्या: _______
दिनांक: ___________
वादी:
[नाम], निवासी [पता]
प्रतिवादी:
[नाम], निवासी [पता]
विषय: प्रोनोट के आधार पर उधार दिये गये धन की वसूली
मान्य न्यायालय के समक्ष,
- वादी ने [तारीख] को प्रतिवादी को [राशि] रुपये उधार दिए थे, जिसका स्पष्ट प्रमाण प्रोनोट [तारीख] में मौजूद है।
- प्रतिवादी ने वादा किया था कि वह धन [तारीख] तक चुका देगा, लेकिन वह समय पर भुगतान करने में विफल रहा है।
- वादी ने कई बार प्रतिवादी से भुगतान करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।
- अब वादी को अपने उधार धन की वसूली की आवश्यकता है।
अतः वादी निवेदन करता है कि न्यायालय:
- प्रतिवादी से उधार धन [राशि] रुपये की वसूली का आदेश दे।
- अन्य उचित आदेश जारी करने की कृपा करें।
वादी का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
15. (अ) संविदा के पालन के वाद के लिए वाद-पत्र का प्रारूप:
मुहम्मदाबाद न्यायालय
विवाद संख्या: _______
दिनांक: ___________
वादी:
[नाम], निवासी [पता]
प्रतिवादी:
[नाम], निवासी [पता]
विषय: संविदा के पालन के लिए वाद
मान्य न्यायालय के समक्ष,
- वादी और प्रतिवादी के बीच [तारीख] को एक संविदा हस्ताक्षरित हुई थी, जिसमें प्रतिवादी ने [कर्म] करने का वादा किया था।
- प्रतिवादी ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया और संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया।
- वादी को इस उल्लंघन से नुकसान हुआ है और वह न्याय की प्राप्ति चाहता है।
अतः वादी निवेदन करता है कि न्यायालय:
- प्रतिवादी को संविदा का पालन करने का आदेश दे।
- वादी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उचित क्षतिपूर्ति का आदेश दे।
- अन्य उचित आदेश जारी करने की कृपा करें।
वादी का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
(ब) लिखित कथन (Written Statement) का प्रारूप:
प्रतिवादी का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
17. (a) शपथ पत्र (Affidavit) का आशय और तैयार करने के महत्वपूर्ण बिंदु:
शपथ पत्र का आशय: शपथ पत्र एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा शपथ के साथ सत्य होने की पुष्टि की जाती है। इसे आमतौर पर न्यायालय, सरकारी विभाग या किसी अन्य अधिकृत संस्था के सामने प्रस्तुत किया जाता है। शपथ पत्र में व्यक्ति द्वारा दिए गए तथ्यों और जानकारी की सत्यता की पुष्टि की जाती है। यह दस्तावेज़ उस व्यक्ति के हस्ताक्षर और शपथ के साथ होता है और आमतौर पर न्यायालय में प्रमाणित किया जाता है।
शपथ पत्र तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें:
- सत्यता: शपथ पत्र में दिए गए सभी तथ्य सच्चे होने चाहिए।
- साक्षात्कार: शपथ पत्र में हस्ताक्षर से पहले संबंधित व्यक्ति को शपथ के साथ पुष्टि करनी चाहिए।
- स्पष्टता: शपथ पत्र को साफ और समझने योग्य भाषा में लिखा जाना चाहिए, ताकि न्यायालय या संबंधित प्राधिकरण को किसी प्रकार की समस्या न हो।
- प्रमाण: शपथ पत्र पर संबंधित अधिकारी या न्यायालय से प्रमाणित हस्ताक्षर की आवश्यकता हो सकती है।
- तारीख और स्थान: शपथ पत्र पर तारीख और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि इसकी वैधता सुनिश्चित हो सके।
(b) शपथ पत्र में संशोधन किया जा सकता है?
शपथ पत्र में संशोधन संभव है, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब उसमें किसी प्रकार की गलती हो या जब नई जानकारी उपलब्ध हो, जो पहले शामिल नहीं की गई थी। संशोधन के लिए एक नया शपथ पत्र तैयार किया जा सकता है और फिर से शपथ ली जाती है। हालांकि, एक बार शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद, उसमें कोई भी संशोधन करना पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए इस पर उचित कानूनी सलाह लेनी चाहिए।
काल्पनिक नामों के आधार पर शपथ पत्र का प्रारूप:
शपथ पत्र का प्रारूप:
शपथ पत्र
मैं, [नाम], पुत्र/पुत्री [पिता का नाम], निवासी [पता], यह शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित तथ्य सत्य और सही हैं:
- मेरी जन्मतिथि [जन्मतिथि] है।
- मैं वर्तमान में [पता] में निवास करता हूँ।
- उपरोक्त सभी तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।
- मुझे यह समझाया गया है कि इस शपथ पत्र में दिए गए किसी भी तथ्य में कोई झूठ या भ्रम हो, तो मैं कानूनी दंड का भागी बन सकता हूँ।
यह शपथ पत्र मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से, बिना किसी दबाव के, और सही तथ्यों के आधार पर तैयार किया है।
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
हस्ताक्षर: ____________________
(शपथ लेने वाले व्यक्ति का नाम)
शपथकर्ता का नाम: [नाम]
साक्षी का नाम: [साक्षी का नाम] (यदि आवश्यक हो)
18. (a) अपील (Appeal) का आशय और प्रारूप:
अपील का आशय: अपील एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक पक्षकार किसी अदालत के निर्णय को उच्च न्यायालय या किसी अन्य अधिकृत न्यायालय में चुनौती देता है। अपील का उद्देश्य निचली अदालत के फैसले को बदलवाना या उसे सुधारना होता है। अपील की प्रक्रिया में, अपीलीय न्यायालय निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करता है और आवश्यकतानुसार नया आदेश जारी करता है।
काल्पनिक तथ्यों के आधार पर अपील का प्रारूप:
अपील का प्रारूप:
आवेदनकर्ता:
[अपीलकर्ता का नाम], निवासी [पता]
प्रतिवादी:
[प्रतिवादी का नाम], निवासी [पता]
संबंधित न्यायालय:
[निचली अदालत का नाम]
अपील संख्या: [संख्या]
तारीख: [तारीख]
विषय: अपील दायर करने हेतु
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [अपीलकर्ता का नाम], इस अपील को प्रस्तुत करता हूँ।
- निचली अदालत ने दिनांक [तारीख] को मामले में निर्णय दिया था, जिसे मैंने असहमति जताई है।
- निचली अदालत का निर्णय गलत था और कानूनी दृष्टिकोण से असंवैधानिक था।
- निर्णय के कारण मुझे भारी नुकसान हुआ है, और मुझे न्याय प्राप्ति हेतु अपील का सहारा लेना पड़ रहा है।
अतः अपीलकर्ता निवेदन करता है कि न्यायालय:
- निचली अदालत के निर्णय को खारिज करे।
- मामले में न्यायसंगत निर्णय देने की कृपा करें।
- अन्य उचित आदेश जारी करें।
अपीलकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
(b) पुनरीक्षण हेतु आवेदन (Review Application) का प्रारूप:
पुनरीक्षण आवेदन का प्रारूप:
आवेदनकर्ता:
[आवेदनकर्ता का नाम], निवासी [पता]
प्रतिवादी:
[प्रतिवादी का नाम], निवासी [पता]
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
विवाद संख्या: [संख्या]
तारीख: [तारीख]
विषय: निर्णय की पुनरीक्षण हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], इस आवेदन के माध्यम से आपके सम्माननीय न्यायालय से निवेदन करता हूँ कि [निर्णय का विवरण] को पुनः समीक्षा किया जाए।
- मुझे यह ज्ञात हुआ है कि निर्णय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य की अनदेखी की गई है।
- पुनरीक्षण की आवश्यकता है ताकि न्यायसंगत और सही निर्णय लिया जा सके।
अतः आवेदनकर्ता निवेदन करता है कि न्यायालय:
- निर्णय का पुनरीक्षण करें।
- सही और न्यायसंगत आदेश जारी करें।
- अन्य उचित आदेश जारी करें।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
19. (a) याचिका (Petition) का आशय और आवश्यक तत्व:
याचिका का आशय: याचिका एक लिखित आवेदन होती है जिसे किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय या किसी अन्य सरकारी अथवा प्राधिकृत निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। याचिका में व्यक्ति अपने अधिकारों या किसी कानूनी प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे पर न्याय की मांग करता है।
याचिका के आवश्यक तत्व:
- शिकायत या आवेदन: याचिका में व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत या आवेदन का विवरण।
- तथ्यों का उल्लेख: याचिका में उन सभी तथ्यों का उल्लेख किया जाता है जिनके आधार पर न्याय की मांग की जा रही है।
- कानूनी आधार: याचिका में वे कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है जिनके तहत आवेदन किया गया है।
- निवेदन: याचिका में अदालत या प्राधिकृत निकाय से की गई अपेक्षाएँ और आदेश की मांग।
- हस्ताक्षर और तारीख: याचिका में याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर और तारीख का उल्लेख जरूरी होता है।
20. निम्नलिखित के विषय में बतलाइये:
(1) वादकालीन आदेश (Interlocutory Order):
वादकालीन आदेश वह आदेश होते हैं जो मुकदमे के दौरान किसी पक्ष द्वारा आवेदन करने पर न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं। ये आदेश मुकदमे की मुख्य सुनवाई से पहले आते हैं और मुख्य मुकदमे पर कोई स्थायी निर्णय नहीं होते हैं, बल्कि समय-समय पर फैसले होते हैं जो मामले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी व्यक्ति को तात्कालिक राहत देने के लिए जारी आदेश या किसी दस्तावेज़ की उपलब्धता की दिशा में आदेश आदि।
(2) निष्पादन (Execution):
निष्पादन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायालय के निर्णय को लागू किया जाता है। यदि कोई पक्षकार न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करता है, तो अदालत निष्पादन आदेश जारी कर सकती है, ताकि निर्णय को साकार किया जा सके। निष्पादन में वह उपाय आते हैं, जैसे संपत्ति की जब्ती, ऋण की वसूली, या अन्य उपाय जो आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक होते हैं।
21. आपराधिक मामलों में अभिवचन और परिवाद का आशय:
अभिवचन (Pleading) का आशय: आपराधिक मामलों में अभिवचन से तात्पर्य उस दस्तावेज़ से है, जिसमें अभियुक्त या प्रतिवादी की ओर से आरोपों का विवरण और उत्तर दिया जाता है। इसमें अभियुक्त या प्रतिवादी अपनी स्थिति और पक्ष को स्पष्ट करता है, ताकि मामले में एक साफ-सुथरी स्थिति सामने आ सके।
परिवाद (Complaint) का आशय: परिवाद एक औपचारिक लिखित शिकायत होती है, जिसे किसी अपराध के बारे में संबंधित अधिकारी या न्यायालय के पास दायर किया जाता है। इसमें अपराध का विवरण, आरोप और घटनाओं का ब्यौरा होता है, जिसे अपराध के अपराधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
परिवाद का प्रारूप:
परिवाद का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
परिवादी:
[नाम], [पता]
प्रतिवादी:
[नाम], [पता]
विषय: अपराध की शिकायत
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [परिवादी का नाम], [पता], यह शिकायत दर्ज कर रहा हूँ कि [प्रतिवादी का नाम], निवासी [पता], ने [अपराध का विवरण] किया है।
- घटनाएँ इस प्रकार हुईं:
- [घटना का विस्तृत विवरण]
- मैं यह शिकायत कर रहा हूँ कि यह अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा [धारा का उल्लेख] के अंतर्गत आता है।
- मैं न्यायालय से निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त अपराध के मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
परिवादी का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
22. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत एक परिवाद का परिचय प्रस्तुत करें:
धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता (IPC) के तहत “हत्या की कोशिश” से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारने की कोशिश की हो, तो वह धारा 307 के अंतर्गत अपराधी माना जाता है, जो एक गंभीर अपराध है।
परिवाद का परिचय (धारा 307 IPC के तहत):
विषय: हत्या की कोशिश के लिए परिवाद
सम्बंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
परिवादी:
[नाम], [पता]
प्रतिवादी:
[नाम], [पता]
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [परिवादी का नाम], यह शिकायत कर रहा हूँ कि [प्रतिवादी का नाम] ने जानबूझकर और पूर्व नियोजित तरीके से मुझे मारने का प्रयास किया।
- घटना दिनांक [तारीख] को [स्थान] हुई। प्रतिवादी ने मुझे [हथियार/ तरीका का विवरण] से हमला किया।
- प्रतिवादी का यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध है।
- मैं न्यायालय से निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त मामले में उचित कार्यवाही की जाए।
परिवादी का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
23. प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का आशय और सिद्धान्त:
FIR का आशय: प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) एक औपचारिक शिकायत होती है जिसे किसी अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है। इसे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है, और इसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है। FIR किसी भी अपराध के शुरुआती रिकॉर्ड के रूप में कार्य करती है।
FIR से संबंधित सिद्धांत:
- सत्यता: FIR में दी गई सूचना सही और सटीक होनी चाहिए।
- समय की प्रासंगिकता: FIR को जल्दी दर्ज कराना ज़रूरी होता है, ताकि तथ्य और साक्ष्य ताजे रहें।
- कानूनी अधिकार: किसी व्यक्ति को FIR दर्ज करने का अधिकार होता है यदि उसे अपराध का शिकार माना जाता है।
- पुलिस की जिम्मेदारी: पुलिस को FIR दर्ज करने के बाद त्वरित और निष्पक्ष जांच करनी होती है।
24. काल्पनिक नामों एवं तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रारूप:
प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का प्रारूप:
पुलिस थाना:
[थाने का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[आवेदनकर्ता का नाम], [पता]
विवरण:
- दिनांक [तारीख] को, समय [समय], स्थान [स्थान] पर, [प्रतिवादी का नाम] ने मुझे [अपराध का विवरण] किया।
- प्रतिवादी ने मुझे [हथियार का विवरण] से हमला किया और मेरी जान को खतरा उत्पन्न किया।
- मैं इस मामले में कार्रवाई की मांग करता हूँ।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
25. (क) पुनरीक्षण (Review) क्या है?
पुनरीक्षण का आशय:
पुनरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके तहत उच्च न्यायालय, सेशन न्यायाधीश या अन्य संबंधित न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा करते हैं। यह उन मामलों में होता है जहां किसी निर्णय में गलती या अपूर्णता हो और सुधार की आवश्यकता होती है।
सेशन न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति:
- सेशन न्यायाधीश: सेशन न्यायाधीश को निचली अदालतों के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति होती है।
- उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालय को मामले के तथ्यों और कानून की पुनः समीक्षा करने का अधिकार होता है।
पुनरीक्षण का प्रारूप:
पुनरीक्षण आवेदन का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[नाम], [पता]
विषय: पुनरीक्षण हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ।
- मेरी यह शिकायत है कि [निर्णय का विवरण] में गंभीर गलती है।
- मैं न्यायालय से निवेदन करता हूँ कि निर्णय की पुनः समीक्षा की जाए।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
(ख) पुनर्विलोकन (Review) क्या है?
पुनर्विलोकन एक प्रक्रिया है जिसमें निचली अदालत के निर्णय पर पुनः विचार किया जाता है। इस प्रक्रिया में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश के पास निर्णय की वैधता की जांच करने का अधिकार होता है।
पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[नाम], [पता]
विषय: पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], न्यायालय से निवेदन करता हूँ कि निर्णय की पुनः जांच की जाए।
- इस मामले में [निर्णय का विवरण] गलत तरीके से लिया गया है।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
26. जमानत (Bail) से आशय:
जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें आरोपी को न्यायालय द्वारा उसे हिरासत से बाहर निकालने की अनुमति दी जाती है, यदि वह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता है। जमानत देने का उद्देश्य आरोपी को उचित प्रक्रिया के तहत कानूनी रूप से न्याय का सामना करने का मौका देना होता है।
जमानत किन मामलों में ली जा सकती है:
- अपराधी का स्वतंत्रता अधिकार: यदि आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, तो वह जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वह कोई गैर-जमानती अपराध नहीं करता है।
- सुनवाई के दौरान: जमानत सुनवाई के दौरान भी दी जा सकती है यदि आरोपी का अपराध हल्का हो।
- तत्काल जमानत: कुछ मामलें ऐसे होते हैं, जिसमें तत्काल जमानत मिल सकती है।
27. वाद को पुनः स्थापित करने के लिए आवेदन का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[नाम], [पता]
विषय: वाद पुनः स्थापित करने हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], इस आवेदन के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि मेरी वाद को पुनः स्थापित किया जाए।
- वाद को कारणवश [कारण] के चलते स्थगित किया गया था, किंतु अब मैं तैयार हूँ।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
28. वाद-पत्र में संशोधन के लिए आवेदन का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[नाम], [पता]
विषय: वाद-पत्र में संशोधन हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], इस आवेदन के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि मेरे वाद-पत्र में कुछ संशोधन किया जाए।
- उपरोक्त संशोधन की आवश्यकता [संशोधन का कारण] के कारण उत्पन्न हुई है।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
29. मृतक वादी के वैध प्रतिनिधि को रिकार्ड पर लाने हेतु आवेदन का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[नाम], [पता]
विषय: मृतक वादी के वैध प्रतिनिधि को रिकार्ड पर लाने हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ कि मृतक वादी [मृतक वादी का नाम] के वैध प्रतिनिधि [नाम] को रिकार्ड पर लाया जाए।
- इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए हैं।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
30. एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[आवेदनकर्ता का नाम], [पता]
विषय: एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ कि मामले में न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री जारी की गई है, जो अवैध और गलत है।
- उक्त डिक्री के संबंध में [डिक्री के बारे में जानकारी], जिसमें मेरी स्थिति को सही तरीके से पेश नहीं किया गया है।
- मैं न्यायालय से निवेदन करता हूँ कि इस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाए और इस मामले में पुनः उचित विचार किया जाए।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
31. (क) भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[आवेदनकर्ता का नाम], [पता]
विषय: भरण-पोषण हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ कि मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं भरण-पोषण के योग्य नहीं हूँ।
- मेरी स्थिति इस प्रकार है: [विवरण]
- मैं न्यायालय से निवेदन करता हूँ कि मेरे भरण-पोषण हेतु उचित आदेश जारी किया जाए।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
31. (ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन पत्र का प्रारूप:
संबंधित पुलिस थाने:
[पुलिस थाने का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[आवेदनकर्ता का नाम], [पता]
विषय: धारा 156(3) के तहत अपराध की जांच हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ कि [अपराध का विवरण] के संबंध में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है।
- इस अपराध के संबंध में [विवरण] के आधार पर पुलिस को आदेश देने की कृपा करें।
- मैं न्यायालय से निवेदन करता हूँ कि धारा 156(3) के तहत पुलिस को जांच का आदेश दिया जाए।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
32. जमानत हेतु आवेदन के विभिन्न प्रारूप:
(i) सामान्य जमानत आवेदन प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[आवेदनकर्ता का नाम], [पता]
विषय: जमानत हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ कि मैं एक आरोपी हूं, जिसे [अपराध का नाम] के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
- मैं आवेदन करता हूँ कि मुझे जमानत दी जाए, क्योंकि [कारण]।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
(ii) जमानत अर्जी आवेदन प्रारूप (यदि जमानत विशेष शर्तों पर हो):
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[आवेदनकर्ता का नाम], [पता]
विषय: विशेष शर्तों पर जमानत हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ कि मुझे [अपराध का नाम] के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
- मैं आवेदन करता हूँ कि मुझे जमानत दी जाए, किन्तु मुझे [विशेष शर्तें] पर जमानत मिलनी चाहिए, जैसे [शर्तों का विवरण]।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
33. (a) हिन्दू विवाह विच्छेद से सम्बन्धित वाद पत्र एवं लिखित कथन का प्रारूप:
हिन्दू विवाह विच्छेद वाद पत्र का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
वादी:
[वादी का नाम], [पता]
प्रतिवादी:
[प्रतिवादी का नाम], [पता]
विषय: हिन्दू विवाह विच्छेद हेतु वाद पत्र
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [वादी का नाम], यह वाद प्रस्तुत करता हूँ कि मेरी और [प्रतिवादी का नाम] के बीच हिन्दू विवाह हुआ था, जो दिनांक [तारीख] को हुआ था।
- विवाह के बाद कई वर्षो से हमारे बीच असहमति और पारिवारिक समस्याएँ उत्पन्न हो चुकी हैं।
- मैं यह निवेदन करता हूँ कि मेरे और [प्रतिवादी का नाम] के विवाह को हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विच्छेदित किया जाए।
वादी का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
(b) मुस्लिम पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध विवाह विघटन के आधार:
मुस्लिम महिला द्वारा पति के खिलाफ विवाह विघटन के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं:
- पति की क्रूरता (Cruelty)
- पति का अन्य विवाह करना (Bigamy)
- पति द्वारा निर्वाह की असमर्थता (Inability to provide maintenance)
- पति का अपहरण या गायब होना (Absence or Abduction)
(c) मुस्लिम पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध विवाह-विघटन के लिए वाद-पत्र एवं प्रतिवादी (पति) की तरफ से प्रतिवाद पत्र:
विवाह विघटन वाद पत्र:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
वादी:
[नाम], [पता]
प्रतिवादी:
[पति का नाम], [पता]
विषय: मुस्लिम विवाह विघटन हेतु वाद पत्र
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [वादी का नाम], यह वाद प्रस्तुत करती हूँ कि मेरे और प्रतिवादी के बीच मुस्लिम विवाह हुआ था।
- प्रतिवादी ने मुझसे क्रूरता की है, और मैं उनसे तलाक चाहती हूँ।
- मैं न्यायालय से निवेदन करती हूँ कि मेरे और प्रतिवादी के बीच विवाह को समाप्त किया जाए।
वादी का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
पति की तरफ से प्रतिवाद पत्र:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
प्रतिवादी:
[पति का नाम], [पता]
विषय: प्रतिवाद पत्र
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [पति का नाम], यह प्रतिवाद प्रस्तुत करता हूँ कि मेरी पत्नी का आरोप निराधार है।
- मैंने अपनी पत्नी के साथ कोई क्रूरता नहीं की है और मैं विवाह के विघटन का विरोध करता हूँ।
- मैं न्यायालय से निवेदन करता हूँ कि विवाह को विघटित नहीं किया जाए।
प्रतिवादी का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
34. नोटिस क्या है? नोटिस के तत्व एवं प्रारूप:
नोटिस एक लिखित सूचना या संदेश होता है, जो एक व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरे व्यक्ति या संस्था को भेजा जाता है, ताकि वह किसी विशेष मामले या कार्यवाही के बारे में सूचित हो। यह कानूनी प्रक्रिया में एक आवश्यक दस्तावेज है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को मामले की जानकारी हो और वे उचित प्रतिक्रिया देने का अवसर पा सकें।
नोटिस के तत्व:
- प्रेषक का नाम और पता: नोटिस भेजने वाले का नाम और पता।
- प्राप्तकर्ता का नाम और पता: नोटिस प्राप्त करने वाले का नाम और पता।
- तारीख: जब नोटिस तैयार किया गया।
- विषय: नोटिस का उद्देश्य या मुद्दा।
- संदर्भ: संबंधित कानूनी प्रावधानों या अनुबंध का संदर्भ, यदि आवश्यक हो।
- संक्षिप्त विवरण: मुद्दे का संक्षिप्त विवरण, जिसमें विवाद या कार्रवाई की जानकारी हो।
- निवारक या नियत कार्यवाही: नोटिस प्राप्तकर्ता से अपेक्षित कार्यवाही या जवाब की समयसीमा।
- हस्ताक्षर: नोटिस भेजने वाले का हस्ताक्षर।
नोटिस का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय / कार्यालय:
[न्यायालय / कार्यालय का नाम]
तारीख: [तारीख]
विषय: [नोटिस का विषय]
प्रेषक:
[प्रेषक का नाम]
[पता]
[संपर्क विवरण]
प्राप्तकर्ता:
[प्राप्तकर्ता का नाम]
[पता]
संदर्भ:
[संदर्भ विवरण, जैसे अनुबंध संख्या, मामला संख्या, आदि]
संबंधित विषय:
[विवाद का विवरण और नोटिस का उद्देश्य]
निवारक कार्यवाही:
[प्राप्तकर्ता से अपेक्षित कार्यवाही और समयसीमा]
हस्ताक्षर:
[प्रेषक का हस्ताक्षर]
[पदनाम, यदि applicable]
[तारीख]
35. विधिक सूचना भेजने के प्रारूप:
(क) किरायेदार द्वारा मकान खाली करने हेतु सूचना:
संबंधित न्यायालय / कार्यालय:
[न्यायालय / कार्यालय का नाम]
तारीख: [तारीख]
प्रेषक:
[प्रेषक का नाम]
[पता]
प्राप्तकर्ता:
[किरायेदार का नाम]
[पता]
विषय: मकान खाली करने हेतु सूचना
प्रिय [किरायेदार का नाम],
- आपको सूचित किया जाता है कि आप हमारे द्वारा किराए पर लिए गए मकान [मकान का पता] में पिछले [महीने] से किराया नहीं चुका रहे हैं।
- इसलिए, आपको सूचित किया जाता है कि आप [तारीख] तक मकान खाली कर दें। यदि आप समय पर मकान खाली नहीं करते हैं, तो हम कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे।
आपका,
[प्रेषक का नाम]
[हस्ताक्षर]
[पदनाम, यदि applicable]
(ख) संविदा निर्धारण के लिए नोटिस:
संबंधित न्यायालय / कार्यालय:
[न्यायालय / कार्यालय का नाम]
तारीख: [तारीख]
प्रेषक:
[प्रेषक का नाम]
[पता]
प्राप्तकर्ता:
[प्रतिवादी का नाम]
[पता]
विषय: संविदा समाप्त करने हेतु नोटिस
प्रिय [प्रतिवादी का नाम],
- यह सूचित किया जाता है कि आपके साथ किए गए अनुबंध (संविदा) [संविदा संख्या / विवरण] के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के कारण हम इसे समाप्त करने का निर्णय ले रहे हैं।
- आपको [संविदा समाप्त करने की तारीख] तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया जाता है।
आपका,
[प्रेषक का नाम]
[हस्ताक्षर]
[पदनाम, यदि applicable]
(ग) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत रेलवे को नोटिस:
संबंधित न्यायालय / कार्यालय:
[न्यायालय / कार्यालय का नाम]
तारीख: [तारीख]
प्रेषक:
[प्रेषक का नाम]
[पता]
प्राप्तकर्ता:
रेलवे विभाग
[पता]
विषय: धारा 80 के तहत नोटिस
प्रिय [रेलवे विभाग का नाम],
- मैं [प्रेषक का नाम], यह नोटिस भेजता हूँ कि [विवाद का विवरण, जैसे चोट लगने या दुर्घटना का विवरण] के संबंध में, मैं न्यायालय में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करने जा रहा हूँ।
- आपको सूचित किया जाता है कि इस घटना के लिए आप जिम्मेदार हैं और मैं [कंपensation, अन्य कानूनी मांगें] की मांग कर रहा हूँ।
- कृपया [समय] के भीतर उत्तर दें, अन्यथा मुझे कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
आपका,
[प्रेषक का नाम]
[हस्ताक्षर]
[पदनाम, यदि applicable]
36. (a) प्रापक (रिसीवर) की नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[आवेदनकर्ता का नाम], [पता]
विषय: प्रापक की नियुक्ति हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ कि मामले में [संपत्ति, व्यवसाय, या मामला का विवरण] की रक्षा और प्रबंधन के लिए प्रापक नियुक्त किया जाए।
- प्रापक को [आवश्यक कार्य, जैसे संपत्ति का संरक्षण, धन की वसूली आदि] की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
(b) समझौता पत्र:
समझौता पत्र एक दस्तावेज है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष एक दूसरे से किसी विवाद या मुद्दे को हल करने के लिए सहमत होते हैं। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है और इसमें समझौते की शर्तों को स्पष्ट किया जाता है। यह आमतौर पर अदालत में विचाराधीन मामलों में एक मध्यस्थ समाधान के रूप में उपयोग किया जाता है।
समझौता पत्र प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
पक्ष 1:
[पक्ष 1 का नाम और पता]
पक्ष 2:
[पक्ष 2 का नाम और पता]
विषय: समझौता पत्र
समझौता विवरण:
- दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से निम्नलिखित शर्तों पर समझौता किया है:
- [शर्तें और विवरण, जैसे धन का भुगतान, संपत्ति का हस्तांतरण, आदि]
समझौता करने वाले पक्षों के हस्ताक्षर:
[पक्ष 1 का नाम और हस्ताक्षर]
[पक्ष 2 का नाम और हस्ताक्षर]
[तारीख]
37. डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन एवं प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
आवेदनकर्ता:
[आवेदनकर्ता का नाम], [पता]
विषय: डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [आवेदनकर्ता का नाम], यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ कि न्यायालय द्वारा [मामला का विवरण] के संबंध में डिक्री जारी की गई थी, लेकिन यह डिक्री अभी तक निष्पादित नहीं की गई है।
- मैं निवेदन करता हूँ कि डिक्री के निष्पादन हेतु उचित आदेश जारी किया जाए।
आवेदनकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
38. बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट का प्रारूप:
संबंधित न्यायालय:
[न्यायालय का नाम]
मामला संख्या:
[संख्या]
याचिकाकर्ता:
[याचिकाकर्ता का नाम], [पता]
विषय: बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए याचिका
सम्माननीय न्यायालय,
- मैं, [याचिकाकर्ता का नाम], यह याचिका प्रस्तुत करता हूँ कि [नाम] को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है।
- मैं न्यायालय से अनुरोध करता हूँ कि [नाम] को तुरन्त रिहा करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी कानूनी नहीं है।
याचिकाकर्ता का नाम: [नाम]
हस्ताक्षर: ___________________
तारीख: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
39. जनहित वाद से आप क्या समझते हैं?
जनहित वाद (Public Interest Litigation – PIL) एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक हित के मामलों में अदालत में याचिका दायर कर सकता है। इसका उद्देश्य उन मुद्दों को उठाना है जो समाज के एक बड़े हिस्से के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, और अन्य सामाजिक मुद्दे। जनहित वाद की विशेषता यह है कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों के बजाय समग्र समाज के कल्याण की चिंता होती है।
न्यायिक सक्रियता और लोक कल्याण में जनहित वाद का महत्व:
- न्यायिक सक्रियता: न्यायालय द्वारा जनहित वादों को स्वीकार कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रशासन और सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करें।
- लोक कल्याण: जनहित वाद का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण करना होता है। यह जनता की आवाज को न्यायालय में पेश करता है।
महत्व: जनहित वाद ने सामाजिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, अधिकारों की रक्षा, और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार।
40. प्रलेखशास्त्र का अर्थ और उद्देश्य:
प्रलेखशास्त्र (Conveyancing) उस विधि और प्रक्रिया का अध्ययन है, जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के अधिकार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें दस्तावेजों का निर्माण और प्रमाणन किया जाता है जो अधिकारों के हस्तांतरण को वैध बनाते हैं। प्रलेखशास्त्र का मुख्य उद्देश्य कानूनी दस्तावेजों का निर्माण, संपत्ति के अधिकारों का सही तरीके से हस्तांतरण, और यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानूनी पहलुओं का पालन किया गया है।
विलेख के विभिन्न भागों: विलेख (Deed) एक कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें पार्टियों के अधिकार, कर्तव्य, और उत्तरदायित्व को स्पष्ट किया जाता है। इसके विभिन्न भाग होते हैं, जैसे:
- प्रस्तावना (Preamble): विलेख की शुरुआत में प्रस्तावना होती है, जिसमें पक्षकारों के नाम, पता, और विलेख के उद्देश्य का उल्लेख होता है। इसका उद्देश्य विलेख के पारस्परिक संदर्भ को स्पष्ट करना होता है।
- निर्णय (Recitals): इसमें पहले के घटनाक्रमों, समझौतों और तथ्यों का विवरण होता है। इसका उद्देश्य विलेख के पीछे की कहानी को स्पष्ट करना होता है।
- धारा (Operative Part): यह विलेख का मुख्य भाग होता है, जिसमें कानूनी रूप से लागू होने वाली शर्तें और पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। यह भाग समझौते का वास्तविक विवरण प्रस्तुत करता है।
- स्वीकृति और हस्ताक्षर (Execution): इसमें पार्टियों के हस्ताक्षर होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वे विलेख में वर्णित शर्तों से सहमत हैं। इसका उद्देश्य कानूनी रूप से दस्तावेज को लागू बनाना होता है।
- साक्षी (Witnesses): विलेख के समापन पर साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि विलेख सही ढंग से निष्पादित हुआ है। इसका उद्देश्य दस्तावेज की वैधता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करना होता है।
41. विक्रय विलेख (Sale-Deed):
विक्रय विलेख वह कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा एक पक्ष (विक्रेता) अपनी सम्पत्ति दूसरे पक्ष (खरीदार) को बेचता है। इसमें विक्रेता सम्पत्ति के अधिकार को खरीदार के नाम पर स्थानांतरित करता है और खरीदार इसे स्वीकार करता है। विक्रय विलेख का उद्देश्य संपत्ति के हस्तांतरण को कानूनी रूप से वैध बनाना होता है।
विक्रय विलेख का प्रारूप:
विक्रय विलेख (Sale-Deed)
यह विक्रय विलेख दिनांक [तारीख] को [स्थान] में संपन्न हुआ। इस विलेख के तहत, [विक्रेता का नाम], निवासी [पता], (यहां “विक्रेता” कहा जाएगा), अपने स्वामित्व की सम्पत्ति स्थित [संपत्ति का पता], जिसे [विवरण], को [खरीदार का नाम], निवासी [पता], (यहां “खरीदार” कहा जाएगा), को विक्रय करता है।
- विक्रेता ने पुष्टि की है कि वह सम्पत्ति का वैध स्वामी है, और उस पर कोई कानूनी दावा, ऋण या अन्य बकाया नहीं है।
- विक्रेता यह स्वीकार करता है कि खरीदार ने सम्पत्ति का मूल्य [राशि] प्राप्त किया है।
- विक्रेता ने सम्पत्ति को पूर्ण रूप से खरीदार को स्थानांतरित कर दिया है और इसके अधिकार को पूर्ण रूप से खरीदार को सौंप दिया है।
हस्ताक्षर:
विक्रेता: [हस्ताक्षर]
खरीदार: [हस्ताक्षर]
साक्षी 1: [हस्ताक्षर]
साक्षी 2: [हस्ताक्षर]
(b) बन्धक विलेख (Mortgage Deed):
बन्धक विलेख वह कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा एक पक्ष अपनी सम्पत्ति को ऋणदाता के पास सुरक्षित रखने के लिए बंधक बनाता है। इसका उद्देश्य ऋण की चुकौती सुनिश्चित करना है।
बन्धक विलेख का प्रारूप:
बन्धक विलेख (Mortgage Deed)
यह बन्धक विलेख दिनांक [तारीख] को [स्थान] में संपन्न हुआ। इस विलेख के तहत, [ऋणकर्ता का नाम], निवासी [पता], (यहां “ऋणकर्ता” कहा जाएगा), अपनी सम्पत्ति [संपत्ति का पता और विवरण], को [ऋणदाता का नाम], निवासी [पता], (यहां “ऋणदाता” कहा जाएगा), के पास बन्धक के रूप में रखता है।
- ऋणकर्ता यह पुष्टि करता है कि वह सम्पत्ति का वैध स्वामी है और सम्पत्ति पर कोई अन्य बकाया नहीं है।
- ऋणकर्ता ने इस सम्पत्ति को ऋणदाता के पास ऋण चुकता करने तक बन्धक के रूप में रखा है।
- यदि ऋणकर्ता ऋण चुकता नहीं करता है, तो ऋणदाता को सम्पत्ति को बेचनें या अन्य कानूनी उपायों को अपनाने का अधिकार होगा।
हस्ताक्षर:
ऋणकर्ता: [हस्ताक्षर]
ऋणदाता: [हस्ताक्षर]
साक्षी 1: [हस्ताक्षर]
साक्षी 2: [हस्ताक्षर]
(c) दान विलेख (Gift Deed):
दान एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति, बिना किसी मूल्य के, किसी अन्य व्यक्ति को सौंपता है। यह स्वाभाविक प्रेम और स्नेहवश किया जाता है। इसके आवश्यक तत्वों में दाता की इच्छा, दान की सम्पत्ति और प्राप्तकर्ता की स्वीकृति शामिल होती है।
दान विलेख का प्रारूप:
दान विलेख (Gift Deed)
यह दान विलेख दिनांक [तारीख] को [स्थान] में संपन्न हुआ। इस विलेख के तहत, [दानकर्ता का नाम], निवासी [पता], (यहां “दानकर्ता” कहा जाएगा), अपनी सम्पत्ति [संपत्ति का पता और विवरण], को [प्राप्तकर्ता का नाम], निवासी [पता], (यहां “प्राप्तकर्ता” कहा जाएगा), को स्वाभाविक प्रेम और स्नेहवश बिना किसी मूल्य के दान करता है।
- दानकर्ता यह पुष्टि करता है कि सम्पत्ति पर कोई ऋण या बकाया नहीं है।
- दानकर्ता ने सम्पत्ति को पूर्ण रूप से प्राप्तकर्ता को दान कर दिया है और इसकी स्वामित्व प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित कर दी है।
- प्राप्तकर्ता ने इस दान को स्वीकार किया है और दानकर्ता की इच्छा के अनुसार सम्पत्ति का स्वामित्व ग्रहण किया है।
हस्ताक्षर:
दानकर्ता: [हस्ताक्षर]
प्राप्तकर्ता: [हस्ताक्षर]
साक्षी 1: [हस्ताक्षर]
साक्षी 2: [हस्ताक्षर]
42. (A) अचल सम्पत्ति के पट्टे की परिभाषा:
अचल सम्पत्ति के पट्टे (Lease of immovable property) एक कानूनी समझौता है जिसमें भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति को एक निश्चित समय के लिए किराए पर दिया जाता है। पट्टा विलेख में पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख होता है।
पट्टा विलेख का प्रारूप:
पट्टा विलेख (Lease Deed)
यह पट्टा विलेख दिनांक [तारीख] को [स्थान] में संपन्न हुआ। इस विलेख के तहत, [पट्टेदार का नाम], निवासी [पता], (यहां “पट्टेदार” कहा जाएगा), अपनी सम्पत्ति [संपत्ति का विवरण] को [पट्टेदार का नाम], निवासी [पता], (यहां “पट्टेदार” कहा जाएगा), को [समयावधि] तक किराए पर देता है। पट्टेदार को सम्पत्ति का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वह किसी भी निर्माण या अन्य गतिविधि करने के लिए अनुमति नहीं रखता है।
हस्ताक्षर:
पट्टेदार: [हस्ताक्षर]
पट्टेदार: [हस्ताक्षर]
साक्षी 1: [हस्ताक्षर]
साक्षी 2: [हस्ताक्षर]
(i) भूमि का पट्टा ईंट भट्ठा चलाने के लिए पट्टा विलेख का प्रारूप:
यह भूमि पट्टा विलेख दिनांक [तारीख] को [स्थान] में संपन्न हुआ। इस विलेख के तहत, [पट्टेदार का नाम], निवासी [पता], अपनी भूमि [भूमि का विवरण] को [पट्टेदार का नाम], निवासी [पता], को ईंट भट्ठा चलाने के लिए पट्टे पर देता है।
हस्ताक्षर:
पट्टेदार: [हस्ताक्षर]
पट्टेदार: [हस्ताक्षर]
(ii) पट्टे का करारनामा विलेख का प्रारूप:
यह पट्टे का करारनामा दिनांक [तारीख] को संपन्न हुआ, जिसमें [पट्टेदार का नाम] और [पट्टेदार का नाम] के बीच निम्नलिखित शर्तों पर समझौता हुआ।
हस्ताक्षर:
पट्टेदार: [हस्ताक्षर]
पट्टेदार: [हस्ताक्षर]
(B) वचन पत्र की आवश्यक शर्तें और प्रारूप:
वचन पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को कोई वचन देता है। इसमें कुछ निश्चित शर्तों का उल्लेख होता है, जैसे कि वह कर्तव्य कब और किस तरह पूरा किया जाएगा।
वचन पत्र का प्रारूप:
हस्ताक्षर:
[हस्ताक्षर]
44. (B) दत्तक विलेख का प्रारूप (Adoption Deed):
दत्तक विलेख (Adoption Deed)
यह दत्तक विलेख दिनांक [तारीख] को [स्थान] में संपन्न हुआ। इस विलेख के द्वारा, [दत्तक माता-पिता का नाम], निवासी [पता], (यहां “दत्तक माता-पिता” कहा जाएगा), अपनी सम्पत्ति और दायित्वों के तहत [दत्तक बालक का नाम], जन्म प्रमाण पत्र संख्या [प्रमाण पत्र संख्या] के तहत, जन्मतिथि [तारीख] और स्थान [स्थान] को, इस विलेख द्वारा पुत्र/पुत्री के रूप में विधिवत रूप से गोद लेते हैं।
- दत्तक माता-पिता ने इस बालक को अपनी सम्पत्ति और परिवार के अधिकारों में पूर्ण रूप से शामिल किया है।
- यह दत्तक विलेख बिना किसी पूर्व शर्त के है और दत्तक बालक ने इसे स्वीकृत किया है।
- दत्तक माता-पिता ने यह पुष्टि की है कि वे बालक की देखभाल, शिक्षा और भविष्य के लिए सभी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे।
हस्ताक्षर: दत्तक माता-पिता: [हस्ताक्षर]
दत्तक बालक (यदि प्रौढ़ है): [हस्ताक्षर]
साक्षी 1: [हस्ताक्षर]
साक्षी 2: [हस्ताक्षर]
45. (क) पंचाट वाद (Arbitration Case) का प्रारूप:
पंचाट वाद (Arbitration Case)
यह वाद दिनांक [तारीख] को [स्थान] में [पंचाट वाद संबंधी प्राधिकरण/न्यायालय का नाम] में दायर किया गया। इसमें वादी [वादी का नाम], निवासी [पता], (यहां “वादी” कहा जाएगा) और प्रतिवादी [प्रतिवादी का नाम], निवासी [पता], (यहां “प्रतिवादी” कहा जाएगा), के बीच [विवाद का संक्षेप में विवरण] के संबंध में पंचाट के माध्यम से समाधान की मांग की गई है।
- वादी और प्रतिवादी के बीच [विवाद का विषय] को लेकर समझौता करने की असफल कोशिशें हो चुकी हैं।
- वादी द्वारा इस विवाद को पंचाट द्वारा हल करने के लिए निर्णय लिया गया है।
- वादी ने यह आवेदन पंचाट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि न्यायालय इसे स्वीकार करके उचित निर्देश जारी करें।
हस्ताक्षर:
वादी: [हस्ताक्षर]
प्रतिवादी: [हस्ताक्षर]
साक्षी 1: [हस्ताक्षर]
साक्षी 2: [हस्ताक्षर]
(ख) लोक अदालत में वाद-पत्र का प्रारूप (Public Forum Case):
लोक अदालत वाद-पत्र (Public Forum Case)
यह वाद दिनांक [तारीख] को [लोक अदालत का नाम], [स्थान] में दायर किया गया। वादी [वादी का नाम], निवासी [पता], (यहां “वादी” कहा जाएगा), और प्रतिवादी [प्रतिवादी का नाम], निवासी [पता], (यहां “प्रतिवादी” कहा जाएगा), के बीच [विवाद का संक्षेप में विवरण] के संबंध में न्याय का आग्रह किया गया है।
- वादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के अनुसार प्रतिवादी ने [विवाद का विषय] में लापरवाही की है, जिसके परिणामस्वरूप वादी को नुकसान हुआ है।
- वादी ने प्रतिवादी से समाधान की मांग की है और यह मामला लोक अदालत में निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- वादी का यह दावा है कि लोक अदालत में न्याय मिल सकता है और इसके माध्यम से विवाद का सुलह किया जा सकता है।
हस्ताक्षर:
वादी: [हस्ताक्षर]
प्रतिवादी: [हस्ताक्षर]
साक्षी 1: [हस्ताक्षर]
साक्षी 2: [हस्ताक्षर]
46. वन्दना उपाध्याय द्वारा टेलीफोन कनेक्शन हेतु उपभोक्ता फोरम में वाद-पत्र:
विपत्ति: वन्दना उपाध्याय ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए फार्म भरा, परन्तु उसे अन्य श्रेणी के लोगों की तुलना में कनेक्शन नहीं मिला। वादी उपभोक्ता के रूप में क्षतिपूर्ति की मांग करती है।
वाद-पत्र:
उपभोक्ता फोरम में वाद
वन्दना उपाध्याय, निवासी [पता], (वादी),
वर्ष [तारीख]
संघर्ष विषय: टेलीफोन कनेक्शन के लिए शुल्क और फार्म भरने के बावजूद कनेक्शन का अस्वीकृत होना।
- वन्दना उपाध्याय ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए टेलीफोन विभाग से आवेदन किया और निर्धारित शुल्क एवं फार्म भर दिए।
- इसके बावजूद, अन्य श्रेणी के लोगों को कनेक्शन मिल गया, जबकि वन्दना उपाध्याय को कोई कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया।
- वन्दना उपाध्याय ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता फोरम में यह वाद दायर किया है और क्षतिपूर्ति की मांग की है।
प्रार्थना:
वादी ने उपभोक्ता फोरम से टेलीफोन कनेक्शन के लिए तुरन्त कार्यवाही करने तथा क्षतिपूर्ति की मांग की है।
हस्ताक्षर:
वादी: [हस्ताक्षर]
साक्षी: [हस्ताक्षर]
तारीख: [तारीख]
47. लोक-अपदूषण (Public Nuisance) को रोकने के लिए वाद:
लोक-अपदूषण वाद का प्रारूप:
वाद-पत्र (Public Nuisance Case)
यह वाद दिनांक [तारीख] को [न्यायालय का नाम], [स्थान] में दायर किया गया। इसमें वादी [वादी का नाम], निवासी [पता], (यहां “वादी” कहा जाएगा), प्रतिवादी [प्रतिवादी का नाम], निवासी [पता], (यहां “प्रतिवादी” कहा जाएगा), के खिलाफ लोक-अपदूषण को रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहा है।
- वादी द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी की गतिविधियाँ [विवाद का विवरण] लोक-अपदूषण उत्पन्न कर रही हैं और इससे जनहित में परेशानी हो रही है।
- वादी ने न्यायालय से यह अनुरोध किया है कि प्रतिवादी के खिलाफ उचित निर्देश जारी किये जाएं ताकि यह अपदूषण रोका जा सके।
प्रार्थना:
वादी न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादी के खिलाफ उचित आदेश जारी किया जाए और अपदूषण को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए।
हस्ताक्षर:
वादी: [हस्ताक्षर]
प्रतिवादी: [हस्ताक्षर]
साक्षी: [हस्ताक्षर]