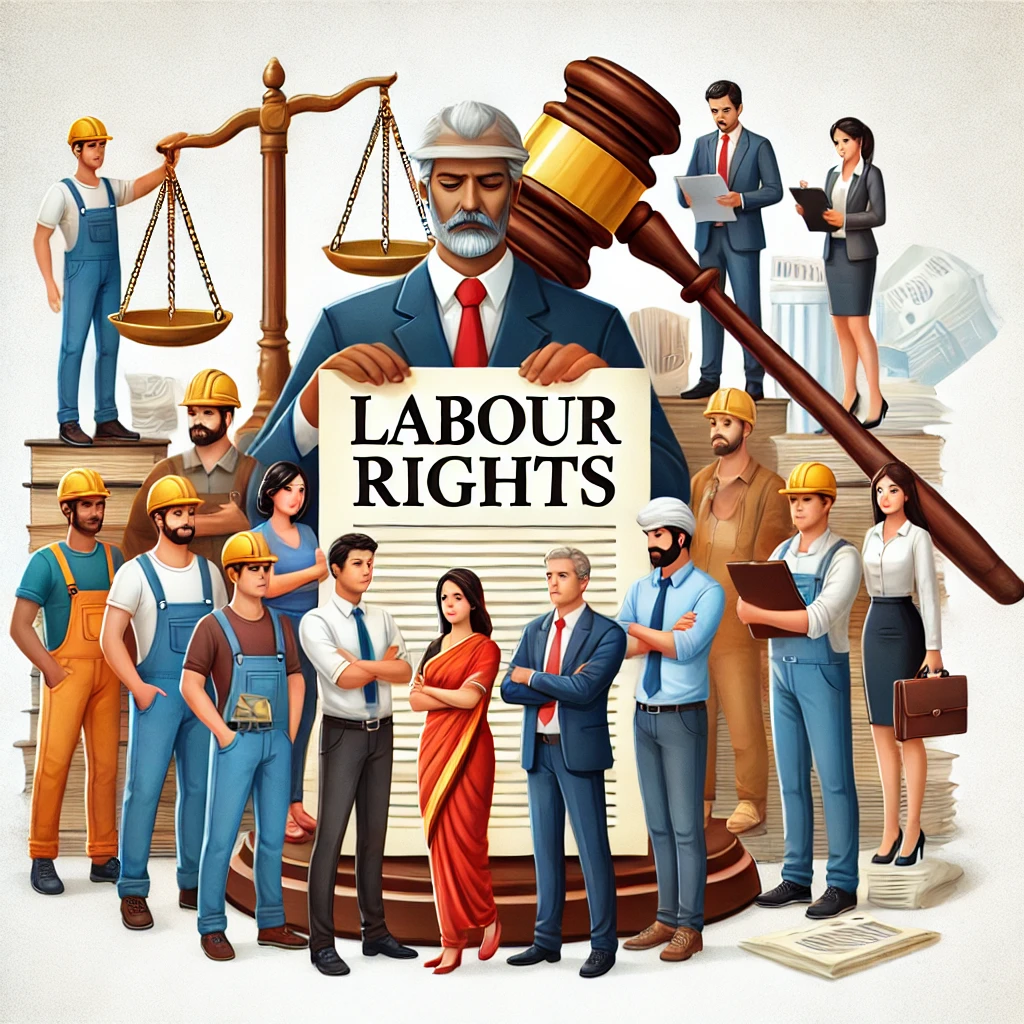शीर्षक: अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 : प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में एक संवैधानिक प्रयास
परिचय
भारत में लाखों श्रमिक आजीविका की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। ये श्रमिक अधिकतर निर्माण, खनन, कृषि, ईंट भट्ठों, और उद्योगों में कार्यरत होते हैं। परंतु प्रवासी होने के कारण वे न तो मूल राज्य की सुविधा प्राप्त कर पाते हैं और न ही कार्यस्थल राज्य में अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 (Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979) पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों के रोजगार, वेतन, रहने की सुविधा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
अधिनियम का उद्देश्य
- अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की भर्ती और नियोजन को विनियमित करना।
- उन्हें उचित कार्यस्थलीय सुविधाएं और न्यूनतम वेतन, आवास, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, आदि उपलब्ध कराना।
- ठेकेदारों और नियोक्ताओं द्वारा उनके शोषण को रोकना।
- प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय श्रमिकों के समान अधिकार दिलाना।
अधिनियम की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि
1970 के दशक में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लाखों श्रमिकों को ठेकेदारों द्वारा अन्य राज्यों में ले जाकर अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कराया जाता था। इस शोषण को रोकने के लिए जस्टिस डी.एन. मिश्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर यह अधिनियम बनाया गया।
प्रमुख परिभाषाएँ
- प्रवासी श्रमिक: वह व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए ठेकेदार के माध्यम से भेजा जाता है और जिसका वेतन ठेकेदार या नियोक्ता द्वारा दिया जाता है।
- ठेकेदार (Contractor): ऐसा व्यक्ति जो श्रमिकों की भर्ती कर उन्हें किसी अन्य राज्य में कार्य के लिए भेजता है।
- स्थापन (Establishment): वह संस्थान, उद्योग या कार्यस्थल जहाँ श्रमिक नियोजित होते हैं।
अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान
1. पंजीकरण और लाइसेंस
- प्रत्येक स्थापन को, जहाँ प्रवासी श्रमिक नियोजित किए जाते हैं, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- ठेकेदारों को श्रमिकों की भर्ती से पहले लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।
2. नियोजन की शर्तें
- प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय श्रमिकों के बराबर वेतन, कार्य के घंटे, छुट्टियाँ, भत्ता इत्यादि देने की बाध्यता है।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ठेकेदार को श्रमिकों को नियोजन की शर्तों की जानकारी देनी होती है।
3. भत्ता और यात्रा सुविधा
- प्रवासी श्रमिकों को कार्यस्थल तक लाने और वापस मूल राज्य तक पहुँचाने की यात्रा सुविधा एवं भत्ता देना अनिवार्य है।
4. आवास, पेयजल और चिकित्सा सुविधा
- स्थापन को श्रमिकों के लिए उचित आवास, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं एवं साफ-सफाई की सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं।
5. वेतन भुगतान
- श्रमिकों को समय पर वेतन देना अनिवार्य है और किसी प्रकार की अवैध कटौती प्रतिबंधित है।
6. रिकॉर्ड एवं निरीक्षण
- नियोक्ता और ठेकेदार को श्रमिकों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है।
- सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को किसी भी समय निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है।
श्रमिकों के अधिकार
- स्थानीय श्रमिकों के समान पारिश्रमिक और सुविधा
- समय पर भुगतान और सुरक्षित कार्य वातावरण
- मूल राज्य तक वापसी यात्रा का खर्च
- स्वास्थ्य सेवाओं और आवास की सुविधा
- शोषण, अनुचित बर्ताव और वेतन कटौती के विरुद्ध शिकायत का अधिकार
दंडात्मक प्रावधान
यदि कोई नियोक्ता या ठेकेदार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो:
- उसे ₹1000 तक का जुर्माना या 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
- बार-बार उल्लंघन पर दंड और अधिक कठोर हो सकता है।
कोविड-19 महामारी और प्रवासी श्रमिक
2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा ने अधिनियम की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े किए। लाखों श्रमिक—
- बिना वेतन, बिना भोजन और यात्रा की सुविधा के अभाव में पैदल अपने राज्यों की ओर लौटते नज़र आए।
- इसने केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों के डेटा, पंजीकरण, और सुरक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की ओर प्रेरित किया।
चुनौतियाँ और कमियाँ
- कम जागरूकता: अधिकांश प्रवासी श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों से अनभिज्ञ होते हैं।
- प्रवर्तन की कमजोरी: निरीक्षण और दंड की प्रक्रिया धीमी और कमजोर है।
- पंजीकरण की कमी: कई ठेकेदार और स्थापन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं।
- राज्यों में समन्वय की कमी: श्रमिकों की ट्रैकिंग और सुविधा हेतु मूल और गंतव्य राज्यों के बीच समन्वय का अभाव है।
सुधार के सुझाव
- डिजिटल पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।
- राज्यों के बीच डेटा शेयरिंग और समन्वय तंत्र मजबूत किया जाए।
- ठेकेदारों की जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था कड़ी की जाए।
- प्रवासी श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रणाली विकसित हो।
निष्कर्ष
अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 भारत में श्रम कानूनों की उस कड़ी का हिस्सा है, जो शोषित, कमजोर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम श्रमिकों के लिए गरिमामयी जीवन, समान अधिकार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। हालांकि व्यवहार में इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया में कई कमियाँ हैं, फिर भी यह अधिनियम प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आज आवश्यकता है कि इसे और अधिक व्यावहारिक, तकनीकी और प्रभावी बनाया जाए ताकि कोई भी श्रमिक अपने हक से वंचित न रह सके।