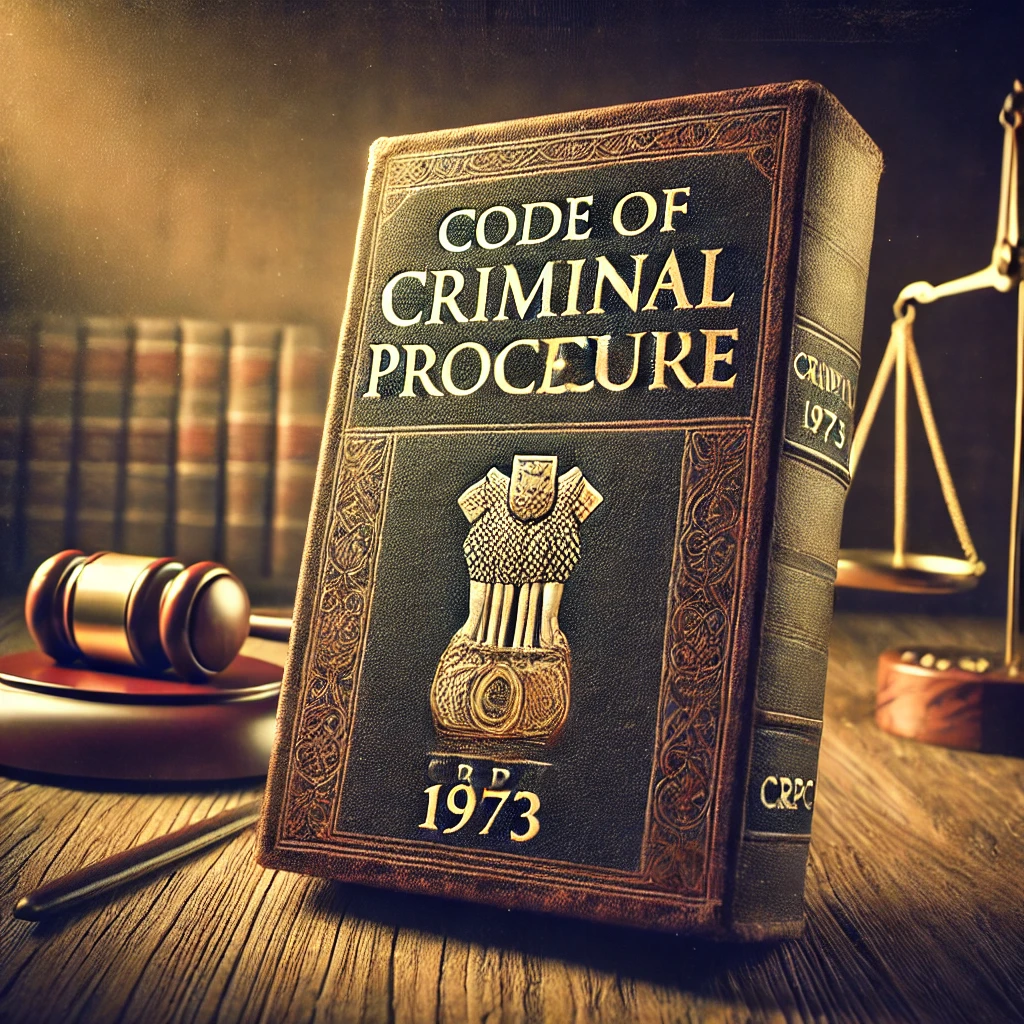“दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973): भारतीय आपराधिक न्याय प्रक्रिया की रीढ़”
🔷 प्रस्तावना:
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure – CrPC, 1973) भारत की प्राथमिक प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून संहिता है, जो यह निर्धारित करती है कि आपराधिक मामलों में जांच, गिरफ्तारी, अभियोजन, सुनवाई, और निर्णय किस प्रकार किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता (IPC) अपराधों और दंड को परिभाषित करती है, जबकि CrPC यह सुनिश्चित करती है कि उन अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया कैसे होगी।
🔷 इतिहास और पृष्ठभूमि:
- मूल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान अस्तित्व में आई।
- समय के साथ कई संशोधन और सुधार किए गए।
- वर्तमान CrPC, 1973 को 25 जनवरी 1974 से पूरे भारत (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, तब) में लागू किया गया।
- यह संहिता संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाती है।
🔷 CrPC का उद्देश्य (Objectives of CrPC):
- आपराधिक मामलों में जांच, जमानत, गिरफ्तारी, साक्ष्य और सुनवाई की प्रक्रिया को नियंत्रित करना।
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हुए अपराधों की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना।
- अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों को न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायिक मंच देना।
- पुलिस, न्यायालय और अभियोजन एजेंसियों के कार्यों को नियंत्रित करना।
🔷 CrPC की संरचना (Structure of CrPC):
CrPC में कुल 37 अध्याय (Chapters) और 484 धाराएँ (Sections) हैं, तथा 2 अनुसूचियाँ (Schedules) हैं। इसके मुख्य भाग हैं:
- प्रारंभिक (Preliminary): परिभाषाएँ, क्षेत्राधिकार
- जांच की प्रक्रिया (Investigation): FIR, जांच अधिकारी की भूमिका
- गिरफ्तारी और बेल (Arrest & Bail): बिना वारंट गिरफ्तारी, जमानत के प्रकार
- अदालतों की शक्तियाँ (Powers of Courts): मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय
- विचारण (Trial): सत्र विचारण, मजिस्ट्रेट विचारण
- साक्ष्य और निर्णय (Evidence & Judgment): गवाह, साक्ष्य की रचना
- अपील, पुनरीक्षण और दया याचिका (Appeal & Revision)
🔷 प्रमुख धाराएँ (Important Sections of CrPC):
| धारा | विषय | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 154 | प्राथमिकी (FIR) | किसी भी अपराध की रिपोर्टिंग |
| 41 | गिरफ्तारी बिना वारंट | पुलिस द्वारा आपात गिरफ्तारी |
| 167 | न्यायिक हिरासत | अधिकतम 15 या 90 दिन की अवधि |
| 200 | परिवाद | मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत |
| 313 | आरोपी का बयान | विचारण के दौरान पूछताछ |
| 320 | समझौता योग्य अपराध | पक्षकारों के बीच समझौता संभव |
| 482 | उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ | न्याय के हित में विशेष शक्तियाँ |
🔷 CrPC के प्रमुख सिद्धांत (Key Principles):
- निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial): अभियुक्त को अपनी बात रखने का पूरा अवसर।
- जमानत का अधिकार (Right to Bail): गैर-गंभीर अपराधों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता।
- FIR का महत्व: किसी अपराध की जांच की पहली सीढ़ी।
- गिरफ्तारी और हिरासत के दिशा-निर्देश: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा-निर्देश (D.K. Basu केस) के अनुसार।
🔷 CrPC में समय-समय पर संशोधन:
- 2005 संशोधन: महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रावधान।
- 2013 संशोधन (निर्भया कांड): यौन अपराधों की प्रक्रिया में कठोरता।
- 2023 – CrPC का प्रतिस्थापन: भारत सरकार ने CrPC को ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)’ से प्रतिस्थापित किया है, जो एक आधुनिक, तकनीकी और पीड़ित-केंद्रित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
🔷 CrPC और भारतीय संविधान:
CrPC भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों, जैसे अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी पर अधिकार) से जुड़े सिद्धांतों के अनुरूप काम करता है।
👉 CrPC यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति बिना उचित प्रक्रिया के दंडित न हो।
🔷 न्यायालयी दृष्टिकोण (Judicial Interpretation):
भारतीय न्यायपालिका ने CrPC की धाराओं की व्याख्या करते हुए इसे और अधिक मानवाधिकार-हितैषी बनाया है।
जैसे:
- D.K. Basu v. State of West Bengal (गिरफ्तारी की प्रक्रिया)
- Lalita Kumari v. State of UP (FIR दर्ज करना अनिवार्य)
🔷 निष्कर्ष:
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) भारतीय न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपराधिक मामलों में न्याय, निष्पक्षता, और पारदर्शिता बनी रहे। भले ही इसे अब BNSS, 2023 से प्रतिस्थापित किया जा रहा हो, लेकिन CrPC ने दशकों तक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा की और भारत को एक मजबूत न्यायिक प्रक्रिया प्रणाली प्रदान की।