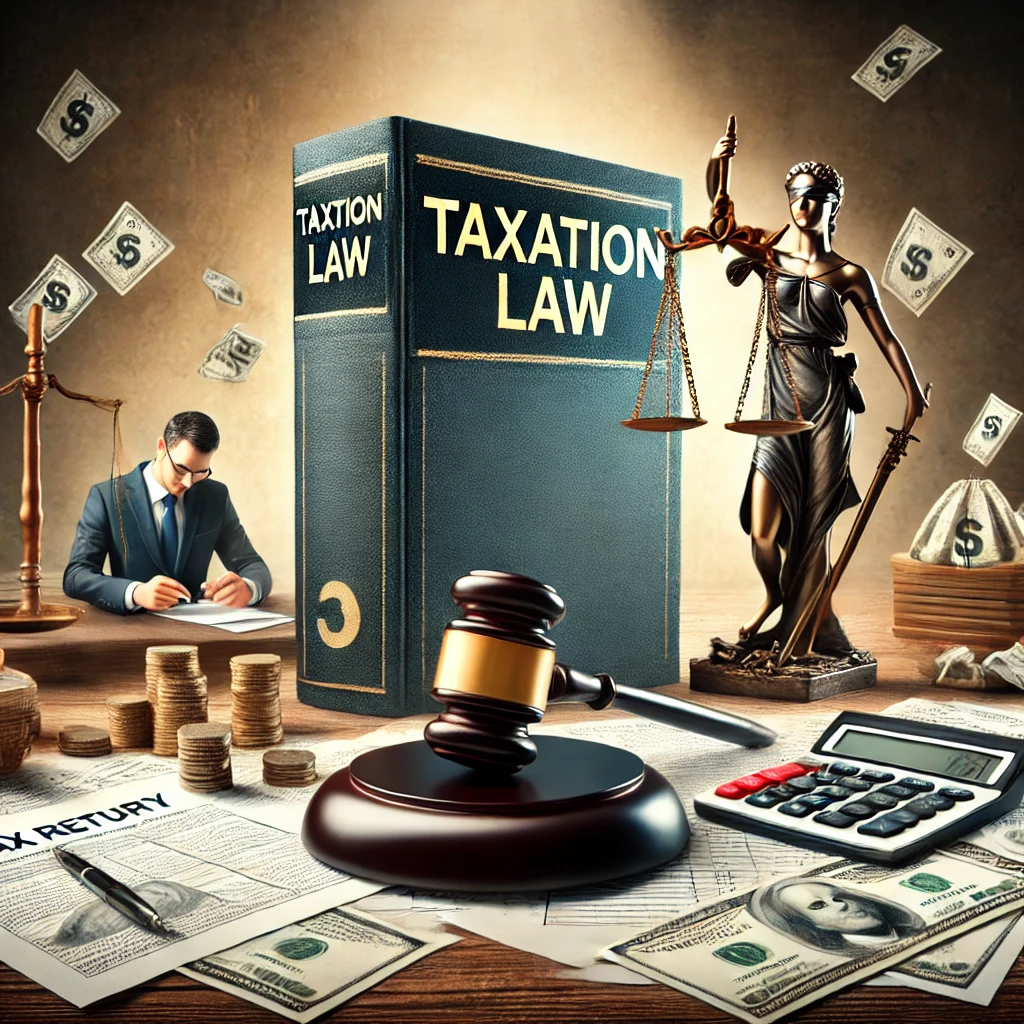कराधान कानून : भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक विस्तृत अध्ययन
प्रस्तावना
कराधान (Taxation) किसी भी आधुनिक राज्य की आर्थिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। राज्य अपने प्रशासनिक कार्य, विकास योजनाएँ, कल्याणकारी योजनाएँ, सुरक्षा व्यवस्था तथा न्यायिक तंत्र को संचालित करने के लिए राजस्व की आवश्यकता रखता है। यह राजस्व मुख्यतः कर (Tax) के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कराधान कानून (Taxation Law) इस प्रक्रिया को कानूनी ढाँचे में नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि करारोपण, करसंग्रहण तथा कर-प्रशासन निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत हो।
कराधान कानून की परिभाषा
कराधान कानून वह विधिक ढाँचा है जिसके अंतर्गत राज्य अपने नागरिकों और संस्थाओं से कर वसूल करता है। यह कानून यह निर्धारित करता है कि –
- कौन-सा कर लगाया जाएगा,
- किस पर लगाया जाएगा,
- कितनी दर से लगाया जाएगा, और
- किस प्रक्रिया से वसूला जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में स्पष्ट प्रावधान है – “कोई कर विधि के प्राधिकार के बिना न लगाया जाएगा और न ही वसूला जाएगा।” इसका अर्थ है कि कराधान केवल वैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही किया जा सकता है।
कराधान का उद्देश्य
कराधान कानून का मूल उद्देश्य केवल राजस्व प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना भी है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं –
- राजस्व संग्रह – सरकार के दैनिक खर्च और विकास योजनाओं हेतु।
- आर्थिक असमानता कम करना – अमीरों पर अधिक कर और गरीबों पर कम कर लगाकर।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना – सार्वजनिक सेवाओं के लिए संसाधन जुटाना।
- आर्थिक विकास को प्रोत्साहन – उद्योगों, कृषि और व्यापार में निवेश हेतु कर रियायतें।
- नियमन और नियंत्रण – कुछ गतिविधियों (जैसे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग) पर कर द्वारा नियंत्रण।
कर के प्रकार
भारतीय कराधान व्यवस्था को मुख्यतः दो वर्गों में बाँटा जाता है –
1. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
प्रत्यक्ष कर वह है जिसे सीधे करदाता की आय या संपत्ति पर लगाया जाता है और जिसका भार वही व्यक्ति वहन करता है।
- आयकर (Income Tax) – व्यक्तियों एवं कंपनियों की आय पर लगाया जाता है।
- कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax) – कंपनियों के मुनाफे पर।
- धनकर (Wealth Tax) / संपत्ति कर – पूर्व में लागू, अब अधिकांश रूप से समाप्त।
- पूँजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) – संपत्ति बेचने पर होने वाले लाभ पर।
2. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं व सेवाओं की खरीद पर लगाया जाता है और उपभोक्ता इसे चुकाता है।
- जी.एस.टी. (Goods and Services Tax) – 2017 से लागू, जिसने वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को समाहित कर दिया।
- सीमा शुल्क (Customs Duty) – आयात-निर्यात पर।
- उत्पाद शुल्क (Excise Duty) – अब अधिकांश जी.एस.टी. में सम्मिलित।
भारतीय कराधान व्यवस्था का संवैधानिक आधार
संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच कराधान संबंधी अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया है –
- संघ सूची (Union List) – आयकर, कंपनी कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर (अब जीएसटी में) आदि पर अधिकार।
- राज्य सूची (State List) – भूमि राजस्व, कृषि कर, बिजली शुल्क आदि।
- समवर्ती सूची (Concurrent List) – बहुत कम कर विषय, परंतु कुछ प्रशासनिक प्रावधान।
अनुच्छेद 265 – विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जा सकता।
अनुच्छेद 246 व सातवीं अनुसूची – कर लगाने की शक्तियों का बंटवारा।
अनुच्छेद 279A – जी.एस.टी. परिषद का गठन।
प्रमुख कराधान कानून
भारत में कराधान संबंधी कई महत्वपूर्ण कानून लागू हैं, जैसे –
- आयकर अधिनियम, 1961 – प्रत्यक्ष कर प्रणाली का मुख्य कानून।
- जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 – वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित।
- कस्टम्स एक्ट, 1962 – आयात-निर्यात शुल्क से संबंधित।
- फाइनेंस एक्ट (वार्षिक) – हर वर्ष संसद द्वारा पारित, जिसमें कर दरें व प्रावधान अपडेट होते हैं।
- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA, 2002) – अवैध धन प्रवाह रोकने हेतु।
न्यायालयों द्वारा कराधान कानून की व्याख्या
भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर कराधान कानून की व्याख्या की है।
- Kesoram Industries Ltd. v. State of Bengal (1964) – कर और शुल्क (Tax vs Fee) के बीच अंतर स्पष्ट किया।
- McDowell & Co. Ltd. v. CTO (1985) – कर चोरी और कर नियोजन (Tax Evasion vs Tax Planning) की अवधारणा।
- Vodafone International Holdings v. UOI (2012) – अंतरराष्ट्रीय कराधान और अप्रत्यक्ष शेयर ट्रांसफर पर ऐतिहासिक निर्णय।
कर चोरी और कर बचाव
कराधान कानून की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि करदाता ईमानदारी से कर अदा करें।
- कर चोरी (Tax Evasion) – कानून का उल्लंघन कर अवैध तरीके से कर से बचना।
- कर बचाव (Tax Avoidance) – कानूनी प्रावधानों का लाभ उठाकर कर देनदारी कम करना।
- कर नियोजन (Tax Planning) – वैध छूटों और कटौतियों का उपयोग कर करभार कम करना।
कराधान कानून की चुनौतियाँ
भारतीय कराधान व्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है –
- जटिलता – अनेक कानून और प्रक्रियाएँ आम नागरिक के लिए कठिन।
- कर चोरी – नकली बिल, हवाला और काला धन जैसी समस्याएँ।
- न्यायसंगतता का अभाव – अमीर और गरीब पर कर का समान अनुपात न होना।
- प्रशासनिक अक्षमता – कर विभाग में भ्रष्टाचार और विलंब।
- अंतरराष्ट्रीय कर विवाद – विदेशी कंपनियों से संबंधित।
कर सुधार और जी.एस.टी.
भारत में कराधान सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम जी.एस.टी. (2017) रहा।
- इससे एक राष्ट्र – एक कर की अवधारणा को बल मिला।
- कई अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर पारदर्शिता बढ़ी।
- ऑनलाइन फाइलिंग और डिजिटल भुगतान से कर चोरी पर नियंत्रण।
हालाँकि, जी.एस.टी. में दरों की जटिलता और छोटे व्यवसायों की दिक्कतें अब भी बनी हुई हैं।
कराधान और आर्थिक विकास
कराधान केवल राजस्व जुटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह विकास का साधन भी है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास – सड़क, रेल, शिक्षा व स्वास्थ्य।
- गरीबी उन्मूलन – सब्सिडी व कल्याण योजनाएँ।
- औद्योगिक प्रोत्साहन – स्टार्टअप व निर्यात क्षेत्र में कर रियायतें।
- पर्यावरण संरक्षण – ग्रीन टैक्स व कार्बन टैक्स।
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
वैश्वीकरण के दौर में कराधान केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs) अलग-अलग देशों के कर ढाँचों का लाभ उठाकर कर बचाती हैं। इस संदर्भ में –
- OECD का BEPS प्रोजेक्ट – कर आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण रोकने हेतु।
- डिजिटल सेवाओं पर कर – जैसे Google Tax।
भारत भी इन वैश्विक कर सुधारों का हिस्सा है।
निष्कर्ष
कराधान कानून किसी भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक ढाँचे का अभिन्न अंग है। यह न केवल सरकार को आवश्यक राजस्व उपलब्ध कराता है, बल्कि आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करता है। भारतीय कराधान व्यवस्था ने स्वतंत्रता के बाद से अनेक सुधार देखे हैं, जिनमें हाल का जी.एस.टी. सबसे बड़ा परिवर्तन है। फिर भी, कर चोरी, जटिल प्रक्रिया और न्यायसंगतता की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।
अतः आवश्यकता इस बात की है कि कराधान कानून को सरल, पारदर्शी और आमजन के लिए सहज बनाया जाए ताकि “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को साकार किया जा सके।