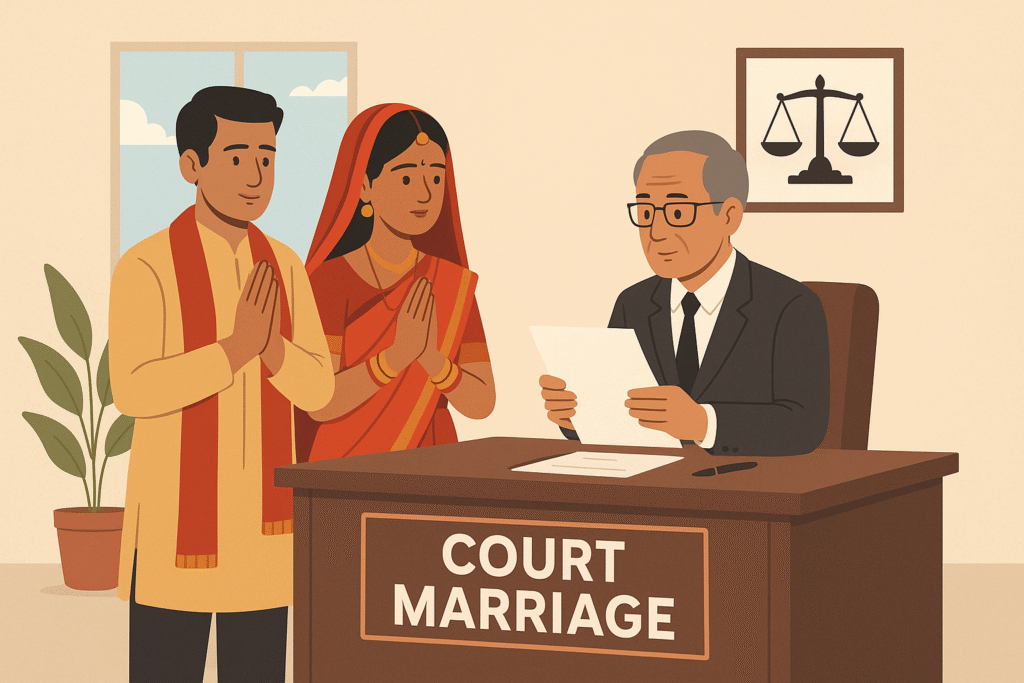कोर्ट मैरिज के नियम और शर्तें: एक विधिक विश्लेषण
(Court Marriage ke Niyam aur Shartein: Ek Vidhik Vishleshan)
भूमिका
कोर्ट मैरिज एक वैधानिक प्रक्रिया है जो दो व्यक्ति, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि के हों, को विवाह के वैधानिक बंधन में बाँधने के लिए “विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954)” के अंतर्गत संपन्न की जाती है। यह विवाह पंजीकरण और कानूनी मान्यता की प्रक्रिया को सरल और न्यायसंगत बनाती है।
कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक शर्तें
1. आयु की शर्त:
- पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
(धारा 4 (c) – विशेष विवाह अधिनियम, 1954)
2. वैवाहिक स्थिति:
- दोनों पक्ष अविवाहित हों, या पूर्व विवाह समाप्त हो चुका हो (तलाकशुदा / विधवा / विधुर)।
- विवाह करते समय दोनों पक्षों में से कोई मानसिक रोग से पीड़ित न हो और विवाह की सहमति देने में सक्षम हो।
(धारा 4 (b) और (d))
3. रक्त-संबंध की निषेधता:
- यदि दोनों पक्ष “नियत रक्त संबंध” (Prohibited Degrees of Relationship) में आते हैं, तो विवाह अमान्य होगा, जब तक कि संबंधित रीति या कानून इसकी अनुमति न दे।
(धारा 4 (e))
4. दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति:
- विवाह बलपूर्वक, धोखे या दबाव में नहीं किया जाना चाहिए।
- दोनों पक्षों की सहमति स्वेच्छा और स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए।
कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया
1. विवाह के लिए सूचना (Notice of Intended Marriage):
- दोनों पक्षों को विवाह अधिकारी (Marriage Officer) के समक्ष “Form” में विवाह की सूचना देनी होती है।
- यह सूचना उस जिले के विवाह अधिकारी को दी जाती है जहाँ पक्षों में से कोई एक कम से कम 30 दिन से निवास कर रहा हो।
(धारा 5)
2. नोटिस का प्रकाशन:
- विवाह अधिकारी द्वारा यह सूचना कार्यालय में सार्वजनिक रूप से चिपकाई जाती है ताकि कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज कर सके।
(धारा 6)
3. आपत्ति और उसकी जांच:
- कोई व्यक्ति यदि विवाह पर आपत्ति करता है, तो उसे 30 दिनों के भीतर विवाह अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा।
- विवाह अधिकारी आपत्ति की जांच करेगा और उपयुक्त निर्णय देगा।
(धारा 7 – 9)
4. विवाह का पंजीकरण और समारोह:
- 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद, यदि कोई आपत्ति नहीं होती, तो विवाह अधिकारी की उपस्थिति में दोनों पक्ष और तीन गवाहों की मौजूदगी में विवाह का पंजीकरण किया जाता है।
- विवाह के समय दोनों पक्षों को यह घोषणा करनी होती है कि वे एक-दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं।
(धारा 11)
5. विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate):
- विवाह के संपन्न होने के बाद विवाह अधिकारी द्वारा विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जो कि वैधानिक साक्ष्य होता है।
(धारा 13)
कोर्ट मैरिज के लाभ
- धर्मनिरपेक्षता: सभी धर्मों के व्यक्ति इस प्रक्रिया के तहत विवाह कर सकते हैं।
- कानूनी सुरक्षा: विवाह को वैधानिक मान्यता और सुरक्षा प्राप्त होती है।
- दहेज प्रथा की रोकथाम: यह प्रक्रिया सादगीपूर्ण होती है, जिससे दहेज की सामाजिक बुराई में कमी आती है।
- अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहन: सामाजिक भेदभाव की दीवारें टूटती हैं।
- साक्ष्य के रूप में विवाह प्रमाणपत्र: पासपोर्ट, वीज़ा, बीमा, संपत्ति और अन्य कानूनी मामलों में उपयोगी होता है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक सर्टिफिकेट
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो (6-6 प्रति पक्ष)
- अविवाहित होने का हलफनामा / तलाक प्रमाण पत्र / मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- तीन गवाहों की पहचान और पते के प्रमाण
निष्कर्ष
कोर्ट मैरिज भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभरी है। यह कानून न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सम्मान देता है, बल्कि विवाह संस्था को भी न्यायिक सुरक्षा देता है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के माध्यम से यह प्रक्रिया पारदर्शी, समतामूलक और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्राप्त करती है, जो एक प्रगतिशील समाज की दिशा में अहम कदम है।